लेखक 👉 स्वामी विवेकानंद परिव्राजक
दुःख=योग-दर्शन के अनुसार चार प्रकार के दु:ख
इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुःख से छूटकर सुख को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य से भिन्न योनियों में दुःख अधिक और सुख कम मिलता है । मनुष्य योनि में दुःख कम और सुख अधिक मिलता है । फिर भी- (चाहे कोई मनुष्य-शरीर भी प्राप्त कर ले, तब भी) दुःखों से पूर्ण रूप से नहीं छूट पाता । जब तक जीवित रहता है, तब तक सामान्य परिस्थितियों में किसी न किसी दुःख से आक्रान्त रहता ही है। हाँ, इन दुःखों से पूर्णतया छूटने का उपाय तो मनुष्य-जन्म में कर सकता है। वह उपाय है- योगाभ्यास । इस उपाय से जीवित रहते हुए समाधि-काल में सम्पूर्ण दुःखों से व्यक्ति छूटकर ईश्वरीय-आनन्द को प्राप्त कर लेता है और इसी उपाय का अभ्यास करते करते जन्म-मरण के चक्र से छूटकर सम्पूर्ण दुःखों से निवृत्ति और मोक्षानन्द की प्राप्ति कर लेता है। जब तक व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वरीय-आनन्द की अनुभूति नहीं कर लेता, तब तक उसकी रुचि सांसारिक-सुख की ओर प्राय: रहती ही है। जीवात्मा स्वभाव से ही सुख को चाहता है, अत: ईश्वरीय आनन्द जब तक उसे प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सांसारिक सुख से ही अपनी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करता है ।परन्तु जैसा विशुद्ध सुख जीवात्मा चाहता है, वैसा उसे संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाता। वह विशुद्ध सुख केवल ईश्वर से ही मिल सकता है, इसीलिये योगाभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। संसार में जो सुख प्राप्त होता है, उसमें अनेक प्रकार के दुःख मिश्रित रहते हैं। महर्षि पतञ्जलि जी महाराज के अनुसार सांसारिक सुखों में चार प्रकार के दुःख मिले रहते हैं । आइये, इन्हें समझने का प्रयत्न करें।
परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च
दु:खमेव सर्वं विवेकिन: ॥ (योग. २/१५)
सूत्रार्थ ➡ परिणाम, ताप और संस्कार दुःख के कारण तथा सत्त्वादि गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण विवेकी (=योगी) व्यक्ति के लिये समस्त पदार्थ दुःख से युक्त है (=उसे पूर्ण सुख किसी भी भौतिक पदार्थ से नहीं मिल सकता)।व्यारव्या ⇨ प्रश्न हो सकता है कि वैदिक मान्यता के अनुसार पुण्य कर्मों का फल सुख और पाप कमों का फल दुःख मिलता है, तो हम पुण्य कर्म करके सुखदायक=(मनुष्य के) जाति, आयु और भोग रूपी फल को प्राप्त करते रहेंगे, इसमें क्या हानि है ? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर इस सूत्र के माध्यम से दिया गया है कि चाहे मनुष्य बनकर सुखदायक जाति, आयु व भोग भी क्यों न प्राप्त कर लेवें इन सांसारिक सुखों में तब भी चार प्रकार के दुःख मिश्रित होने के कारण सभी भौतिक सुख त्याज्य ही हैं । अतः इनसे पूर्ण रूप से छूटने के लिये योगाभ्यास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना ही चाहिये ।
(१) परिणाम दुःख ➧ जब कोई व्यक्ति अपनी इन्द्रियों द्वारा रूप, स्स आदि का सेवन करके कुछ समय के लिये थोड़ी-सी तृप्ति जैसी अनुभव करता है, तो वह भौतिक सुख कहलाता है और इन्द्रियों की चंचलता के कारण कुछ अशान्ति-सी अनुभव करता है, तो वह दुःख कहलाता है। व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इन्द्रियों से इन भोगों को भोग-भोग कर अपनी इच्छाओं को शान्त कर लूँगा । परन्तु ऐसा होता नहीं है बल्कि ऐसा कहना चाहिये कि- 'भोगों को बार-बार भोग कर इच्छाओं को शान्त कर देना', असम्भव है । कारण-कि भोगों को भोगने पर उस वस्तु से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख में व्यक्ति का राग बढ़ जाता है, तथा इन्द्रियों की भोगने की शक्ति भी बढ़ जाती है। परन्तु इच्छा कुछ देर के लिये तो शान्त हो जाती है, पूर्ण रूप से शान्त नहीं हो पाती । इसका कारण यह रहता है कि-इन्द्रियों का भोगों को भोगने का सामर्थ्य सीमित है। कुछ देर तक किसी भोग को भोगते रहने पर उस इन्द्रिय का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। परन्तु मन की= (आत्मा की) इच्छा पूरी नहीं हो पाती। व्यक्ति और भोगना चाहता है, इन्द्रिय का सामर्थ्य समाप्त हो जाने से वह भोग नहीं पाता। परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को दुःख होता है। यह दुःख भोगों को भोगने के परिणाम के रूप में होता है, इसलिये इसे 'परिणाम दुःख' कहते हैं। एक बार उस वस्तु का भोग करने पर इन्द्रिय का जो सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, कुछ काल के पश्चात् इन्द्रिय में वह सामर्थ्य पुन: संचित हो जाता है। अब की बार व्यक्ति और अधिक वेग से उस भोग को भोगता है, परन्तु परिणाम फिर भी वही रहता है। थोड़ी ही देर में इन्द्रिय फिर से शिथिल हो जाती है, तथा इच्छा होते हुए भी व्यक्ति भोग नहीं पाता। इससे उसे दुःख होता है। इस प्रकार बार बार इन भोगों का अभ्यास करते रहने से इन्द्रियों का भी भोगों को भोगने का सामर्थ्य बढ़-सा जाता है, और साथ साथ इच्छा भी बढ़ जाती है। इन्द्रियों का सामर्थ्य चाहे जितना भी बढ़ जाये, तब भी भोगों को भोगने से इच्छाएँ शान्त नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप दुःख ही हाथ लगता है । इसीलिये इसे 'परिणाम दुःख' कहते हैं । अत: सुख का उपाय- 'भोगों का अभ्यास करना' नहीं है, बल्कि 'योग का अभ्यास करना' है ।
उदाहरण➩ जैसे एक व्यक्ति को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है। वह पहली बार दो-चार रसगुल्ले खा कर सुख का अनुभव करता है। वह और खाना चाहता है, परन्तु रसनेन्द्रिय का सामर्थ्य समाप्त हो जाने के कारण और खा नहीं पाता। दो-चार दिन के पश्चात् पुनः रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है। अब की बार पांच-छः रसगुल्ले खा जाता है, परन्तु इच्छा और अधिक खाने की बनी ही रहती है। सामर्थ्य न होने से खा नहीं सकता । यदि जबरदस्ती खा भी लेवे, तो पेट खराब हो जाने से रोग के कारण सुख के स्थान पर दुःख ही बढ़ता है। इस प्रकार वह अभ्यास करते करते १०-१० अथवा १२-१४ रसगुल्ले तक खा लेने का सामर्थ्य बढ़ा लेता है । परन्तु इच्छाएँ पूर्ण रूप से फिर भी शान्त नहीं होती। परिणाम 'दुःख' ही रहता है। इसी प्रकार से सिगरेट, शराब आदि पीने वालों तथा सिनेमा आदि देख्ने वालों के दृष्टान्त भी समझ लेने चाहिये । इसीलिये महर्षि व्यासजी ने इस सूत्र के भाष्य में कहा है - 'तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति । अर्थात्सु ख का उपाय - भोगाभ्यास नहीं है, (बल्कि योगाभ्यास है) ।
(२) ताप दुःरव ➧ भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि जड़ पदार्थों तथा पुत्र-परिवार आदि चेतन प्राणियों से मनुष्य सुख प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति इन जड़-चेतन पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुख में बाधा डालता है, तो उस सुख भोगने वाले व्यक्ति को दुःख का अनुभव होता है। यह दुःख बाधा डालने के बाद होता है और यदि बाधा डालने से पहले ही पता चल जाये कि- 'अमुक व्यक्ति मेरे अमुक सुख में बाधा डालेगा', तो बाधा डालने से पहले भी दु:ख होता है , चाहे वह व्यक्ति बाद में बाधा डाल सके या न डाल सके। यदि बाधा डाल देवे, तो और अधिक दुःख होता है । इसे 'ताप दुःख' कहते हैं ।
उदाहरण ➩ कल्पना कीजिये, हमारे पास बहुत उत्तम 'ध्वन्यंकन-यन्त्र' (=टेप-रिकार्डर) है । हमारा पड़ोसी हमसे वह यन्त्र मांग कर ले जाना चाहता है। हम उसे यन्त्र देना नहीं चाहते। जब हमें पता चलेगा कि 'कल वह यन्त्र मांगने के लिए आयेगा' तो हमें सूचना मिलते ही दुःख होना प्रारम्भ हो जायेगा। यदि वह अगले दिन मांगने आ ही जाये, और पड़ोसी होने केनाते से, इच्छा न होते हुए भी हमें यन्त्र देना ही पड़े, तो और दुःख होगा और यह तब तक होता रहेगा जब तक कि वह यन्त्र हमारे पास सुरक्षित लौट नहीं आवेगा। साथ ही यह भी मन में भय बना रहेगा कि कहीं पड़ोसी व्यक्ति हमारा यन्त्र खराब न कर देवे। इसे ताप दुःख कहते हैं। इसी प्रकार से कोई अन्य कीमती वस्तु (कपड़े, करदीप=(टोच), कार आदि वाहन) मांगने पर होने वाले दुःख के उदाहरण भी समझे जा सकते हैं। यदि हम कपड़े के व्यापारी हैं, और हमारे बाजार में एक और नई दुकान कपड़े की खुलने वाली हो, तो उससे हमारे व्यापार में धन की कमी होने से हमें दुःख होगा, वह भी ताप दुःख है, इत्यादि ।
(३) संस्कार दुःख➧ जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से सुख भोगता है, तो मन पर सुख के संस्कार पड़ जाते हैं। ये ही संस्कार कुछ समय के पश्चात् उस व्यक्ति को पूर्व भोगे हुए सुख की ओर पुनः प्रेरित करते हैं। परन्तु जब किन्हीं कारणों से उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो व्यक्ति दुःख का अनुभव करता है। यह दुःख संस्कारों के कारण से होता है, इसलिये इसे 'संस्कार दुःख' कहते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी वस्तु से दुःख प्राप्त करता है, तो मन पर दुःख के संस्कार पड़ जाते हैं। जब वह दुःखदाई वस्तु पुनः सामने उपस्थित हो जाती है, अथवा वह व्यक्ति उस दुःखदाई वस्तु का स्मरण कर लेता हैं तो वे ही दुःख के संस्कार पुनः दुःख को उत्पन्न कर देते हैं। यह दुःख भी संस्कारों के कारण से होता है, अत: इसे भी 'संस्कार दुःख कहते हैं ।
(३) संस्कार दुःख➧ जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से सुख भोगता है, तो मन पर सुख के संस्कार पड़ जाते हैं। ये ही संस्कार कुछ समय के पश्चात् उस व्यक्ति को पूर्व भोगे हुए सुख की ओर पुनः प्रेरित करते हैं। परन्तु जब किन्हीं कारणों से उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो व्यक्ति दुःख का अनुभव करता है। यह दुःख संस्कारों के कारण से होता है, इसलिये इसे 'संस्कार दुःख' कहते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी वस्तु से दुःख प्राप्त करता है, तो मन पर दुःख के संस्कार पड़ जाते हैं। जब वह दुःखदाई वस्तु पुनः सामने उपस्थित हो जाती है, अथवा वह व्यक्ति उस दुःखदाई वस्तु का स्मरण कर लेता हैं तो वे ही दुःख के संस्कार पुनः दुःख को उत्पन्न कर देते हैं। यह दुःख भी संस्कारों के कारण से होता है, अत: इसे भी 'संस्कार दुःख कहते हैं ।
उदाहरण ➩ कल्पना कीजिये, कोई व्यक्ति प्रतिदिन कार से अपने कार्यालय में जाता है । कार में यात्रा करने पर वह सुख का अनुभव करता है। यदि किसी दिन उसकी कार रास्ते में ही खराब हो जाये अथवा पहिया पंक्चर हो जाये और उसे टैक्सी भी न मिले, बस में ही यात्रा करनी पड़े, तो उसे दुःख होगा। उसने कार से होने वाले सुख के संस्कार अपने मन पर डाल लिये थे। जब वह सुख किसी दिन नहीं मिला, तो उन संस्कारों के कारण उसे दुःख उठाना पड़ा। इसी प्रकार से चाय, पान, बीडी का सेवन करने वालों को जब ये वस्तुएँ यात्रा आदि में अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पातीं, तब उन्हें जो दुःख होता है, उसे प्राय: सभी लोग जानते है। यह सब 'संस्कार दुःख' कहलाता है। दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का अपमान कर दिया। उससे उसे दुःख हुआ। जब अपमान करने वाला व्यक्ति उसके सामने आयेगा अथवा वह अपमानित व्यक्ति उस अपमान करने वाले व्यक्ति का स्वयं स्मरण कर लेगा, तो उसे उन संस्कारों के कारण दुःख होना आरम्भ हो जाएगा जो संस्कार उसने अपमान होते समय अपने मन पर डाल लिये थे। इसी प्रकार से-किसी से धोखा खाने वाला व्यक्ति, किसी से मार खाने वाला व्यक्ति, किसी अन्य प्रकार की हानि उठाने वाला व्यक्ति भी, सम्बन्धित धोख़ेबाज या पीटने वाले व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हो जाने पर अथवा उनका स्मरण कर लेने पर जिस दुःख का अनुभव करता है, वह भी 'संस्कार-दुःख' कहलाता है।
(४) गुणवृत्तिविरोधदुःरव➧ योग-दर्शन के व्यास भाष्य के आधार पर इस दुःख के दो स्वरूप समझ में आते हैं । 'गुण' का अर्थ है - सत्त्व, रज और तम नामक सूक्ष्मतम कण, जिनके समुदाय का नाम 'प्रकृति' है। 'वृत्ति' का अर्थ है- स्वभाव ।
गुणवृत्तिविरोधदुःरव का पहला स्वरूप➭
(क) चित्त में गुणों का परिवर्तन - प्रकृति से उत्पन्न सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। चित्त (अथवा मन) भी त्रिगुणात्मक है । इन तीनों गुणों (=सत्त्व, रज और तम) की वृत्तियों (=स्वभाव) में परस्पर विरोध है। यथा-सत्त्व सुख् को उत्पन्न करता है। रज दुःख को उत्पन्न करता है और तम मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सत्त्व धार्मिक प्रवृत्तियों =(न्याय, दया और परोपकार, कर्तव्य-पालन आदि) को उत्पन्न करता है और रुज अधार्मिक प्रवृत्तियों=(पक्षपात, हिंसा, चोरी, स्वार्थ आदि) को उत्पन्न करता है। चित्त में स्थित इन गुणों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है । इन गुणों का व्यापार (=कार्य करना) चंचल है । इनका व्यापार चंचल होने से चित्त में स्थित इन गुणों के प्रभाव में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कभी व्यक्ति सत्त्वगुण के प्रभाव से परोपकार, न्याय, दया, धर्म आदि से युक्त होता है, तो वह सुख का अनुभव करता है । परन्तु किसी कारणवश रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव से उनकी यह स्थिति छूट जाती है, और वह स्वार्थ, पक्षपात, हिंसा, चोरी आदि के विचारों से युक्त हो जाता है, तो उसे दुःख होना आरम्भ हो जाता है। यह दुःख इन गुणों की वृत्तियों=(स्वभाव) के परस्पर विरुद्ध होने से होता है, इसलिये इसे 'गुणवृत्ति-विरोध दुःख' कहते हैं।
उदाहरण ➩ सत्त्वगुण के प्रभाव से मन (=चित्त) में यह विचार उत्पन्न होता है कि - चोरी नहीं करनी चाहिये, मेहनत से काम कर खाना अच्छा है। रजोगुण के प्रभाव से मन में एक विरुद्ध विचार उत्पन्न होता है कि - 'एक बार चोरी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। २०,००० रुपये मिल जायेंगे, आगे फिर चोरी नहीं करेंगे। अब इन दोनों वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से युद्ध चलता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप व्यक्ति व्याकुल (=दुःखी) हो जाता है। क्योंकि यह दुःख वृत्तियों के विरोध से होता है, अतः गुणवृत्तिविरोध-दुःख कहलाता है। इसी प्रकार से - सत्त्वगुण-समय हो गया है, अब घर चलना चाहिए।रजोगुण-घर तो रोज समय पर ही जाते हैं, आज तो सिनेमा देख ही लेते हैं। कुछ देर से घर पहुँच जाएंगे। फिर इन वृत्तियों में युद्ध और फिर चित्त की व्याकुलता आदि होना- सर्वत्र समझ लेना चाहिए।
गुणवृत्तिविरोधदुःरव का दूसरा स्वरूप➭
(ख) प्रत्येक भौतिक पदार्थ दुःख से युक्त है - प्रकृति से उत्पन्न सभी पदार्थ सत्त्व, रुज और तम से युक्त हैं।प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कम या अधिक मात्रा में इन तीनों गुणों (=सूक्ष्मतम परमाणुआं) का समावेश है। और प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान होते हुए, अपने अपने स्वभाव के कारण, सुख-दुःख और अज्ञान को ये तीनों गुण, कम या अधिक मात्रा में उत्पन्न करते ही रहते हैं। क्योंकि रजोगुण भी इन तीनों में से एक है, अत: यह भी प्रत्येक पदार्थ में रहता हुआ कम या अधिक दुःख को उत्पन्न करता ही है। जिस पदार्थ में जिस गुण की अधिकता होती है, वह पदार्थ उस गुण के नाम से कहा जाता है और उसका प्रभाव भी उसी गुण के अनुसार होता है। जैसे-
उदाहरण ➩ चावल, दूध, बादाम, घी आदि पदार्थ यद्यपि तीनों गुणों के सम्मिश्रण से बनते हैं, फिर भी इनमें सत्त्वगुण की अधिकता होने और 'सुख देना' रूपी सत्त्व-गुण का प्रभाव विशेष होने से, ये सत्त्वप्रधान पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार से मिर्च-मसाले आदि रुज: प्रधान पदार्थ तथा मद्य-मांस आदि तम:प्रधान पदार्थ कहलाते हैं।
इतना होने पर भी चावल, दूध, घी, बादाम आदि सात्त्विक पदार्थों में, रजोगुण की अल्प मात्रा होने पर भी वह अल्प दुःख को उत्पन्न करता ही है। यद्यपि इन सात्त्विक पदार्थों का सेवन करते समय रजोगुण से उत्पन्न उस अल्प दु:ख की सामान्य व्यक्ति को कोई स्पष्ट अनुभूति नहीं होती। फिर भी उपादान-कारण के नियम से योगाभ्यासी व्यक्ति उस दुःख का बुद्धि से अनुभव कर लेता है कि- (उत्पादन का नियम) जब इसमें रुजोगुण विद्यमान है, तो दुःख को भी अवश्य ही उत्पन्न करेगा। क्योंकि द्रव्य और गुण का नित्य सम्बन्ध है। इस प्रकार से योगाभ्यासी व्यक्ति सब पदार्थों को कम या अधिक दुःख से युक्त देखता है। क्योंकि इन पदार्थों में दुःख का कम या अधिक होना, गुणों की परस्पर विरुद्ध वृत्तियों के कारण से होता है, अतः इसे गुणवृत्तिविरोध-दुःख कहते हैं।
जब योगाभ्यासी बौद्धिक स्तर पर प्रत्येक पदार्थ को कम या अधिक दुःख से युक्त अनुभव करता है, तो सूत्र के शब्दों- दुःखमेव सर्वं विवेकिन: के अनुसार सम्पूर्ण जगत् के भौतिक पदार्थ उस विवेकी(=योगाभ्यासी) को दुःखमय दीखते हैं, और उसे इस दुःखमय संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यही वैराग्य आगे चलकर उसे समाधि और मोक्ष तक पहुँचा देता है। इसके बिना दुःखों से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है ।
यदि व्यक्ति इन दुःखों से छूटने के लिए उपर्युक्त वैराग्य-प्राप्ति की प्रक्रिया को नहीं अपनाता तो वह इतना ही नहीं कि जीवन भर दु:खों को भोगता है, बल्कि जन्म-जन्मान्तरों तक इन दुःखों की कीचड़ में गहरा-गहरा धँसता चला जाता है और मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाँ बैठता है। इन दुःखों का विस्तार जन्म-जन्मान्तरों तक होता है, जो कि व्यास-भाष्य के आधार पर इस प्रकार से है -
परिणाम, ताप आदि दुःखों का विस्तार ➢
जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक सुख को भोगता है, तो उसे उस सुख में राग हो जाता है। वह उस सुख की पुन: प्राप्ति जिस भी किसी प्रकार से हो, करना चाहता है। चाहे उसे उस सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, स्श्वित आदि कोई भी पाप क्यों न करना पड़े। जैसा कि आजकल प्रायः होता ही है। लोग कार, कोठी, मान-प्रतिष्ठा आदि से सुख प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त रिश्र्वत, चोरी आदि पाप करते ही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन लौकिक सुखों को भोग-भोग कर भी इच्छाएँ तो पूरी होती नहीं। यहां जीते जी भी इच्छाओं के पूरा न होने के कारण परिणाम के रूप में दुःख भोगना पड़ता है और इन पापों के फलस्वरूप अगले जन्मों में भी पशु-पक्षीयों आदि की योनियों में विविध दुःख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि वैदिक सिद्धान्त में- "किया हुआ कर्म (कभी) निष्फल नहीं होता।" इन सुखों की प्राप्ति के लिये व्यक्ति सुख के राग से प्रेरित होकर कर्म करता है, अत:परिणाम दुःख के अन्तर्गत रागज कर्म माने जाते हैं।
परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सुख में बाधक बनता है, तो दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति से द्वेष कर लेता है। और उस द्वेष के कारण से वह उस व्यक्ति की हानि (=मारना, पीटना, विरोध करना, मिथ्या आरोप लगाना, यहां तक कि हत्या भी) कर देता है। फिर इन दुष्कर्मों का फल भी उसे नीच योनियों में जा-जाकर भोगना पड़ता है। इस प्रकार से ताप दु:ख के अन्तर्गत द्वेषज कर्म हो जाते हैं।
संस्कार दुःख के अन्तर्गत रागज और द्वेषज दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सुख भोगने पर सुख के संस्कार पड़ते हैं और दुःख भोगने पर दुःख के संस्कार पड़ जाते हैं। सुख के संस्कार राग को उत्पन्न करते हैं तथा दुःख के संस्कार द्वेष को। फिर व्यक्ति उन राग व द्वेषों से प्रेरित होकर पुन: नये कर्म करता है उस सुख की प्राप्ति के लिए और दुःख की निवृत्ति के लिए। राग और द्वेष के कारण किये गये इन सकाम कर्मों (=पाप-पुण्यों) का फल फिर उसे अगले जन्मो में भोगना पड़ता है और फिर यह चक्र यहीं समाप्त नहीं हो जाता। अगले जन्मों में व्यक्ति पुनः इन संस्कारों से पाप-पुण्य कर्म करता और नया सुख-दुःख भोग-भोग कर संस्कारों को और अधिक बढ़ाता जाता है। इस प्रकार संस्कारों से नये कर्म, नये कर्मों से नया फल (सुख-दुःख), और फिर इन फलों (=सुख-दुःख) से नये संस्कार बनते जाते हैं तथा जन्म-जन्मान्तरों तक व्यक्ति (आत्मा) विभिन्न योनियों में विविध दुःख भोगता हुआ अपनी महती हानि कर लेता है।
(४) गुणवृत्तिविरोधदुःरव➧ योग-दर्शन के व्यास भाष्य के आधार पर इस दुःख के दो स्वरूप समझ में आते हैं । 'गुण' का अर्थ है - सत्त्व, रज और तम नामक सूक्ष्मतम कण, जिनके समुदाय का नाम 'प्रकृति' है। 'वृत्ति' का अर्थ है- स्वभाव ।
गुणवृत्तिविरोधदुःरव का पहला स्वरूप➭
(क) चित्त में गुणों का परिवर्तन - प्रकृति से उत्पन्न सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक हैं। चित्त (अथवा मन) भी त्रिगुणात्मक है । इन तीनों गुणों (=सत्त्व, रज और तम) की वृत्तियों (=स्वभाव) में परस्पर विरोध है। यथा-सत्त्व सुख् को उत्पन्न करता है। रज दुःख को उत्पन्न करता है और तम मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सत्त्व धार्मिक प्रवृत्तियों =(न्याय, दया और परोपकार, कर्तव्य-पालन आदि) को उत्पन्न करता है और रुज अधार्मिक प्रवृत्तियों=(पक्षपात, हिंसा, चोरी, स्वार्थ आदि) को उत्पन्न करता है। चित्त में स्थित इन गुणों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है । इन गुणों का व्यापार (=कार्य करना) चंचल है । इनका व्यापार चंचल होने से चित्त में स्थित इन गुणों के प्रभाव में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कभी व्यक्ति सत्त्वगुण के प्रभाव से परोपकार, न्याय, दया, धर्म आदि से युक्त होता है, तो वह सुख का अनुभव करता है । परन्तु किसी कारणवश रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव से उनकी यह स्थिति छूट जाती है, और वह स्वार्थ, पक्षपात, हिंसा, चोरी आदि के विचारों से युक्त हो जाता है, तो उसे दुःख होना आरम्भ हो जाता है। यह दुःख इन गुणों की वृत्तियों=(स्वभाव) के परस्पर विरुद्ध होने से होता है, इसलिये इसे 'गुणवृत्ति-विरोध दुःख' कहते हैं।
उदाहरण ➩ सत्त्वगुण के प्रभाव से मन (=चित्त) में यह विचार उत्पन्न होता है कि - चोरी नहीं करनी चाहिये, मेहनत से काम कर खाना अच्छा है। रजोगुण के प्रभाव से मन में एक विरुद्ध विचार उत्पन्न होता है कि - 'एक बार चोरी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। २०,००० रुपये मिल जायेंगे, आगे फिर चोरी नहीं करेंगे। अब इन दोनों वृत्तियों में परस्पर विरोध होने से युद्ध चलता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप व्यक्ति व्याकुल (=दुःखी) हो जाता है। क्योंकि यह दुःख वृत्तियों के विरोध से होता है, अतः गुणवृत्तिविरोध-दुःख कहलाता है। इसी प्रकार से - सत्त्वगुण-समय हो गया है, अब घर चलना चाहिए।रजोगुण-घर तो रोज समय पर ही जाते हैं, आज तो सिनेमा देख ही लेते हैं। कुछ देर से घर पहुँच जाएंगे। फिर इन वृत्तियों में युद्ध और फिर चित्त की व्याकुलता आदि होना- सर्वत्र समझ लेना चाहिए।
गुणवृत्तिविरोधदुःरव का दूसरा स्वरूप➭
(ख) प्रत्येक भौतिक पदार्थ दुःख से युक्त है - प्रकृति से उत्पन्न सभी पदार्थ सत्त्व, रुज और तम से युक्त हैं।प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कम या अधिक मात्रा में इन तीनों गुणों (=सूक्ष्मतम परमाणुआं) का समावेश है। और प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान होते हुए, अपने अपने स्वभाव के कारण, सुख-दुःख और अज्ञान को ये तीनों गुण, कम या अधिक मात्रा में उत्पन्न करते ही रहते हैं। क्योंकि रजोगुण भी इन तीनों में से एक है, अत: यह भी प्रत्येक पदार्थ में रहता हुआ कम या अधिक दुःख को उत्पन्न करता ही है। जिस पदार्थ में जिस गुण की अधिकता होती है, वह पदार्थ उस गुण के नाम से कहा जाता है और उसका प्रभाव भी उसी गुण के अनुसार होता है। जैसे-
उदाहरण ➩ चावल, दूध, बादाम, घी आदि पदार्थ यद्यपि तीनों गुणों के सम्मिश्रण से बनते हैं, फिर भी इनमें सत्त्वगुण की अधिकता होने और 'सुख देना' रूपी सत्त्व-गुण का प्रभाव विशेष होने से, ये सत्त्वप्रधान पदार्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार से मिर्च-मसाले आदि रुज: प्रधान पदार्थ तथा मद्य-मांस आदि तम:प्रधान पदार्थ कहलाते हैं।
इतना होने पर भी चावल, दूध, घी, बादाम आदि सात्त्विक पदार्थों में, रजोगुण की अल्प मात्रा होने पर भी वह अल्प दुःख को उत्पन्न करता ही है। यद्यपि इन सात्त्विक पदार्थों का सेवन करते समय रजोगुण से उत्पन्न उस अल्प दु:ख की सामान्य व्यक्ति को कोई स्पष्ट अनुभूति नहीं होती। फिर भी उपादान-कारण के नियम से योगाभ्यासी व्यक्ति उस दुःख का बुद्धि से अनुभव कर लेता है कि- (उत्पादन का नियम) जब इसमें रुजोगुण विद्यमान है, तो दुःख को भी अवश्य ही उत्पन्न करेगा। क्योंकि द्रव्य और गुण का नित्य सम्बन्ध है। इस प्रकार से योगाभ्यासी व्यक्ति सब पदार्थों को कम या अधिक दुःख से युक्त देखता है। क्योंकि इन पदार्थों में दुःख का कम या अधिक होना, गुणों की परस्पर विरुद्ध वृत्तियों के कारण से होता है, अतः इसे गुणवृत्तिविरोध-दुःख कहते हैं।
जब योगाभ्यासी बौद्धिक स्तर पर प्रत्येक पदार्थ को कम या अधिक दुःख से युक्त अनुभव करता है, तो सूत्र के शब्दों- दुःखमेव सर्वं विवेकिन: के अनुसार सम्पूर्ण जगत् के भौतिक पदार्थ उस विवेकी(=योगाभ्यासी) को दुःखमय दीखते हैं, और उसे इस दुःखमय संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यही वैराग्य आगे चलकर उसे समाधि और मोक्ष तक पहुँचा देता है। इसके बिना दुःखों से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है ।
यदि व्यक्ति इन दुःखों से छूटने के लिए उपर्युक्त वैराग्य-प्राप्ति की प्रक्रिया को नहीं अपनाता तो वह इतना ही नहीं कि जीवन भर दु:खों को भोगता है, बल्कि जन्म-जन्मान्तरों तक इन दुःखों की कीचड़ में गहरा-गहरा धँसता चला जाता है और मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाँ बैठता है। इन दुःखों का विस्तार जन्म-जन्मान्तरों तक होता है, जो कि व्यास-भाष्य के आधार पर इस प्रकार से है -
परिणाम, ताप आदि दुःखों का विस्तार ➢
जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक सुख को भोगता है, तो उसे उस सुख में राग हो जाता है। वह उस सुख की पुन: प्राप्ति जिस भी किसी प्रकार से हो, करना चाहता है। चाहे उसे उस सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, स्श्वित आदि कोई भी पाप क्यों न करना पड़े। जैसा कि आजकल प्रायः होता ही है। लोग कार, कोठी, मान-प्रतिष्ठा आदि से सुख प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त रिश्र्वत, चोरी आदि पाप करते ही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन लौकिक सुखों को भोग-भोग कर भी इच्छाएँ तो पूरी होती नहीं। यहां जीते जी भी इच्छाओं के पूरा न होने के कारण परिणाम के रूप में दुःख भोगना पड़ता है और इन पापों के फलस्वरूप अगले जन्मों में भी पशु-पक्षीयों आदि की योनियों में विविध दुःख भोगने पड़ते हैं। क्योंकि वैदिक सिद्धान्त में- "किया हुआ कर्म (कभी) निष्फल नहीं होता।" इन सुखों की प्राप्ति के लिये व्यक्ति सुख के राग से प्रेरित होकर कर्म करता है, अत:परिणाम दुःख के अन्तर्गत रागज कर्म माने जाते हैं।
परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सुख में बाधक बनता है, तो दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति से द्वेष कर लेता है। और उस द्वेष के कारण से वह उस व्यक्ति की हानि (=मारना, पीटना, विरोध करना, मिथ्या आरोप लगाना, यहां तक कि हत्या भी) कर देता है। फिर इन दुष्कर्मों का फल भी उसे नीच योनियों में जा-जाकर भोगना पड़ता है। इस प्रकार से ताप दु:ख के अन्तर्गत द्वेषज कर्म हो जाते हैं।
संस्कार दुःख के अन्तर्गत रागज और द्वेषज दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सुख भोगने पर सुख के संस्कार पड़ते हैं और दुःख भोगने पर दुःख के संस्कार पड़ जाते हैं। सुख के संस्कार राग को उत्पन्न करते हैं तथा दुःख के संस्कार द्वेष को। फिर व्यक्ति उन राग व द्वेषों से प्रेरित होकर पुन: नये कर्म करता है उस सुख की प्राप्ति के लिए और दुःख की निवृत्ति के लिए। राग और द्वेष के कारण किये गये इन सकाम कर्मों (=पाप-पुण्यों) का फल फिर उसे अगले जन्मो में भोगना पड़ता है और फिर यह चक्र यहीं समाप्त नहीं हो जाता। अगले जन्मों में व्यक्ति पुनः इन संस्कारों से पाप-पुण्य कर्म करता और नया सुख-दुःख भोग-भोग कर संस्कारों को और अधिक बढ़ाता जाता है। इस प्रकार संस्कारों से नये कर्म, नये कर्मों से नया फल (सुख-दुःख), और फिर इन फलों (=सुख-दुःख) से नये संस्कार बनते जाते हैं तथा जन्म-जन्मान्तरों तक व्यक्ति (आत्मा) विभिन्न योनियों में विविध दुःख भोगता हुआ अपनी महती हानि कर लेता है।
प्रश्न:- क्या इन दुःखों से छूटने का कोई उपाय है ?
उत्तर - जी हाँ ! केवल एक ही उपाय है- 'योगाभ्यास', जिसका संकेत हम पहले कर चुके हैं। महर्षि पतञ्जलि जी के ही शब्दों में - "विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:" (योग २/२६) अर्थात् स्थिर (=दृढ़) तत्त्वज्ञान ही इन दुःखों से छूटने का उपाय है। यह तत्त्वज्ञान उपर्युक्त प्रक्रिया से ही-सांसारिक सुखों में चार प्रकार का दुःख अनुभव करने से और योग के आठ अंगों का आचरण करने से ही संभव है। इस विषय में योग दर्शन का यह सूत्र द्रष्टव्य है- "योगाड्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते:" (योग. २/२८) अर्थात् योग के (आठ) अंगों का अनुष्ठान (=आचरण) करने से अविद्या का नाश और ज्ञान का विकास होता जाता है, जब तक कि विवेकख्याति (=तत्त्वज्ञान) न हो जाते। और फिर इस तत्त्वज्ञान का निश्चित परिणाम वैराग्य प्राप्ति होता है। वैराग्य से समाधि और समाधि से संस्कारों की दग्धबीजभाव अवस्था (=भूने हुए बीजों के समान अवस्था) और फिर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष में जीवात्मा इन सब दुःखों से छूटकर ईश्वर के नित्य आनन्द को भोगता है। कितने काल तक? जब तक यह संसार ३६,००० बार बने और बिगड़े। एक बार संसार के बनने और बिगड़ने का समय दोनों मिलकर ८ अरब ६४ करोड़ × ३६,०००=३१ नील १० खरब और ४० अरब वर्ष बनता है। इतने लम्बे काल तक सम्पूर्ण दुःखों से छूटकर ईश्वर का नित्य आनन्द भोगने के लिये क्यों न तप (=परिश्रम) किया जाये? जो भी बुद्धिमान व्यक्ति इस उपर्युक्त प्रक्रिया को समझ लेगा, वह अवश्य ही इसके लिये तप करेगा। क्योंकि "बुद्धिमान् व्यक्ति का तप से अतिरिक्त और कहीं भी कल्याण नहीं है।" इसी भाव को महाराज भर्तृहरि जी ने इस पंक्ति में व्यक्त किया है-
"सखे ! नान्यच्छ्रेयोजगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥" (भर्तृ. वैराग्य । ४८)
इस प्रकार से व्यक्ति तप करता हुआ दुःखों से छूटने का प्रयत्न करे। बिना तप किये ये दुःख नहीं छूटेंगे। यह सत्य है कि तप करना कठिन है और लोग कहते हैं कि हमसे कठिन कार्य नहीं होता। पस्नतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति तप नहीं करना चाहता या नहीं करता, वह सुख को भी तो प्राप्त नहीं करना चाहता या नहीं करता, (वह सुख को भी - तो प्राप्त नहीं कर सकता) ईश्वर का यह नियम है कि जो तप करेगा, वही सुख प्राप्त कर सकेगा। अतः चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि सुख चाहिये, तो तप करना ही पड़ेगा। धन कमाना भी तो कठिन है, फिर उसके लिये भी तो लोग तप करते हैं। इस सम्बन्ध में लोग क्यों नहीं कहते कि-'धन कमाना कठिन है, हम धन नहीं कमाएँगे।' क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है, इसलिये धन कमाने के लिये पूरा तप करते हैं। बस यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि- दुःख से छूटे बिना और सुख को प्राप्त किये बिना भी गुजारा नहीं है, इसके लिये भी तप कीजिये।
अब दुःख से छूटने के लिये इसके कारणों और निवारण के उपायों को जानना होगा। आइये, इन्हें जानने का प्रयत्न करें। दुःख से छूटना और ईश्वरीय आनन्द को प्राप्त करना ही मुक्ति है। अत: दर्शन के माध्यम से इसे इस प्रकार से समझना चाहिये।
मनुष्य के पास अनेक प्रकार की वस्तुएँ हैं। उन वस्तुओं को वह अपनी सम्पत्ति समझता है। इसी सम्पत्ति को ही 'स्व' नाम से कहते हैं। और अपने आपको वह उस सम्पत्ति= (स्व) का मालिक समझता है। इस मालिक को 'स्वामी' नाम से कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी सम्पत्तियों और स्वयं में एक सम्बन्ध बना लेता है-
सम्पत्ति और मालिक का सम्बन्ध | इसी को ' स्व - स्वामी-सम्बन्ध' कहते हैं ।
मनुष्य के पास कुछ जड़ वस्तुएँ होती हैं। जड़ वस्तुएँ भी दो प्रकार की होती हैं। (१) बाह्य और (२) आन्तरिक ।
(१) बाह्य जड़ वस्तुएँ - भूमि , मकान, धन, वस्त्र, आभूषण, बिस्तर, पात्र, पुस्तक आदि ।
(२) आन्तरिक जड़ वस्तुएँ - शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि ।
व्यक्ति इन दोनों प्रकार की जड़ वस्तुओं को अपनी सम्पत्ति समझता है और स्वयं को इन वस्तुओं का मालिक मानता है। जब वह स्वयं को इन वस्तुओं का मालिक मान लेता है, तो उसमें इन वस्तुओं के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। 'ये मेरी वस्तुएँ हैं, मैं ये वस्तुएँ किसी को नहीं दूँगा।' इस प्रकार का ममत्व उत्पन्न हो जाता है। इन वस्तुओं में जब इस प्रकार का ममत्व उत्पन्न होता है, तो इनके नष्ट हो जाने का भय भी व्यक्ति को सताने लगता है। यदि इन वस्तुओं में से कोई वस्तु नष्ट हो जाये, तो दुःख भी होता है। इस ममत्व को ही 'स्व-स्वामी -सम्बन्ध' के नाम से कहते हैं ।
इस 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' के कारण व्यक्ति में 'अभिमान' नाम का एक अन्य दोष उत्पन्न होता है। वह सोचता है कि- 'मेरे पास इतनी वस्तुएँ हैं। ये सब मेरी हैं। दूसरों के पास क्या है ? कुछ भी नहीं है। अथवा मेरी तुलना में बहुत कम हैं। इत्यादि। इस अभिमान के कारण व्यक्ति में दूसरों से घृणा उत्पन्न होती है। वह दूसरों को हीन (घटिया) और अपने आप को उत्तम मानने लगता है। इससे वह दूसरों के साथ उचित व्यवहास=(न्याय) नहीं कर पाता और अन्याय का व्यवहार करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह यम-नियमों का आचरण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तथा ईश्वर से भी दूर चला जाता है।
जड़ वस्तुओं के अतिरिक्त व्यक्ति के पास कुछ चेतन प्राणी भी होते हैं, जिन्हें वह 'अपना' मानता है। जैसे परिवार के सदस्य=माता, पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटियाँ, पोते-पोतियाँ इत्यादि। इन सब चेतनों को वह अपना=(अपनी सम्पत्ति के रूप में अथवा अपनी आत्मा का ही अंश) मानता है। यदि कोई उससे कहे कि- 'अपना एक बेटा धर्म की रक्षा के लिये दे दो।' तो वह उसे नहीं देता। वह सोचता है कि - ' यह बेटा मेरा है। मैंने अपने सुख के लिये इसे उत्पन्न किया है। दूसरों के लिये नहीं उत्पन्न किया यह ' स्व -स्खामी-सम्बन्ध' कहलाता है। व्यक्ति उस बेटे पर या अपनी किसी पूर्वोक्त जड़ वस्तु पर अपना ही एकाधिकार बनाये रखना चाहता है। वह उसे केवल अपने ही सुख के लिये उपयोग करना चाहता है। यदि कभी किसी सामाजिक कार्य में वह उस वस्तु को दे भी देता है, तो लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा आदि से प्रेरित होकर देता है। निष्काम भाव से वह उस वस्तु का दान नहीं कर पाता। क्योंकि वह ऐसा मानता है कि- ' ये सब वस्तुएँ या व्यक्ति मेरे हैं। मैं इन्हें दूसरों के सुख के लिये क्यों दूँ ? यदि दूँ भी, तो मुझे भी इसके बदले में कुछ धन-सम्मान आदि मिलना चाहिये ।' अनेक बार ये एषणाएँ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि व्यक्ति इन्हें समझ नहीं पाता कि मैं एषणाओं से प्रेरित होकर अपनी वस्तुएँ सामाजिक कार्य में दान दे रहा हूँ। यह सब 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' कहलाता है।
चेतन पुत्र आदि के शरीर, धन आदि की वृद्धि को देखकर व्यक्ति प्रसन्न होता है और मानता है कि 'मेरी वृद्धि हो रही है।' तथा पुत्र के शरीर, धन आदि की हानि को देखकर दुःखी होता है और मानता है कि 'मेरी हानि हो रही है। यह सब अपनापन जो उसमें जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि वह पुत्रादि को अपनी आत्मा का अंश माने बैठा है। इसीलिये उसकी वृद्धि को अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ प्रसन्न होता है और उसकी हानि को अपनी हानि मानता हुआ दु:खी होता है। यह सब 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' कहलाता है।
उत्तर - जी हाँ ! केवल एक ही उपाय है- 'योगाभ्यास', जिसका संकेत हम पहले कर चुके हैं। महर्षि पतञ्जलि जी के ही शब्दों में - "विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय:" (योग २/२६) अर्थात् स्थिर (=दृढ़) तत्त्वज्ञान ही इन दुःखों से छूटने का उपाय है। यह तत्त्वज्ञान उपर्युक्त प्रक्रिया से ही-सांसारिक सुखों में चार प्रकार का दुःख अनुभव करने से और योग के आठ अंगों का आचरण करने से ही संभव है। इस विषय में योग दर्शन का यह सूत्र द्रष्टव्य है- "योगाड्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते:" (योग. २/२८) अर्थात् योग के (आठ) अंगों का अनुष्ठान (=आचरण) करने से अविद्या का नाश और ज्ञान का विकास होता जाता है, जब तक कि विवेकख्याति (=तत्त्वज्ञान) न हो जाते। और फिर इस तत्त्वज्ञान का निश्चित परिणाम वैराग्य प्राप्ति होता है। वैराग्य से समाधि और समाधि से संस्कारों की दग्धबीजभाव अवस्था (=भूने हुए बीजों के समान अवस्था) और फिर मोक्ष हो जाता है। मोक्ष में जीवात्मा इन सब दुःखों से छूटकर ईश्वर के नित्य आनन्द को भोगता है। कितने काल तक? जब तक यह संसार ३६,००० बार बने और बिगड़े। एक बार संसार के बनने और बिगड़ने का समय दोनों मिलकर ८ अरब ६४ करोड़ × ३६,०००=३१ नील १० खरब और ४० अरब वर्ष बनता है। इतने लम्बे काल तक सम्पूर्ण दुःखों से छूटकर ईश्वर का नित्य आनन्द भोगने के लिये क्यों न तप (=परिश्रम) किया जाये? जो भी बुद्धिमान व्यक्ति इस उपर्युक्त प्रक्रिया को समझ लेगा, वह अवश्य ही इसके लिये तप करेगा। क्योंकि "बुद्धिमान् व्यक्ति का तप से अतिरिक्त और कहीं भी कल्याण नहीं है।" इसी भाव को महाराज भर्तृहरि जी ने इस पंक्ति में व्यक्त किया है-
"सखे ! नान्यच्छ्रेयोजगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥" (भर्तृ. वैराग्य । ४८)
इस प्रकार से व्यक्ति तप करता हुआ दुःखों से छूटने का प्रयत्न करे। बिना तप किये ये दुःख नहीं छूटेंगे। यह सत्य है कि तप करना कठिन है और लोग कहते हैं कि हमसे कठिन कार्य नहीं होता। पस्नतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति तप नहीं करना चाहता या नहीं करता, वह सुख को भी तो प्राप्त नहीं करना चाहता या नहीं करता, (वह सुख को भी - तो प्राप्त नहीं कर सकता) ईश्वर का यह नियम है कि जो तप करेगा, वही सुख प्राप्त कर सकेगा। अतः चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि सुख चाहिये, तो तप करना ही पड़ेगा। धन कमाना भी तो कठिन है, फिर उसके लिये भी तो लोग तप करते हैं। इस सम्बन्ध में लोग क्यों नहीं कहते कि-'धन कमाना कठिन है, हम धन नहीं कमाएँगे।' क्योंकि वे जानते हैं कि इसके बिना गुजारा नहीं है, इसलिये धन कमाने के लिये पूरा तप करते हैं। बस यही बात हम भी कहना चाहते हैं कि- दुःख से छूटे बिना और सुख को प्राप्त किये बिना भी गुजारा नहीं है, इसके लिये भी तप कीजिये।
अब दुःख से छूटने के लिये इसके कारणों और निवारण के उपायों को जानना होगा। आइये, इन्हें जानने का प्रयत्न करें। दुःख से छूटना और ईश्वरीय आनन्द को प्राप्त करना ही मुक्ति है। अत: दर्शन के माध्यम से इसे इस प्रकार से समझना चाहिये।
दुःख का कारण=स्व-स्वामि-सम्बन्ध
सम्पत्ति और मालिक का सम्बन्ध | इसी को ' स्व - स्वामी-सम्बन्ध' कहते हैं ।
मनुष्य के पास कुछ जड़ वस्तुएँ होती हैं। जड़ वस्तुएँ भी दो प्रकार की होती हैं। (१) बाह्य और (२) आन्तरिक ।
(१) बाह्य जड़ वस्तुएँ - भूमि , मकान, धन, वस्त्र, आभूषण, बिस्तर, पात्र, पुस्तक आदि ।
(२) आन्तरिक जड़ वस्तुएँ - शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि ।
व्यक्ति इन दोनों प्रकार की जड़ वस्तुओं को अपनी सम्पत्ति समझता है और स्वयं को इन वस्तुओं का मालिक मानता है। जब वह स्वयं को इन वस्तुओं का मालिक मान लेता है, तो उसमें इन वस्तुओं के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। 'ये मेरी वस्तुएँ हैं, मैं ये वस्तुएँ किसी को नहीं दूँगा।' इस प्रकार का ममत्व उत्पन्न हो जाता है। इन वस्तुओं में जब इस प्रकार का ममत्व उत्पन्न होता है, तो इनके नष्ट हो जाने का भय भी व्यक्ति को सताने लगता है। यदि इन वस्तुओं में से कोई वस्तु नष्ट हो जाये, तो दुःख भी होता है। इस ममत्व को ही 'स्व-स्वामी -सम्बन्ध' के नाम से कहते हैं ।
इस 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' के कारण व्यक्ति में 'अभिमान' नाम का एक अन्य दोष उत्पन्न होता है। वह सोचता है कि- 'मेरे पास इतनी वस्तुएँ हैं। ये सब मेरी हैं। दूसरों के पास क्या है ? कुछ भी नहीं है। अथवा मेरी तुलना में बहुत कम हैं। इत्यादि। इस अभिमान के कारण व्यक्ति में दूसरों से घृणा उत्पन्न होती है। वह दूसरों को हीन (घटिया) और अपने आप को उत्तम मानने लगता है। इससे वह दूसरों के साथ उचित व्यवहास=(न्याय) नहीं कर पाता और अन्याय का व्यवहार करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह यम-नियमों का आचरण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तथा ईश्वर से भी दूर चला जाता है।
जड़ वस्तुओं के अतिरिक्त व्यक्ति के पास कुछ चेतन प्राणी भी होते हैं, जिन्हें वह 'अपना' मानता है। जैसे परिवार के सदस्य=माता, पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटियाँ, पोते-पोतियाँ इत्यादि। इन सब चेतनों को वह अपना=(अपनी सम्पत्ति के रूप में अथवा अपनी आत्मा का ही अंश) मानता है। यदि कोई उससे कहे कि- 'अपना एक बेटा धर्म की रक्षा के लिये दे दो।' तो वह उसे नहीं देता। वह सोचता है कि - ' यह बेटा मेरा है। मैंने अपने सुख के लिये इसे उत्पन्न किया है। दूसरों के लिये नहीं उत्पन्न किया यह ' स्व -स्खामी-सम्बन्ध' कहलाता है। व्यक्ति उस बेटे पर या अपनी किसी पूर्वोक्त जड़ वस्तु पर अपना ही एकाधिकार बनाये रखना चाहता है। वह उसे केवल अपने ही सुख के लिये उपयोग करना चाहता है। यदि कभी किसी सामाजिक कार्य में वह उस वस्तु को दे भी देता है, तो लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा आदि से प्रेरित होकर देता है। निष्काम भाव से वह उस वस्तु का दान नहीं कर पाता। क्योंकि वह ऐसा मानता है कि- ' ये सब वस्तुएँ या व्यक्ति मेरे हैं। मैं इन्हें दूसरों के सुख के लिये क्यों दूँ ? यदि दूँ भी, तो मुझे भी इसके बदले में कुछ धन-सम्मान आदि मिलना चाहिये ।' अनेक बार ये एषणाएँ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि व्यक्ति इन्हें समझ नहीं पाता कि मैं एषणाओं से प्रेरित होकर अपनी वस्तुएँ सामाजिक कार्य में दान दे रहा हूँ। यह सब 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' कहलाता है।
चेतन पुत्र आदि के शरीर, धन आदि की वृद्धि को देखकर व्यक्ति प्रसन्न होता है और मानता है कि 'मेरी वृद्धि हो रही है।' तथा पुत्र के शरीर, धन आदि की हानि को देखकर दुःखी होता है और मानता है कि 'मेरी हानि हो रही है। यह सब अपनापन जो उसमें जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि वह पुत्रादि को अपनी आत्मा का अंश माने बैठा है। इसीलिये उसकी वृद्धि को अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ प्रसन्न होता है और उसकी हानि को अपनी हानि मानता हुआ दु:खी होता है। यह सब 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' कहलाता है।
इन सब जड़ वस्तुओं और चेतन प्राणियों के अतिरिक्त व्यक्ति के पास अनेक प्रकार की विद्याएँ, कलाएँ भी होती हैं। जैसे गणित, भूगोल, खगोल-विज्ञान, संगीत, दर्शन-विद्या, प्रवचन कला, अध्यापन कला, भोजन बनाना इत्यादि। इन अनेक प्रकार की विद्याओं/ कलाओं को भी व्यक्ति अपनी मानता है। अर्थात् वह यह मानता है कि इन सब विद्याओं, कलाओं का उत्पादक, रक्षक, स्वामी मैं ही हूँ। यह स्व-स्वामी-सम्बन्ध' है। इससे फिर उसमें अभिमान, घृणा आदि दोष उत्पन्न होते हैं। और पूर्ववत् वह यम - नियमों से तथा ईश्वर से दूर चला जाता है।
वास्तव में व्यक्ति के पास जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं, चाहे वे जड़ वस्तुएँ (भूमि , भवन, धन, शरीर, मन, बुद्धि आदि) हों; चाहे चेतन पुत्र, पौत्रादि हों; चाहे विद्याएँ, कलाएँ (अध्यापन, प्रवचनादि) हों, वे सब सम्पत्तियाँ ईश्वर की हैं, मनुष्य की अपनी नहीं हैं। वे सब वस्तुएँ ईश्वर ने उत्पन्न की हैं, वही उनका रक्षक, पालक है, वही उन सबका व्यवस्थापक है। इन सबका आदि मूल ईश्वर है। ईश्वर ही उन सबका स्वामी है, मनुष्य तो उन वस्तुओं का 'प्रयोक्ता ' मात्र है। ईश्वर ने मनुष्य को 'प्रयोग' करने के लिये वे सब वस्तुएँ और विद्याएँ दी हैं परन्तु भूल से
मनुष्य अपने आपको उन वस्तुओं और विद्याओं का मालिक (स्वामी) मान बैठता है। इसीलिये वह दुःखी भी होता है। इस 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को हटाने के लिये व्यक्ति स्वयं को उन वस्तुओं, विद्याओं का स्वामी न माने, बल्कि 'प्रयोक्ता' माने।
उदाहरण - एक व्यक्ति एक कम्पनी में प्रबन्धक के पद पर कार्य करता है। उस प्रबन्धक को कम्पनी की ओर से प्रबन्धादि कार्यों को करने के लिये एक कमरा, मेज़-कुर्सी, कागज़-पेन, वातानुकूलित यन्त्र, एक कार आदि वस्तुएँ दी गई हैं। वह प्रबन्धक इन सब वस्तुओं को कम्पनी की मानता है और इन सब का प्रयोग भी करता जाता है। अपने आप को वह इन वस्तुओं का 'प्रयोक्ता' मानता है, 'स्वामी' नहीं मानता। यदि कोई व्यक्ति कम्पनी की इन वस्तुओं को हानि पहुँचाने लगे, तो उससे इन वस्तुओं की रक्षा भी करता है, तब भी वह वस्तुओं
का 'स्वामी' कम्पनी को ही मानता है। यदि रक्षा के लिये पूरा प्रयत्न करने पर भी कोई वस्तु (कुर्सी आदि) टूट जाती हैं, तो उसे नहीं होता। वह सोचता है - 'मैंने इन वस्तुओं का प्रयोग किया। इनकी रक्षा करने का भी प्रयत्न किया। इस प्रकार से मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा निभाया। फिर भी यदि यह कुर्सी टूट गई, तो कम्पनी की कुर्सी टूटी, मेरी तो है नहीं। कम्पनी मुझे दूसरी कुर्सी मँगवा कर देगी। इस प्रकार से वह दुःखी नहीं होता। क्योंकि वह प्रबन्धक उन सब कुर्सी आदि वस्तुओं का 'स्वामी' कम्पनी को मानता है और स्वयं को 'प्रयोक्ता' मानता है। उसने उन वस्तुओं के साथ 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' नहीं जोड़ा और दुःखी भी नहीं हुआ।
अब दूसरे पक्ष में कल्पना करते हैं कि- जैसी कुर्सी उसके कार्यालय में थी, वैसी ही एक कुर्सी उसके अपने घर पर भी थी। यदि किसी दिन उसके अपने घर की कुर्सी टूट जाये, तो उसे दुःख होता है। तब वह सोचता है- 'हाय ! मेरी कुर्सी टूट गई ।' उस घर की कुर्सी के साथ वह 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' जोड़ लेता है, परिणाम स्वरूप उसे दुःख होता है।
इस उदाहरण के अनुसार हम 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को कैसे हटायें ? जितनी भी हमारे पास जड़ वस्तुएँ=(भूमि , भवन, धन, शरीर, बुद्धि, मन आदि) हैं; चेतन प्राणी= (पुत्र, पौत्र, भाई-बहन, माता-पिता आदि) हैं; और विद्याएँ, कलाएँ=(अध्यापन, प्रवचन, संगीत, विज्ञान, गणित आदि) हैं; इन सबका स्वामी 'ईश्वर' को मानें। ऐसा सोचें-'ये सब वस्तुएँ, विद्याएँ, कलाएँ ईश्वर ने हमें 'प्रयोग करने के लिये=(सांसारिक व्यवहारों की सिद्धि तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिये) दी हैं। इन सबका उत्पादक, रक्षक, पालक, व्यवस्थापक, 'स्वामी' तो ईश्वर ही है। हम ईश्वर-प्रदत्त इन वस्तुओं, विद्याओं का प्रयोग करेंगे, इनकी यथाशक्ति रक्षा करेंगे, इनकी वृद्धि करेंगे और योग्य व्यक्तियों के लिये उपर्युक्त वस्तुओं, विद्याओं को खर्च करेंगे। ईश्वर का हमारे लिये ऐसा ही आदेश है। इन वस्तुओं की रक्षा आदि करने पर भी यदि कोई वस्तु नष्ट भी हो जाएगी, तो हम दुःखरी नहीं होंगे। क्योंकि वह वस्तु हमारी नहीं है, ईश्वर की है।'
इस प्रकार से 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को हमें दूर करना चाहिये। जब हम उक्त प्रक्रिया से 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को दूर कर देंगे, तो हममें से अभिमान, राग, ईष्ष्या-द्वेष, घृणा, अन्याय आदि सभी दोष दूर हो जायेंगे। तब यम-नियमों का आचरण भी अच्छी प्रकार से हो पाएगा और हम ईश्वर के निकट होते चले जाएँगे। आनन्द का जीवन जीयेंगे, दूसरों के जीवन में भी आनन्द उत्पन्न करेंगे। ईश्वर के निकट होते-होते, ईश्वर का साक्षात्कार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे।
दुःख का आदि मूल कारण =: 'मिथ्याज्ञान' है। 'मिथ्याज्ञान' का ही दूसरा नाम 'अविद्या' है। आइये, इसे थोड़ा विस्तार से समझने और यह जानने का प्रयत्न करें, कि अविद्या क्या है और इससे दुःख कैसे उत्पन्न होता है ! इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिये हम योगदर्शन का यह सूत्र लेते हैं -
अनित्याशुचिदुत्नखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ (योगदर्शन २/५)
अर्थात् (१) अनित्य को नित्य समझना (२) अशुचि को शुचि समझना (३) दु:ख को सुख समझना और (४) अनात्मा को आत्मा समझना; अविद्या है। इस प्रकार से अविद्या के चार भाग हुए। साथ ही साथ इन चारों बातों को उल्टा करके भी देख् लीजिये। अर्थात् (१) नित्य को अनित्य समझना (२) शुचि को अशुचि समझना, (३) सुख
को दुःख समझना और (४) आत्मा को अनात्मा समझना भी अविद्या ही है। संक्षेप में अविद्या की परिभाषा यह हुई कि- जो वस्तु जैसी हो, उसको वैसा न समझकर, कुछ और ही समझना या उससे उल्टा समझना='अविद्या' है। और जैसे को तैसा समझना 'विद्या' है।
(१) अनित्य को नित्य समझना - नित्य का अर्थ होता है, जो वस्तु सदा रहे, कभी नष्ट न हो। नित्य शब्द में आरम्भ में 'अ' अक्षर जोड़कर (नञ्तत्पुरुष समास के अनुसार) शब्द बना लिया - अनित्य। अब इसका अर्थ उल्टा हो गया=जो वस्तु सदा न रहे, नष्ट हो जाये। तो अब प्रथम अविद्या का स्वरूप हो गया=अनित्य ( नष्ट होने वाली) वर्तुओं को नित्य (नष्ट न होने वाली) मानना। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ हैं, जो समय आने पर या कभी भी नष्ट हो जाती हैं। जैसे-शरीर, धन, सम्पत्ति, पुत्र-परिवार, पद-प्रतिष्ठा आदि।ये सब वस्तुएँ अनित्य कहलाती हैं, क्योंकि ये कभी भी नष्ट हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। परन्तु संसार के लोग इन अनित्य वस्तुओं को नित्य (सदा रहेंगी), ऐसा मानते हैं। इसीलिये दुःखी होते हैं।
यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाये कि- आपका शरीर नित्य है या अनित्य ? तो वह उत्तर देगा- अनित्य ! अर्थात् सदा जीवित नहीं रहेगा। शब्दों से तो उत्तर ठीक है। परन्तु क्या यह बात वास्तव में मन, बुद्धि में बैठ गई ? नहीं। मन में तो यही समझता है कि - मैं सदा जीवित रहूँगा, कभी नहीं मँगा। इसी का नाम अविद्या है।
ज्ञान दो प्रकार का है। (१) शाब्दिक ज्ञान (२) वास्तविक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान उसे कहते हैं- जब ज्ञान कुछ और हो एवं आचरण कुछ और हो। जैसे- सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहता है - " मैं जानता हूँ, सिगरेट पीने से नुकसान होता है।" परन्तु फिर भी वह पीता है। आचरण, ज्ञान के अनुसार नहीं है, उससे भिन्न है। अत: सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का ज्ञान- 'शाब्दिक ज्ञान' है।
'वास्तविक ज्ञान' उसे कहते हैं- जब ज्ञान भी वैसा और आचरण भी वैसा। अर्थात् दोनों समान हों, भिन्न नहीं। जैसे- बिजली की तार को छूने से नुकसान होता है=(करण्ट लगता है, मृत्यु भी हो सकती है)। इस बात को जानने वालों का आचरण भी वैसा ही है। बिजली की तार को कोई नहीं छूता। इसे 'वास्तविक ज्ञान' कहते हैं। जो व्यक्ति शब्दों से कहता है- मैं सदा जीवित नहीं रहूँगा। परन्तु मन में ऐसा मानता है और आचरण भी ऐसा है कि- मैं सदा जीवित रहूँगा; उसका ज्ञान 'शाब्दिक' है। और शाब्दिक ज्ञान ठीक होते हुए भी आचरण वैसा न होना अथवा शाब्दिक ज्ञान भी गलत होना- ये दोनों ही 'अविद्या' है। वास्तविक ज्ञान का ही दूसरा नाम=यथार्थ ज्ञान, तत्त्वज्ञान या विद्या है ।
वास्तव में व्यक्ति के पास जितनी भी सम्पत्तियाँ हैं, चाहे वे जड़ वस्तुएँ (भूमि , भवन, धन, शरीर, मन, बुद्धि आदि) हों; चाहे चेतन पुत्र, पौत्रादि हों; चाहे विद्याएँ, कलाएँ (अध्यापन, प्रवचनादि) हों, वे सब सम्पत्तियाँ ईश्वर की हैं, मनुष्य की अपनी नहीं हैं। वे सब वस्तुएँ ईश्वर ने उत्पन्न की हैं, वही उनका रक्षक, पालक है, वही उन सबका व्यवस्थापक है। इन सबका आदि मूल ईश्वर है। ईश्वर ही उन सबका स्वामी है, मनुष्य तो उन वस्तुओं का 'प्रयोक्ता ' मात्र है। ईश्वर ने मनुष्य को 'प्रयोग' करने के लिये वे सब वस्तुएँ और विद्याएँ दी हैं परन्तु भूल से
मनुष्य अपने आपको उन वस्तुओं और विद्याओं का मालिक (स्वामी) मान बैठता है। इसीलिये वह दुःखी भी होता है। इस 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को हटाने के लिये व्यक्ति स्वयं को उन वस्तुओं, विद्याओं का स्वामी न माने, बल्कि 'प्रयोक्ता' माने।
उदाहरण - एक व्यक्ति एक कम्पनी में प्रबन्धक के पद पर कार्य करता है। उस प्रबन्धक को कम्पनी की ओर से प्रबन्धादि कार्यों को करने के लिये एक कमरा, मेज़-कुर्सी, कागज़-पेन, वातानुकूलित यन्त्र, एक कार आदि वस्तुएँ दी गई हैं। वह प्रबन्धक इन सब वस्तुओं को कम्पनी की मानता है और इन सब का प्रयोग भी करता जाता है। अपने आप को वह इन वस्तुओं का 'प्रयोक्ता' मानता है, 'स्वामी' नहीं मानता। यदि कोई व्यक्ति कम्पनी की इन वस्तुओं को हानि पहुँचाने लगे, तो उससे इन वस्तुओं की रक्षा भी करता है, तब भी वह वस्तुओं
का 'स्वामी' कम्पनी को ही मानता है। यदि रक्षा के लिये पूरा प्रयत्न करने पर भी कोई वस्तु (कुर्सी आदि) टूट जाती हैं, तो उसे नहीं होता। वह सोचता है - 'मैंने इन वस्तुओं का प्रयोग किया। इनकी रक्षा करने का भी प्रयत्न किया। इस प्रकार से मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा निभाया। फिर भी यदि यह कुर्सी टूट गई, तो कम्पनी की कुर्सी टूटी, मेरी तो है नहीं। कम्पनी मुझे दूसरी कुर्सी मँगवा कर देगी। इस प्रकार से वह दुःखी नहीं होता। क्योंकि वह प्रबन्धक उन सब कुर्सी आदि वस्तुओं का 'स्वामी' कम्पनी को मानता है और स्वयं को 'प्रयोक्ता' मानता है। उसने उन वस्तुओं के साथ 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' नहीं जोड़ा और दुःखी भी नहीं हुआ।
अब दूसरे पक्ष में कल्पना करते हैं कि- जैसी कुर्सी उसके कार्यालय में थी, वैसी ही एक कुर्सी उसके अपने घर पर भी थी। यदि किसी दिन उसके अपने घर की कुर्सी टूट जाये, तो उसे दुःख होता है। तब वह सोचता है- 'हाय ! मेरी कुर्सी टूट गई ।' उस घर की कुर्सी के साथ वह 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' जोड़ लेता है, परिणाम स्वरूप उसे दुःख होता है।
इस उदाहरण के अनुसार हम 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को कैसे हटायें ? जितनी भी हमारे पास जड़ वस्तुएँ=(भूमि , भवन, धन, शरीर, बुद्धि, मन आदि) हैं; चेतन प्राणी= (पुत्र, पौत्र, भाई-बहन, माता-पिता आदि) हैं; और विद्याएँ, कलाएँ=(अध्यापन, प्रवचन, संगीत, विज्ञान, गणित आदि) हैं; इन सबका स्वामी 'ईश्वर' को मानें। ऐसा सोचें-'ये सब वस्तुएँ, विद्याएँ, कलाएँ ईश्वर ने हमें 'प्रयोग करने के लिये=(सांसारिक व्यवहारों की सिद्धि तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिये) दी हैं। इन सबका उत्पादक, रक्षक, पालक, व्यवस्थापक, 'स्वामी' तो ईश्वर ही है। हम ईश्वर-प्रदत्त इन वस्तुओं, विद्याओं का प्रयोग करेंगे, इनकी यथाशक्ति रक्षा करेंगे, इनकी वृद्धि करेंगे और योग्य व्यक्तियों के लिये उपर्युक्त वस्तुओं, विद्याओं को खर्च करेंगे। ईश्वर का हमारे लिये ऐसा ही आदेश है। इन वस्तुओं की रक्षा आदि करने पर भी यदि कोई वस्तु नष्ट भी हो जाएगी, तो हम दुःखरी नहीं होंगे। क्योंकि वह वस्तु हमारी नहीं है, ईश्वर की है।'
इस प्रकार से 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को हमें दूर करना चाहिये। जब हम उक्त प्रक्रिया से 'स्व-स्वामी-सम्बन्ध' को दूर कर देंगे, तो हममें से अभिमान, राग, ईष्ष्या-द्वेष, घृणा, अन्याय आदि सभी दोष दूर हो जायेंगे। तब यम-नियमों का आचरण भी अच्छी प्रकार से हो पाएगा और हम ईश्वर के निकट होते चले जाएँगे। आनन्द का जीवन जीयेंगे, दूसरों के जीवन में भी आनन्द उत्पन्न करेंगे। ईश्वर के निकट होते-होते, ईश्वर का साक्षात्कार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे।
दुःख का कारण = अविद्या
अनित्याशुचिदुत्नखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ (योगदर्शन २/५)
अर्थात् (१) अनित्य को नित्य समझना (२) अशुचि को शुचि समझना (३) दु:ख को सुख समझना और (४) अनात्मा को आत्मा समझना; अविद्या है। इस प्रकार से अविद्या के चार भाग हुए। साथ ही साथ इन चारों बातों को उल्टा करके भी देख् लीजिये। अर्थात् (१) नित्य को अनित्य समझना (२) शुचि को अशुचि समझना, (३) सुख
को दुःख समझना और (४) आत्मा को अनात्मा समझना भी अविद्या ही है। संक्षेप में अविद्या की परिभाषा यह हुई कि- जो वस्तु जैसी हो, उसको वैसा न समझकर, कुछ और ही समझना या उससे उल्टा समझना='अविद्या' है। और जैसे को तैसा समझना 'विद्या' है।
(१) अनित्य को नित्य समझना - नित्य का अर्थ होता है, जो वस्तु सदा रहे, कभी नष्ट न हो। नित्य शब्द में आरम्भ में 'अ' अक्षर जोड़कर (नञ्तत्पुरुष समास के अनुसार) शब्द बना लिया - अनित्य। अब इसका अर्थ उल्टा हो गया=जो वस्तु सदा न रहे, नष्ट हो जाये। तो अब प्रथम अविद्या का स्वरूप हो गया=अनित्य ( नष्ट होने वाली) वर्तुओं को नित्य (नष्ट न होने वाली) मानना। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ हैं, जो समय आने पर या कभी भी नष्ट हो जाती हैं। जैसे-शरीर, धन, सम्पत्ति, पुत्र-परिवार, पद-प्रतिष्ठा आदि।ये सब वस्तुएँ अनित्य कहलाती हैं, क्योंकि ये कभी भी नष्ट हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। परन्तु संसार के लोग इन अनित्य वस्तुओं को नित्य (सदा रहेंगी), ऐसा मानते हैं। इसीलिये दुःखी होते हैं।
यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाये कि- आपका शरीर नित्य है या अनित्य ? तो वह उत्तर देगा- अनित्य ! अर्थात् सदा जीवित नहीं रहेगा। शब्दों से तो उत्तर ठीक है। परन्तु क्या यह बात वास्तव में मन, बुद्धि में बैठ गई ? नहीं। मन में तो यही समझता है कि - मैं सदा जीवित रहूँगा, कभी नहीं मँगा। इसी का नाम अविद्या है।
ज्ञान दो प्रकार का है। (१) शाब्दिक ज्ञान (२) वास्तविक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान उसे कहते हैं- जब ज्ञान कुछ और हो एवं आचरण कुछ और हो। जैसे- सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कहता है - " मैं जानता हूँ, सिगरेट पीने से नुकसान होता है।" परन्तु फिर भी वह पीता है। आचरण, ज्ञान के अनुसार नहीं है, उससे भिन्न है। अत: सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का ज्ञान- 'शाब्दिक ज्ञान' है।
'वास्तविक ज्ञान' उसे कहते हैं- जब ज्ञान भी वैसा और आचरण भी वैसा। अर्थात् दोनों समान हों, भिन्न नहीं। जैसे- बिजली की तार को छूने से नुकसान होता है=(करण्ट लगता है, मृत्यु भी हो सकती है)। इस बात को जानने वालों का आचरण भी वैसा ही है। बिजली की तार को कोई नहीं छूता। इसे 'वास्तविक ज्ञान' कहते हैं। जो व्यक्ति शब्दों से कहता है- मैं सदा जीवित नहीं रहूँगा। परन्तु मन में ऐसा मानता है और आचरण भी ऐसा है कि- मैं सदा जीवित रहूँगा; उसका ज्ञान 'शाब्दिक' है। और शाब्दिक ज्ञान ठीक होते हुए भी आचरण वैसा न होना अथवा शाब्दिक ज्ञान भी गलत होना- ये दोनों ही 'अविद्या' है। वास्तविक ज्ञान का ही दूसरा नाम=यथार्थ ज्ञान, तत्त्वज्ञान या विद्या है ।
अब कुछ ही तत्त्वज्ञानी लोगों को छोड़कर, शेष सभी लोगों में यह अविद्या गहरी जड़ें जमा कर बैठी है- कि 'हम सदा जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। और जब मृत्यु आती है, तब रोते हैं, दुःखी होते हैं। इस दुःख का कारण- 'अनित्य शरीर को नित्य मानना', उक्त चार में से प्रथम अविद्या ही है।
प्रश्न = आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों में यह अविद्या है। और वे अनित्य शरीर को नित्य मानते हैं।
उत्तर= किसी भी व्यक्ति का व्यवहार/आचरण उसके वास्तविक ज्ञान की स्थिति को बतलाता है। उदाहरण- कुछ लोग दिल्ली से मुम्बई तक रेल में यात्रा कर रहे थे। बच्चे भी थे, कुछ बड़े (प्रौढ़) भी थे। रेल यात्रा सुखद रही। सब बच्चे हँसते-खेलते, रेल की सीटों पर कुदते-नाचते मुम्बई पहुँच गये। मुम्बई पहुँचने पर प्रौढ़ व्यक्तियों ने बच्चों से कहा- 'चलो, रेल से नीचे उतरो, मुम्बई आ गया है।' बच्चों को रेलयात्रा में बड़ा आनन्द आया था। वे रेल को छोड़ना नहीं चाहते थे। परन्तु प्रौढ़ व्यक्तियों के आदेश के कारण उन्हें रेल छोड़नी पड़ी । बड़ा कष्ट हुआ। प्रौढ़ व्यक्तियों को रेल छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ , बच्चों को कष्ट हुआ। क्यों ? प्रौढ़ व्यक्ति 'विद्या' में थे, वे वास्तव में जानते थे- रेल की सीटें हमें मुम्बई यात्रा तक ही मिली हैं। मुम्बई में वे छोड़नी पड़ेंगी। और उन्होंने मुम्बई में सीटें छोड़ देने का मन बना लिया था। अत: उन्हें रेल छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ। बच्चे 'अविद्या' में थे। उन्होंने रेल यात्रा में सुख का अनुभव करने के बाद यह मान लिया था- कि रेल की ये सीटें सदा हमारे साथ रहेंगी और हम सदा इसी तरह रेल में आनन्द मनाते रहेंगे। इसी अविद्या के कारण- जब बच्चों को मुम्बई में सीटें छोड़नी पड़ीं- तो दुःख हुआ।
संसार के लोगों की भी यही स्थिति है। ईश्वर की ओर से मनुष्यों को कुछ वर्ष तक जीने के लिये शरीर मिला है। लोगों ने अविद्या से यह मान लिया कि हम सदा जीयेंगे। मृत्यु आने पर जब शरीर छोड़ना पड़ा तो दुःख हुआ। जैसे बच्चे अविद्या के कारण रेल छोड़ते समय दुःखी हुऐ, वैसे ही संसार के लोग भी अविद्या के कारण मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय दुःखी हुए। उनके दुःखी होने के व्यवहार से पता चलता है कि लोगों में अविद्या है=(शाब्दिक ज्ञान है)। इस शाब्दिक ज्ञान=अविद्या से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वास्तविक कल्याण तो 'तत्त्वज्ञान' या 'विद्या' से ही होता है। अविद्या तो दुःख को ही उत्पन्न करती है।
इसी प्रकार से धन-सम्पत्ति, पुत्र परिवार, पद-प्रतिष्ठा आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये, कि ये सब भी 'अनित्य' ही हैं=(कभी भी नष्ट हो सकती हैं) परन्तु लोग इन सबको भी नित्य=(सदा हमारे साथ रहेंगी) ऐसा मानते हैं। अर्थात् 'अविद्या' में हैं। इसी अविद्या के कारण ही, जब इनमें से कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, तब दुःखी होते, रोते-चिल्लाते हैं। अत: दुःख का कारण अविद्या ही है। यह चर्चा हुई-अनित्य को नित्य मानना- अविद्या है, इस भाग की ।
अब इसे उल्टा करके देखिये। अर्थात् नित्य वस्तु को अनित्य मानना भी अविद्या है। आत्मा नित्य है या अनित्य ? नित्य। क्या आत्मा की उत्पत्ति होती है ? नहीं। क्या आत्मा का विनाश होता है ?
नहीं। आप कौन हैं - शरीर या आत्मा ? आत्मा। तो आप=(आत्मा) मर जाएँगे ? नहीं। तो फिर मरने से क्यों डरते हो। क्यों दुःखी होते हो। उत्तर स्पष्ट है- 'अविद्या' के कारण। 'आत्मा न जन्म लेता है न मरता है' यह सब शाब्दिक ज्ञान है। मन में तो अविद्या ही है- कि मैं मर जाऊँगा।' इसी अविद्या के कारण व्यक्ति मृत्यु से डरता है और दुःखी होता है। यहाँ तक अविद्या के चार भागों में से प्रथम भाग की चर्चा हुई। अब दूसरे भाग को देखिये।
(२) अशुचि को शुचि समझना - शुचि का अर्थ है- शुद्ध। इस 'शुचि' शब्द में भी पूर्ववत् 'अ' अक्षर जोड़ देने पर शब्द बन जाएगा- 'अशुचि'। और अर्थ भी उल्टा हो जाएगा- अशुद्ध। तो दूसरी अविद्या
हुई- अशुद्ध को शुद्ध मानना। इसके भी दो रूप हैं। (क) अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध मानना, (ख) अशुद्ध कर्मों को शुद्ध मानना।
(क) कुछ वस्तुएँ अशुद्ध हैं - जैसे शरीर, मांस, शराब, अण्डे, अफीम , तम्बाकू आदि। लोग इन शरीर आदि वस्तुओं को शुद्ध मानते हैं- यह अविद्या है। जब पुरुष, स्त्रियों को देखते हैं अथवा स्त्रियाँ, पुरुषों को देखती हैं; तो उन्हें एक दूसरे के शरीर अशुद्ध प्रतीत नहीं होते, बल्कि बहुत शुद्ध दीखते हैं। यही अविद्या है। शरीर वास्तव में कितना अशुद्ध है, यह बात तब समझ में आती है, जब कुछ गम्भीरता से इस प्रकार से शरीर के सम्बन्ध में चिन्तन किया जाये। शरीर में मल-मूत्र, रक्त, मांस, चर्बी आदि भरा पड़ा है। प्रतिदिन शौच, स्नानादि करके इसे जीवनभर शुद्ध करते रहते हैं, तब भी पूरा शुद्ध नहीं हो पाता। प्रतिदिन नया नया मल शरीर में उत्पन्न होता ही रहता है। चौबीस घण्टे शुद्ध वायु= (ओक्सीजन) का ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु= (कार्बन डाइ ओक्साइड) छोड़ते रहते है। जुकाम, बुखार, टी.बी., कैंसर, एड्स आदि जैसे भयंकर रोग इस शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। एक इंजक्शन की सुई एक व्यक्ति को लगाकर, वही सुई दूसरे व्यक्ति को नहीं लगा सकते।अन्यथा एक व्यक्ति का रोग दूसरे को लग सकता है। डॉक्टर लोग घाव पर पट्टी बाँध कर साबुन से हाथ धोते हैं । मृत्यु होने पर इस अशुद्ध शरीर को लोग दो दिन भी घर में रखना नहीं चाहते। इत्यादि घटनाओं से पता चलता है कि यह शरीर कितना अशुद्ध है। फिर भी आज संसार के लोग इस अशुद्ध शरीर को अत्यन्त शुद्ध मानकर इसके पीछे दिवाने=( पागल) हो रहे हैं। यह घोर अविद्या नहीं तो और क्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान लेने पर इसके प्रति राग=(Attachment) उत्पन्न होता है। जब यह शरीर अपना अशुद्ध रूप दिखाता है, तब व्यक्ति को दुःख होता है, आश्चर्य होता है कि -
'अरे! यह वही शरीर है जिसे मैं अत्यन्त शुद्ध मानता था। इसमें तो टी.बी; रक्त कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न हो गये हैं।'
इसी प्रकार से खान-पान के क्षेत्र में मांस, अण्डे, शराब, अफीम, तम्बाकू, गुटका-मसाला आदि वस्तुएँ भी अशुद्ध, (अभक्ष्य) और स्वास्थ्य एवं बुद्धिनाशक हैं। इन्हें भी लोग अशुद्ध नहीं मानते अथवा अशुद्ध मानते हुए भी इनका सेवन करते हैं, यह सब भी अविद्या है। ऐसी वस्तुओं का सेवन करने से फिर अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुःख भोगने पड़ते हैं । इस प्रकार से यह 'अविद्या' दुःखों का कारण बनती है।
(ख) कुछ कर्म अशुद्ध हैं - जैसे क्रोध करना, असत्य बोलना, चोरी, रिश्वत लेना-देना आदि। इन अशुद्ध कर्मों को भी लोग अशुद्ध=(बुरा) नहीं मानते। बल्कि परिस्थितियों आदि के अनेक बहाने बनाकर इन अशुद्ध कर्मों को करते रहते हैं। इन अशुद्ध =(बुरे) क्मों को शुद्ध मानना और करना अथवा बुरा मानते हुए भी परिस्थितियों के बहाने से करने में दोष न मानना अविद्या है। बुरे कर्म तो बुरे ही हैं। उनका तो दण्ड ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी बहाने से करें। क्या मजबूरी से चोरी करने पर वह अपराध नहीं माना जाता ? यदि आप कमजोर हैं और चोरी, झूठ, रिश्वत आदि बुरे कर्मों से बच नहीं पा रहे हैं; तो अपनी कमजोरी स्वीकार कीजिये । बहाने बनाने से आप इन बुरे कर्मों को करने पर, दोष से मुक्त नहीं हो जाएँगे। परन्तु परिस्थितियों के बहाने से इन बुरे कर्मों को करते हुए भी इनमें दोष न मानना अविद्या है। इसके कारण आगे इन करमों का दण्ड=(दुःख) भोगना पड़ेगा। इस प्रकार यह अविद्या दुःख का कारण बनेगी।
अब इसे भी उल्टा करके देख लीजिये। अर्थात् शुद्ध वस्तुओं (घी, दूध, फल, सात्त्विक भोजनादि) को अशुद्ध या पुराना भोजन मानकर इससे घृणा करना, इसका सेवन न करना भी अविद्या है । इसी प्रकार से सत्य बोलना, प्रेम-सभ्यता-नम्रता से व्यवहार करना, सेवा, दया, परोपकार आदि शुभ कर्मों को अशुभ कर्म मानना अथवा इन्हें पिछड़े कर्म मानकर इनसे घृणा करना भी अविद्या ही है। अब अविद्या के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे।
(३) दुःख को सुख समझना - दुःख दो प्रकार का है । (१) शुद्ध दुःख। जैसे-सिरदर्द, पेट दर्द आदि होने पर होता है। इसे तो सभी लोग दुःख ही मानते हैं। इसे सुख कोई भी नहीं मानता। परन्तु (२) दुःख, सुख में मिश्रित है, जो कि चार प्रकार का है। परिणाम दुःख , ताप दुःख, संस्कार दुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख । इसकी व्याख्या आप प्रथम लेख में पढ़ चुके हैं। संसार की वस्तुओं में विद्यमान इन चार दुःखों को व्यक्ति दुःख नहीं मानता, बल्कि वस्तुओं में शुद्ध सुख मानता है। अब इसे भी उल्टा करके देख लीजिये। अर्थात् सुख को दुःख समझना अविद्या है। माता-पिता की सेवा, बड़ों का आदर-सम्मान करना, विद्या-सत्संग, ईश्वर की उपासना आदि कर्मों में सुख मिलता है। परन्तु संसार के लोग (विशेष रूप से आजकल की नई पीढ़ी के युवा लोग) इन कर्मों में दु:ख का अनुभव करते हैं। और इन सुखदायक कर्मों की खिल्ली उड़ाते हैं । यह भी अविद्या ही है। यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसके कारण व्यक्ति दुःखी होता रहता है। अब अविद्या के चौथे भाग को देख्िये।
(४) अनात्मा को आत्मा समझना - आत्मा का अर्थ है- चेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ दो हैं। एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा = (ईश्वर)। आत्मा शब्द में आरम्भ में 'अन्' जोड़कर (नञ् तत्पुरुष समास
के अनुसार) शब्द बना लिया- अनात्मा। अब इसका अर्थ भी उलट गया। 'अनात्मा' का अर्थ बना- जो आत्मा नहीं है = (जीवात्मा और ईश्वर से भिन्न वस्तुएँ)। जीवात्मा (या जीव) तथा ईश्वर से भिन्न बहुत सी जड़ वस्तुएँ हैं । जैसे शरीर, मन, इन्द्रियाँ, धन-सम्पत्ति, पुत्रादि के शरीर, मूर्तियाँ, चित्र आदि । इन अनात्मा= (जड़) वस्तुओं को लोग आत्मा मानते हैं। अर्थात् या तो अपनी आत्मा का ही रूप मानते हैं, या अपनी आत्मा का एक हिस्सा मानते हैं। या इन जड़ वस्तुओं को चेतन तत्त्व मानते हैं। जैसे जड़ मूर्तियों को चेतन ईश्वर मानकर उन्हें खिलाना-पिलाना, सुलाना-जगाना, नहलाना-धुलाना आदि व्यवहार करते हैं। यह सब अविद्या है ।
प्रश्न = आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों में यह अविद्या है। और वे अनित्य शरीर को नित्य मानते हैं।
उत्तर= किसी भी व्यक्ति का व्यवहार/आचरण उसके वास्तविक ज्ञान की स्थिति को बतलाता है। उदाहरण- कुछ लोग दिल्ली से मुम्बई तक रेल में यात्रा कर रहे थे। बच्चे भी थे, कुछ बड़े (प्रौढ़) भी थे। रेल यात्रा सुखद रही। सब बच्चे हँसते-खेलते, रेल की सीटों पर कुदते-नाचते मुम्बई पहुँच गये। मुम्बई पहुँचने पर प्रौढ़ व्यक्तियों ने बच्चों से कहा- 'चलो, रेल से नीचे उतरो, मुम्बई आ गया है।' बच्चों को रेलयात्रा में बड़ा आनन्द आया था। वे रेल को छोड़ना नहीं चाहते थे। परन्तु प्रौढ़ व्यक्तियों के आदेश के कारण उन्हें रेल छोड़नी पड़ी । बड़ा कष्ट हुआ। प्रौढ़ व्यक्तियों को रेल छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ , बच्चों को कष्ट हुआ। क्यों ? प्रौढ़ व्यक्ति 'विद्या' में थे, वे वास्तव में जानते थे- रेल की सीटें हमें मुम्बई यात्रा तक ही मिली हैं। मुम्बई में वे छोड़नी पड़ेंगी। और उन्होंने मुम्बई में सीटें छोड़ देने का मन बना लिया था। अत: उन्हें रेल छोड़ने में कष्ट नहीं हुआ। बच्चे 'अविद्या' में थे। उन्होंने रेल यात्रा में सुख का अनुभव करने के बाद यह मान लिया था- कि रेल की ये सीटें सदा हमारे साथ रहेंगी और हम सदा इसी तरह रेल में आनन्द मनाते रहेंगे। इसी अविद्या के कारण- जब बच्चों को मुम्बई में सीटें छोड़नी पड़ीं- तो दुःख हुआ।
संसार के लोगों की भी यही स्थिति है। ईश्वर की ओर से मनुष्यों को कुछ वर्ष तक जीने के लिये शरीर मिला है। लोगों ने अविद्या से यह मान लिया कि हम सदा जीयेंगे। मृत्यु आने पर जब शरीर छोड़ना पड़ा तो दुःख हुआ। जैसे बच्चे अविद्या के कारण रेल छोड़ते समय दुःखी हुऐ, वैसे ही संसार के लोग भी अविद्या के कारण मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय दुःखी हुए। उनके दुःखी होने के व्यवहार से पता चलता है कि लोगों में अविद्या है=(शाब्दिक ज्ञान है)। इस शाब्दिक ज्ञान=अविद्या से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वास्तविक कल्याण तो 'तत्त्वज्ञान' या 'विद्या' से ही होता है। अविद्या तो दुःख को ही उत्पन्न करती है।
इसी प्रकार से धन-सम्पत्ति, पुत्र परिवार, पद-प्रतिष्ठा आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये, कि ये सब भी 'अनित्य' ही हैं=(कभी भी नष्ट हो सकती हैं) परन्तु लोग इन सबको भी नित्य=(सदा हमारे साथ रहेंगी) ऐसा मानते हैं। अर्थात् 'अविद्या' में हैं। इसी अविद्या के कारण ही, जब इनमें से कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, तब दुःखी होते, रोते-चिल्लाते हैं। अत: दुःख का कारण अविद्या ही है। यह चर्चा हुई-अनित्य को नित्य मानना- अविद्या है, इस भाग की ।
अब इसे उल्टा करके देखिये। अर्थात् नित्य वस्तु को अनित्य मानना भी अविद्या है। आत्मा नित्य है या अनित्य ? नित्य। क्या आत्मा की उत्पत्ति होती है ? नहीं। क्या आत्मा का विनाश होता है ?
नहीं। आप कौन हैं - शरीर या आत्मा ? आत्मा। तो आप=(आत्मा) मर जाएँगे ? नहीं। तो फिर मरने से क्यों डरते हो। क्यों दुःखी होते हो। उत्तर स्पष्ट है- 'अविद्या' के कारण। 'आत्मा न जन्म लेता है न मरता है' यह सब शाब्दिक ज्ञान है। मन में तो अविद्या ही है- कि मैं मर जाऊँगा।' इसी अविद्या के कारण व्यक्ति मृत्यु से डरता है और दुःखी होता है। यहाँ तक अविद्या के चार भागों में से प्रथम भाग की चर्चा हुई। अब दूसरे भाग को देखिये।
(२) अशुचि को शुचि समझना - शुचि का अर्थ है- शुद्ध। इस 'शुचि' शब्द में भी पूर्ववत् 'अ' अक्षर जोड़ देने पर शब्द बन जाएगा- 'अशुचि'। और अर्थ भी उल्टा हो जाएगा- अशुद्ध। तो दूसरी अविद्या
हुई- अशुद्ध को शुद्ध मानना। इसके भी दो रूप हैं। (क) अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध मानना, (ख) अशुद्ध कर्मों को शुद्ध मानना।
(क) कुछ वस्तुएँ अशुद्ध हैं - जैसे शरीर, मांस, शराब, अण्डे, अफीम , तम्बाकू आदि। लोग इन शरीर आदि वस्तुओं को शुद्ध मानते हैं- यह अविद्या है। जब पुरुष, स्त्रियों को देखते हैं अथवा स्त्रियाँ, पुरुषों को देखती हैं; तो उन्हें एक दूसरे के शरीर अशुद्ध प्रतीत नहीं होते, बल्कि बहुत शुद्ध दीखते हैं। यही अविद्या है। शरीर वास्तव में कितना अशुद्ध है, यह बात तब समझ में आती है, जब कुछ गम्भीरता से इस प्रकार से शरीर के सम्बन्ध में चिन्तन किया जाये। शरीर में मल-मूत्र, रक्त, मांस, चर्बी आदि भरा पड़ा है। प्रतिदिन शौच, स्नानादि करके इसे जीवनभर शुद्ध करते रहते हैं, तब भी पूरा शुद्ध नहीं हो पाता। प्रतिदिन नया नया मल शरीर में उत्पन्न होता ही रहता है। चौबीस घण्टे शुद्ध वायु= (ओक्सीजन) का ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु= (कार्बन डाइ ओक्साइड) छोड़ते रहते है। जुकाम, बुखार, टी.बी., कैंसर, एड्स आदि जैसे भयंकर रोग इस शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। एक इंजक्शन की सुई एक व्यक्ति को लगाकर, वही सुई दूसरे व्यक्ति को नहीं लगा सकते।अन्यथा एक व्यक्ति का रोग दूसरे को लग सकता है। डॉक्टर लोग घाव पर पट्टी बाँध कर साबुन से हाथ धोते हैं । मृत्यु होने पर इस अशुद्ध शरीर को लोग दो दिन भी घर में रखना नहीं चाहते। इत्यादि घटनाओं से पता चलता है कि यह शरीर कितना अशुद्ध है। फिर भी आज संसार के लोग इस अशुद्ध शरीर को अत्यन्त शुद्ध मानकर इसके पीछे दिवाने=( पागल) हो रहे हैं। यह घोर अविद्या नहीं तो और क्या है। अशुद्ध शरीर को शुद्ध मान लेने पर इसके प्रति राग=(Attachment) उत्पन्न होता है। जब यह शरीर अपना अशुद्ध रूप दिखाता है, तब व्यक्ति को दुःख होता है, आश्चर्य होता है कि -
'अरे! यह वही शरीर है जिसे मैं अत्यन्त शुद्ध मानता था। इसमें तो टी.बी; रक्त कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न हो गये हैं।'
इसी प्रकार से खान-पान के क्षेत्र में मांस, अण्डे, शराब, अफीम, तम्बाकू, गुटका-मसाला आदि वस्तुएँ भी अशुद्ध, (अभक्ष्य) और स्वास्थ्य एवं बुद्धिनाशक हैं। इन्हें भी लोग अशुद्ध नहीं मानते अथवा अशुद्ध मानते हुए भी इनका सेवन करते हैं, यह सब भी अविद्या है। ऐसी वस्तुओं का सेवन करने से फिर अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुःख भोगने पड़ते हैं । इस प्रकार से यह 'अविद्या' दुःखों का कारण बनती है।
(ख) कुछ कर्म अशुद्ध हैं - जैसे क्रोध करना, असत्य बोलना, चोरी, रिश्वत लेना-देना आदि। इन अशुद्ध कर्मों को भी लोग अशुद्ध=(बुरा) नहीं मानते। बल्कि परिस्थितियों आदि के अनेक बहाने बनाकर इन अशुद्ध कर्मों को करते रहते हैं। इन अशुद्ध =(बुरे) क्मों को शुद्ध मानना और करना अथवा बुरा मानते हुए भी परिस्थितियों के बहाने से करने में दोष न मानना अविद्या है। बुरे कर्म तो बुरे ही हैं। उनका तो दण्ड ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी बहाने से करें। क्या मजबूरी से चोरी करने पर वह अपराध नहीं माना जाता ? यदि आप कमजोर हैं और चोरी, झूठ, रिश्वत आदि बुरे कर्मों से बच नहीं पा रहे हैं; तो अपनी कमजोरी स्वीकार कीजिये । बहाने बनाने से आप इन बुरे कर्मों को करने पर, दोष से मुक्त नहीं हो जाएँगे। परन्तु परिस्थितियों के बहाने से इन बुरे कर्मों को करते हुए भी इनमें दोष न मानना अविद्या है। इसके कारण आगे इन करमों का दण्ड=(दुःख) भोगना पड़ेगा। इस प्रकार यह अविद्या दुःख का कारण बनेगी।
अब इसे भी उल्टा करके देख लीजिये। अर्थात् शुद्ध वस्तुओं (घी, दूध, फल, सात्त्विक भोजनादि) को अशुद्ध या पुराना भोजन मानकर इससे घृणा करना, इसका सेवन न करना भी अविद्या है । इसी प्रकार से सत्य बोलना, प्रेम-सभ्यता-नम्रता से व्यवहार करना, सेवा, दया, परोपकार आदि शुभ कर्मों को अशुभ कर्म मानना अथवा इन्हें पिछड़े कर्म मानकर इनसे घृणा करना भी अविद्या ही है। अब अविद्या के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे।
(३) दुःख को सुख समझना - दुःख दो प्रकार का है । (१) शुद्ध दुःख। जैसे-सिरदर्द, पेट दर्द आदि होने पर होता है। इसे तो सभी लोग दुःख ही मानते हैं। इसे सुख कोई भी नहीं मानता। परन्तु (२) दुःख, सुख में मिश्रित है, जो कि चार प्रकार का है। परिणाम दुःख , ताप दुःख, संस्कार दुःख और गुणवृत्तिविरोध दुःख । इसकी व्याख्या आप प्रथम लेख में पढ़ चुके हैं। संसार की वस्तुओं में विद्यमान इन चार दुःखों को व्यक्ति दुःख नहीं मानता, बल्कि वस्तुओं में शुद्ध सुख मानता है। अब इसे भी उल्टा करके देख लीजिये। अर्थात् सुख को दुःख समझना अविद्या है। माता-पिता की सेवा, बड़ों का आदर-सम्मान करना, विद्या-सत्संग, ईश्वर की उपासना आदि कर्मों में सुख मिलता है। परन्तु संसार के लोग (विशेष रूप से आजकल की नई पीढ़ी के युवा लोग) इन कर्मों में दु:ख का अनुभव करते हैं। और इन सुखदायक कर्मों की खिल्ली उड़ाते हैं । यह भी अविद्या ही है। यह अविद्या का तीसरा भाग है। इसके कारण व्यक्ति दुःखी होता रहता है। अब अविद्या के चौथे भाग को देख्िये।
(४) अनात्मा को आत्मा समझना - आत्मा का अर्थ है- चेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ दो हैं। एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा = (ईश्वर)। आत्मा शब्द में आरम्भ में 'अन्' जोड़कर (नञ् तत्पुरुष समास
के अनुसार) शब्द बना लिया- अनात्मा। अब इसका अर्थ भी उलट गया। 'अनात्मा' का अर्थ बना- जो आत्मा नहीं है = (जीवात्मा और ईश्वर से भिन्न वस्तुएँ)। जीवात्मा (या जीव) तथा ईश्वर से भिन्न बहुत सी जड़ वस्तुएँ हैं । जैसे शरीर, मन, इन्द्रियाँ, धन-सम्पत्ति, पुत्रादि के शरीर, मूर्तियाँ, चित्र आदि । इन अनात्मा= (जड़) वस्तुओं को लोग आत्मा मानते हैं। अर्थात् या तो अपनी आत्मा का ही रूप मानते हैं, या अपनी आत्मा का एक हिस्सा मानते हैं। या इन जड़ वस्तुओं को चेतन तत्त्व मानते हैं। जैसे जड़ मूर्तियों को चेतन ईश्वर मानकर उन्हें खिलाना-पिलाना, सुलाना-जगाना, नहलाना-धुलाना आदि व्यवहार करते हैं। यह सब अविद्या है ।
लोग शरीर को, (जो कि आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न है, जड़ है), आत्मा (या चेतन) मानते हैं। यह अविद्या है। जड़ शरीर को चेतन आत्मा मान लेने से, इस अविद्या से, शरीर में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो कि दुःख का कारण बनती है, (जब शरीर मरने पर जड़ प्रतीत होता है)। इसी प्रकार से मन भी जड़ वस्तु है, इसे भी अविद्या के कारण लोग चेतन मान लेते हैं। फिर शिकायत करते हैं- 'मन बड़ा चंचल है। मानता नहीं है। संसार में भटकाता रहता है। यह सब मानना अविद्या है। इसके कारण व्यक्ति मन का नियन्त्रण कर नहीं पाते और अनेक दुःख भोगते हैं। स्कूटर, कार आदि जड़ वस्तुएँ हैं=(स्वयं क्रिया नहीं कर सकतीं)। इनको तो लोग जड़ मान चुके हैं, अत: शिकायत नहीं करते- 'कि मेरा स्कूटर या कार नहीं मानती। यह सड़क से अपने आप नीचे उतर जाती है। परन्तु मन के बारे में अविद्या है। जबकि मन भी कार आदि के समान ही जड़ है, लेकिन लोग इसे चेतन मानते हैं ।
ऐसे ही धन-सम्पत्ति, पुत्रादि के शरीर इत्यादि वस्तुओं के सम्बन्ध में जानना चाहिये कि- ये भी अनात्मा=(आत्मा रूप या हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं) हैं। परन्तु अविद्या के कारण लोग इन वस्तुओं को भी अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं। फिर दुःखी होते हैं।
प्रश्न = आप कैसे कह सकते हैं कि लोग धन-सम्पत्ति आदि को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं ?
उत्तर = जब व्यापार में या और भी किसी वस्तु कार आदि के टूट जाने पर धन की हानि होती है, तब व्यक्ति के हृदय पर झटका=(Heart-Attack) लगता है। कभी-कभी मृत्यु तक भी हो जाती है। यह तभी होता है, जब व्यक्ति उन सम्पत्तियों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। जब उन सम्पत्तियों की वृद्धि होती है, तो अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ खुश होता है। जब सम्पत्तियाँ नष्ट होती हैं, तो आत्मा का नाश मानता हुआ दुःखी होता है। ऐसा मानना अविद्या ही तो है। जबकि आत्मा उन कार, मकान, धनादि सम्पत्तियों से बिल्कुल भिन्न वस्तु है। कार आदि के नष्ट होने से आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वह पूरी तरह सुरक्षित है। परन्तु लोग अविद्या के कारण दुःखी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार आदि सम्पत्तियों की रक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कार आदि के नष्ट होने पर आत्मा तो नष्ट होता नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि- कार आदि सम्पत्तियाँ, जीवन-रक्षा एवं मोक्ष-प्राप्ति का साधन हैं। इन साधनों की सुरक्षा और उपयोग तो करना चाहिये। परन्तु ये साधन अनित्य होने के कारण कभी भी नष्ट हो सकते हैं। पूरी सुरक्षा करने का प्रयत्न करने पर भी यदि ये नष्ट हो जायें, तब दुःखी नहीं होना चाहिये। तब विद्यापूर्वक ऐसे सोचना चाहिये- "कार आदि वस्तुएँ अनित्य हैं । कभी न कभी तो नष्ट होंगी ही। हमने इनकी सुरक्षा का पूरा प्रयत्न किया। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर भी यदि नष्ट हो गईं, तो हम=(आत्मा) तो सुरक्षित हैं, फिर दोबारा धन कमा कर पुन: प्राप्त कर लेंगे।" यदि ऐसे सोचेंगे, तो 'विद्या' के कारण दुःखी नहीं होंगे। अन्यथा अविद्या के कारण अवश्य दुःखी होंगे।
अब अन्त में इसे भी उलट कर देख लीजिये। अर्थात् आत्मा को अनात्मा=(चेतन को जड़) मानना भी अविद्या है। ईश्वर चेतन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है। वह हमारी सब भावनाओं व कर्मों को समझता एवं देख्ता है। तदनुसार ठीक-ठीक न्याय से हमारे कर्मों का फल भी देता है। ऐसे चेतन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर के बारे में पाप कर्म करते समय ऐसा सोचना, कि- 'मुझे कोई नहीं देख, जान रहा। ईश्वर तो यहाँ है नहीं। या ईश्वर को जड़ मूर्ति के रूप में मानकर हमारे पाप कर्मों का वह द्रष्टा=(ज्ञाता/साक्षी) नहीं है', ऐसा सोचना भी अविद्या ही है। इसका आगे दण्ड/दुःख मिलेगा।
इसी तरह से सामने उपस्थित बुद्धिमान् व्यक्ति को भी मूर्ख समझकर ऐसा सोचना-'कि यह व्यक्ति मेरी चालाकी को क्या समझ पाएगा!' यह भी अविद्या ही है। इस अविद्या के कारण व्यक्ति पाप/अपराध कर्म करता रहता है। और आगे चलकर इन कर्मों का दुःख रूप फल ईश्वर एवं अन्य अधिकारी मनुष्यों से प्राप्त करता रहता है। यह चौथे प्रकार की अविद्या की चर्चा पूर्ण हुई।
सार यह है कि हमारे दुःखों का अधिकतम कारण हमारी अपनी अविद्या ही है। आइये, अगले लेखों में इसे दूर करने के उपायों को समझने का प्रयत्न करें।
वैदिक दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप निम्न बतलाया गया है।
तात्पर्य यह हुआ कि समस्त दुःखों से छूटकर ईश्वर के पूर्ण, स्थायी परम आनन्द को प्राप्त कर लेना मुक्ति है। वैदिक दर्शनों, उपनिषदों और वेदों के अनुसार यही मुक्ति का स्वरूप है।
उदाहरणार्थ-कठोपनिषद् में कहा है-
वेद में भी ऐसा ही कहा है-
उपर्युक्त मुक्ति को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, इस विषय पर अब विचार करते हैं।
जैसा कि ऊपर उपनिषद् के वचन और वेद के मन्त्र में बतलाया गया है कि-ईश्वर को जानकर ही मनुष्य दुःखों से पूर्णतया छूट सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से दर्शनों में भी मुक्ति प्राप्त करने का उपाय ज्ञान=तत्त्वज्ञान बतलाया गया है। इस संसार में तीन तत्त्व हैं-ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। अतः इन तीन तत्त्वों को ठीक ठीक व्यावहारिक रूप से जान लेना ही मुक्ति का उपाय है। परन्तु इन तीनों में भी मुख्य रूप से ईश्वर को जानना। यद्यपि दु:खों से छूटने और परम आनन्द को प्राप्त करने का सीधा उपाय तो ईश्वर को जानना ही है, जैसा कि वेदमन्त्र में कहा गया था। परन्तु ईश्वर अत्यन्त सूक्ष्म है, आत्मा और प्रकृति को जाने बिना वह जाना ही नहीं जाना, इसलिये ऐसा कह देते हैं कि तीनों तत्त्वों का ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। इससे दोनों बातों में कोई विरोध नहीं आता। चाहे ऐसा कहें कि- ईश्वर को जानना मुक्ति का उपाय है, चाहे ऐसा कह दें कि- तीन तत्त्वों का जानना मुक्ति का उपाय है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता।
तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति होती है इस तथ्य को अब दर्शन शास्त्रों में देखना है
उपर्युक्त प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया कि तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। परन्तु क्या तत्त्वज्ञान होते ही मुक्ति हो जाती है अथवा अन्य भी कुछ कार्य करना पड़ता है ? अन्तत: तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे।
'तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया' को समझने के लिये हम न्यायदर्शन के निम्न सूत्र का आश्रय लेते हैं ।
दुःख भी हट जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी।
ऐसे ही धन-सम्पत्ति, पुत्रादि के शरीर इत्यादि वस्तुओं के सम्बन्ध में जानना चाहिये कि- ये भी अनात्मा=(आत्मा रूप या हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं) हैं। परन्तु अविद्या के कारण लोग इन वस्तुओं को भी अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं। फिर दुःखी होते हैं।
प्रश्न = आप कैसे कह सकते हैं कि लोग धन-सम्पत्ति आदि को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं ?
उत्तर = जब व्यापार में या और भी किसी वस्तु कार आदि के टूट जाने पर धन की हानि होती है, तब व्यक्ति के हृदय पर झटका=(Heart-Attack) लगता है। कभी-कभी मृत्यु तक भी हो जाती है। यह तभी होता है, जब व्यक्ति उन सम्पत्तियों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। जब उन सम्पत्तियों की वृद्धि होती है, तो अपनी आत्मा की वृद्धि मानता हुआ खुश होता है। जब सम्पत्तियाँ नष्ट होती हैं, तो आत्मा का नाश मानता हुआ दुःखी होता है। ऐसा मानना अविद्या ही तो है। जबकि आत्मा उन कार, मकान, धनादि सम्पत्तियों से बिल्कुल भिन्न वस्तु है। कार आदि के नष्ट होने से आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वह पूरी तरह सुरक्षित है। परन्तु लोग अविद्या के कारण दुःखी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कार आदि सम्पत्तियों की रक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कार आदि के नष्ट होने पर आत्मा तो नष्ट होता नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि- कार आदि सम्पत्तियाँ, जीवन-रक्षा एवं मोक्ष-प्राप्ति का साधन हैं। इन साधनों की सुरक्षा और उपयोग तो करना चाहिये। परन्तु ये साधन अनित्य होने के कारण कभी भी नष्ट हो सकते हैं। पूरी सुरक्षा करने का प्रयत्न करने पर भी यदि ये नष्ट हो जायें, तब दुःखी नहीं होना चाहिये। तब विद्यापूर्वक ऐसे सोचना चाहिये- "कार आदि वस्तुएँ अनित्य हैं । कभी न कभी तो नष्ट होंगी ही। हमने इनकी सुरक्षा का पूरा प्रयत्न किया। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। फिर भी यदि नष्ट हो गईं, तो हम=(आत्मा) तो सुरक्षित हैं, फिर दोबारा धन कमा कर पुन: प्राप्त कर लेंगे।" यदि ऐसे सोचेंगे, तो 'विद्या' के कारण दुःखी नहीं होंगे। अन्यथा अविद्या के कारण अवश्य दुःखी होंगे।
अब अन्त में इसे भी उलट कर देख लीजिये। अर्थात् आत्मा को अनात्मा=(चेतन को जड़) मानना भी अविद्या है। ईश्वर चेतन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है। वह हमारी सब भावनाओं व कर्मों को समझता एवं देख्ता है। तदनुसार ठीक-ठीक न्याय से हमारे कर्मों का फल भी देता है। ऐसे चेतन, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर के बारे में पाप कर्म करते समय ऐसा सोचना, कि- 'मुझे कोई नहीं देख, जान रहा। ईश्वर तो यहाँ है नहीं। या ईश्वर को जड़ मूर्ति के रूप में मानकर हमारे पाप कर्मों का वह द्रष्टा=(ज्ञाता/साक्षी) नहीं है', ऐसा सोचना भी अविद्या ही है। इसका आगे दण्ड/दुःख मिलेगा।
इसी तरह से सामने उपस्थित बुद्धिमान् व्यक्ति को भी मूर्ख समझकर ऐसा सोचना-'कि यह व्यक्ति मेरी चालाकी को क्या समझ पाएगा!' यह भी अविद्या ही है। इस अविद्या के कारण व्यक्ति पाप/अपराध कर्म करता रहता है। और आगे चलकर इन कर्मों का दुःख रूप फल ईश्वर एवं अन्य अधिकारी मनुष्यों से प्राप्त करता रहता है। यह चौथे प्रकार की अविद्या की चर्चा पूर्ण हुई।
सार यह है कि हमारे दुःखों का अधिकतम कारण हमारी अपनी अविद्या ही है। आइये, अगले लेखों में इसे दूर करने के उपायों को समझने का प्रयत्न करें।
दुःरव का निवारण=दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप और उसके उपाय
इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुखों एवं दुःखों को भोगता है। यदि कुछ गम्भीरता से विचार किया जाये, तो यह पता चलता है कि पशु-पक्षी आदि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों को दुःख कम और सुख अधिक प्राप्त होता है। और यदि कुछ और अधिक गम्भीरता से विचार किया जाये, तो यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य आदि सभी प्राणी सुख को तो प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु दुःख को नहीं चाहते। दु:ख से छूटने और सुख को प्राप्त करने के लिये सभी प्राणी अपनी अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न भी करते हैं। पर्तु ईश्वर के द्वारा न्यायपूर्ण ढंग से रचे हुए इस संसार में केवल मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो सब प्रकार के दुःखों से पुरुषार्थ करने पर छूट सकता है। अन्य प्राणियों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने अपने पशु-पक्षी आदि शरीरों के द्वारा पुरुषार्थ करके समस्त दुःखों से छूट सकें। इन सांसारिक दुःखों से छूटने और ईश्वर के परम आनन्द को प्राप्त करने का नाम ही वैदिक दर्शनों, उपनिषदों एवं वेदों में मुक्ति है ।वैदिक दर्शनों में मुक्ति का स्वरूप निम्न बतलाया गया है।
(१) तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ॥ (न्याय दर्शन १/१/२२)
अर्थात् सब प्रकार के दुःखों से बिल्कुल छूट जाना अपवर्ग=मुक्ति है।
(२) तदभावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्षः । (वैशेषिकदर्शन ५/२/१८)
अर्थात् वर्तमान शरीर के छूट जाने पर नये=अगले शरीर के साथ सम्बन्ध न होना (और अगले शरीर के साथ सम्बन्ध न होने से) अगला जन्म न होना (तथा जन्म न होने पर दुःखों की प्राप्ति न होना=दुःखों से छूट जाना) मोक्ष=मुक्ति है ।
(३) ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥ (वेदान्तदर्शन ४/४/५)
अर्थात् जैमिनि आचार्य का मत है कि जब आत्मा (इन शरीर आदि के बन्धनों से छूटकर) ब्रह्म = परमात्मा के धर्म=आनन्द गुण से युक्त होकर सर्वत्र स्वच्छन्द विचरता है, तो उसे मुक्ति कहते हैं ।
(४) अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ (सांख्यदर्शन १/१)
अर्थात् तीन प्रकार के=(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक) दुःखों से सर्वथा छूट जाना पुरुष=आत्मा का अन्तिम लक्ष्य है, (इसी को मुक्ति कहते हैं) ।
(५) पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः
कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।। (योगदर्शन ४/३४)
अर्थात् आत्मा के प्रयोजन=लक्ष्य=(मुक्ति) को जो शरीर, इन्द्रियाँ आदि पदार्थ पूरा करा चुके हैं, उनका प्रकृति में विलीन हो जाना और आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर (ईश्वर के आनन्द में मग्न हो जाना) मुक्ति है।तात्पर्य यह हुआ कि समस्त दुःखों से छूटकर ईश्वर के पूर्ण, स्थायी परम आनन्द को प्राप्त कर लेना मुक्ति है। वैदिक दर्शनों, उपनिषदों और वेदों के अनुसार यही मुक्ति का स्वरूप है।
उदाहरणार्थ-कठोपनिषद् में कहा है-
अशब्दम......! अनाद्यनन्तं महत: परं श्रुवं निचाय्य
तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ (कठोपनिषद् ३/१५)
अर्थात् उस अनादि अनन्त, संसार के समस्त पदार्थों से भी सूक्ष्म, स्थिर ब्रह्म को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु आदि दुःखों से छूट पाता है। तब क्योंकि वह ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, इसलिये उस ईश्वर के आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाता है और समस्त दुःखो से छुटकारा पा लेता है, यही मुक्ति है।वेद में भी ऐसा ही कहा है-
वेदाहमेतं पुरुष.. तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः
पन्था विद्यतेऽयनाय ।। (यजुर्वेद ३१/१८)
अर्थात् उसी महान् पुरुष=परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु आदि बड़े-बड़े दुःखों से पार हो सकता है, (और ईश्वर के आनन्द को प्राप्त कर सकता है) दुःखों से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। वेद की दृष्टि में भी यही मुक्ति की अवस्था है।उपर्युक्त मुक्ति को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है, इस विषय पर अब विचार करते हैं।
जैसा कि ऊपर उपनिषद् के वचन और वेद के मन्त्र में बतलाया गया है कि-ईश्वर को जानकर ही मनुष्य दुःखों से पूर्णतया छूट सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से दर्शनों में भी मुक्ति प्राप्त करने का उपाय ज्ञान=तत्त्वज्ञान बतलाया गया है। इस संसार में तीन तत्त्व हैं-ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। अतः इन तीन तत्त्वों को ठीक ठीक व्यावहारिक रूप से जान लेना ही मुक्ति का उपाय है। परन्तु इन तीनों में भी मुख्य रूप से ईश्वर को जानना। यद्यपि दु:खों से छूटने और परम आनन्द को प्राप्त करने का सीधा उपाय तो ईश्वर को जानना ही है, जैसा कि वेदमन्त्र में कहा गया था। परन्तु ईश्वर अत्यन्त सूक्ष्म है, आत्मा और प्रकृति को जाने बिना वह जाना ही नहीं जाना, इसलिये ऐसा कह देते हैं कि तीनों तत्त्वों का ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। इससे दोनों बातों में कोई विरोध नहीं आता। चाहे ऐसा कहें कि- ईश्वर को जानना मुक्ति का उपाय है, चाहे ऐसा कह दें कि- तीन तत्त्वों का जानना मुक्ति का उपाय है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता।
तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति होती है इस तथ्य को अब दर्शन शास्त्रों में देखना है
(१) ज्ञानान्मुक्तिः ॥ (सांख्यदर्शन ३/२३)
तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति होती है ।
(२) बन्धो विपर्ययात् ।। (सांख्यदर्शन ३/२४)
इसके विपरीत अर्थात् मिथ्याज्ञान से बन्धन=दुःख होता है।
(३) विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ (योगदर्शन २/२६)
अर्थात् विवेकख्याति=तत्वज्ञान=ईश्वर, आत्मा और प्रकृति का यथार्थ एवं स्थिर=(दृढ़) ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है ।
(४) धर्मविशेषप्रसूताद्..तत्वज्ञानान्निःश्रेयसम् ॥ (वैशेषिकदर्शन १/१/४)
अर्थात् तत्त्वज्ञान नामक धर्मविशेष से नि:श्रेयस=मोक्ष की प्राप्ति होती है ।
(५) प्रमाणप्रमेय...तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः ।। (न्यायदर्शन १/१/१)
अर्थात् प्रमाण, प्रमेय आदि १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सूत्र में कथित प्रमेय नामक पदार्थ के अन्तर्गत आत्मा आदि तत्त्व आ जाते हैं। अत: सार यह हुआ कि-ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के तत्त्वज्ञान=यथार्थज्ञान=सम्यग्ज्ञान से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं।उपर्युक्त प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया कि तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। परन्तु क्या तत्त्वज्ञान होते ही मुक्ति हो जाती है अथवा अन्य भी कुछ कार्य करना पड़ता है ? अन्तत: तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे।
'तत्त्वज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया' को समझने के लिये हम न्यायदर्शन के निम्न सूत्र का आश्रय लेते हैं ।
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुक्तरोत्तरापाये
तदनन्तरापायादपवर्गः ॥ (न्यायदर्शन १/१/२)
अर्थात् दुःख, जन्म, प्रवृत्ति=(सकाम कर्म=पाप-पुण्य) , दोष=(राग, द्वेष, व मोह) और मिथ्याज्ञान में से अगले-अगले पदार्थों के हट जाने पर, उसके पश्चात् जो बचे रहे उसके भी हट जाने से, अपवर्ग=मुक्ति हो जाती है। अर्थात् इन पाँच पदार्थों में से उल्टे क्रम से एक-एक पदार्थ हटता जाएगा और अन्त में दुःख के हट जाने पर मुक्ति हो जाएगी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है । उल्टे क्रम से हटने का अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले मिथ्याज्ञान हटेगा, फिर दोष हटेंगे, फिर प्रवृत्ति हटेगी, फिर जन्म हटेगा और अन्त में दुःख हट जाएगा, जबदुःख भी हट जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी।
मोक्ष-प्राप्ति का उपाय बतलाया गया था तत्त्वज्ञान। उसका इस प्रक्रिया से क्या सम्बन्ध है ? देखिये, प्रस्तुत सूत्र में= (मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया वाले सूत्र में) जो पाँच पदार्थ बतलाये गये हैं, उनमें से जो सबसे पहले हटने वाला पदार्थ है, वह है मिथ्याज्ञान। और जो मोक्ष-प्राप्ति का उपाय है वह है तत्त्वज्ञान। ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। संसार में यह नियम है कि दो विरोधी गुण एक ही समय में, एक ही वस्तु में, साथ-साथ रह नहीं सकते, एक समय में एक ही रह सकता है। इसलिये जब मनुष्य में मिथ्याज्ञान विद्यमान होता है, तब तत्त्वज्ञान नहीं होता और जब तत्त्ज्ञान आता है तब मिथ्याज्ञान नहीं ठहर सकता। यही मोक्ष प्राप्ति के उपाय=(तत्वज्ञान) का और प्रस्तुत सूत्र में कही गई मोक्ष-प्राप्ति की प्रक्रिया का सम्बन्ध है कि - तत्त्वज्ञान के प्राप्त हो जाने पर मिथ्याज्ञान हट जाता है। और मिथ्याज्ञान के हट जाने पर क्रमश: दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुःख भी हट जाते हैं, तब मुक्ति हो जाती है। अत: तत्त्वज्ञान को मोक्षप्राप्ति का उपाय ठीक ही कहा गया है।
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि- तत्त्वज्ञान तो मिथ्याज्ञान का विरोधी है, इसलिये जब तत्त्वज्ञान प्राप्त होता तो मिथ्याज्ञान हट जाता है। परन्तु मिथ्याज्ञान के हट जाने पर दोष, प्रवृत्ति, जन्म एवं दु:ख क्यों हट जाते हैं? इनका आपस में क्या सम्बन्ध है?
इस प्रश्न का समाधान यह है कि- संसार में एक नियम है-
कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। जैसे बिजली के न रहने पर पंखा, मशीन आदि नहीं चलते। बिजली उनके चलाने का कारण है और पंख्रे मशीन आदि का चलना उसका कार्य है। जब बिजली नहीं रहती तो वह कार्य भी नहीं रहता। ठीक इसी नियम के अनुसार ये पांचों पदार्थ भी एक-दूसरे के कारण हैं। इनमें परस्पर कारण-कार्य सम्बन्ध है। अर्थात् जो सूत्र में पहले स्थान पर बतलाया गया दुःख है, उसका कारण- सुत्र में दूसरे स्थान पर बतलाया गया जन्म है। जब किसी का जन्म हो जाता है, तभी उसे अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते है। इसी प्रकार से जन्म का कारण सूत्र में तीसरे स्थान पर बतलाया गया प्रवृत्ति (सकाम कर्म) है। प्रवृत्ति का कारण=सूत्र में चौथे स्थान पर बतलाया गया दोष=(राग, द्वेष व मोह) है। और इन दोषों का भी कारण- सूत्र में पांचवे स्थान पर बतलाया गया मिथ्याज्ञान है। क्योंकि नियम यह है कि- कारण के हटने से कार्य हटता है इसलिये इन सबका आदि मूल कारण हुआ मिथ्याज्ञान। अत: सबसे पहले मिथ्याज्ञान को ही हटाना होगा। फिर मिथ्याज्ञान के हट जाने पर उसका कार्य-दोष हट जाएगा। फिर दोष का कार्य- प्रवृत्ति हट जाएगी। फिर प्रवृत्ति
का कार्य- जन्म हट जाएगा। और अन्त में जन्म का भी कार्य-दुःख हट जाएगा। इसलिये सूत्रकार आचार्य मह्षि गौतम जी महाराज ने इस क्रम से इन पाँच पदार्थों को में रखा है। क्योंकि दुःख का आदि मूल कारण मिथ्याज्ञान है और वह हटेगा अपने विरोधी-तत्त्वज्ञान से। इसलिये मुक्ति का उपाय-तत्त्वज्ञान भी दर्शनों, उपनिषदों और वेदों में यथार्थ ही कहा गया है।
अब इन पाँच पदार्थों के सम्बन्ध में थोड़ा विचार करना है कि उल्टे क्रम से हटने वाले मिथ्याज्ञान दोष आदि पदार्थों का स्वरूप क्या है।
(१) मिथ्याज्ञान - इस शब्द का सीधा- सा अर्थ है-किसी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप हो, उस वस्तु के सम्बन्ध में वैसा न जानना, बल्कि उससे विपरीत=(उल्टा) समझना मिथ्याज्ञान है। संसार में मुख्य रूप से तीन तत्त्व हैं-ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन्हीं के सम्बन्ध में प्राय: सब मिथ्याज्ञान रहता है। यही दुःख का आदि मूल कारण है। जैसे-आत्मा और ईश्वर-जो कि आंख से न दिखने वाले पदार्थ हैं, इनकी सत्ता को न मानना । जड़ पदार्थों=(शरीर मन, इन्द्रियों आदि) को चेतन समझना। संसार में जो अनेक प्रकार के दुःख्मिश्रित सुख मिलते हैं, न्हें ही विशुद्ध सुख मानना और ऐसा मानना कि ये ही, जो पाँच इन्द्रियों से भोगे जाने वाले रूप, स्स, गन्ध, स्पर्श व शब्द के सांसारिक सुख हैं, सब से उत्तम सुख हैं, इनसे ऊँचा एवं विशुद्ध, ईश्वर से प्राप्त होने वाला पूर्ण और स्थायी सुख संसार में कोई नहीं है। शरीर, धन-सम्पत्ति, रूप-यौवन, पुत्र-परिवार और सूर्य-चन्द्रमा-पृथ्वी आदि जो नाशवान् पदार्थ हैं अर्थात् एक न एक दिन ये सब नष्ट हो जाएँगे, सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे-ऐसे अनित्य पदार्थों को नित्य मानना अर्थात् ऐसा मानना कि ये सब पदार्थ सदा हमारे साथ रहेंगे, कभी हम से अलग नहीं होंगे, कभी विनाश नहीं होगा-सब मिथ्याज्ञान है। और इसके अतिरिक्त चोरी आदि निन्दित कर्मों को उत्तम कर्म मानना अथवा उसमें बुराई न मानना। अच्छे कर्मों का अच्छा फल=सुख और बुरे करमों का बुरा फल=दुःख होता है इस प्रकार के कर्म-फल-सिद्धान्त को न मानना। ईश्वर न्यायकारी है-हमारे अच्छे बुरे सब कर्मों को ठीक-ठीक देखता=जानता और सब प्राणियों के साथ पूरा-पूरा न्याय करता है इस प्रकार से ईश्वर को न्यायकारी न मानना। आत्मा एक नित्य पदार्थ है, जो इस वर्तमान शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर को प्राप्त करता है ऐसा न मानना और इसके स्थान पर यह कहना कि- अगला जन्म किसने देखा है ? यह सब मिथ्याज्ञान है। और भी-मुक्ति के सम्बन्ध में ऐसा सोचना कि वहां तो ये संसार के सुख-(सुन्दर-२ दृश्य, स्वादिष्ट भोजन, भोग के सामान आदि) होंगे नहीं, तो ऐसे भयंकर मोक्ष में हम जाकर क्या करेगे, जहां संसार के सब के सब सुख्र ही हम से छूट जाएँगे-यह सब भी मिथ्याज्ञान है। इस मिथ्याज्ञान से दोष उत्पन्न होता है।
(२) दोष - यह दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसके सम्बन्ध में महर्षि गौतम जी महाराज ने कहा है-
कहलाने लगते हैं। इन दोषों से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
(३) प्रवृत्ति - यह भी दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है-सकाम-कर्म। सकाम- कर्म उसे कहते है - जो कर्म सांसारिक फल=(धन सम्मान भोग के साधन आदि) को लक्ष्य बनाकर पाप पुण्य के रूप में किया जाये। और निष्काम-कर्म उसे कहते हैं-जो कर्म ईश्वर-प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर पुण्य के रूप में किया जाये। (कोई भी पाप निष्काम कर्म नहीं कहला सकता, इसमें केवल पुण्य ही आते हैं। अब जो पाप-पुण्य रूपी सकाम-कर्म हैं वे अनेक प्रकार के हैं। ऐसे कर्म-मन, वाणी और शरीर से किये जाते हैं। महर्षि वात्स्यायन जी महाराज ने इन कर्मों का २० भागों में विभाजन किया है। अर्थात् १० प्रकार के पाप-कर्म और इनसे विपरीत १० प्रकार के पुण्य कर्म। पहले पाप-कर्मों का वर्णन करते हैं ।
(क) शरीर से किये जाने वाले ३ कर्म-हिंसा करना, चोरी करना और व्यभिचार करना ।
(ख) वाणी से किये जाने वाले ४ कर्म-झूठ बोलना, कठोर बोलना, निन्दा-चुगली करना और वाणी का व्यर्थ प्रयोग करना=(बिना प्रसंग या आवश्यकता के बोलना) ।
(ग) मन से किये जाने वाले ३ कर्म-दूसरों के प्रति मन में बुरी भावनाएँ रखना, दूसरों के वस्तुओं को प्राप्त करके उन्हें अपना बनाने की इच्छा रखना और नास्तिकता अर्थात् ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि पर विश्वास न करना। इसके विपरीत पुण्य कर्म ये हैं।
(क) शरीर से ३ कर्म-दान देना, दूसरों की रक्षा करना और दूसरों की सेवा करना ।
(ख) वाणी से ४ कर्म-सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मीठा बोलना तथा वेद आदि सत्य-शास्त्रों का स्वाध्याय करना=(पढ़ना-पढ़ाना)।
(ग) मन से ३ कर्म-दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, दूसरों की वस्तुएँ लेने की इच्छा न रखना बल्कि अपने परिश्रम से धनादि कमाने की इच्छा रखना (और वह भी उतनी मात्रा में जितनी आवश्यकता हो, इससे अधिक की इच्छा न रखना) और आस्तिकता अर्थात् ईश्वर आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल आदि में श्रद्धा-विश्वास रखना।
ये सब प्रकार के कर्म जब सांसारिक फल को लक्ष्य बनाकर किये जाते हैं, तो सकाम-कर्म कहलाते हैं। जब राग-द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो सकाम-कर्म कहलाते हैं। इन्हीं को प्रवृत्ति नाम दिया गया है। जब राग-द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन दोषों के कारण से यह प्रवृत्ति भी कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और जब यह कारण रूपी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो इसका कार्य रूपी फल=जन्म भी हो जाता है, जो कि सूत्र में दूसरे स्थान पर कहा गया है।
यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि- तत्त्वज्ञान तो मिथ्याज्ञान का विरोधी है, इसलिये जब तत्त्वज्ञान प्राप्त होता तो मिथ्याज्ञान हट जाता है। परन्तु मिथ्याज्ञान के हट जाने पर दोष, प्रवृत्ति, जन्म एवं दु:ख क्यों हट जाते हैं? इनका आपस में क्या सम्बन्ध है?
इस प्रश्न का समाधान यह है कि- संसार में एक नियम है-
कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। जैसे बिजली के न रहने पर पंखा, मशीन आदि नहीं चलते। बिजली उनके चलाने का कारण है और पंख्रे मशीन आदि का चलना उसका कार्य है। जब बिजली नहीं रहती तो वह कार्य भी नहीं रहता। ठीक इसी नियम के अनुसार ये पांचों पदार्थ भी एक-दूसरे के कारण हैं। इनमें परस्पर कारण-कार्य सम्बन्ध है। अर्थात् जो सूत्र में पहले स्थान पर बतलाया गया दुःख है, उसका कारण- सुत्र में दूसरे स्थान पर बतलाया गया जन्म है। जब किसी का जन्म हो जाता है, तभी उसे अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते है। इसी प्रकार से जन्म का कारण सूत्र में तीसरे स्थान पर बतलाया गया प्रवृत्ति (सकाम कर्म) है। प्रवृत्ति का कारण=सूत्र में चौथे स्थान पर बतलाया गया दोष=(राग, द्वेष व मोह) है। और इन दोषों का भी कारण- सूत्र में पांचवे स्थान पर बतलाया गया मिथ्याज्ञान है। क्योंकि नियम यह है कि- कारण के हटने से कार्य हटता है इसलिये इन सबका आदि मूल कारण हुआ मिथ्याज्ञान। अत: सबसे पहले मिथ्याज्ञान को ही हटाना होगा। फिर मिथ्याज्ञान के हट जाने पर उसका कार्य-दोष हट जाएगा। फिर दोष का कार्य- प्रवृत्ति हट जाएगी। फिर प्रवृत्ति
का कार्य- जन्म हट जाएगा। और अन्त में जन्म का भी कार्य-दुःख हट जाएगा। इसलिये सूत्रकार आचार्य मह्षि गौतम जी महाराज ने इस क्रम से इन पाँच पदार्थों को में रखा है। क्योंकि दुःख का आदि मूल कारण मिथ्याज्ञान है और वह हटेगा अपने विरोधी-तत्त्वज्ञान से। इसलिये मुक्ति का उपाय-तत्त्वज्ञान भी दर्शनों, उपनिषदों और वेदों में यथार्थ ही कहा गया है।
अब इन पाँच पदार्थों के सम्बन्ध में थोड़ा विचार करना है कि उल्टे क्रम से हटने वाले मिथ्याज्ञान दोष आदि पदार्थों का स्वरूप क्या है।
(१) मिथ्याज्ञान - इस शब्द का सीधा- सा अर्थ है-किसी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप हो, उस वस्तु के सम्बन्ध में वैसा न जानना, बल्कि उससे विपरीत=(उल्टा) समझना मिथ्याज्ञान है। संसार में मुख्य रूप से तीन तत्त्व हैं-ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन्हीं के सम्बन्ध में प्राय: सब मिथ्याज्ञान रहता है। यही दुःख का आदि मूल कारण है। जैसे-आत्मा और ईश्वर-जो कि आंख से न दिखने वाले पदार्थ हैं, इनकी सत्ता को न मानना । जड़ पदार्थों=(शरीर मन, इन्द्रियों आदि) को चेतन समझना। संसार में जो अनेक प्रकार के दुःख्मिश्रित सुख मिलते हैं, न्हें ही विशुद्ध सुख मानना और ऐसा मानना कि ये ही, जो पाँच इन्द्रियों से भोगे जाने वाले रूप, स्स, गन्ध, स्पर्श व शब्द के सांसारिक सुख हैं, सब से उत्तम सुख हैं, इनसे ऊँचा एवं विशुद्ध, ईश्वर से प्राप्त होने वाला पूर्ण और स्थायी सुख संसार में कोई नहीं है। शरीर, धन-सम्पत्ति, रूप-यौवन, पुत्र-परिवार और सूर्य-चन्द्रमा-पृथ्वी आदि जो नाशवान् पदार्थ हैं अर्थात् एक न एक दिन ये सब नष्ट हो जाएँगे, सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे-ऐसे अनित्य पदार्थों को नित्य मानना अर्थात् ऐसा मानना कि ये सब पदार्थ सदा हमारे साथ रहेंगे, कभी हम से अलग नहीं होंगे, कभी विनाश नहीं होगा-सब मिथ्याज्ञान है। और इसके अतिरिक्त चोरी आदि निन्दित कर्मों को उत्तम कर्म मानना अथवा उसमें बुराई न मानना। अच्छे कर्मों का अच्छा फल=सुख और बुरे करमों का बुरा फल=दुःख होता है इस प्रकार के कर्म-फल-सिद्धान्त को न मानना। ईश्वर न्यायकारी है-हमारे अच्छे बुरे सब कर्मों को ठीक-ठीक देखता=जानता और सब प्राणियों के साथ पूरा-पूरा न्याय करता है इस प्रकार से ईश्वर को न्यायकारी न मानना। आत्मा एक नित्य पदार्थ है, जो इस वर्तमान शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर को प्राप्त करता है ऐसा न मानना और इसके स्थान पर यह कहना कि- अगला जन्म किसने देखा है ? यह सब मिथ्याज्ञान है। और भी-मुक्ति के सम्बन्ध में ऐसा सोचना कि वहां तो ये संसार के सुख-(सुन्दर-२ दृश्य, स्वादिष्ट भोजन, भोग के सामान आदि) होंगे नहीं, तो ऐसे भयंकर मोक्ष में हम जाकर क्या करेगे, जहां संसार के सब के सब सुख्र ही हम से छूट जाएँगे-यह सब भी मिथ्याज्ञान है। इस मिथ्याज्ञान से दोष उत्पन्न होता है।
(२) दोष - यह दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसके सम्बन्ध में महर्षि गौतम जी महाराज ने कहा है-
प्रवर्तनालक्षणा दोषाः ।। (न्यायदर्शन १/१/१८)
अर्थात् दोष वे हैं जो व्यक्ति को अच्छे-बुरे कर्म करने के लिये प्रेरित करते हैं। वे हैं- राग-द्वेष आदि । इनसे प्रेरित होकर व्यक्ति अच्छे-बुरे कर्म करता है। इन दोषों का कारण है मिथ्याज्ञान। अत: जब व्यक्ति में उपर्युक्त मिथ्याज्ञान विद्यमान होता है, तो उसके कारण से राग-द्वेष आदि दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। जो वस्तुएँ मिथ्याज्ञान के कारण से व्यक्ति को अपने अनुकूल दिखाई देती हैं, उन में तो राग उत्पन्न हो जाता है। और जो प्रतिकूल दिखाई देती हैं, उनमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से मिथ्याज्ञान-कारण और दोष कार्यकहलाने लगते हैं। इन दोषों से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
(३) प्रवृत्ति - यह भी दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ होता है-सकाम-कर्म। सकाम- कर्म उसे कहते है - जो कर्म सांसारिक फल=(धन सम्मान भोग के साधन आदि) को लक्ष्य बनाकर पाप पुण्य के रूप में किया जाये। और निष्काम-कर्म उसे कहते हैं-जो कर्म ईश्वर-प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर पुण्य के रूप में किया जाये। (कोई भी पाप निष्काम कर्म नहीं कहला सकता, इसमें केवल पुण्य ही आते हैं। अब जो पाप-पुण्य रूपी सकाम-कर्म हैं वे अनेक प्रकार के हैं। ऐसे कर्म-मन, वाणी और शरीर से किये जाते हैं। महर्षि वात्स्यायन जी महाराज ने इन कर्मों का २० भागों में विभाजन किया है। अर्थात् १० प्रकार के पाप-कर्म और इनसे विपरीत १० प्रकार के पुण्य कर्म। पहले पाप-कर्मों का वर्णन करते हैं ।
(क) शरीर से किये जाने वाले ३ कर्म-हिंसा करना, चोरी करना और व्यभिचार करना ।
(ख) वाणी से किये जाने वाले ४ कर्म-झूठ बोलना, कठोर बोलना, निन्दा-चुगली करना और वाणी का व्यर्थ प्रयोग करना=(बिना प्रसंग या आवश्यकता के बोलना) ।
(ग) मन से किये जाने वाले ३ कर्म-दूसरों के प्रति मन में बुरी भावनाएँ रखना, दूसरों के वस्तुओं को प्राप्त करके उन्हें अपना बनाने की इच्छा रखना और नास्तिकता अर्थात् ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि पर विश्वास न करना। इसके विपरीत पुण्य कर्म ये हैं।
(क) शरीर से ३ कर्म-दान देना, दूसरों की रक्षा करना और दूसरों की सेवा करना ।
(ख) वाणी से ४ कर्म-सत्य बोलना, हितकारी बोलना, मीठा बोलना तथा वेद आदि सत्य-शास्त्रों का स्वाध्याय करना=(पढ़ना-पढ़ाना)।
(ग) मन से ३ कर्म-दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, दूसरों की वस्तुएँ लेने की इच्छा न रखना बल्कि अपने परिश्रम से धनादि कमाने की इच्छा रखना (और वह भी उतनी मात्रा में जितनी आवश्यकता हो, इससे अधिक की इच्छा न रखना) और आस्तिकता अर्थात् ईश्वर आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल आदि में श्रद्धा-विश्वास रखना।
ये सब प्रकार के कर्म जब सांसारिक फल को लक्ष्य बनाकर किये जाते हैं, तो सकाम-कर्म कहलाते हैं। जब राग-द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो सकाम-कर्म कहलाते हैं। इन्हीं को प्रवृत्ति नाम दिया गया है। जब राग-द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन दोषों के कारण से यह प्रवृत्ति भी कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और जब यह कारण रूपी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो इसका कार्य रूपी फल=जन्म भी हो जाता है, जो कि सूत्र में दूसरे स्थान पर कहा गया है।
(४) जन्म - जन्म का अभिप्राय है-आत्मा का शरीर, मन, इन्द्रियों आदि के साथ संयोग होकर कुछ कर्म आदि करने में समर्थ हो जाना। जब सकाम-कर्म करते हैं तो उसके फल के रूप में जन्म प्राप्त होता ही है। क्योंकि यह सिद्धान्त है कि-किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। प्रत्येक किये हुये कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के कारण कोई व्यक्ति भले ही ऐसा मानता हो कि-भगवान के सामने प्रार्थना आदि करने से किये हुए पाप क्षमा हो जाते हैं। परन्तु व्यवहार अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पाप=(अपराध) क्षमा नहीं होते। क्योंकि प्रत्येक देश में अपराध करने पर वहाँ की दण्ड-संहिता के अनुसार अपराधी को दण्ड दिया जाता है। यदि अपराध क्षमा कर दिये जाते, तो उन देशों में न तो पुलिस की आवश्यकता रह जाती, न वकीलों की, न न्यायाधीशों की, न जेलों की और न जल्लाद=(फाँसी पर चढ़ाने वाले कर्मचारी) की। ऐसी परिस्थिति में अपराध दिन दूगने और रात चौगुने बढ़ जाते। तब तो सामान्य जीवन भी जीना कठिन हो जाता। अत: जब मनुष्य लोग भी देश की शासन-प्रणाली को व्यवस्थित बनाये रखने और न्यायप्रिय होने के कारण अपराध क्षमा नहीं करते, तो पूर्ण न्यायकारी परमेश्वर पाप क्षमा क्यों करेगा ? और यदि वह भी पाप क्षमा करने लग जाये तो संसार में पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा और उसके राज्य में भी अव्यवस्था फैल जाएगी। ऐसे अन्यायकारी एवं अव्यवस्थित राज्य वाले न्यायाधीश और राजा रूपी ईश्वर को कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति अपना उपास्य=(उपासना करने योग्य) स्वीकार नहीं करेगा। अत: यह निश्चित सिद्धान्त है कि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है इसी सिद्धान्त के अनुसार जो पुण्य कर्म होते हैं, उनका फल ऊत्तम जन्म=(मनुष्य आदि) के रूप में मिलता है और जो पाप-कर्म होते हैं, उनका फल निकृष्ट जन्म=(पशु, पक्षी, कीड़े-मकौड़े, समुद्री जीव-जन्तु आदि) के रूप में मिलता है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति=(पाप-पुण्य सकाम कर्म) जन्म रूपी कार्य का कारण बन जाती है। और जब जन्म रूपी कारण उपस्थित हो जाता है तो इसका दुःख रूपी कार्य भी उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति मृत्यु आदि दुःखों से बचने के लिये मृत्यु को रोकना चाहता है। परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि मृत्यु को रोकने से मृत्यु नहीं रुकेगी, यदि मृत्यु को रोकना है तो उसके कारण=जन्म को रोकना होगा। क्योंकि जन्म ही तो दुःख का कारण है।
(५) दुःरव - इसे सब जानते ही हैं। महर्षि गौतम जी महाराज ने भी इसकी परिभाषा इसी प्रकार से की है।
ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम मानव जीवन के इस चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति को सिद्ध करने में समर्थ हो सकें ।
मानव जीवन के इस चरम लक्ष्य=मोक्ष-प्राप्ति तक पहुँचने के लिये व्यक्ति को प्रतिदिन दोनों समय=(प्रातः तथा सायं) नियमपूर्वक ईश्वर की उपासना करनी चाहिये। ईश्वर की उपासना को जीवन का सबसे मुख्य कार्य समझना चाहिये। क्योंकि इसी से जीवन का मुख्य लक्ष्य सिद्ध होता है। और व्यक्ति वर्तमान में भी रग-द्वेष, अविद्या आदि क्लेशों से बचा रहता है।
ईश्वर की उपासना में ओ३म् का जप, गायत्री मन्त्र का जप और वैदिक-संध्या के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना होता है। और ये सब=(जप आदि) अर्थ सहित करने चाहिये। परन्तु जप आदि प्रारम्भ करने से पूर्व मोक्ष-प्राप्ति का जो मुख्य साधन पहले बताया जा चुका है-तत्त्वज्ञान. उसका सम्पादन अवश्य करना चाहिये। तत्त्वज्ञान का अर्थ है-संसार के पदार्थों का वास्तविक ज्ञान। संसार में तीन पदार्थ हैं-ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के स्वरूप का चिन्तन उपासना से पूर्व अवश्य करना चाहिये, जिससे कि यह तत्त्वज्ञान हमारे अन्दर स्थिर हो जाए और हम इसी के अनुसार अपने जीवन को ऊँचा उठाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन तीन तत्त्वों का चिन्तन इस रूप में करना चाहिये-
इस विषय में सर्वप्रथम ईश्वर का चिन्तन करना चाहिये । ईश्वर का चिन्तन करते समय प्रथम पुरुष (III Person) के शब्दों= ('वह' आदि) का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसके स्थान पर मध्यम पुरुष = (II Person) के शब्दों=('आप' आदि) का प्रयोग करना चाहिए। 'वह ईश्वर' ऐसा प्रयोग करने से यह भ्रान्ति उत्पन्न होती है कि ईश्वर कहीं दूर रहता है। परिणाम यह होता है कि ईश्वर के साथ उपासक का सीधा सम्बन्ध नहीं बन पाता और उससे ज्ञान व आनन्दादि की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जब ईश्वर सर्व्यापक है, अर्थात हमारे अन्दर, बाहर, आगे, पीछे, दाएँ, बाएँ, पास और दूर सभी जगह विद्यमान है तो उसे आप आदि शब्दों से सम्बोधित क्यों न किया जाये, जिससे कि ईश्वर से साक्षात् सम्बन्ध स्थापित हो सके। परन्तु ईश्वर को निकट मानते हुए भी उसे अपनी आत्मा में ढूंढना चाहिये, अपने शरीर में दाएँ-बाएँ अथवा शरीर से बाहर दाएँ-बाएँ नहीं । क्योंकि दो त्त्वों का सम्मेलन=(मिलना=साक्षात्कार) वहीं पर हो सकता है, जहां पर वे दोनों तत्त्व विद्यमान हों। ईश्वर तो सर्वव्यापक है परन्तु हम=(आत्मा) सर्वव्यापक नहीं हैं। इसलिये जहां पर हमें अपने अस्तित्व की अनुभूति
होती है, वहीं पर ईश्वर की खोज करनी चाहिये । इस प्रक्रिया को ठीक प्रकार से न समझने के कारण उपासक=(साधक) को उपासना=( साधना) में सफलता नहीं मिल पाती ।
उपासना में सफलता प्राप्त करने के लिये ईश्वर-जीव-प्रकृति को इस रूप में समझना चाहिये । ईश्वर = साध्य है, जीव= साधक है। और प्रकृति = साधन है। पहले ईश्वर - साध्य का चिन्तन करेंगे । जैसे
ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। (आर्यसमाज का दूसरा नियम)
अर्थात् हे परम रक्षक प्रभो ! आप सत् हैं अर्थात् सत्यस्वरूप, एक सत्तात्मक पदार्थ हैं, आप तीनों काल में विद्यमान रहते हैं । आप चित् हैं अर्थात् चेतन हैं, सब कुछ जानते हैं। आप आनन्दस्वरूप हैं, आप में दुःख का लेशमात्र भी नहीं है । आप निराकार हैं अर्थात्आ पकी कोई आकृति, रंगरूप या मूर्ति नहीं है । आप सर्वशक्तिमान् हैं। अर्थात् संसार की उत्पत्ति करने, पालन करने, विनाश करने और सब जीवों को कर्मों का फल देने में आप किसी की सहायता नहीं लेते, ये सब कार्य आप अपनी ही शक्ति से पूर्ण कर लेते हैं । हे परमप्रिय परमात्मन् ! आप न्यायकारी हैं, जो व्यक्ति जैसा= (अच्छा या बुरा) और जितना कर्म करता है, उसे वैसा=(अच्छा और बुरा) और उतना ही फल देते हैं। आप दयालु हैं, आपने सब प्राणियों पर दया करके उन्हें सुख के सब साधन प्रदान किये हैं। आप अजन्मा हैं, अर्थात् आपका न तो जीवों के समान शरीर से संयोग रूपी जन्म होता है और न ही पृथ्वी, सूर्य आदि जड़ पदार्थों के समान नया ही जन्म होता है । आप अनन्त हैं अर्थात् आप इतने विशाल हैं कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप निर्विकार हैं अर्थात् जैसे दूध, फल आदि जड़ पदार्थों में गलना - सड़ना और वृक्ष आदि पदार्थों में घटना-बढ़ना रूपी विकार उत्पन्न होते रहते हैं, आप में ऐसे विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। हे दयानिधान प्रभो ! आप अनादि हैं, आपकी उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई। आप अनुपम हैं अर्थात् आपकी पूर्ण उपमा कोई भी नहीं है। आपके स्वरूप को समझाने के लिये संसार में जो जो उपमाएं दी जाती हैं, वे सब हीन उपमाएं हैं। आप सर्वाधार हैं, जैसे हमारा आधार यह पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार सूर्य है, सूर्य का आधार आकाश-गंगा है, वैसे ही आप हमारे तथा पृथ्वी आदि सब पदार्थों के आधार हैं। आपके ही आधार से से सारा संसार स्थित है। हे प्रभो ! आप सर्वेश्वर हैं, आप ही संसार के सब पदार्थों = (धन, सम्पति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, वृक्ष-वनस्पति, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, आकाशादि) के स्वामी=( पालक) हैं। आप सर्वव्यापक हैं अर्थात् स्थूल से स्थूल पदार्थों पृथ्वी-पर्वतादि में तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों परमाणु और आत्मादि में आप सर्वत्र विद्यमान हैं। आप सर्वान्तर्यामी हैं, आप सबके अन्दर विद्यमान होकर सबका नियन्त्रण करते हैं। हे परमशक्तिमान् प्रभो ! आप अजर हैं ? अर्थात्आ प कभी बूढ़े =(अशक्त) नहीं होते। हे भगवन् ! आप अमर हैं, अर्थात् आप कभी मरते नहीं हैं। संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। आप अभय हैं, आपको कभी भी किसी से भी भय नहीं लगता। आप नित्य हैं अर्थात् आपकी उत्पत्ति के तीन कारण= (निमित्त कारण, उपादान-कारण और साधारण कारण) नहीं है इसलिये न तो कभी आपकी उत्पत्ति हुई है और न ही कभी आपका विनाश होगा। आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। आप पवित्र हैं अर्थात् आप न तो स्वयं कभी पाप करते हैं और न ही कभी किसी को पाप करते की प्रेरणा करते हैं। हे दीनरक्षक प्रभो ! आप सृष्टिकर्ता हैं, आप ही इस दृश्य और अदृश्य जगत् की रचना करने वाले हैं। हे परम दयालु भगवन् ! इस संसार में केवल मात्र आप ही उपासना करने योग्य हैं, अन्य कोई जड़-चेतन पदार्थ उपासनीय नहीं है जो व्यक्ति आप को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करते हैं, वे सदा पशुओं के समान दुःख ही भोगते हैं। हे कृपानिधान प्रभो ! हम पर कृपा कीजिए, हम सदा आपकी ही उपासना करें और आप हमें सदा अपना ज्ञान, बल और आनंद देते रहे। (उपर्युक्त स्वरूपवाला 'ईश्वर'=साध्य= प्राप्त करने योग्य है।)
(५) दुःरव - इसे सब जानते ही हैं। महर्षि गौतम जी महाराज ने भी इसकी परिभाषा इसी प्रकार से की है।
बाधनालक्षणं दुःखम् ॥ (न्यायदर्शन १/१/२१)
अर्थात् जो हमें बाधा, पीड़ा, ताप या कष्ट होता है, वही दुःख है। जब व्यक्ति जन्म=(शरीर) धारण कर लेता है, तो अनेक प्रकार के दुःख उसे भोगने पड़ते हैं। यद्यपि पुण्य-कर्मों के फलरवरूप मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है और पाप-कर्मों के फल स्वरूप पशु-पक्षी आदि का जन्म प्राप्त होता है। इसी कारण से मनुष्य-जन्म में सुख अधिक और पशु-पक्षी आदि जन्म में दुःख अधिक मिलता है। इस का यही प्रमाण है कि चाहे कितना ही धनहीन या साधन हीन मनुष्य हो, वह कुत्ता, घोड़ा आदि पशु-शरीर को कभी भी प्राप्त करना नहीं चाहता। उसे साधनहीन होते हुए भी पशु-शरीर की अपेक्षा मनुष्य-शरीर में ही अधिक सुख दिखाई देता है। परन्तु मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने पर भी दुःखो से पूरी तरह से नहीं छूट पाता। मनुष्यों को पशु- पक्षी आदि की अपेक्षा तो कम दुःख भोगना पड़ता है, परन्तु कोई न कोई दुःख लगा ही रहता है। उदाहरण के लिये-कोई व्यक्ति किसी वस्तु=(धन सम्मान आदि) को प्राप्त करना चाहता है जब वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती तो उसे दुःख होता है। उस वस्तु की प्राप्ति के लिये जो परिश्रम करना पड़ता है, उस में दुःख होता है। बहुत परिश्रम करने पर भी वह वस्तु बहुत-थोड़ी मात्रा में मिलती है, तब दुःख होता है। और जितनी मात्रा में मिल पाती है, उसे भी यदि कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले जाये, तो दुःख होता है। व्यक्ति रोगी नहीं होता चाहता परन्तु रोगी हो जाता है, तो दुःख होता है। व्यक्ति अपने पुत्र-परिवार आदि की वृद्धि देखना चाहता है, जब सन्तान ही प्राप्त नहीं होती, तो दुःख होता है। यदि सन्तान हो भी जाये और विकलांग हो तो दुःख होता है। यदि पूरे अंगों वाली हो जाये, परन्तु पूर्ण स्वस्थ न हो, तो दुःख होता है। यदि पूर्ण स्वस्थ भी हो और आज्ञाकारी न हो, तो दुःख होता है। इस प्रकार से मनुष्य-जन्म पाकर भी अनेक प्रकार के दुःख भोगने पड़ते हैं। इस संसार में रहते हुए प्रत्येक बुद्धिमान् व्यक्ति उपर्युक्त दुःखों का अनुभव कर सकता है। इन सब दुःखों से पूरी तरह से छूट जाने और ईश्वर के परम आनन्द को प्राप्त करने का नाम ही मुक्ति है, जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है। और इस मुक्ति को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही इस सूत्र में बतलाई गई है। अर्थात् कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है इस सिद्धान्त के अनुसार दुःख के कारण जन्म, जन्म के कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के कारण दोष और दोष के कारण मिथ्याज्ञान को हटा देने से मोक्ष-प्राप्ति संभव है। और दुःखों के आदि- मूल कारण मिथ्याज्ञान को हटाने का एक मात्र उपाय इसका विरोधी तत्त्वज्ञान ही है, इसके अतिरिक्त मोक्ष-प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है।ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम मानव जीवन के इस चरम लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति को सिद्ध करने में समर्थ हो सकें ।
दुःख का निवारण=ईश्वर-जीव-प्रकृति का चिन्तन
ईश्वर की उपासना में ओ३म् का जप, गायत्री मन्त्र का जप और वैदिक-संध्या के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करना होता है। और ये सब=(जप आदि) अर्थ सहित करने चाहिये। परन्तु जप आदि प्रारम्भ करने से पूर्व मोक्ष-प्राप्ति का जो मुख्य साधन पहले बताया जा चुका है-तत्त्वज्ञान. उसका सम्पादन अवश्य करना चाहिये। तत्त्वज्ञान का अर्थ है-संसार के पदार्थों का वास्तविक ज्ञान। संसार में तीन पदार्थ हैं-ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के स्वरूप का चिन्तन उपासना से पूर्व अवश्य करना चाहिये, जिससे कि यह तत्त्वज्ञान हमारे अन्दर स्थिर हो जाए और हम इसी के अनुसार अपने जीवन को ऊँचा उठाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन तीन तत्त्वों का चिन्तन इस रूप में करना चाहिये-
इस विषय में सर्वप्रथम ईश्वर का चिन्तन करना चाहिये । ईश्वर का चिन्तन करते समय प्रथम पुरुष (III Person) के शब्दों= ('वह' आदि) का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसके स्थान पर मध्यम पुरुष = (II Person) के शब्दों=('आप' आदि) का प्रयोग करना चाहिए। 'वह ईश्वर' ऐसा प्रयोग करने से यह भ्रान्ति उत्पन्न होती है कि ईश्वर कहीं दूर रहता है। परिणाम यह होता है कि ईश्वर के साथ उपासक का सीधा सम्बन्ध नहीं बन पाता और उससे ज्ञान व आनन्दादि की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जब ईश्वर सर्व्यापक है, अर्थात हमारे अन्दर, बाहर, आगे, पीछे, दाएँ, बाएँ, पास और दूर सभी जगह विद्यमान है तो उसे आप आदि शब्दों से सम्बोधित क्यों न किया जाये, जिससे कि ईश्वर से साक्षात् सम्बन्ध स्थापित हो सके। परन्तु ईश्वर को निकट मानते हुए भी उसे अपनी आत्मा में ढूंढना चाहिये, अपने शरीर में दाएँ-बाएँ अथवा शरीर से बाहर दाएँ-बाएँ नहीं । क्योंकि दो त्त्वों का सम्मेलन=(मिलना=साक्षात्कार) वहीं पर हो सकता है, जहां पर वे दोनों तत्त्व विद्यमान हों। ईश्वर तो सर्वव्यापक है परन्तु हम=(आत्मा) सर्वव्यापक नहीं हैं। इसलिये जहां पर हमें अपने अस्तित्व की अनुभूति
होती है, वहीं पर ईश्वर की खोज करनी चाहिये । इस प्रक्रिया को ठीक प्रकार से न समझने के कारण उपासक=(साधक) को उपासना=( साधना) में सफलता नहीं मिल पाती ।
उपासना में सफलता प्राप्त करने के लिये ईश्वर-जीव-प्रकृति को इस रूप में समझना चाहिये । ईश्वर = साध्य है, जीव= साधक है। और प्रकृति = साधन है। पहले ईश्वर - साध्य का चिन्तन करेंगे । जैसे
कि - स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ (यजुर्वेद ४०/८)
अर्थात् हे परम पिता प्रभो ! आप सर्वव्यापक हैं, सबका नियन्त्रण करने वाले हैं, आप कभी शरीर धारण नहीं करते, आप छिद्र आदि दोषों से रहित हैं, नस-नाड़ियों के बन्धन में कभी नहीं आते. आप सब प्रकार से शुद्ध हैं और आप कभी भी पाप नहीं करते । हे सबके पालक परमेश्वर ! आप सर्वज्ञ हैं=(सब कुछ जानते हैं) आप ही ने हमारे मन को बनाया और चलने का सामर्थ्य प्रदान किया हैं, आप सर्वशक्तिमान्=(सभी सम्भव कार्यों को अपनी शक्ति से पूरा कर लेते हैं ) आप स्वयंसिद्ध हैं=(आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है) और आपने ही अपनी सनातन=(अनादि) जीव रूपी प्रजा के लिये परम पवित्र वेद का ज्ञान प्रदान किया है। हे पिता! हम आपकी ही उपासना करते हैं, हमें ज्ञान, बल, आनन्द दीजिये ।
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपर पुरुषविशेष ईश्वरः ।। (योगदर्शन १-२४)
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥ (योगदर्शन १-२५)
स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ।। (योगदर्शन १-२६)
तस्य वाचकः प्रणव: ॥ (योगदर्शन १-२७)
अर्थात् हे प्रभो ! आप अविद्या आदि पांच क्लेशों से, शुभाशुभ कर्मों से, उन कर्मों के फलों से तथा उन फलों की वासनाओं = (संस्कारों) से तीनों कालों में सर्वथा रहित हैं और सब जीवों से विशेष=(भिन्न) सत्ता रखते हैं, ऐसे आप ईश्वर हैं। हे परमात्मन् ! आप में सबसे अधिक ज्ञान है, आप से बड़ा ज़ानी इस संसार में कोई नहीं है । आपके तुल्य=(बराबर) ज्ञान रखने वाला भी कोई नहीं है । हे पूज्य परमेश्वर ! जितने शरीरधारी गुरु आज तक इस सृष्टि में हुए हैं आज है और आगे होंगे, आप उन सब गुरुओं के भी गुरु हैं । इसी प्रकार से पिछली सृष्टियों में भी जितने शरीरधारी गुरु हुए थे और अगली सृष्टियों में भी जितने गुरु होंगे, आप उन सबके भी गुरु हैं । क्योंकि अन्य सब गुरु शरीर को धारण करके और आप द्वारा प्रदत्त विद्या को पढ़कर ही गुरु बन पाते हैं और काल के कारण शरीर छूट जाने पर गुरु बनकर विद्या नहीं पढ़ा सकते । परन्तु आप कभी शरीर को धारण नहीं करते, इसलिये काल कभी भी आपका विनाश नहीं कर सकता और आप सदा सबके गुरु बने रहते हैं। हे परम कृपालु परमात्मन् ! आपका निज और सबसे प्रिय नाम 'ओ३म्' है। हम आपकी ही उपासना करते हैं। हमें ज्ञान, बल, आनन्द दीजिये ।ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। (आर्यसमाज का दूसरा नियम)
अर्थात् हे परम रक्षक प्रभो ! आप सत् हैं अर्थात् सत्यस्वरूप, एक सत्तात्मक पदार्थ हैं, आप तीनों काल में विद्यमान रहते हैं । आप चित् हैं अर्थात् चेतन हैं, सब कुछ जानते हैं। आप आनन्दस्वरूप हैं, आप में दुःख का लेशमात्र भी नहीं है । आप निराकार हैं अर्थात्आ पकी कोई आकृति, रंगरूप या मूर्ति नहीं है । आप सर्वशक्तिमान् हैं। अर्थात् संसार की उत्पत्ति करने, पालन करने, विनाश करने और सब जीवों को कर्मों का फल देने में आप किसी की सहायता नहीं लेते, ये सब कार्य आप अपनी ही शक्ति से पूर्ण कर लेते हैं । हे परमप्रिय परमात्मन् ! आप न्यायकारी हैं, जो व्यक्ति जैसा= (अच्छा या बुरा) और जितना कर्म करता है, उसे वैसा=(अच्छा और बुरा) और उतना ही फल देते हैं। आप दयालु हैं, आपने सब प्राणियों पर दया करके उन्हें सुख के सब साधन प्रदान किये हैं। आप अजन्मा हैं, अर्थात् आपका न तो जीवों के समान शरीर से संयोग रूपी जन्म होता है और न ही पृथ्वी, सूर्य आदि जड़ पदार्थों के समान नया ही जन्म होता है । आप अनन्त हैं अर्थात् आप इतने विशाल हैं कि आपकी कोई सीमा ही नहीं है। आप निर्विकार हैं अर्थात् जैसे दूध, फल आदि जड़ पदार्थों में गलना - सड़ना और वृक्ष आदि पदार्थों में घटना-बढ़ना रूपी विकार उत्पन्न होते रहते हैं, आप में ऐसे विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होते। हे दयानिधान प्रभो ! आप अनादि हैं, आपकी उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई। आप अनुपम हैं अर्थात् आपकी पूर्ण उपमा कोई भी नहीं है। आपके स्वरूप को समझाने के लिये संसार में जो जो उपमाएं दी जाती हैं, वे सब हीन उपमाएं हैं। आप सर्वाधार हैं, जैसे हमारा आधार यह पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार सूर्य है, सूर्य का आधार आकाश-गंगा है, वैसे ही आप हमारे तथा पृथ्वी आदि सब पदार्थों के आधार हैं। आपके ही आधार से से सारा संसार स्थित है। हे प्रभो ! आप सर्वेश्वर हैं, आप ही संसार के सब पदार्थों = (धन, सम्पति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्य, वृक्ष-वनस्पति, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, आकाशादि) के स्वामी=( पालक) हैं। आप सर्वव्यापक हैं अर्थात् स्थूल से स्थूल पदार्थों पृथ्वी-पर्वतादि में तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों परमाणु और आत्मादि में आप सर्वत्र विद्यमान हैं। आप सर्वान्तर्यामी हैं, आप सबके अन्दर विद्यमान होकर सबका नियन्त्रण करते हैं। हे परमशक्तिमान् प्रभो ! आप अजर हैं ? अर्थात्आ प कभी बूढ़े =(अशक्त) नहीं होते। हे भगवन् ! आप अमर हैं, अर्थात् आप कभी मरते नहीं हैं। संसार की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। आप अभय हैं, आपको कभी भी किसी से भी भय नहीं लगता। आप नित्य हैं अर्थात् आपकी उत्पत्ति के तीन कारण= (निमित्त कारण, उपादान-कारण और साधारण कारण) नहीं है इसलिये न तो कभी आपकी उत्पत्ति हुई है और न ही कभी आपका विनाश होगा। आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। आप पवित्र हैं अर्थात् आप न तो स्वयं कभी पाप करते हैं और न ही कभी किसी को पाप करते की प्रेरणा करते हैं। हे दीनरक्षक प्रभो ! आप सृष्टिकर्ता हैं, आप ही इस दृश्य और अदृश्य जगत् की रचना करने वाले हैं। हे परम दयालु भगवन् ! इस संसार में केवल मात्र आप ही उपासना करने योग्य हैं, अन्य कोई जड़-चेतन पदार्थ उपासनीय नहीं है जो व्यक्ति आप को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करते हैं, वे सदा पशुओं के समान दुःख ही भोगते हैं। हे कृपानिधान प्रभो ! हम पर कृपा कीजिए, हम सदा आपकी ही उपासना करें और आप हमें सदा अपना ज्ञान, बल और आनंद देते रहे। (उपर्युक्त स्वरूपवाला 'ईश्वर'=साध्य= प्राप्त करने योग्य है।)
अब हम अपने स्वरूप का=(जीव=साधक का) चिन्तन करेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने वाले साधक हम स्वयं जीव = ( आत्मा) हैं ।
है परम दयालु भगवन् ! मैं साधक=आत्मा हूँ। मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सत् हूँ मैं चित्=चेतन=(ज़ञानवान् ) हूँ। परन्तु मेरा ज्ञान इतना अल्प है कि केवल अपने ज्ञान से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य और शरीरादि साधनों के बिना अपने आपको पहचान भी नहीं सकता कि 'मैं कौन हूँ ? मैं अत्यन्त अणुरूप=(छोटा) और एकदेशी हूँ । आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य एवं मन, बुद्धि, शरीरादि साधनों से ही मैं कुछ कर्म कर पाता हूँ। हे परमात्मन् ! आपने मुझे सामर्थ्य प्रदान करके भी कर्म करने में स्वतन्त्र छोड़ा है, अत: मैं कर्म करने में स्वतन्त्र होने के कारण कुछ अच्छे बुरे कर्म कर लेता हूँ। परन्तु उन किये हुए कर्मों का फल भोगने में आपकी न्याय व्यवस्था के आधीन रहता हूँ। मुझे अपने किये हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किये पापों के फल से मैं कभी बच नहीं सकता। इन कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, मन बुद्धि आदि पर नहीं। हे परमात्मन् ! मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो मेरा निवासस्थान है। यह शरीर मरणधर्मा है, परन्तु मैं नित्य हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता और न कभी मरता हूँ। मैं इस शरीर में हृदय में रहता हूँ। हे प्रभो ! मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ। आप मुझे जिस-जिस शरीर के साथ संयुक्त कर देते हैं , उस उस शरीर वाले नाम से लोग मुझे पुकारने लगते हैं। मैं इन तीनों लिंगों से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, लिंग तो शरीरों के हैं। हे परमात्मन् ! मेरा इन शरीरों के साथ सम्बन्ध अनित्य है और शरीरों के समान अन्य सम्बन्धियों = (माता,पिता, भाई, बहन आदि) के साथ भी सम्बन्ध अनित्य है। इस शरीर के छूटने पर ये सभी सांसारिक सम्बन्ध भी छूट जायेंगे। आदि सृष्टि से लेकर अब तक न जाने कितने आत्माओं के साथ मेरा सम्बन्ध बना और टूटा है। न जाने कितने व्यक्तियों का मैं पिता बना, माता बना, भाई बना, बहन बना, पुत्र बना, पुत्री बना। न जाने कितने पशुप्षियों के शरीर मैंने अपने कर्म-फलानुसार धारण किये होंगे। इन सबकी गणना करना भी कठिन है। प्रभो ! जब तक मुझ में अविद्या बनी रहेगी, तब तक मैं इस जन्म-मरण के चक्र से छूट नहीं पाऊँगा। जैसा मैं आत्मा हूँ वैसे ही संसार के समस्त प्राणी भी मेरे समान ही आत्माएं हैं । हमारे स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है, सब एक समान हैं। हम सब में जो अन्तर दिखाई देता है, वह शरीर, बुद्धि, ज्ञान, बल, कर्मों आदि के कारण से है, आत्माओं के अपने स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हे परमात्मन् ! मैं आपकी उपासना करने में सफल हो सकूं, इसलिये मुझे ज्ञान, बल और आनन्द प्रदान कीजिए ।
अब हम प्रकृति= साधन का चिन्तन करेंगे।
है परम कृपालु भगवन् ! यह प्रकृति आपको प्राप्त करने का साधन है। महर्षि कपिल जी के कथनानुसार प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से है - सत्त्व, रज और तम, इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणुओं की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। इस अवस्था में इन परमाणुओं में गति उत्पन्न करके आप सर्वप्रथम महत्तत्व= (बुद्धि) को बनाते हैं। फिर महत्तत्व से अहंकार नामक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। फिर अहंकार से - हे भगवन् ! आप सोलह पदार्थ बनाते हैं-५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, १ मन और ५ तन्मात्राएँ=(सूक्ष्मभूत) । फिर ५ तन्मात्राओं' से आप पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ५ स्थूलभूतों को उत्पन्न करते हैं । फिर इन ५ स्थूलभूतों से ही आप वृक्ष-वनस्पतियों, पशु-पक्षी, मनुष्यादि शरीरों को उत्पन्न करते हैं । हे भगवन् ! यह समस्त सूक्ष्म व स्थूल संसार आप ही ने बनाया है। सारे संसार के जीव और प्रकृति के सारे परमाणु मिलकर केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं बना सकते, इस संसार से हम लौकिक सुख् को और मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं, अत: आपने इन्हीं दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ही इस संसार को बनाया है। यह संसार हमारे प्रयोजनों में से 'लौकिक सुख' रूपी प्रयोजन गौण तथा 'मोक्ष' रूपी प्रयोजन मुख्य है। हे परम दयालु भगवन् ! हमें ज्ञान, बल व सामर्थ्य दीजिए कि हम इस संसार को सदा मोक्ष प्राप्ति का साधन ही मानें कभी भी इसे जीवन का अन्तिम साध्य स्वीकार न करें।
इन तीन तत्त्वों के स्वरूप के चिन्तन के पश्चात् विधिवत् ओ३म्आ दि का जप, गायत्री मन्त्र का जप और वैदिक संध्या अर्थ सहित करनी चाहिये। यही ईश्वर-उपासना का स्वरूप है । इसी के माध्यम से व्यक्ति उन्नति करता हुआ समाधि को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर सबको दुःखों से छुड़ाकर मोक्ष का आनन्द प्रदान करे, यही कामना है।
है परम दयालु भगवन् ! मैं साधक=आत्मा हूँ। मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सत् हूँ मैं चित्=चेतन=(ज़ञानवान् ) हूँ। परन्तु मेरा ज्ञान इतना अल्प है कि केवल अपने ज्ञान से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य और शरीरादि साधनों के बिना अपने आपको पहचान भी नहीं सकता कि 'मैं कौन हूँ ? मैं अत्यन्त अणुरूप=(छोटा) और एकदेशी हूँ । आप द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य एवं मन, बुद्धि, शरीरादि साधनों से ही मैं कुछ कर्म कर पाता हूँ। हे परमात्मन् ! आपने मुझे सामर्थ्य प्रदान करके भी कर्म करने में स्वतन्त्र छोड़ा है, अत: मैं कर्म करने में स्वतन्त्र होने के कारण कुछ अच्छे बुरे कर्म कर लेता हूँ। परन्तु उन किये हुए कर्मों का फल भोगने में आपकी न्याय व्यवस्था के आधीन रहता हूँ। मुझे अपने किये हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किये पापों के फल से मैं कभी बच नहीं सकता। इन कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, मन बुद्धि आदि पर नहीं। हे परमात्मन् ! मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो मेरा निवासस्थान है। यह शरीर मरणधर्मा है, परन्तु मैं नित्य हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता और न कभी मरता हूँ। मैं इस शरीर में हृदय में रहता हूँ। हे प्रभो ! मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ और न ही नपुंसक हूँ। आप मुझे जिस-जिस शरीर के साथ संयुक्त कर देते हैं , उस उस शरीर वाले नाम से लोग मुझे पुकारने लगते हैं। मैं इन तीनों लिंगों से रहित शुद्ध आत्मा हूँ, लिंग तो शरीरों के हैं। हे परमात्मन् ! मेरा इन शरीरों के साथ सम्बन्ध अनित्य है और शरीरों के समान अन्य सम्बन्धियों = (माता,पिता, भाई, बहन आदि) के साथ भी सम्बन्ध अनित्य है। इस शरीर के छूटने पर ये सभी सांसारिक सम्बन्ध भी छूट जायेंगे। आदि सृष्टि से लेकर अब तक न जाने कितने आत्माओं के साथ मेरा सम्बन्ध बना और टूटा है। न जाने कितने व्यक्तियों का मैं पिता बना, माता बना, भाई बना, बहन बना, पुत्र बना, पुत्री बना। न जाने कितने पशुप्षियों के शरीर मैंने अपने कर्म-फलानुसार धारण किये होंगे। इन सबकी गणना करना भी कठिन है। प्रभो ! जब तक मुझ में अविद्या बनी रहेगी, तब तक मैं इस जन्म-मरण के चक्र से छूट नहीं पाऊँगा। जैसा मैं आत्मा हूँ वैसे ही संसार के समस्त प्राणी भी मेरे समान ही आत्माएं हैं । हमारे स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है, सब एक समान हैं। हम सब में जो अन्तर दिखाई देता है, वह शरीर, बुद्धि, ज्ञान, बल, कर्मों आदि के कारण से है, आत्माओं के अपने स्वरूप में कोई भेद नहीं है। हे परमात्मन् ! मैं आपकी उपासना करने में सफल हो सकूं, इसलिये मुझे ज्ञान, बल और आनन्द प्रदान कीजिए ।
अब हम प्रकृति= साधन का चिन्तन करेंगे।
है परम कृपालु भगवन् ! यह प्रकृति आपको प्राप्त करने का साधन है। महर्षि कपिल जी के कथनानुसार प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से है - सत्त्व, रज और तम, इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणुओं की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। इस अवस्था में इन परमाणुओं में गति उत्पन्न करके आप सर्वप्रथम महत्तत्व= (बुद्धि) को बनाते हैं। फिर महत्तत्व से अहंकार नामक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। फिर अहंकार से - हे भगवन् ! आप सोलह पदार्थ बनाते हैं-५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, १ मन और ५ तन्मात्राएँ=(सूक्ष्मभूत) । फिर ५ तन्मात्राओं' से आप पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ५ स्थूलभूतों को उत्पन्न करते हैं । फिर इन ५ स्थूलभूतों से ही आप वृक्ष-वनस्पतियों, पशु-पक्षी, मनुष्यादि शरीरों को उत्पन्न करते हैं । हे भगवन् ! यह समस्त सूक्ष्म व स्थूल संसार आप ही ने बनाया है। सारे संसार के जीव और प्रकृति के सारे परमाणु मिलकर केवल अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं बना सकते, इस संसार से हम लौकिक सुख् को और मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं, अत: आपने इन्हीं दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ही इस संसार को बनाया है। यह संसार हमारे प्रयोजनों में से 'लौकिक सुख' रूपी प्रयोजन गौण तथा 'मोक्ष' रूपी प्रयोजन मुख्य है। हे परम दयालु भगवन् ! हमें ज्ञान, बल व सामर्थ्य दीजिए कि हम इस संसार को सदा मोक्ष प्राप्ति का साधन ही मानें कभी भी इसे जीवन का अन्तिम साध्य स्वीकार न करें।
इन तीन तत्त्वों के स्वरूप के चिन्तन के पश्चात् विधिवत् ओ३म्आ दि का जप, गायत्री मन्त्र का जप और वैदिक संध्या अर्थ सहित करनी चाहिये। यही ईश्वर-उपासना का स्वरूप है । इसी के माध्यम से व्यक्ति उन्नति करता हुआ समाधि को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर सबको दुःखों से छुड़ाकर मोक्ष का आनन्द प्रदान करे, यही कामना है।
॥ ओ३म् शम् ॥
नोट : ओ३म् जप, गायत्री जप और वैदिक संध्या को विधिपूर्वक किसी योगाभ्यासी से सीख लेना चाहिये और सही विधि से ही करना चाहिये, तभी लाभ होता है, अन्यथा नहीं ।




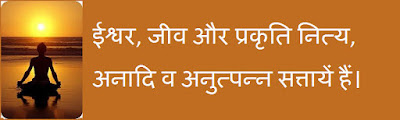
नमस्ते आर्य जी, इतने बड़े पोस्ट को आप ने टाइप कर लिखा है?
जवाब देंहटाएं