लेखक 👉 स्वामी सत्यपति परिब्राजक
आदर्श जीवन
- सौभाग्य से उपलब्ध मानव जीवन को आदर्शरूप में जीना चाहिए ।
- जो व्यक्ति पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों को यथावत् जानकर उनका उपयोग लेता है, वही वास्तव में आदर्श मनुष्य है । आदर्शों पर चलने (पालन करने) के लाभ और न करने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है; ऐसा सोचना बहुत उच्च और तीक्ष्ण बुद्धि वाले का काम है।
- मनुष्य उसी को कहना चाहिए जो अच्छी प्रकार सोच-विचारकर कार्य करता है ।
- मनुष्यशरी देकर ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दे दिया है कि व्यक्ति पृथिवी से लेकर ईश्वरपर्यन्त सत्य को जानकर उनका ठीक उपयोग कर सकता है। परन्तु अपने हठ, प्रयोजन -सिद्धि, दुराग्रह, मिथ्या- अभिमान, दोषों से प्यार, अविद्यादि के कारण असत्य की ओर झुक जाता है ।
- मनुष्य का आत्मा ही सत्यासत्य को जानता है अन्य किसी पशु पक्षी का नहीं, परन्तु फिर भी हठ, दुराग्रह, अपने प्रयोजन की सिद्धि में सत्य से असत्य की ओर झुक जाता है ।
- किसी भी सिद्धान्त को प्रथम शब्दप्रमाण पर विश्वास करके जानना, मानना, फिर उसे आचरण में लाना, फिर उससे संतुष्ट होना। अन्तिम सत्य-असत्य को जानने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा दें, उन्हें आचरण में भी लाएँ। जैसे महर्षि दयानन्द जी ने अपने मन्तव्यामन्तव्य सिद्धान्त, नियम निश्चित किए और उनको धारण किया ।
- ईश्वर है केवल इतने मात्र से विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है बल्कि हम उससे कितना लाभ ले रहे हैं, यह मुख्य है। तुलनात्मक अध्ययन करो कि जो सिद्धान्त में जानता हूँ, अन्यों को बताता हूँ, क्या में स्वयं उन पर चलता हूँ, मेरे आचरण-व्यवहार में उनका कितना भाग है।
जीवन का मुख्य लक्ष्य
- ईश्वरप्राप्ति ही मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, अन्य कोई वस्तु नहीं,यह लक्ष्य हमेशा स्थिर रखना, अत्यन्त पुरुषार्थसाध्य है ।
प्रश्न➨ हम ईश्वर-प्राप्ति को ही मुख्य लक्ष्य क्यों मानते हैं, अन्य प्रयोजन भी तो हैं ?
उत्तर➨ प्रत्येक प्राणी समस्त क्लेश, दुःख से छूटना चाहता है और नित्यानन्द की प्राप्ति करना चाहता है; यह प्रयोजन बिना ईश्वर- प्राप्ति के सिद्ध नहीं हो सकता। हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय को जानने, आचरण में लाने से ईश्वरप्राप्ति होती है, ये मुख्य साधन हैं।
- प्रत्येक क्षण ईश्वर का ही विचार, चिन्तन, मनन, उसी की उपासना करना सभी कार्यों से उत्तम है। अन्य कोई भी कार्य इतना उत्तम नहीं है।
- ईश्वर की उपासना, उसी में तल्लीन रहना, अन्य किसी भी वस्तु को न चाहना अत्यन्त आनन्दप्रद है और अन्य वस्तु प्रकृति, जीव और जगत् की उपासना करना, उसी में तल्लीन रहना, ईश्वर को छोड़ देना क्लेशों, अविद्या, अधर्म, अन्याय की प्राप्ति करवाता है।
- ईश्वरप्रणिधान में रहते हुए, ईश्वरोपासना में अपने आप को स्थिर करते हुए अपने विचारों, कार्यों को करना लाभप्रद है, इसके विपरीत हानिकारक है।
प्रश्न➨ ईश्वर ने यह सृष्टि किस प्रयोजन से बनाई? न बनाता तो किसी जीव को सुख-दुःख भी न होता ईश्वर स्वयं भी आराम से प्रकृति के साथ पड़ा रहता ?
उत्तर➨ ईश्वर कभी भी भूल नहीं करता न आगे करेगा क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह सृष्टि हम जीवों के कल्याणार्थ कर्मों का फल देने के लिए और प्राकृतिक गुणों को प्रकाशित करने के लिए बनाई है, अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। पड़े रहना जीव का स्वभाव नहीं है, कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना उसका स्वभाव है इसलिए ईश्वर ने सृष्टि व्यर्थ नहीं बनाई है। इसलिए इस बात में कोई सन्देह नहीं करना चाहिए।
- व्यक्ति प्राय: या तो अपनी, अन्य जीवात्माओं की या प्रकृति से बने पदार्थों से सम्बन्धित ज्ञान-कर्म-उपासना में लगा रहता है। ईश्वर को तो प्राय: भूले ही रहता है ।
- ईश्वर हर क्षण हमारे प्रत्येक ज्ञान-कर्म-उपासना को जान रहे हैं। और उसी के अनुरूप ही सुख-दुखरूपी फल भी देंगे; यह बात हर समय मन में बैठी रहे और इस पर दृढ़ निश्वय भी हो। हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों को देखकर उनका अच्छा ही फल दे। इस दृष्टि से ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते हैं परन्तु कुछ सीमा तक ही मानते हैं। जैसे कि बुरे कार्य करते समय सोचते हैं कि ईश्वर नहीं देख रहा है; यह असत्य व्यवहार है ।
- हम चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय न हो, सभी कर्मों का ठीक-ठीक फल मिले। इसलिए ईश्वर पर कुछ विश्वास भी करते हैं परन्तु बुरे कर्म का बुरा फल देखकर बुरे-कार्य करने से नहीं डरते अर्थात् ईश्वर को भुला देते हैं; यह असत्य व्यवहार है।
- ईश्वर सब की आत्मा में बैठा है और प्रत्येक कार्य के पूर्व सब को सत्योपदेश कर रहा है। जो व्यक्ति उसके संकेत को समझ=जान लेता है और यदि उस संकेत के अनुरूप चलता है तो बहुत सी बाधाओं से बच जाता है ।
- ईश्वर प्रतिदिन समझाता, संकेत करता है फिर भी उसकी बात नहीं मानते परन्तु वह सत्योपदेश देने से नहीं हटता। सदा सच्चे मित्र की भाँति साथ निभाता, हम ही उसे छोड़ देते हैं। परन्तु जब हमारी कोई बात नहीं मानता, सुनता, पालन करता तो हम उस व्यक्ति से द्वेष करते, बुरा-भला कहते, कठोर बोलते हैं। ईश्वर को मित्र बनाने के लिए उस जैसा व्यवहार करना पड़ेगा।
- जब व्यक्ति किसी भी स्थिति में ईश्वर को छोड़ देता है तो अपने मन, संस्कारों, बाह्य आलम्बनों के कारण सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए कभी भी, किसी भी स्थिति में ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए ।
- ईश्वर हमारे साथ है। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है तो चिन्ता किस बात की, जब सब कुछ ईश्वर का ही है।
- अपने शरीर के एक-एक अंग को देखो ईश्वर से कितनी सहायता मिली है । हाथ, अंगुली, हृदय आदि प्राणी को जीवित रखने में कितने सहायक हैं? क्या हम इसे स्वतन्त्र रूप में बना सकते हैं? ऐसा सोचने, समझने, जानने, सत्य को ग्रहण करने की इच्छा होने पर ही व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है।
- ईश्वर हर समय हमें अच्छे-बुरे कार्यों के प्रति संकेत करते हैं; इस माध्यम से दुःख से बचाकर सुख देना चाहते हैं। परन्तु हम ईश्वराज्ञा का पालन नहीं करते। फिर ईश्वर न्यायानुसार दण्ड देते हैं वह भी हमारे ही कल्याण के लिए है ताकि हम पाप से बच जाएँ।
- ईश्वरप्राप्ति कितना महान्, पुरुषार्थसाध्य, कठिन कार्य है। जिसका यह लक्ष्य है उसे व्यर्थ विचार, चिन्तन, अन्य व्यर्थ शारीरिक क्रिया करने का समय नहीं मिलता। क्योंकि इस महान् लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना समय, चिन्तन, एकाग्रता अपेक्षित है, उतना अन्य के लिए नहीं। उसे तो केवल जो अपने लक्ष्य के साधक द्रव्य हैं उनको ही ग्रहण करना होता है। एक क्षण भी उसका व्यर्थ नहीं जाता। यदि गलती से ऐसा करता है तो उसे अत्यन्त ग्लानि, पश्चात्ताप होता है। क्योंकि यह जीवन अमूल्य है। समय बीता ही जा रहा है। एक क्षण भी यदि लक्ष्य को भूल जाता है तो पतित हो जाता है। उसका सारा ध्यान लक्ष्य प्राप्ति में ही होता है। संसार के जो आवश्यक व्यवहार हैं उनको गौण रूप में करता हुआ न के बराबर करता है।
- अपने लक्ष्य-सिद्धि की योग्यता बनाने हेतु अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है परन्तु यदि उसके लिए कोई योजना, विधि, वैसा पुरुषार्थ नहीं है तो इसका अर्थ है कि अभी लक्ष्य समझ में नहीं आया। यदि साधनों के प्रति रुचि नहीं है, आलस्य-प्रमाद है तो उसे ठीक करना मुख्य है। ईश्वरप्राप्ति लक्ष्य रखनेवाले के लिए शारीरिक बाधाएँ नाममात्र हैं क्योंकि यह ईश्वरप्राप्ति का सारा कार्य मानसिक स्तर पर होता है। इन सभी के पीछे यह है कि ये सभी कार्य बिना ईश्वर की सहायता के सम्भव नहीं है। जिसका ईश्वरप्राप्ति लक्ष्य बन जाता है उसकी बाह्य सांसारिक विषयों में रुचि, आकर्षण नहीं रहता।
लक्ष्य से पतित होने के कारण➤
(१) "ईश्वरप्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य है, जिसके तुल्य और अधिक कोई लक्ष्य नहीं है" ऐसा मानना छोड़ देगा तो ईश्वरप्राप्ति से दूर हो जाएगा।(२) ईश्वर-प्राप्ति के लिए पूर्ण और अत्यन्त पुरुषार्थ नहीं करेगा तो ईश्वर-प्राप्ति से दूर हो जाएगा ।
(३) यम-नियमों का मन-वचन-कर्म से पूर्ण पालन नहीं करेगा तो ईश्वर-प्राप्ति से दूर हो जाएगा ।
(४) विरोधीतत्त्व, अधर्म, अन्याय, प्रतिपक्षभावना से विरोध का अभाव ये सब उसे लक्ष्य से पतित करते हैं।
५. कठोपनिषद् में बताया कि ब्रह्म विद्या को सुनने और कहने वाला दुर्लभ होता है। यह उस समय की बात जब आध्यात्मबहुल समाज था। आज की तो बात ही क्या जब सभी के लौकिक लक्ष्य बने हुए हैं।
६. जो व्यक्ति वेदों, ऋषियों, महापुरुषों, गुरुओं के आदर्श, सत्यवादिता, यम नियमों का पालन, योगाभ्यास आदि को मस्तिष्क में रखता है, और संकल्प करता है कि इनके विरुद्ध एक भी चेष्ट नहीं करूँगा, वही व्यक्ति
इस योग मार्ग पर टिक सकता है अन्यथा ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं जो संन्यास लेने के पश्चात् भी गृहस्थ बने।
- यदि हमारा ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य है तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। अपना आत्मनिरीक्षण करो कि हम इस मार्ग में कितना बढ़ रहे हैं।
- संसार में अपमान होगा, गालियाँ मिलेगी। सब प्रतिकूलताएँ होगी। सबको सहन करना, यह छुरे की धार है।
- बुरा लगना, बुरा मानना अथवा ऐसा व्यवहार करना कि दूसरे को लगे कि हम उनसे नाराज हैं यह सब योग में बाधक है ।
- कठोपनिषद् में नचिकेता की कथा आई है । विद्वानों के द्वारा उसकी दो प्रकार से व्याख्या की गई है➧ (१) आलंकारिकरूप में जिसमें नचिकेता को जीवात्मा और यमाचार्य को ईश्वर के रूप में वर्णन किया गया है। (२) नचिकेता शिष्य के रूप में और यमाचार्य एक आचार्य के रूप में ऐतिहासिक घटना है। जो भी हो कथा के अन्त में प्रसंग है– नचिकेता जैसा शिष्य और यमाचार्य जैसा आचार्य मिलना कठिन है। पुनः ईश्वर का स्वरूप बताया है कि-सारे वेद जिसे कहते हैं। सारे तप, ब्रह्मचर्यादि जिसके लिए किए जाते हैं, उसका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ वह 'ओ३म्' है। आचार्य नचिकेता को कहते हैं कि "उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत"। यह मार्ग छुरे की धार के समान है ।
- जिसे ईश्वरप्राप्ति करनी हो उसे नचिकेता की तरह योग्यता बनानी पड़ेगी। उस कथा में यदि नचिकेता को जीवात्मा के रूप में लेते हैं तो यमाचार्य ईश्वर है अर्थात् ईश्वर की दृष्टि में जो पात्र है, जो उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसे ही अपना साक्षात्कार करवाता है। ईश्वर परीक्षा लेता है - जैसे कि नचिकेता को विभिन्न प्रलोभन देकर परीक्षा ली गई थी । परन्तु जिसे केवल सत्य को ही जानने की चाह हो वह इन प्रलोभनों में नहीं फँसता । यमाचार्य ने कहा जल्दी अविद्यान्धकार से जागो। योगी लोग इसे छुरे की धार भी कहते हैं ।
- ईश्वर का देश की दृष्टि से न आदि है न अन्त है। यह बहुत ही कठिन और गम्भीर विषय है। वह ईश्वर दिखाई भी नहीं देता। प्राय: व्यक्ति संसार में सभी वस्तुओं को आदि और अन्त सहित देखता है अतः उसे ईश्वर के विषय में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई विचित्रपदार्थ होगा? बड़े बड़े बुद्धिमान् भी इस बात पर चकरा जाते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं । पूर्ण रूपेण ईश्वर को जान जाएँ ऐसा सम्भव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। परन्तु कुछ ज्ञानादि गुण जो अनुमान से सिद्ध होते हैं उनके माध्यम से ईश्वर को जान सकते हैं और उन्हीं गुणों को मानकर उसकी आज्ञानुसार चलें ।
- ईश्वर को किसी भी स्थिति में गौण नहीं मानना चाहिए। क्योंकि न तो ईश्वर के तुल्य कोई है न अधिक है। वैसे भी दो समान वस्तुओं में एक ही वांछित (यह लेना वह नहीं ऐसी) नहीं हो सकती परन्तु विशेषता के कारण एक के उत्कृष्ट सिद्ध होते ही दूसरी निकृष्ट सिद्ध हो जाती है। उत्कृष्ट वांच्छित तथा निकृष्ट सदा हेय होती है। ईश्वर उत्कृष्टतम सिद्ध है। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ईश्वर के तुल्य हो। अतः ईश्वर को सदा मुख्य मानना चाहिए ।
- यदि संसार में कुछ करना शेष रह गया है तो समाधि नहीं प्राप्त होगी। केवल एक ही कार्य शेष रहना चाहिए ईश्वर का साक्षात्कार करना और करवाना। मन में ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए कि हाय ! यह लौकिक कार्य नहीं किया।
- यदि महत्परिमाण वाले ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं तो हम जो जीवात्मा अणुपरिमाण वाले हैं जिसका भी आदि, अन्त नहीं है, फिर भी उसकी सत्ता मानते हैं इसलिए यदि ईश्वर का आदि अन्त पकड़ में नहीं आता तो भी जीवात्मा की तरह उसकी सत्ता माननी चाहिए ईश्वर का निषेध भी नहीं करना चाहिए ।
विवेक-वैराग्य
- १. समाधिप्राप्त एक विवेकी वैदिक विद्वान् का जितना मूल्य है, उतना सहस्र करोड़ों वैज्ञानिकों का नहीं है।
- २. जो व्यक्ति दुःख को दुःख, सुख को सुख, अनित्य को अनित्य, नित्य को नित्य आदि इस प्रकार सत्य को जानता, मानता है, वह विवेक को प्राप्त होता है ।
- ३. जब तक संसार की प्रत्येक वस्तु को अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मा के रूप में नहीं देख लेंगे, तब तक अविद्या में फँसे रहेंगे ।
- ४. विवेकी, वैरागी अत्यन्त गम्भीर रहता है, उसे समाधि प्राप्ति के उपायों को अपनाने के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर के अतिरिक्त उसके लिए कोई आश्चर्यजनक वस्तु नहीं रह जाती।
- ५. अभी जो संसार में विचित्रता, आश्चर्य दिखता है वह प्रकृति का विभिन्न रूप है, एक दिन यह अपने कारण में विलीन हो जाएगी।
- ६. सांसारिक भोग भोगने से उतना सुख नहीं मिलता जितना सांसारिक भोगों की इच्छा छोड़ने से मिलता है।
- ७. जो वस्तुएँ त्याग दी हैं अथवा अप्राप्य हैं, उनकी प्राप्ति की इच्छा मूर्खों का लक्षण है वह चाहे विषयों के प्रति आसक्ति हो या अन्य व्यक्तियों के प्रति, राग-द्वेष। मन में अभी भी यदि लौकिक चर्चा, लौकिक- व्यवहार, रूपादि विषयों को देखने की इच्छा है तो अभी योग मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं ।
- ८. अन्तिम निर्णय होने पर सन्तोष की स्थिति आती है तथा लगता है कि मुझमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, चाहे जितना भोगों को भोग लें ।
- ९. योगी बार-बार अपने शरीर को देखता है कि लगातार उससे मल निकल रहा है तथा ऐसे ही अन्यों के शरीर हैं। इसलिए उसे अपने और अन्यों के शरीरों में आसक्ति नहीं होती ।
- १०. योगी बनना हो तो समस्त सृष्टि के नाम-रूप को समाप्त कर दो अन्यथा समाधि की आशा छोड़ दो ।
- ११. जब व्यक्ति देखता है कि नाम=व्यक्ति का नाम और रूप=शरीर ही नहीं रहेगा। कौन, किसका, क्या ये भी नहीं रहेगा तो अभिमान क्यों? जब व्यक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु को बौद्धिक रूप से प्रलय में गया देखता है तो उसे पता चलता है कि एक तिल मात्र वस्तु भी मेरी नहीं है। उसका सारा अभिमान, स्वस्वामि-सम्बन्ध, नहीं रहता। मान-अपमान की कोई चिन्ता नहीं होती ।
- १२. योगी के लिए दृश्य = कार्यजगत् रहता हुआ भी बौद्धिक स्तर पर नहीं रहता है क्योंकि कार्य में ही कारण विद्यमान होता है। योगी कार्य को कारण में लीन देखता है ।
- १३. विवेक-वैराग्य युक्त योगाभ्यासी में कुछ विशेष करने की आग विचित्र होती है। हर समय सीमा पर तैनात सैनिक की तरह सतर्क सावधान रहता है, कोई भी त्रुटि न हो ऐसा प्रयास करता है ।
- १४. जब पता है कि यह विषय हमारे काम का नहीं है; इनकी पूर्ति सम्भव ही नहीं है तो ऐसी इच्छा करना व्यर्थ है और यह ईश्वर की दृष्टि से उचित भी नहीं है। जैसे रूपादि विषयों में आसक्ति रखना, किसी के प्रति काम-वासना रखना ।
- १५. व्यक्ति विषयों की ओर दौड़ता है, परन्तु मृगतृष्णा की तरह कुछ भी हाथ में नहीं आता, वैसी ही 'अतृप्ति' की स्थिति रहती है, परन्तु फिर भी अविद्या, अज्ञानता से उस ओर आकर्षित होता है ।
- १६. शास्त्रों में जो महत्त्वपूर्ण बातें लिखीं हैं, उनको हमेशा मन-मस्तिष्क में रखना चाहिए क्योंकि वे बातें आपत्तिकाल में ढ़ाल का कार्य करती है। उनसे बहुत से समाधान हो जाते हैं। उन आदर्शों को हमेशा सामने रखकर चलें अन्यथा संसार के आलम्बन हमें आकर्षित कर लेंगे ।
- १७. ईश्वरप्रदत्त यह शरीर साधन रूप में मिला है इसका सदुपयोग न करने से अनन्त-अज्ञान-दुःख फल मिलेगा। ऐसे ही गुरु आचार्य के रूप में मार्गदर्शन, अवसर, साधन भी उपलब्ध हैं, फिर भी विवेक-वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो हम में कमी है ।
- १८. जो सम्मान से विष के तुल्य डरना कहा है वह यही तो है कि स्वयं की अच्छी से अच्छी वस्तु का भी त्याग कर देना।
- १९. सब कुछ ईश्वर का ही मानना, किंचित मात्र भी अपना न मानना, कोई ननुनच न होना। ईश्वर, वेद, ऋषियों के आचरण के विरुद्ध अपनी बात हो तो उसको छोड़ देना। ऐसी स्थिति होने पर ही ईश्वर की सहायता से समाधि की प्राप्ति हो सकती है ।
मनोनियन्त्रण
(i) उत्तम स्थिति➠ व्यक्ति हर क्षण मन को बाह्य लौकिक, हानिकारक और अनावश्यक विषयों में जाने से ऐसे रोके रखता है जैसे अग्नि के जलाने के स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति हर समय उससे दूर रहता है। इस स्थिति में कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ता है ।
(ii) मध्यम स्थिति➠ मन को विषयों में चलाने से पहले रोक लेना।
(iii) निम्न स्थिति➠ मन को विषयों में ले जाकर फिर रोक पाना।
२. व्यक्ति यदि एक क्षण भी मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण को छोड़ देता है तो उसी समय यम-नियमों का भंग कर देता है और विनाशकारी कार्य कर लेता है। ऐसे ही जब व्यक्ति ईश्वर से सम्बन्ध तोड़ लेता है तो उसी समय प्रकृति से जुड़ जाता है और अज्ञान रूपी अन्धकार को प्राप्त होता है ।
३. जैसे चालक गाड़ी की गति से अधिक गति अपने मन में रखता है तभी गाड़ी पर नियन्त्रण कर पाता है। ऐसे ही अत्यधिक वेगवान् वस्तु मन को चलाने, नियन्त्रण में रखने के लिए आत्मा को उससे अधिक शीघ्रातिशीघ्र इच्छाएँ, योजनाएँ बनाने, बदलने में समर्थ होना पड़ेगा, अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
४. मन तो वास्तव में वस्तु का सही स्वरूप दिखाता है, परन्तु हम स्वयं अपनी भावनाएँ उस वस्तु से जोड लेते हैं और प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए बड़ी सावधानी रखकर उस विषय के संस्कार न उठाना चाहिए।
५. मन-वचन-कर्म से हम जो भी कार्य करते हैं उन सभी कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं हमारा है, हम स्वयं कर्ता हैं, मन, इन्द्रियाँ तो जड़ हैं ।
६. हँसी-मजाक करते समय व्यक्ति को बाह्यवृत्ति के रूप में व्यर्थ और अनावश्यक विचार-चिन्तन करना पड़ता है ताकि सामने वालों का अधिकाधिक मनोरंजन हो सके। इस स्थिति में मन की चंचल अवस्था होती है ।
७. मन को जड़ मानने और इच्छानुसार चलाने के अभ्यासक्रम में पहले शरीर को स्थिर रखना। इसके लिए जिस अंग में लगे कि प्रतिकूलता सी है उसे बलपूर्वक न हिलाना, वहाँ से इच्छा को हटा लेना। ऐसे ही सारे शरीर से करना ।
पुन: मन को इच्छापूर्वक स्थिर करना। इसके लिए मन और जीवात्मा के गुण-धर्म जानना । सारे व्यवहारों में जो भी क्रियाएँ होती हैं, उसमें जीवात्मा की इच्छा, प्रयत्न, मन को प्रेरणा देना, मन द्वारा बुद्धि इन्द्रियों को प्रेरणा देना आदि जानना। इतना जानने के पश्चात् मन को रोकने में सफलता मिलेगी। इच्छा, ज्ञान रोकने पर मन को भी रोक सकते हैं। मन को रोकने का अभ्यास करने पर उसे जहाँ चाहे जिस विषय में लगा सकते हैं ।
८. पाँच वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति उठाते हैं तो उसके पीछे संस्कार, अभ्यास, अविद्या, राग-द्वेष, रजो- तमो गुण आदि कारण होते हैं। इन कारणों और वृत्तियों को हटाना जीवात्मा के अधीन है।
संस्कार
- १. जो व्यवहार आत्मा को, मन को शुद्ध करता है वह संस्कार है। संस्कार की परिभाषा, लाभ, अच्छे संस्कार कैसे बनाएँ, बुरे कैसे हटाएँ, इसका परिज्ञान होना चाहिए।
- २. अपने अच्छे संस्कारों को हमेशा उभारे रखने का प्रयास करें, इन्हीं संस्कारों से जीवन बदल सकते हैं, अन्यथा यूँ ही कीड़े-मकौड़ों की भाँति जीवन जीने से क्या फायदा।
- ३. संस्कार दग्ध तब कहा जाता है कि जब विषय सामने आने पर भी अपना प्रभाव न दिखाए। समाधि अवस्था में योगी अपने संस्कारों को जब देखता है तो उनके परिणाम, प्रभाव, हानियाँ देखकर अभ्यास-वैराग्य से उन संस्कारों को दग्धबीज करता जाता है ।
- ४. व्यक्ति प्राय: शरीर की आवश्यकतानुसार भोजन नहीं खाता बल्कि मुझे कब तक रस, सुख मिल रहा है, इस मापदण्ड से खाता है। व्यक्ति संयमपूर्वक यदि थोड़ी भूख रखकर भोजन खाता है तो थोड़ी देर पश्चात् देखता है कि उसने ठीक भोजन खाया है। इसलिए इतनी भूख रखकर भोजन खाओ कि जितना खाया उसका आधा और भी खाया जा सके, तभी व्यक्ति स्वस्थ, दीर्घायु और सुख से रह सकता है। ये भी कोई बुद्धिमत्ता है कि खानेवाली अच्छी वस्तु के कारण अपनी रस इन्द्रिय पर संयम ही खो दे। केवल थोड़े समय के सुख के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ से नष्ट होने वाले संस्कार बना ले।
- ५. आठ प्रकार के मैथुनों से, अश्लील फिल्मी गीत सुनने, अश्लील दृश्य देखने, श्रृंगारादि करने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है, कामुकता, अशान्ति और चंचलता बढ़ती है।
भाषा
- १. योगाभ्यासी को लौकिकों की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए; जैसे ये, वो, हो गया अथवा क्या है? बल्कि आदरसूचक, प्रेमपूर्वक कोमल वाक्य बोलने चाहिए। इसके लिए पहले मानसिकरूप में इस प्रकार की भाषा का अभ्यास करना पड़ेगा। पुन: वाणी से, शरीर से वैसा ही व्यवहार करना। परन्तु आज ऐसा सिखाया नहीं जाता है, यदि कोई सिखाए तो कोई सीखने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में योग- मार्ग पर नहीं बढ़ा जा सकता ।
- २. भाषा व्यवहार करते समय यह ध्यान रखना है कि यदि किसी को आप समझा रहे हैं तो आपकी भाषा से सामने वाले को सुख भी हो और समझने में सरलता हो। सामने वाले को लगे कि वह मेरे हित के लिए कह रहा है। इस प्रकार से व्यवहार करने से ही सूक्ष्मता से अहिंसा आदि का पालन हो पाएगा और योग में गति होगी। अपने संस्कारों को जान पाएँगें, दूर कर पाएँगे। यदि भाषा कठोर, आदेशात्मक बोलेंगे तो उससे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा ही, आपको चाहे पकड़ में आए या न आए।
- ३. किसी के नाम के साथ 'जी' मात्र लगाने से यह सिद्ध नहीं होता कि मैं उसका आदर करता हूँ। मन में वैसी ही आदरभावना, वैसा ही भाषा-व्यवहार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो योग-मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। सम्मान के साथ उसके हित के लिए अपना हित त्याग करना भी सम्मिलित है। हम प्राय: किसी के नाम के साथ 'जी' को शब्द मात्र समझकर लगा देते हैं। परन्तु यदि आत्मनिरीक्षण करके देखें कि क्या मैं उसका सम्मान करता हूँ? हित चाहता हूँ? तो संकोच होता है, स्वयं को उससे बड़ा मानते हैं, अभिमान से युक्त हैं जो जीवन नष्ट करनेवाला है। ऐसा करके सामनेवाले को अपने आत्मा के तुल्य नहीं मान रहे हैं ।
- ४. कई बार भाषा में जानबूझकर मधुरता लाकर किसी के नाम के साथ 'जी' कहते हैं। वह सब समाज को अच्छा दिखाने के लिए अथवा गुरु/आचार्यों के नियमों के भय आदि से करते हैं, परन्तु मन में वैसी भावना नहीं होती क्योंकि व्यवहार में वैसा अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते। इससे उस समय भावना का भी पता चलता है कि हम उसका कितना हित चाहते हैं।
- ५. बोलते समय, शरीर से व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि इससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब तक बात मन में है, तब तक अपनी है। जब बोल दी तो अपनी नहीं रही, इसका अन्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- ६. दोष दिखानेवाली, उलाहने वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मन-वचन-कर्म से शुद्ध, मधुर, सत्य व्यवहार करना चाहिए।
- ७. बोलते समय=व्यवहार करते समय भाषा मधुर, प्रिय, सत्य, प्रेम से बोलना, उसके साथ वैसे ही हाव-भाव भी होने चाहिए, ऐसा न लगे कि अपनी ऐंठ में खड़ा है।
- ८. भाषा में जब कठोरता, अधिकार, आदेशात्मकता आती है तो व्यक्ति अपने मन में यमनियमों का हनन करता है। इसका दुष्परिणाम वाणी से विवाद, झगड़ा, फिर आगे चलकर शरीर से भी हो सकता है।
- ९. किसी को अनुशासन में रखने वाली भाषा प्रारम्भिक योगाभ्यासी को नहीं बोलनी चाहिए। इससे वाणी में कठोरता और मन में द्वेषादि उत्पन्न हो जाएँगे। अपने मित्रों, सहपाठियों से बहुत मधुर व्यवहार करना चाहिए। बार-बार पूछने पर भी वाणी में कठोरता न आए इस बात का ध्यान रखने पर विवेक-वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है।
- १०. जब तक समाधि प्राप्त नहीं हुई तब तक कठोर भाषा, खण्डन-मण्डन, विरोध आदि करने से वैराग्य का स्तर गिरता है। संसार का तो यही स्वभाव है इसलिए सहन करो अन्यथा द्वेष बढ़ेगा, दु:खी रहेंगे ।
- ११. बार-बार बताए जाने पर भी कोई साथी गलत कार्य करता है, तो बताने वाला अपने मन में क्षोभ उत्पन्न कर लेता है कि क्या व्यक्ति है, बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है? बताने वाले के द्वारा उस समय प्राय: यम-नियमों का हनन होता है उससे उसका सारा योगाभ्यास निष्फल हो जाता है ।
आत्मचिन्तन
२. आत्मनिरीक्षण करते रहना कि आज का दिन कैसे गया, आध्यात्मिक पथ पर कुछ आगे बढ़े अथवा कोई उपलब्धि प्राप्त की अथवा वैसे ही पशुओं की तरह खाते-पीते समय बिता दिया ।
३. जो विद्या, अविद्या के स्वरूप को यथावत् नहीं जानता वह योगी नहीं बन सकता। यह शरीर मेरा है यह अविद्या है। ईश्वर ने यह शरीर मेरे प्रयोग के लिए दिया है ऐसा समर्पण विद्या है। इस प्रकार जानने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सत्पुरुषों का संग अत्यन्त उच्चकोटि का साधन है। इसी प्रकार जीव का स्वभाव स्वरूप से शुद्ध लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अशुद्ध प्रतीत होता है अत: वह देखता है कि कहीं मैं भोक्ता न बन जाऊँ? प्रकृति में सुख दुःख दोनों हैं किन्तु दु:ख अधिक है अतः योगाभ्यासी उसे दुःख ही मानता है। ईश्वर में केवल सुख है दुःख नहीं ईश्वर शुद्धस्वरूप है। जो इन सब बातों को जानता है वह समाधि प्राप्त करता है ।
४. जीवात्मा के गुणों का तो प्रत्यक्ष होगा लेकिन उसका यह छोर है, यहाँ तक समाप्त है ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होगा ।
५. जीवात्मा ईश्वर की तरह चेतन, शुद्ध, प्रकृति दोष से रहित, परिणामरहित, मिश्रणरहित, अनन्त ( काल की दृष्टि से) है, जो व्यक्ति ऐसा अनुभव कर लेता है तो वह बहुत सी बाधाओं से बच जाता है ।
६. स्थिर वस्तु ही परिवर्तनशील वस्तुओं को देख सकती है। अत: आत्मा विभिन्न विषयों, वृत्तियों को चित्र रूप में देखता है जैसे नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति नदी में बहती हुई लकड़ी आदि को देखता है। स्थिर में कोई परिवर्तन नहीं होता।
७. आत्मा से बाहर सभी विषय जड़ हैं। जड़ वस्तुओं को चलाने हेतु चेतन की आवश्यकता होती है जैसे कार को। वैसे ही मन जड़ है अत: इसको चेतन आत्मा चलाता है ।
८. आत्मा केवल द्रष्ट मात्र है, कोई भोग उसमें नहीं जाता ।
९. सुख-दुःख जीवात्मा के नैमैत्तिक गुण हैं, प्रकृति के स्वाभाविक गुण हैं। जैसे प्रकृति के अन्य रूप, रस आदि गुण हैं वैसे ही सुख दुःख भी हैं। जैसे अन्य गुणों का अनुभव प्रकृति स्वयं नहीं करती वैसे ही सुख दु:ख का अनुभव नहीं करती। जीवात्मा उन गुणों का अनुभव करता है। यह सृष्टि संघातरूप होने से इसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु जीवात्मा के लिए है ।
१०. जेसे चोराहे पर ट्रेफिकवाला खड़ा है, उल्लंघन करने पर तुरन्त दण्ड देगा। क्या इस प्रकार ईश्वर आपको जँच गया है? इसके साथ यह भी मन में हो कि ➧
i. ईश्वर कण-कण में विद्यमान है। अन्दर भी है, बाहर भी है ।
ii. ईश्वर सर्वज्ञ (तीनों कालों का), सर्वशक्तिमान्, ऐश्वर्यशाली है।
iii. ईश्वर न्यायकारी है, सदा तीनों कालों में न्याय ही करता है ।
iv. ईश्वर सभी को एक दृष्टि से देखता है ।
v. ईश्वर के आनन्द की कोई सीमा नहीं है ।
vi. चाहे कुछ भी हो ईश्वर अपनी व्यवस्था, अनुशासन भंग नहीं करता ।
vii. ईश्वर सृष्टि का रचयिता भी है इसलिए सृष्टिक्रम से ईश्वर को मन में बिठाया जा सकता है। कितना गम्भीर ज्ञान-विज्ञान है, वैज्ञानिक इससे परे हैं। जीव का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, वह तो अपना भी ज्ञान नहीं कर सकता, सृष्टि बनाना आदि तो दूर की बात है। अपने कर्मों का पूर्णरूपेण ज्ञान नहीं कर सकता और फल भी स्वयं नहीं भोग सकता। प्रकृति भी जड़ होने से अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती ।
११. यदि प्राकृतिक विषयों से कुछ मिलना होता तो उसके गुण जीव में आने चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है। सभी विषयों को भोगने के पश्चात् कुछ मात्रा में क्षणक सुख की अनुभूति होती है, परन्तु स्थिति वेसी की
वैसी रहती है; ऐसा जानकर व्यक्ति विषयों में आसक्त नहीं होता।
१२. व्यक्ति अपने को बहुत सुन्दर, बलवान, हृष्ट-पुष्ट समझता है, जबकि इस शरीर में कितनी अशुद्धि, मल भरा पड़ा है, क्षणभंगुर है पता नहीं कब चला जाए। कितनी ढेर सारी विपत्तियाँ होते हुए भी इसको अच्छा मानता, इसकी पुष्टि करता, पालन करता, इसी के लिए सारा जीवन लगा देता, अहो ! केसा आश्चर्य है।
१३. स्नान करे अथवा अन्य शुद्धि करके व्यक्ति शरीर को शुद्ध मानता है परन्तु जब जीवात्मा इस शरीर छोड़ता तो इतनी दुर्गन्ध आती है कि समीप नहीं रुक सकते। बीमार होने पर अपने ही शरीर से घृणा
सी होने लगती है ।
१४. मेरे कपड़े अच्छे हों, मैल दब जाए इसलिए नील दूँ , बाल अर्थात् चोटी इस प्रकार व्यवस्थित हो, बाल अच्छे कटे हों, अधिक बड़े न हों जिससे में सुन्दर दिखूँ; इन भावनाओं से विषयों में रुचि और ईश्वर में अरुचि उत्पन्न होती है। कपड़ों का प्रयोजन केवल शरीर ढकने के लिए होना चाहिए। इतना तो ठीक है कि कपड़ा मैला न हो, फटा न हो। परन्तु अन्दर जो दिखाने की भावना होती है, वह प्राय: पकड़ में नहीं आती। कपड़ों की वैसी स्थिति, अनुकूलता न होने पर उससे द्वेष होता है। यह सब योग में बाधक हे।
१५. शरीर ही व्यक्ति का स्वरूप होता तो हर समय शरीर की अनुभूति होनी चाहिए थी; जबकि ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। परन्तु यह तो अनुभूति रहती है कि में हूँ, में देख, सुन, जान, क्रिया कर रहा हूँ, विचार-चिन्तन कर रहा हूँ। इसलिए आँख, नाक, कान, पाँव आदि शरीर तो मेरे साधन हैं, में इनका प्रयोक्ता मात्र हूँ। शरीरादि पदार्थ जड़ हैं, में चेतन हूँ , दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव एक नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे में घुलमिल भी नहीं सकते ।
१६. अपने शरीर को बार-बार शीशे में देखते रहना, शरीर की सुन्दरता में ही लगे रहना; इससे अपने शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती है ओर अन्य शरीर को भोगने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ऐसे ही अपने शरीर को अन्य शरीरों की अपेक्षा बलवान् देखने से राग-द्वेष बढते हें।
१७. जब व्यक्ति के पास कीमती द्रव्यों की वृद्धि होती है व्यक्ति प्राय: उन द्रव्यों की वृद्धि के साथ-साथ अपने को भी बड़ा मानने लगता है; यह अविद्या है, इसका निदान इस प्रकार से करना चाहिए कि गुण तो द्रव्य के हैं परन्तु अपने ऊपर लागू क्यों करता हूँ ? यह वृत्ति-सारूप्यम् है। शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि जड़ हैं, में चेतन हूँ, इनमें परिवर्तन होने से मेरी कोई वृद्धि नहीं होगी।
१८. जो व्यक्ति अपने सभी क्रिया-व्यवहार करते हुए ध्यान रखता है कि समाज, राष्ट्र, विश्व, संस्था, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही बुरे कार्य से बच सकता है ।
१९. अपने दोषों को जानने, मानने, समझने, उनको दूर करने में जितना परिश्रम, तपस्या होनी चाहिए, उतनी नहीं कर रहे हैं। अन्यों को छोड़ो पहले स्वयं के दोष जानो, तभी कुछ सफलता मिलेगी अन्यथा वेसे ही खाते-पीते रहोगे।
२०. अन्य की बात अन्य व्यक्ति से करना, चुगली करना, व्यर्थ बातें करना आदि करते समय व्यक्ति को पहले सात्त्विक स्थिति में बुरा लगता है, परन्तु पश्चात् इतनी रुचि हो जाती है कि उसे बुरा ही नहीं मानता।सुनने वाले की भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। ये योग के बाधक हें ।
२१. ईश्वर साक्षात्कार होते हुए भी मेरे अन्दर कितनी सूक्ष्म अविद्या बैठी है इस प्रकार अपने दोषों को देखकर हटने की प्रवृत्ति चलती रहती है, साधारण की तो बात ही क्या ! जैसे अतिसुन्दररूप को देखकर सम्तुष्ट हो जाऊंगा; यह भावना प्राय: प्रत्येक व्यक्ति में जो ईश्वर साक्षात्कारी नहीं है, किसी न किसी रूप में रहती है; यहाँ तक कि आचार्य, गुरु या वेदवेत्ता हो। यदि वह ईश्वर को नहीं जानता, उसे अविद्या नहीं छोड़ेगी ।
२२. जेसा पुरुषार्थ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं वेसा ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। जेसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या आवश्यक वस्तु हो, उसके न मिलने पर अथवा बिछुड़ जाने पर उसकी प्राप्ति की एक तड़प सी लग जाती है। परन्तु जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया हे, उसका ध्यान-उपासना-कृतज्ञता नहीं करते तो भी कोई ग्लानि, पश्चात्ताप, उसकी प्राप्ति की वेसी तड़प नहीं होती; यह ईश्वर के प्रति अन्याय हे, कृतघ्नता है ।
२३. जब भी किसी इन्द्रिय के भोग की इच्छा, आकर्षण होता है तभी विषय-प्राप्ति की योजना, बाधकों का प्रतिकार, साधनों की प्राप्ति, अन्य भी अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिसा आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में समझना चाहिए। व्यक्ति विषय की केवल इच्छा मात्र से क्लेशित होना शुरु हो जाता है, यदि मानसिक स्तर पर सूृक्ष्मता से परीक्षण करे तो पता चल जाएगा ।
१. वक्ता का क्या तात्पर्य है, उसे समझनेवाला व्यक्ति ऊहवान् होना चाहिए। तात्पर्य मुख्य होता है, तात्पर्य समझते समय वक्ता के वाक्य, शब्द गौण हो जाते हैं।
२. ब्रह्मविद्या बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है। इसको समझने के लिए मन-वाणी-शरीर से भी गम्भीर होना पड़ता है ।
३. पहले व्यक्ति को सिद्धान्तों का परिज्ञान अच्छी प्रकार होना चाहिए, जैसे कि कैसे यम-नियमों का पालन होता है। यथा कोई किसी को मिलने का वचन दे, कोई वस्तु देने का वचन दे, तो उसी समय उस कार्य को करने चाहिए। नहीं करता है तो उसका विश्वास नहीं रहता। व्यक्ति स्वयं उन सिद्धान्तों का ईश्वर की सहायता से ज्ञाता अर्थात् साक्षात् करने वाला हो या शब्द-प्रमाण पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसे स्मरण रखे तभी वह सिद्धान्तों
का पालन करेगा। जब भी यम-नियमों का भंग होता दिखेगा, वह इसके आधार पर रुकेगा ।
४. योगाभ्यासी को अपने सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिए और इतना दृढ़ भी होना चाहिए कि इसके विपरीत किचित् मात्र भी नही चलूँगा। जैसे सिद्धान्त निश्चित किया कि मुक्ति में जो-जो बाधक तत्त्व हैं, उनको ग्रहण नहीं करूँगा, विषयों के प्रति संयम रखूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, अनित्याशुचिदु:खानात्मसु.....वाले सूत्र के आधार पर अपने व्यवहार का परीक्षण करता रहँगा। इसके विपरीत एक भी विचार आए तो तुरन्त प्रतिपक्ष भावना से उसे हटाऊँगा अन्यथा उसका फल घोर अज्ञान, अन्धकार भोगना पड़ेगा ।
५. जब व्यक्ति मन में ऐसा दृढ़ संकल्प रखता है कि मुझे केवल सत्य को ही जानना है, में सत्य को ही ग्रहण करूँगा, अन्य नहीं। तब व्यक्ति अन्तिम सत्य को जानने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है और उसे तब सूक्ष्म विषय पकड़ में आते हें।
६. वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, शब्दप्रमाण, अनुमानप्रमाण ये सब सत्य हें। परन्तु जब व्यक्ति इनमें से एक विषय का प्रत्यक्ष करता हे तभी वह सूक्ष्म विषयों तक पहुँच पाता है। बिना एक विषय का प्रत्यक्ष किए केवल शाब्दिक रूप में ही जान सकता है। सूक्ष्म विषयों को जानने का यह एक ढंग हे।
७. कोई भी विचार, क्रिया, चिन्तन यदि सत्यासत्य को जानने की पाँच कसौटियों के विरुद्ध है तो उस समय अपनी बात छोड़कर पाँच कसोटियों की बात मान्य रखना, अन्यथा विनाश होगा ।
८. जो व्यक्ति ऋषि दयानन्द के १० नियमों, ५१ मन्तव्यों, ५ कसोटियों को आदर्श मानकर चलता है, वह सोचता है कि कहीं में ईश्वर, ऋषियों, गुरुओं की दृष्टि में बुग न बन जाऊँ। वही योग-पथ पर आगे बढ़ सकता हे ।
९. जो बात मन में न बेठे उसे पाँच कसौटियों पर कसे; इस प्रकार प्रत्येक क्रिया व्यवहार को प्रमाणित करना ।
१०. जीवन में किसी सिद्धान्त को अन्तिमरूप में देना अत्यन्त परिश्रमसाध्य है, जेसे हम अनन्तकाल से मरते-जन्मते आ रहे हैं। इस प्रकार अन्तिम सत्य को जानना, मानना अत्यन्त कठिन है ।
११. जब प्रमाणों से सिद्ध बात को सत्य मानेंगे तब यह बात जँचेगी कि हम भी पशु-पक्षी आदि योनियों में गए थे। ऐसे ही अन्य बाते हें, स्वयं को ही प्रमाण मानने पर कुछ समझ नहीं आएगा ।
१२. किसी पदार्थ के कुछ गुण प्रत्यक्ष दिखते हैं, कुछ अनुमान से दिखते हैं। पदार्थ के सभी गुण प्रत्यक्ष हों तभी उस की सत्ता मानी जाए, ऐसा नियम नहीं है। जेसे भूमि के सभी गुण जाने बिना भी हम उसकी सत्ता मानते हैं। ऐसे ही ईश्वर की सत्ता माननी चाहिए ।
१३. व्यक्ति प्रायः अपनी सत्ता को तो मानता है, परन्तु ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। वह कहता है ईश्वर अनादि, अनन्त है, उसकी सत्ता कैसे मानें तो जेसे हम भी अनादि हैं परन्तु अपनी सत्ता मानते हें,ऐसे ही ईश्वर की सत्ता मानें। यदि कोई कहे जीव तो एकदेशी है ईश्वर अनन्त है तो वहाँ समझना चाहिए कि यद्यपि जीव एकदेशी है परन्तु उसको किसी ने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, अनुमान से ही मानते हैं ऐसे ही ईश्वर के अन्य गुणों को मानकर उसकी सत्ता स्वीकार करे।
१५. शरीर ही व्यक्ति का स्वरूप होता तो हर समय शरीर की अनुभूति होनी चाहिए थी; जबकि ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। परन्तु यह तो अनुभूति रहती है कि में हूँ, में देख, सुन, जान, क्रिया कर रहा हूँ, विचार-चिन्तन कर रहा हूँ। इसलिए आँख, नाक, कान, पाँव आदि शरीर तो मेरे साधन हैं, में इनका प्रयोक्ता मात्र हूँ। शरीरादि पदार्थ जड़ हैं, में चेतन हूँ , दोनों के गुण-कर्म-स्वभाव एक नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे में घुलमिल भी नहीं सकते ।
१६. अपने शरीर को बार-बार शीशे में देखते रहना, शरीर की सुन्दरता में ही लगे रहना; इससे अपने शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती है ओर अन्य शरीर को भोगने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ऐसे ही अपने शरीर को अन्य शरीरों की अपेक्षा बलवान् देखने से राग-द्वेष बढते हें।
१७. जब व्यक्ति के पास कीमती द्रव्यों की वृद्धि होती है व्यक्ति प्राय: उन द्रव्यों की वृद्धि के साथ-साथ अपने को भी बड़ा मानने लगता है; यह अविद्या है, इसका निदान इस प्रकार से करना चाहिए कि गुण तो द्रव्य के हैं परन्तु अपने ऊपर लागू क्यों करता हूँ ? यह वृत्ति-सारूप्यम् है। शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि जड़ हैं, में चेतन हूँ, इनमें परिवर्तन होने से मेरी कोई वृद्धि नहीं होगी।
१८. जो व्यक्ति अपने सभी क्रिया-व्यवहार करते हुए ध्यान रखता है कि समाज, राष्ट्र, विश्व, संस्था, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही बुरे कार्य से बच सकता है ।
१९. अपने दोषों को जानने, मानने, समझने, उनको दूर करने में जितना परिश्रम, तपस्या होनी चाहिए, उतनी नहीं कर रहे हैं। अन्यों को छोड़ो पहले स्वयं के दोष जानो, तभी कुछ सफलता मिलेगी अन्यथा वेसे ही खाते-पीते रहोगे।
२०. अन्य की बात अन्य व्यक्ति से करना, चुगली करना, व्यर्थ बातें करना आदि करते समय व्यक्ति को पहले सात्त्विक स्थिति में बुरा लगता है, परन्तु पश्चात् इतनी रुचि हो जाती है कि उसे बुरा ही नहीं मानता।सुनने वाले की भी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। ये योग के बाधक हें ।
२१. ईश्वर साक्षात्कार होते हुए भी मेरे अन्दर कितनी सूक्ष्म अविद्या बैठी है इस प्रकार अपने दोषों को देखकर हटने की प्रवृत्ति चलती रहती है, साधारण की तो बात ही क्या ! जैसे अतिसुन्दररूप को देखकर सम्तुष्ट हो जाऊंगा; यह भावना प्राय: प्रत्येक व्यक्ति में जो ईश्वर साक्षात्कारी नहीं है, किसी न किसी रूप में रहती है; यहाँ तक कि आचार्य, गुरु या वेदवेत्ता हो। यदि वह ईश्वर को नहीं जानता, उसे अविद्या नहीं छोड़ेगी ।
२२. जेसा पुरुषार्थ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए करते हैं वेसा ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। जेसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या आवश्यक वस्तु हो, उसके न मिलने पर अथवा बिछुड़ जाने पर उसकी प्राप्ति की एक तड़प सी लग जाती है। परन्तु जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया हे, उसका ध्यान-उपासना-कृतज्ञता नहीं करते तो भी कोई ग्लानि, पश्चात्ताप, उसकी प्राप्ति की वेसी तड़प नहीं होती; यह ईश्वर के प्रति अन्याय हे, कृतघ्नता है ।
२३. जब भी किसी इन्द्रिय के भोग की इच्छा, आकर्षण होता है तभी विषय-प्राप्ति की योजना, बाधकों का प्रतिकार, साधनों की प्राप्ति, अन्य भी अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिसा आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में समझना चाहिए। व्यक्ति विषय की केवल इच्छा मात्र से क्लेशित होना शुरु हो जाता है, यदि मानसिक स्तर पर सूृक्ष्मता से परीक्षण करे तो पता चल जाएगा ।
सिद्धान्तों का परिज्ञान
१. वक्ता का क्या तात्पर्य है, उसे समझनेवाला व्यक्ति ऊहवान् होना चाहिए। तात्पर्य मुख्य होता है, तात्पर्य समझते समय वक्ता के वाक्य, शब्द गौण हो जाते हैं।
२. ब्रह्मविद्या बहुत सूक्ष्म और गम्भीर है। इसको समझने के लिए मन-वाणी-शरीर से भी गम्भीर होना पड़ता है ।
३. पहले व्यक्ति को सिद्धान्तों का परिज्ञान अच्छी प्रकार होना चाहिए, जैसे कि कैसे यम-नियमों का पालन होता है। यथा कोई किसी को मिलने का वचन दे, कोई वस्तु देने का वचन दे, तो उसी समय उस कार्य को करने चाहिए। नहीं करता है तो उसका विश्वास नहीं रहता। व्यक्ति स्वयं उन सिद्धान्तों का ईश्वर की सहायता से ज्ञाता अर्थात् साक्षात् करने वाला हो या शब्द-प्रमाण पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसे स्मरण रखे तभी वह सिद्धान्तों
का पालन करेगा। जब भी यम-नियमों का भंग होता दिखेगा, वह इसके आधार पर रुकेगा ।
४. योगाभ्यासी को अपने सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिए और इतना दृढ़ भी होना चाहिए कि इसके विपरीत किचित् मात्र भी नही चलूँगा। जैसे सिद्धान्त निश्चित किया कि मुक्ति में जो-जो बाधक तत्त्व हैं, उनको ग्रहण नहीं करूँगा, विषयों के प्रति संयम रखूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, अनित्याशुचिदु:खानात्मसु.....वाले सूत्र के आधार पर अपने व्यवहार का परीक्षण करता रहँगा। इसके विपरीत एक भी विचार आए तो तुरन्त प्रतिपक्ष भावना से उसे हटाऊँगा अन्यथा उसका फल घोर अज्ञान, अन्धकार भोगना पड़ेगा ।
५. जब व्यक्ति मन में ऐसा दृढ़ संकल्प रखता है कि मुझे केवल सत्य को ही जानना है, में सत्य को ही ग्रहण करूँगा, अन्य नहीं। तब व्यक्ति अन्तिम सत्य को जानने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है और उसे तब सूक्ष्म विषय पकड़ में आते हें।
६. वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, शब्दप्रमाण, अनुमानप्रमाण ये सब सत्य हें। परन्तु जब व्यक्ति इनमें से एक विषय का प्रत्यक्ष करता हे तभी वह सूक्ष्म विषयों तक पहुँच पाता है। बिना एक विषय का प्रत्यक्ष किए केवल शाब्दिक रूप में ही जान सकता है। सूक्ष्म विषयों को जानने का यह एक ढंग हे।
७. कोई भी विचार, क्रिया, चिन्तन यदि सत्यासत्य को जानने की पाँच कसौटियों के विरुद्ध है तो उस समय अपनी बात छोड़कर पाँच कसोटियों की बात मान्य रखना, अन्यथा विनाश होगा ।
८. जो व्यक्ति ऋषि दयानन्द के १० नियमों, ५१ मन्तव्यों, ५ कसोटियों को आदर्श मानकर चलता है, वह सोचता है कि कहीं में ईश्वर, ऋषियों, गुरुओं की दृष्टि में बुग न बन जाऊँ। वही योग-पथ पर आगे बढ़ सकता हे ।
९. जो बात मन में न बेठे उसे पाँच कसौटियों पर कसे; इस प्रकार प्रत्येक क्रिया व्यवहार को प्रमाणित करना ।
१०. जीवन में किसी सिद्धान्त को अन्तिमरूप में देना अत्यन्त परिश्रमसाध्य है, जेसे हम अनन्तकाल से मरते-जन्मते आ रहे हैं। इस प्रकार अन्तिम सत्य को जानना, मानना अत्यन्त कठिन है ।
११. जब प्रमाणों से सिद्ध बात को सत्य मानेंगे तब यह बात जँचेगी कि हम भी पशु-पक्षी आदि योनियों में गए थे। ऐसे ही अन्य बाते हें, स्वयं को ही प्रमाण मानने पर कुछ समझ नहीं आएगा ।
१२. किसी पदार्थ के कुछ गुण प्रत्यक्ष दिखते हैं, कुछ अनुमान से दिखते हैं। पदार्थ के सभी गुण प्रत्यक्ष हों तभी उस की सत्ता मानी जाए, ऐसा नियम नहीं है। जेसे भूमि के सभी गुण जाने बिना भी हम उसकी सत्ता मानते हैं। ऐसे ही ईश्वर की सत्ता माननी चाहिए ।
१३. व्यक्ति प्रायः अपनी सत्ता को तो मानता है, परन्तु ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। वह कहता है ईश्वर अनादि, अनन्त है, उसकी सत्ता कैसे मानें तो जेसे हम भी अनादि हैं परन्तु अपनी सत्ता मानते हें,ऐसे ही ईश्वर की सत्ता मानें। यदि कोई कहे जीव तो एकदेशी है ईश्वर अनन्त है तो वहाँ समझना चाहिए कि यद्यपि जीव एकदेशी है परन्तु उसको किसी ने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, अनुमान से ही मानते हैं ऐसे ही ईश्वर के अन्य गुणों को मानकर उसकी सत्ता स्वीकार करे।
१७. जो बात हमारे मन में नहीं बेठती हम उसकी सत्ता नहीं मानते,परन्तु जब सत्यासत्य की ५ कसौटियों पर परीक्षण करें तो यह बात गलत सिद्ध होगी। इस सिद्धान्त को मन में बेठाने हेतु अपनी बुद्धि को नीचा और पाँच कसौटियों की बातें ऊँची रखनी पड़ेंगी। इसलिए वेद, ऋषि, शास्त्रों की बातों को ऊँची मानना, अपनी बुद्धि को नीचा।
१५. ये बातें सिद्धरूप में विद्यमान हों कि में जीव अणु हूँ। कर्म करने में स्वतन्त्र हूँ। यह शरीर कर्मफल है। मैं अनेक योनियों में जाता हूँ। अनादि हूँ। वर्तमान से ही भूत, भविष्य दोनों सिद्ध होते हैं। जेसे वर्तमान में हमने जन्म लिया है, ऐसे ही अनादि से अनन्त काल तक इसी प्रकार मरते-जन्मते रहेंगे। ये सिद्धान्त पाँच कसौटियों के द्वारा सिद्ध करके मन में अच्छी प्रकार से बिठा लेने चाहिए, कोई भी संशय न रहे, तब व्यक्ति इस जन्म-मरण के चक्र से छूटना चाहेगा और उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा ।
१६. सृष्टिक्रम अर्थात् जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होगी। जो वस्तु संयोग से बनी है उसका वियोग भी होगा। जिसका आदि है उसका अन्त भी है। इन्हीं के अनुकूल सत्पुरुषों के आचरण प्रमाण है। इनके विरुद्ध कोई भी प्रमाण - तर्क नहीं मिलेगा। जब उसकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है तो अपनी गलत मान्यता को हटा देता है। क्योंकि वह सोचता है कि मैं तो अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् हूँ। मैं तो लाखों बार गलत सोचता हूँ, मानता हूं। उदाहरण-जैसे अनेक बार विषयों में दुख प्रत्यक्ष करके भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूं।
१७. हम कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, कुछ बुरे भी। उन सभी कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका फल देनेवाला कोई नहीं है। भले ही हम बुरे कर्मों का फल नहीं चाहते किन्तु अच्छे कर्मों का फल अवश्य चाहते हैं। परन्तु अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म का भी फल अवश्य मिलेगा।
१८. हेय-हेयहेतु को जानकर छोड़ देना, हान- हानोपाय को जानकर ग्रहण करना सत्य है। किन्तु यह जानना बड़े पुरुषार्थ की बात है कि कौन सी वस्तु ग्राह्य और कौन सी अग्राह्य है। संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा जो योग = समाधि में बाधक तत्त्व है वह अग्राह्य है और साधक तत्त्व ग्राह्य है, जैसे ईश्वर ।
१९. काल और देश की दृष्टि से ईश्वर अनादि है, अनन्त है। वह हर क्षण प्रत्येक जीव के कर्मों को देखता, हिसाब रखता, कर्मों का फल देता है; यह बहुत गम्भीर सिद्धान्त है, इसे हर समय सामने रखें। जब व्यक्ति इसके विरुद्ध विचार उठाता है तो वह तर्क उठाता है कि ये जो लाखों प्रकार की योनियाँ हैं, लाखों जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं यह बिना ईश्वर के कैसे अपने आप हो रहा है?
इस प्रकार प्रश्नोत्तर प्रक्रिया द्वारा इस सिद्धान्त को मन, आत्मा में दृढ़ करना। इसके लिए चाहे अनेक वर्षों तक बार-बार अभ्यास निरन्तर दृढ़ता से करना पड़ेगा। जीव अल्पज्ञ होने से बास- बार अविद्या में गिरता है किन्तु ऐसा करने पर ही व्यक्ति योग-मार्ग पर टिक सकता है।
२०. तीनों कालों में जीव, मूलप्रकृति, कार्यजगत् ये व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है। यह विचार व्यवहारिकरूप में दिन भर मन मस्तिष्क में उपस्थित रखना चाहिए ।
२२. किसी भी गुण की प्राप्ति और दोष की निवृत्ति के लिए विद्या, बुद्धि, दृढ -संकल्प शक्ति, अत्यन्त पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है ।
२३. आत्मा के अस्तित्व के लिए संसार की कोई भी वस्तु अत्यावश्यक नहीं है। ऐसी भावना वाला किसी पदार्थ में तृष्णा नहीं रखता। मिला तो ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है । यही गुण-वैतृष्ण्यम् है ।
२४. किसी पदार्थ में रुचि बनाने के लिए उस पदार्थ के गुणों और उनसे होनेवाले निज सम्बन्धित लाभ को जानना आवश्यक है तभी उस पदार्थ की अनिवार्यता समझ में आएगी, वह पदार्थ चाहे ईश्वर हो ।
२५. जहाँ-जहाँ वस्तु क्रिया करेगी वहाँ-वहाँ उसके गुण प्रकट होंगे ।
२६. वस्तु की सदा वर्त्तमानता में प्रमाण-अभाव से भाव, भाव से अभाव नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान जीव की सत्ता सदा रहती है, केवल अनेक योनियों के शरीरों से जीव का संयोग- वियोग होता रहता है ।
२७. कोई वस्तु अपने आप बनी है यह कथन ही गलत है क्योंकि विद्यमान से ही कर्म आरम्भ होता है और बनी हुई वस्तु बनने के पश्चात विद्यमान हो सकती है व्योंकि बनने के पूर्व वह नहीं होती है। अब यदि कहो वस्तु विद्यमान थी तो उसके बनने का कोई अर्थ नहीं, वह तो है ही। यदि कहो वस्तु विद्यमान नहीं थी तो बनना कर्म आरम्भ कैसे हुआ? इसलिए कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती अपितु अपने से भिन्न कर्ता द्वारा बनाई जाती है। जैसे कहा जाए कि पृथिवी अपने आप बन गई है, तो जिस को पृथिवी कह रहे हैं अपने आप बनी है वह तो बनने के पहले से ही है, अब बनेगी क्यों? यदि पृथिवी पहले स्वयं नहीं थी तो किससे बनी?
२८. अपनी आत्मा को अच्छा लगना अन्तिम कसौटी नहीं है क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ होने से त्रुटियाँ कर सकता है, जब आत्मा सत्य, विद्या के अनुकूल आचरण करता है अर्थात् शब्दादि प्रमाणों के अनुकूल चलता है तो ठीक विचार करता है। जब व्यक्ति पाँच कसौटियों के आधार पर ही किसी बात को जानना चाहता है तब सत्य को प्राप्त करता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं । यदि केवल अपनी आत्मा ही की मानेंगे तो ईश्वर हाथ में नहीं आएगा। जब भी शब्दप्रमाण, ईश्वर, महापुरुष आदि के विरुद्धआचरण हो तो उस समय स्वयं को झूठा और उन प्रमाणों को ठीक मानना, तब तो ईश्वर, आध्यात्मिक विषय आदि की बात मन में बैठेगी, अन्यथा नहीं।
२९. सत्य और असत्य का निश्चय करने की कसौटियाँ -
(१) ईश्वर-ईश्वर के जो गुण=न्याय, कर्म=पक्षपातराहित्य, स्वभाव सत्य, न्याय, दया, परोपकारिता, निष्कामता हैं, इनके अनुकूल जो-जो आचरण है, वह सत्य है।
(२) जैसे बिना कारण और कर्त्ता के कोई कार्य नहीं होता। किसी कार्य के कम से कम तीन कारण अवश्य होते हैं। और कम से कम तीन वस्तुएँ होनी आवश्यक है। कारण-साधारण कारण, कर्ता-निमित्त कारण, उपादान -जो कार्य की मूल सामग्री है। ईश्वर- जीव - प्रकृति में ये तीनों कारण न होने से ये कार्य वस्तु नहीं हैं अर्थात् अनादि अनन्त हैं। इस परीक्षा के जो-जो अनुकूल है वह सत्य है।
(३) ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव या तो वेद से जाने जाते हैं या फिर सृष्टिक्रम को देखकर इससे, ईश्वर का कर्त्तापन, गुण, कर्म स्वभाव देखे-जाने जाते हैं।
(४) सृष्टि और सृष्टि के पदार्थों से ऐसा निश्चित करना कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी है। वह हर समय हमें देख, सुन, जान रहा है। मन-वचन-कर्म से किया गया कोई भी कार्य उससे छुप नहीं सकता। वह हमें न्यायानुसार हमारे कर्मों का फल देगा। क्योंकि ऐसा अन्य कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो हमें और हमारे कर्मों को पूर्ण रूपेण जान सके और ठीक-ठीक न्यायानुसार फल भी दे सके। केवल ईश्वर ही ऐसा है यह निश्चित करने पर व्यक्ति सारे कर्तव्य कर्मों को ईश्वराज्ञानुसार और ईश्वर को ही समर्पण करके उसके गुण-कर्म - स्वभाव के अनुकूल ही करता है। उसे कोई भी लौकिक इच्छा नहीं रहती क्योंकि कोई भी लौकिक पदार्थ कर्मों का फल देने में न तो समर्थ है न ही ऐसी योग्यता है। वह पूर्ण निष्कामता से कार्य करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है ।
(५) जहाँ-जहाँ कार्य दिखता है वहाँ वहाँ कर्ता भी होता है। ईश्वर आँखों से तो प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु सृष्टि में जो उसके गुण-कर्म-स्वभाव प्रत्यक्ष होते हैं उसी से ईश्वर का निश्चय होता है ।
(६) सृष्टिक्रम-सृष्टि का यह नियम है कि जो उत्पन्न होता है वह समाप्त भी होता है क्योंकि वह संयोगजन्य है। जिसमें संयोग होता है उसमें वियोग भी निश्चित होगा। अत: जन्म- मृत्यु, दुःख सुख ये सृष्टि में अनिवार्य हैं। ऐसा ही जानना, मानना सत्य है। ऐसा जानना, मानना कि सृष्टि जड़ है, ईश्वर ने इसे बनाया है । हमे यह केवल धर्म- अर्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि हेतु उपयोग करने के लिए दी है अत: इसके अनुकूल ही आचरण करना। जो-जो नियम ईश्वर ने सृष्टि के लिए बनाए हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वैसा ही आचरण करना, यही सत्य है इसके विपरीत असत्य है ।
(७) सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो सदा रहेगी। क्योंकि सत्व, रज, तम परिवर्तनशील होने से इनसे बनी प्रत्येक वस्तु भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, अन्तत: समाप्त ही होगी ।
(८) सृष्टि की कोई भी वस्तु का सर्वदा अभाव नहीं होगा बल्कि वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी। परन्तु वही वस्तु एक बार समाप्त होने पर पुनः उन्हीं परमाणुओं से, वही वस्तु नहीं बन सकती ।
(९) जो-जो वस्तु अवयवों के संयोग से बनी है, तोड़ने से टूटती है और बनाने से बनती है, वह जड़ है।
(१०) कौन सा कार्य कब, कितना, किसलिए करना चाहिए, यह सब सत्यासत्य जानने के अन्तर्गत हैं। कर्मफल तक यह नियम लागू होगा कि इस अमुक कार्य को करने से क्या, कैसे अच्छा-बुरा फल मिलेगा, इसलिए कर्मफल का अनुमान करना चाहिए । जैसे उपासना काल में यदि उपासना के अतिरिक्त अन्य विचार करते हैं तो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे हिंसा होगी और ईश्वर के प्रति इस प्रकार के अनुचित व्यवहार से इसका भयानक दण्ड मिलेगा ।
३०. क्या सोचना, क्या विचारना, क्या देखना, क्या सुनना यह श्रवण- मनन-निदिध्यासन-साक्षात्कार तक इतना सत्यासत्य को जानने का क्षेत्र है। व्यर्थ न बोलना, न सुनना, न देखना। आवश्यक ही सब कार्य करना। अन्यथा जीवन नहीं सुधरेगा। योगी बनने की बात तो दूर, एक अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकते ।३
१. उपासना में मन को इधर-उधर विषयों में जहाँ भी ले जाते हैं, सर्वव्यापक होने से ईश्वर वहाँ है। परन्तु व्यक्ति को यह भ्रान्ति होती है कि मैं ईश्वर की सत्ता से बाहर हूँ; यह मिथ्या मानसिकता है। ईश्वर हर क्षण, सर्वत्र हमें देख, सुन, जान रहा है; इस प्रकार जानते हुए ही व्यक्ति को समर्पण करना चाहिए। परन्तु यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते, यह कारण है ।
३२. ईश्वरोपासना, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, आत्मनिरीक्षण आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें उत्साह बढ़ता ही जाता है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि पुराने अभ्यास के कारण संस्कार बाधित करते हैं और अच्छे संस्कार कम हैं। परन्तु क्लेशमुक्त होने के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ ही पड़ेगा। भोगेच्छा=एषणाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। अन्यथा या तो मृत्यु अथवा अन्य कोई वस्तु बलात् छुड़़वा देगी । जैसे सांख्य में कहा--श्येनवत् सुखदुःखी त्याग-वियोगाभ्याम् ॥ ४/५ ॥
१५. ये बातें सिद्धरूप में विद्यमान हों कि में जीव अणु हूँ। कर्म करने में स्वतन्त्र हूँ। यह शरीर कर्मफल है। मैं अनेक योनियों में जाता हूँ। अनादि हूँ। वर्तमान से ही भूत, भविष्य दोनों सिद्ध होते हैं। जेसे वर्तमान में हमने जन्म लिया है, ऐसे ही अनादि से अनन्त काल तक इसी प्रकार मरते-जन्मते रहेंगे। ये सिद्धान्त पाँच कसौटियों के द्वारा सिद्ध करके मन में अच्छी प्रकार से बिठा लेने चाहिए, कोई भी संशय न रहे, तब व्यक्ति इस जन्म-मरण के चक्र से छूटना चाहेगा और उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा ।
१६. सृष्टिक्रम अर्थात् जो वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होगी। जो वस्तु संयोग से बनी है उसका वियोग भी होगा। जिसका आदि है उसका अन्त भी है। इन्हीं के अनुकूल सत्पुरुषों के आचरण प्रमाण है। इनके विरुद्ध कोई भी प्रमाण - तर्क नहीं मिलेगा। जब उसकी आत्मा में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है तो अपनी गलत मान्यता को हटा देता है। क्योंकि वह सोचता है कि मैं तो अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् हूँ। मैं तो लाखों बार गलत सोचता हूँ, मानता हूं। उदाहरण-जैसे अनेक बार विषयों में दुख प्रत्यक्ष करके भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूं।
१७. हम कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, कुछ बुरे भी। उन सभी कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनका फल देनेवाला कोई नहीं है। भले ही हम बुरे कर्मों का फल नहीं चाहते किन्तु अच्छे कर्मों का फल अवश्य चाहते हैं। परन्तु अच्छे कर्म के साथ बुरे कर्म का भी फल अवश्य मिलेगा।
१८. हेय-हेयहेतु को जानकर छोड़ देना, हान- हानोपाय को जानकर ग्रहण करना सत्य है। किन्तु यह जानना बड़े पुरुषार्थ की बात है कि कौन सी वस्तु ग्राह्य और कौन सी अग्राह्य है। संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा जो योग = समाधि में बाधक तत्त्व है वह अग्राह्य है और साधक तत्त्व ग्राह्य है, जैसे ईश्वर ।
१९. काल और देश की दृष्टि से ईश्वर अनादि है, अनन्त है। वह हर क्षण प्रत्येक जीव के कर्मों को देखता, हिसाब रखता, कर्मों का फल देता है; यह बहुत गम्भीर सिद्धान्त है, इसे हर समय सामने रखें। जब व्यक्ति इसके विरुद्ध विचार उठाता है तो वह तर्क उठाता है कि ये जो लाखों प्रकार की योनियाँ हैं, लाखों जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं यह बिना ईश्वर के कैसे अपने आप हो रहा है?
इस प्रकार प्रश्नोत्तर प्रक्रिया द्वारा इस सिद्धान्त को मन, आत्मा में दृढ़ करना। इसके लिए चाहे अनेक वर्षों तक बार-बार अभ्यास निरन्तर दृढ़ता से करना पड़ेगा। जीव अल्पज्ञ होने से बास- बार अविद्या में गिरता है किन्तु ऐसा करने पर ही व्यक्ति योग-मार्ग पर टिक सकता है।
२०. तीनों कालों में जीव, मूलप्रकृति, कार्यजगत् ये व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है। यह विचार व्यवहारिकरूप में दिन भर मन मस्तिष्क में उपस्थित रखना चाहिए ।
- अनावश्यक और हानिकारक विचारों और पदार्थों का संग्रह न करना अपरिग्रह है। मन में काम, क्रोध, अविद्यादि क्लेशों को रखना परिग्रह है। इस प्रकार मन से अपरिग्रह का पालन करना अत्यन्त पुरुषार्थसाध्य है। हर समय ईश्वर को ही विषय बनाकर ग्रहण करके रखना और संसार को मन-वचन-कर्म से छोड़े रखना। यह अपरिग्रह का पालन है। जब व्यक्ति मन-वचन-कर्म से पूर्णरूपेण अपरिग्रह का पालन करता है तो उसे यह सूक्ष्म विद्या समझ में आती है अन्यथा तो व्यक्ति शाब्दिकरूप में ही जान पाता है ।
- जब व्यक्ति सभी वस्तुओं से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर का ही सब कुछ मानता है तो इन सूक्ष्म विषयों को जान पाता है। क्योंकि इन वस्तुओं पर अपना स्वामित्व रखना परिग्रह है। इस प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं से मन-वचन-कर्म से जब व्यक्ति अलग होकर विचारता है तो उसे सूक्ष्म विषय समझ में आते हैं। जैसे व्यक्ति मन को तो स्वयं चलाता है परन्तु मन के वशीभूत होकर विषयों की ओर आकर्षित होता हैं। जब व्यक्ति देखता है कि ये तो सभी जड़ - पदार्थ हैं, सब कुछ ईश्वर का ही है मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अपने सामर्थ्य से अपना ज्ञान भी नहीं कर सकता, विषयों को भोगना तो दूर की बात है। तब व्यक्ति का स्वस्वामि सम्बन्ध टूटता है और ईश्वर से सम्बन्ध जुड़ता है ।
- हम बहुत सी वस्तुओं को व्यवहार में केवल शब्दप्रमाण से जानते हैं और व्यवहार करते हैं और उस वस्तु की सत्ता भी मानते हैं। ऐसे ही ईश्वर के विषय में शाब्दिक प्रमाण वेद है, वेद स्वत: सिद्ध है क्योंकि वह ईश्वरकृत है और ईश्वर कभी असत्य नहीं कहता ।
- जो अपने साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, मित्र हैं यदि वे विपरीत व्यवहार करते हैं अथवा अनुकूल कार्य नहीं करते हैं तो मन में यह नहीं आना चाहिए कि यह क्यों नहीं करता, मैं तो करता हूँ, अथवा सामनेवाला अपने कार्य की ओर ध्यान क्यों नहीं देता?
- वैराग्य कोई बाहर से आनेवाली वस्तु नहीं है बल्कि अपने अन्दर ही है। केवल अपने ज्ञान की दिशा को मोड़ना है। उत्कृष्ट ज्ञान की उच्चता ही वैराग्य है ।
- पाँच परीक्षाओं के आधार पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, विकृति के स्वरूप को जानना कि जीव में न तो स्वयं का ज्ञान करने का सामर्थ्य है, न बल है, न स्वयं कोई क्रिया कर सकता है और प्रकृति-विकृति जड़़ है। उसमें कोई ज्ञान ही नहीं है कि कोई वस्तु कैसे बनती है जैसे तिल का दाना और ईश्वर जो जीवों को सामर्थ्य देता, साधन देता ताकि सारे व्यवहार सिद्ध कर सके और प्रकृति-विकृति को भी रूपान्तरित करके उसके गुण, सामर्थ्य को प्रकाशित करता है। इस प्रकार सब कुछ का देने वाला केवल ईश्वर ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति सोचता, विचारता, चिन्तन करता है। वह सारी वस्तुओंं का स्वामी ईश्वर को मानकर उसकी आज्ञानुसार ही उन का उपयोग करता है। यह ईश्वरसमर्पण=ईश्वरप्रणिधान है। यही ईश्वरसाक्षात्कार की विधि है जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता अथवा इस स्थिति को बनाकर छोड़ देता है वह अवश्य ही अविद्या अन्धकार में गिरता है। अनन्त अज्ञान, दु:खादि फलों को भोगता है। जो व्यक्ति इस विधि से करता है उसे ईश्वर संकल्प मात्र से अपना साक्षात्कार करवाता है और सुख देता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ईश्वर जिसको केवल संकल्प मात्र से साक्षात्कार करवाता है उसकी इतनी अधिक योग्यता होती है।
२२. किसी भी गुण की प्राप्ति और दोष की निवृत्ति के लिए विद्या, बुद्धि, दृढ -संकल्प शक्ति, अत्यन्त पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है ।
२३. आत्मा के अस्तित्व के लिए संसार की कोई भी वस्तु अत्यावश्यक नहीं है। ऐसी भावना वाला किसी पदार्थ में तृष्णा नहीं रखता। मिला तो ठीक है नहीं मिला तो भी ठीक है । यही गुण-वैतृष्ण्यम् है ।
२४. किसी पदार्थ में रुचि बनाने के लिए उस पदार्थ के गुणों और उनसे होनेवाले निज सम्बन्धित लाभ को जानना आवश्यक है तभी उस पदार्थ की अनिवार्यता समझ में आएगी, वह पदार्थ चाहे ईश्वर हो ।
२५. जहाँ-जहाँ वस्तु क्रिया करेगी वहाँ-वहाँ उसके गुण प्रकट होंगे ।
२६. वस्तु की सदा वर्त्तमानता में प्रमाण-अभाव से भाव, भाव से अभाव नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान जीव की सत्ता सदा रहती है, केवल अनेक योनियों के शरीरों से जीव का संयोग- वियोग होता रहता है ।
२७. कोई वस्तु अपने आप बनी है यह कथन ही गलत है क्योंकि विद्यमान से ही कर्म आरम्भ होता है और बनी हुई वस्तु बनने के पश्चात विद्यमान हो सकती है व्योंकि बनने के पूर्व वह नहीं होती है। अब यदि कहो वस्तु विद्यमान थी तो उसके बनने का कोई अर्थ नहीं, वह तो है ही। यदि कहो वस्तु विद्यमान नहीं थी तो बनना कर्म आरम्भ कैसे हुआ? इसलिए कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती अपितु अपने से भिन्न कर्ता द्वारा बनाई जाती है। जैसे कहा जाए कि पृथिवी अपने आप बन गई है, तो जिस को पृथिवी कह रहे हैं अपने आप बनी है वह तो बनने के पहले से ही है, अब बनेगी क्यों? यदि पृथिवी पहले स्वयं नहीं थी तो किससे बनी?
२८. अपनी आत्मा को अच्छा लगना अन्तिम कसौटी नहीं है क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ होने से त्रुटियाँ कर सकता है, जब आत्मा सत्य, विद्या के अनुकूल आचरण करता है अर्थात् शब्दादि प्रमाणों के अनुकूल चलता है तो ठीक विचार करता है। जब व्यक्ति पाँच कसौटियों के आधार पर ही किसी बात को जानना चाहता है तब सत्य को प्राप्त करता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं । यदि केवल अपनी आत्मा ही की मानेंगे तो ईश्वर हाथ में नहीं आएगा। जब भी शब्दप्रमाण, ईश्वर, महापुरुष आदि के विरुद्धआचरण हो तो उस समय स्वयं को झूठा और उन प्रमाणों को ठीक मानना, तब तो ईश्वर, आध्यात्मिक विषय आदि की बात मन में बैठेगी, अन्यथा नहीं।
२९. सत्य और असत्य का निश्चय करने की कसौटियाँ -
(१) ईश्वर-ईश्वर के जो गुण=न्याय, कर्म=पक्षपातराहित्य, स्वभाव सत्य, न्याय, दया, परोपकारिता, निष्कामता हैं, इनके अनुकूल जो-जो आचरण है, वह सत्य है।
(२) जैसे बिना कारण और कर्त्ता के कोई कार्य नहीं होता। किसी कार्य के कम से कम तीन कारण अवश्य होते हैं। और कम से कम तीन वस्तुएँ होनी आवश्यक है। कारण-साधारण कारण, कर्ता-निमित्त कारण, उपादान -जो कार्य की मूल सामग्री है। ईश्वर- जीव - प्रकृति में ये तीनों कारण न होने से ये कार्य वस्तु नहीं हैं अर्थात् अनादि अनन्त हैं। इस परीक्षा के जो-जो अनुकूल है वह सत्य है।
(३) ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव या तो वेद से जाने जाते हैं या फिर सृष्टिक्रम को देखकर इससे, ईश्वर का कर्त्तापन, गुण, कर्म स्वभाव देखे-जाने जाते हैं।
(४) सृष्टि और सृष्टि के पदार्थों से ऐसा निश्चित करना कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी है। वह हर समय हमें देख, सुन, जान रहा है। मन-वचन-कर्म से किया गया कोई भी कार्य उससे छुप नहीं सकता। वह हमें न्यायानुसार हमारे कर्मों का फल देगा। क्योंकि ऐसा अन्य कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो हमें और हमारे कर्मों को पूर्ण रूपेण जान सके और ठीक-ठीक न्यायानुसार फल भी दे सके। केवल ईश्वर ही ऐसा है यह निश्चित करने पर व्यक्ति सारे कर्तव्य कर्मों को ईश्वराज्ञानुसार और ईश्वर को ही समर्पण करके उसके गुण-कर्म - स्वभाव के अनुकूल ही करता है। उसे कोई भी लौकिक इच्छा नहीं रहती क्योंकि कोई भी लौकिक पदार्थ कर्मों का फल देने में न तो समर्थ है न ही ऐसी योग्यता है। वह पूर्ण निष्कामता से कार्य करता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है ।
(५) जहाँ-जहाँ कार्य दिखता है वहाँ वहाँ कर्ता भी होता है। ईश्वर आँखों से तो प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु सृष्टि में जो उसके गुण-कर्म-स्वभाव प्रत्यक्ष होते हैं उसी से ईश्वर का निश्चय होता है ।
(६) सृष्टिक्रम-सृष्टि का यह नियम है कि जो उत्पन्न होता है वह समाप्त भी होता है क्योंकि वह संयोगजन्य है। जिसमें संयोग होता है उसमें वियोग भी निश्चित होगा। अत: जन्म- मृत्यु, दुःख सुख ये सृष्टि में अनिवार्य हैं। ऐसा ही जानना, मानना सत्य है। ऐसा जानना, मानना कि सृष्टि जड़ है, ईश्वर ने इसे बनाया है । हमे यह केवल धर्म- अर्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि हेतु उपयोग करने के लिए दी है अत: इसके अनुकूल ही आचरण करना। जो-जो नियम ईश्वर ने सृष्टि के लिए बनाए हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए वैसा ही आचरण करना, यही सत्य है इसके विपरीत असत्य है ।
(७) सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो सदा रहेगी। क्योंकि सत्व, रज, तम परिवर्तनशील होने से इनसे बनी प्रत्येक वस्तु भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, अन्तत: समाप्त ही होगी ।
(८) सृष्टि की कोई भी वस्तु का सर्वदा अभाव नहीं होगा बल्कि वह अपनी सूक्ष्म अवस्था में चली जाएगी। परन्तु वही वस्तु एक बार समाप्त होने पर पुनः उन्हीं परमाणुओं से, वही वस्तु नहीं बन सकती ।
(९) जो-जो वस्तु अवयवों के संयोग से बनी है, तोड़ने से टूटती है और बनाने से बनती है, वह जड़ है।
(१०) कौन सा कार्य कब, कितना, किसलिए करना चाहिए, यह सब सत्यासत्य जानने के अन्तर्गत हैं। कर्मफल तक यह नियम लागू होगा कि इस अमुक कार्य को करने से क्या, कैसे अच्छा-बुरा फल मिलेगा, इसलिए कर्मफल का अनुमान करना चाहिए । जैसे उपासना काल में यदि उपासना के अतिरिक्त अन्य विचार करते हैं तो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इससे हिंसा होगी और ईश्वर के प्रति इस प्रकार के अनुचित व्यवहार से इसका भयानक दण्ड मिलेगा ।
३०. क्या सोचना, क्या विचारना, क्या देखना, क्या सुनना यह श्रवण- मनन-निदिध्यासन-साक्षात्कार तक इतना सत्यासत्य को जानने का क्षेत्र है। व्यर्थ न बोलना, न सुनना, न देखना। आवश्यक ही सब कार्य करना। अन्यथा जीवन नहीं सुधरेगा। योगी बनने की बात तो दूर, एक अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकते ।३
१. उपासना में मन को इधर-उधर विषयों में जहाँ भी ले जाते हैं, सर्वव्यापक होने से ईश्वर वहाँ है। परन्तु व्यक्ति को यह भ्रान्ति होती है कि मैं ईश्वर की सत्ता से बाहर हूँ; यह मिथ्या मानसिकता है। ईश्वर हर क्षण, सर्वत्र हमें देख, सुन, जान रहा है; इस प्रकार जानते हुए ही व्यक्ति को समर्पण करना चाहिए। परन्तु यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहते, यह कारण है ।
३२. ईश्वरोपासना, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, आत्मनिरीक्षण आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें उत्साह बढ़ता ही जाता है। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि पुराने अभ्यास के कारण संस्कार बाधित करते हैं और अच्छे संस्कार कम हैं। परन्तु क्लेशमुक्त होने के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ ही पड़ेगा। भोगेच्छा=एषणाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। अन्यथा या तो मृत्यु अथवा अन्य कोई वस्तु बलात् छुड़़वा देगी । जैसे सांख्य में कहा--श्येनवत् सुखदुःखी त्याग-वियोगाभ्याम् ॥ ४/५ ॥
३३. उपस्थित को छोड़ना, अनुपस्थित को पकड़ना इस न्याय के अनुसार जो ईश्वर सदा हमारे पास है, उसे तो छोड़ देते हैं, व्यर्थ लौकिक वस्तुओं, विचारों में लगे रहते हैं। ऐसे ही सभी जगह समझना चाहिए, जहाँ-जहाँ हम उत्कृष्ट वस्तु को छोड़ देते हैं और गौण=निकृष्ट को ग्रहण करते हैं। यह हमारी अज्ञानता है ।
३४. क्या कोई ऐसा साधन=उपाय है कि जिससे शरीर सदा जीवित रहे? आज कोई है जिसका शरीर सदियों से चला आ रहा है, कोई नहीं। यदि सूक्ष्मता से देखें तो पता चलेगा कि हम नहीं जानते हैं कि अगले क्षण हम जीवित रहेंगे। पता नहीं किस घटना से यह शरीर चला जाए, यदि इस प्रकार से न भी जाए तो भी स्वाभाविक मृत्यु तो निश्चित ही है। इसी प्रकार सारे शरीर मरेंगे। वर्तमान में जो व्यवहार हो रहा है वह शरीर ही के कारण है। शरीर ही नहीं रहेगा तो ये राग-द्वेष भी नहीं रहेंगे। तो जब कोई रहेगा ही नहीं तो क्या राग-द्वेष करना। सामनेवाला अपनी तरह ही आत्मा है। आत्मरूप में तो हम एक दूसरे को जान भी नहीं सकते। जब सभी ईश्वर के पुत्र हैं तो शरीर की दृष्टि से सभी-भाई-भाई भी हैं। ईश्वर की आज्ञानुसार उसे अपनी आत्मा के तुल्य मानना पड़ेगा अन्यथा राग द्वेष होगा और मुक्ति भी नहीं होगी ।
३५. प्राय: व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य करूँ, सभी लोगों, समाज, देश, विश्व में मेरी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान हो। परन्तु वह यह नहीं सोचता कि क्या लोग उसके कार्य के अनुसार उसे पूरा-पूरा सम्मान दे सकते हैं? इतना ही नहीं वे तो उस कार्य को पूरा जान भी नहीं सकते। फिर क्यों उनके पीछे भागना ? परन्तु ईश्वर तो सब कुछ जानता है, प्रत्येक कर्म का न्यायानुसार ठीक-ठीक फल देता है इसलिए उसको ही समर्पण करना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं ।
३६. उपासना काल में यह नियम बना लेना चाहिए किपहला - अब में ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय का चिन्तन नहीं करूँगा, यदि कोई अति आवश्यक कार्य आ जाए तो उसे निपटाकर पुन: उपासना करें परन्तु अब वह विषय न हो केवल ईश्वर ही हो ।दूसरा - मन को जड़ मानकर अपनी इच्छानुसार ही चलाना है ऐसा उसके मन में दृढ़ निश्चय हो ।तीसरा - व्यक्ति प्रायः लौकिक विषयों में सुख और ईश्वर में दु:ख मानता है । जब उसे पता चलता है कि ईश्वर में तो अनन्त सुख है और लौकिक सुख दुःखमिश्रित है तो वह लौकिक सुख को छोड़कर ईश्वर की इच्छा करता हुआ उपासना करता है । अत: ऐसा ही करूँगा।
३७. जब तक संसार अनित्य दिखेगा तब तक ईश्वर विषय बना रहेगा लौकिक पदार्थ विषय नहीं बनेगा। जब संसार आलम्बन बन गया तो ईश्वर छूट जाएगा। अर्थात् जब तक संसार में कोई प्रयोजन शेष है तब तक संसार नित्य दिखेगा और आलम्बन बना रहेगा। प्रयोजन के अभाव से उसका आलम्बन भी नहीं रहेगा। संसार के किसी भी पदार्थ की यदि इच्छा है तो ईश्वर आलम्बन का विषय नहीं बनेगा ।
३८. ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि हैं यह बात बुद्धि में बैठे बिना व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। लाखों भौतिक वैज्ञानिक जितना भी प्रयत्न करें परन्तु बिना वेद, दर्शन, उपनिषद् के इन तीनों को ठीक प्रकार से नहीं जान सकते, न ही इनका ठीक उपयोग कर सकते। बुद्धि में बैठाने के उपाय--पहला - यह निर्णय करना कि ये तीनों अनादि हैं।दूसरा - यह निर्णय करना कि तीनों को अनादि जानकर ही व्यक्ति की उन्नति होती है ।तीसरा - उसमें जो संशय, भ्रान्ति हो उनको दूर करना ।चौथा - तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव का निश्चित ज्ञान करना वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना, मानना ।पाँचवा - इस निश्चित ज्ञान को स्थिर बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना।
३९. ईश्वर कैसी विचित्र वस्तु है जो न हिलती-डुलती है लेकिन प्रकृति के परमाणुओं को किस क्रम से जोड़कर कौन से पदार्थ बनाने हैं, उनको किस स्थान पर व्यवस्थित रखना है, जीवों को गति देना आदि ये सभी कार्य करती है। ईश्वर के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिना हिले डुले कोई कार्य कर सके। अन्य वस्तुओं का हिलने-डुलने का सामर्थ्य भी ईश्वरप्रदत्त है। उस सामर्थ्य के बिना तो वे पदार्थ निष्क्रिय हैं ।
(१) ईश्वर है या नहीं, उसके होने की क्या आवश्यकता है ?
(२) यदि ईश्वर है तो कैसा है ?
(३) उसकी प्राप्ति से क्या होता है ?
(४) उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं ?(५) उसकी प्राप्ति में बाधक क्या हैं ?ये सभी विषय अत्यन्त पुरुषार्थ से निश्चित सिद्ध होते हैं और निश्चित ज्ञान न होने पर प्राय: एक बड़ी समस्या बन जाती है।४०. व्यक्ति अपने विचारों और संस्कारों के आधार पर ही खड़ा हैै। यदि अत्यन्त पुरुषार्थ करे तो इन विचारों, संस्कारों में परिवर्तन करके उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता है।
४१. ईश्वर न्यायकारी है। ऐसे किसी एक गुण को यदि व्यक्ति व्यवहारिक रूप में जान लेता है तो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता है। ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप-विभिन्न योनियों का निर्माण, सुख-दुःख में भिन्नता आदि के द्वारा देखा जा सकता है ।
४२. ईश्वर और जीव के छः सम्बन्ध हैं - १.पिता-पुत्र, २.माता-पुत्र, ३. गुरु-शिष्य, ४. उपास्य-उपासक, ५. राजा - प्रजा, ६. व्यापक-व्याप्य। जो व्यक्ति इन छः सम्बन्धों को अपने जीवन में क्रियात्मकरूप में लाता है, वह जीवन में उन्नति करता और योगी बनता है। ये सम्बन्ध स्वयं ईश्वर ने बनाए हैं, मनुष्य ने नहीं । ये सम्बन्ध तीनों कालों में रहते हैं। न इनका कोई प्रारम्भ न अन्त। जब व्यक्ति इस प्रकार से जानता है तो मान-अपमान, हानि-लाभ से व्यथित नहीं होता है। सभी को अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। क्योंकि ईश्वर के साथ हमारे इन सम्बन्धों के कारण हम सब भाई-भाई हैं ।
४३. व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध तीनों कालों में रहता है; ऐसा विचारता हुआ व्यक्ति सभी के साथ उचित व्यवहार करता है। वह सभी को लौकिक दृष्टि से माता-पिता, भाई- बहन के समान देखता है। वह सभी में ईश्वर और सभी को ईश्वर का ही मानता है। वह देखता है कि मुझमें, सामनेवाले में, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी ईश्वर है, हर क्षण देख-सुन जान रहा कैसी गम्भीर अवस्था है! कितना गम्भीर विषय है! इस प्रकार जानता हुआ व्यक्ति कभी पाप नहीं करता है अपितु वह स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देता है।४४. व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध तीनों कालों में रहता है चाहे सृष्टि हो अथवा प्रलय। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो तीनों कालों में ईश्वर से बाहर जा सके और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो इतना सूक्ष्म स्थान बना सके कि जहाँ ईश्वर न जा सके । कैसी विचित्र अवस्था है?
४५. जैसे हम लोक में माता-पिता से प्रत्यक्ष बात करते हैं ऐसे ही ईश्वर को सम्बोधन करना कि आप ही मेरे नित्य माता-पिता हैं। लौकिक सम्बन्ध तो अनित्य हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति के व्यवहार में यह विषय क्रियान्वित हो जाता है तब वह ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता है अन्यथा शाब्दिक रूप में ही जानता हैैं।
४६. जब तक अपने साथ रहने वाले व्यक्ति, मित्र आदि के लिए अपनी आत्मा के समान सुख की इच्छा और दुःख से द्वेष करते हैं, नहीं चाहते, तब तक यम नियमों का पालन तथा उचित व्यवहार नहीं कर सकते । आर्य समाज का सातवाँ नियम "सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्त्तना चाहिए" यही कहता है । ऐसा करने से ही सर्वागीण उन्नति हो सकती है।
४७. जब तक व्यक्ति को व्यवहार में शतप्रतिशत यह समझ में नहीं आता कि ईश्वर हमारे मन-वचन-कर्म से होने वाले प्रत्येक कर्मों को जान रहा है और न्यायानुसार उनका फल भी देगा, तब तक व्यक्ति ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव, वेद विद्या को नहीं समझ सकता ।४८. अभी जो आप दोष कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि एक तो आप ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ न्यायकारी नहीं मानते और दूसरा अपने दोषों को अच्छा मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जब तक दोष वास्तविकरूप में समझ नहीं आएँगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी।
४९. गुणों को ग्रहण करने में अत्यन्त पुरुषार्थ, तप, त्याग करना पड़ता है, इसलिए अपुरुषार्थी गुणों को ग्रहण नहीं करते ।
५०. प्रश्न ➧ ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अनादि क्यों है ?
उत्तर ➨ तीनों के गुण स्वाभाविक होने से अर्थात् इनके तीन कारण -उपादान, साधारण और निमित्त कारण न होने से। जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण नहीं होते हैं वह वस्तु अनादि होती है । ऐसे ही जिसके विनाश के तीन कारण नहीं हैं वह अनन्त होती है । जब व्यक्ति इन तीनों के स्वरूप को ठीक-ठीक जान लेता है तब वह इन तीनों के साथ उचित व्यवहार करता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों काल की दृष्टि से अनादि अनन्त हें, यह बड़ा गम्भीर सिद्धान्त है। बड़े-बड़े विद्वान् भी इसको समझ नहीं पाते ।
५१. वर्तमान में जो भोगविषयों, जड़ पदार्थों में आकर्षण इसलिए है कि अभी यह समझ में नहीं आया है कि वे पदार्थ मेरे आत्मा के गुण-कर्म-स्वभाव से विरुद्ध हैं ।
५२. किसी पदार्थ में आकर्षण तब हटता है जब उसके दोष दिखते हैं। जैसे इन जड़ पदार्थों तथा अन्य चेतन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है वह अविद्या है। इनको ग्रहण करना अपरिग्रह का पालन नहीं करना है ।
५३. किसी वस्तु में आकर्षण तब होता है जब उस पदार्थ के गुण प्रत्यक्ष हो । इस प्रकार सभी पदार्थों में जानना चाहिए।५४. पूर्ण रूप से मन-वचन-कर्म से प्रतिबन्ध लगा देना कि एक भी कार्य बिना पाँच कसौटियों पर परीक्षा किए नहीं करूँगा तब जाकर व्यक्ति गुणों को ग्रहण और दोषों को छोड़ सकता है ।
५५. जब व्यक्ति ईश्वर-प्रणिधान सतत बनाए रखता है अर्थात् सर्वज्ञ,सर्वव्यापक न्यायाकारी ईश्वर सतत मेरे मन-वचन-कर्म से किए जाने वालेप्रत्येक अच्छे-बुरे कमों को देख रहा है तथा सारे कर्म उसको समर्पित करता है तब जाकर व्यक्ति पाप कर्म से बच सकता है अन्यथा प्रायः पाप कर्म कर ही डालता है। क्योंकि जीवात्मा या तो अच्छा कार्य करेगा या फिर बुरा कार्य करेगा।
व्यवहार
१. अच्छा व्यवहार अर्थात् मन से अच्छा सोचना, विचारना, वाणी से मीठा, शुद्ध, प्रिय, सत्य, कोमल बोलना, शुद्ध निष्काम कर्म - ये सब इसलिए करना कि लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मान-सम्मान होगा; ऐसी भावना योग में बाधक है। बल्कि इसलिए करना कि यह हमारा धर्म है, कर्तव्य है, ईश्वर का आदेश है, तभी जीवन की सफलता है।
२. बिना अभ्यास के कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस विषय के संस्कार कम होते हैं अथवा नहीं होते। इसलिए सत्य-व्यवहार सीखना हो तो बड़े पुरुषार्थ, तप, श्रद्धापूर्वक उसका अभ्यास करो। इससे उस विषय के संस्कार बनेंगे पुन: यह व्यवहार जीवन का एक अंग बन जाएगा। ऐसे ही सभी कार्यों में समझना चाहिए ।
३. अपने अधीन, आश्रित अथवा किसी की स्वतन्त्रता को भंग करके आग्रहपूर्वक अपनी बात मनवाने की मन से भी चेष्टा करना आत्मतुल्य व्यवहार नहीं है जैसे हम अपनी स्वतन्त्रता भंग नहीं करना चाहते ।
४. आवश्यक विचारना, बोलना, देखना, सुनना आदि सभी व्यवहार योगपथ पर आगे बढ़ाने में सहायक हैं ।
५. इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पुराने व्यक्तित्व, पुराने विचार, मान्यताएँ, संस्कार को मारकर नया जन्म लेना पड़ता है। सभी लौकिक, व्यापारिक वृत्तियों को छोड़ना पड़ता है। जैसे बालक के नए-नए संस्कार बनते हैं वैसे हमें भी नए आध्यात्मिक संस्कार बनाने पड़ते है । एक नए बालक की भाँति मन- मस्तिष्क में तीव्र अनुकरण की शक्ति और वैसा ही शुद्ध मन-मस्तिष्क हो । पुराना व्यवहार, भाषा, मानसिकता को मार देना पड़ता कि ऐसा व्यवहार नहीं करुँगा अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकता। पहले इतनी पात्रता बनानी है फिर योग-विद्या आएगी ।
६. व्यवहार, धर्म, योगाभ्यास की बात पर अधिकाधिक समय लगाओ, इधर-उधर की बातें मत करो, अन्यथा मुख्य बात रह जाएगी और व्यर्थ की बातों में रुचि बढ़ जाएगी ।
७. व्यक्ति प्रायः सामने वाले को अपने ही मापदणंड से तोलता है, अपने दृष्टिकोण से उसके विषय में विचारता है। अपनी इस सीमित दृष्टि के कारण सामने वाले से प्राय: दुर्व्यवहार कर बैठता है परन्तु जब समग्र दृष्टिकोण को लेकर सोचता-विचारता है तो सामने वाले के साथ उचित व्यवहार कर पाता है ।
८. ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे लगे कि इस कार्य का पता किसी को चल गया तो क्या होगा? अर्थात् मन में इस प्रकार भय, शंका, लज्जा होती हो तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यद्यपि अपनी आत्मा का कुछ नहीं नष्ट होगा पुनरपि अपनी आत्मा की पवित्रता के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए ।
९. जब तक मन में यह मानकर बैठे हैं कि में बहुत कुछ जानता हूँ तब तक दोष दूर नहीं होंगे। जब तक विरोधी तत्त्व को नहीं जानेंगे तब तक सत्य हाथ में नहीं आएगा और जब तक झूठ और झूठ से होनेवाली हानियों को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जान सकते ।
१०. में कार्य बहुत कम करू और अन्य करते रहें, यह बिगड़ने की स्थिति है और भले ही अन्य कार्य करें या न करें मैं तो करुँगा, यह निर्माण की स्थिति है ।
११. जो ऊँचे विवेक-वैराग्यवाला है, वह स्वयं अपना सुख त्याग करके अन्यों को सुख देता है। क्योंकि इससे जो उपलब्धि होती है वह उस वस्तु से मिलनेवाली उपलब्धि से बड़ी है। बड़ी उपलब्धि को छोड़कर छोटी को पकड़ना मनुष्यता नहीं है ।
१२. उत्तरदायित्व का निभाना, मानव निर्माण का एक मुख्य साधन है ।
१३. सोचो-विचारो कि जो कार्य कर रहें हैं वह कैसे सुन्दर, कम समय में, कम व्यय में हो सकता है। कार्य को करते समय आदि से अन्त तक उसके विषय में विचारो कि इससे क्या-क्या लाभ और हानियाँ हो सकती हैं ।
१४. जो कार्य जिस क्रम से होता है उसको उसी क्रम से करना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता है। ईश्वर प्राप्ति से पहले विवेक-वैराग्य, सावधानी, सतर्कता, गम्भीरता होना क्रम है। मीमांसा के ५वें अध्याय इसकी चर्चा आई है।
१५. जो व्यक्ति वृद्धों, विद्वानों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश, बल ये चारों बढ़ते हैं क्योंकि विद्वान् लोग उसे चलते-फिरते, उठते-बैठते सब प्रकार के व्यवहार सिखलाते हैं। जो सेवा नहीं करता है उसके इन चारों का नाश होता है । व्यक्ति जब जिज्ञासु हो तभी सिखाने वाले से अथवा ऋषिकृत-ग्रन्थों से सीख सकता है ।
१६. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्यासत्य को विचार करके करने चाहिए अर्थात् क्या सत्य है, क्या झूठ है यह सभी कार्यों में देखना चाहिए ।
१७. व्यवहार में यदि मन-इन्द्रियों पर संयम नहीं करते, नियन्त्रण नहीं करते तो यह असत्य व्यवहार होने से इसका दण्ड मिलेगा ।
१८. दूसरे से व्यवहार करते समय सामने वाले को अपनी आत्मा के तुल्य मानना और हम सब ईश्वर की सन्तान हैं, ऐसी भावना रखकर ही व्यक्ति उचित व्यवहार कर सकता है। अन्यथा उसका योगाभ्यास तो व्यर्थ हो जाएगा।
१९. सामने वाला तो हठता करेगा, नहीं मानेगा, यह तो उसका व्यवहार है किन्तु उसके व्यवहार के कारण अपने व्यवहार को नहीं बिगाड़ना और उसको भी अपना मानकर सिखाना है ।
२०. सामनेवाला विपरीत व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा उल्टा व्यवहार करता है, तब भी मन में उसके प्रति मित्रता का भाव रखना। यह अहिंसा का पालन है, यही धर्म है।
२१. मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में उपेक्षा का अर्थ यह नहीं है कि उस अमुक व्यक्ति से, जो विपरीत व्यवहार करता है, उससे अप्रीति करना, उसकी अवनति चाहना बल्कि उससे भी प्रीति करना, उसकी उन्नति की भी कामना करना ।
२२. यदि सामनेवाला अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाता तो ऐसा नहीं करना कि यदि वह नहीं करता है तो उसका कार्य में कर देता ह। मन में भी नहीं मानना कि यह अच्छा व्यक्ति नहीं है क्योंकि इसके व्यवहार से अन्यों को कष्ट होता है। ऐसा करते-मानते हुए हम उसके प्रति न्याय=अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। अत: वहाँ उसके कर्तव्य से उसे अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। अवगत करवाते समय उसके प्रति हित की भावना, भाषा मधुर, सरल हो। उसको कर्तव्य न करने से हानियाँ और करने का लाभ, कर्तव्य का निर्वहन कैसे करें, आदि बताएँ। कैसे समय का सदुपयोग करके कार्य को किया जाए, यही आदर्श व्यवहार है ।
२३. व्यक्ति अपने और अपने से सम्बद्ध व्यक्ति का मानसिक, वाचनिक और शारीरिक व्यवहारों से जीवन सुधारता और बिगाड़ता है; इस विषय में अपना आत्मनिरीक्षण करते रहें। इसमें एक भाग यह है कि जैसे अपने लिए सुख और सुख-साधन चाहते हैं तथा दुःख और दुःख के साधन हेय मानते हैं वैसा ही अन्यों के लिए चाहें । यह भाग अपने और अपने से सम्बद्ध व्यक्ति के साथ मानसिक - वाचनिक व्यवहारों को उचित बनाता है।
२४. जो व्यक्ति बार-बार बताने समझाने पर भी वैसे नहीं मानता न करता है उसको ऋषि ने शूद्र कहा है। बतानेवाला ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा करने लगता है। वहाँ यदि सुननेवाला यह नहीं सोचता कि बास-बार बताए जाने पर भी यदि मैं वैसा नहीं करुँगा तो बताने वाला बताना ही छोड़ देगा, तब वह व्यक्ति नहीं जानता कि निर्माण कार्य कैसे होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, लगन से सुनता, मानता, करता है वही निर्माण कार्य जानता है और बतानेवाला भी उसे उतनी ही लगन से बताता है, सिखाता है ।
२५. अपने आचार्य के भी गुणों को ही ग्रहण करने चाहिए और दोषों को छोड़ देने चाहिए। क्योंकि आचार्य भी जीवात्मा होने से अल्पज्ञ है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी सर्वगुण सम्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य में भी दोष तो होंगे ही, परन्तु उन दोषों को जानकर उनको छोड़ना ही बुद्धिमत्ता है।
२६. गुरुजनों के जो दोष दिखाई देते हैं उसके विषय में या तो उनसे शंका के रूप में पूछो कि मुझे ये दोष लगते हैं? यदि दोष होगा तो हटाया जाएगा अथवा यदि दोष नहीं है तो समझा दिया जाएगा । मन में क्षोभ नहीं रखना चाहिए, इससे राग-द्वेष पैदा होगा। दोष बताने का यह भी अर्थ नहीं है कि थोड़ी सी गलती हुई तुरन्त बता दिया, यह भी अच्छा नहीं है। कुछ सीमा तक सहन भी करना है । परन्तु जहाँ सामाजिक हानि होती हो, वहाँ कोमल भाषा में बताना चाहिए । बोलते समय भाषा मधुर, कोमल शब्द, दूसरे को ऐसा लगे कि ये मेरा हितैषी है, शब्दों में जितना समय लगाना चाहिए, उतना लगाना, धीरे-धीरे स्पष्ट बोलना; यह उत्तम भाषा व्यवहार है, इसी से यमनियमों का पालन होता है।
२७. जैसा बाहर व्यवहार है वैसा ही मन में भी होना चाहिए। जैसे बाहर से सत्य बोल तो रहे हैं परन्तु मन में दोष दिखाने, अपमानित करने, नीचा दिखाने अथवा डॉट लगवाने की भावना हो तो यमनियमों का पालन नहीं होगा।
२८. जो गुरुजी, वेद, ऋषि कहते हैं एक व्यक्ति वैसा हटाया जाएगा अथवा यदि दोष नहीं है तो समझा दिया जाएगा। मन में क्षोभ नहीं रखना चाहिए, इससे राग-द्वेष पैदा होगा। दोष बताने का यह भी अर्थ नहीं है कि थोड़ी सी गलती हुई तुरन्त बता दिया, यह भी अच्छा नहीं है। कुछ सीमा तक सहन भी करना है। परन्तु जहाँ सामाजिक हानि होती हो, वहाँ कोमल भाषा में बताना चाहिए। बोलते समय भाषा मधुर, कोमल शब्द, दूसरे को ऐसा लगे कि ये मेरा हितैषी है, शब्दों में जितना समय लगाना चाहिए, उतना लगाना, धीरे-धीरे स्पष्ट बोलना; यह उत्तम भाषा व्यवहार है, इसी से यमनियमों का पालन होता है।
२७. जैसा बाहर व्यवहार है वैसा ही मन में भी होना चाहिए। जैसे बाहर से सत्य बोल तो रहे हैं परन्तु मन में दोष दिखाने, अपमानित करने, नीचा दिखाने अथवा डॉट लगवाने की भावना हो तो यमनियमों का पालन नहीं होगा।
२८. जो गुरुजी, वेद, ऋषि कहते हैं एक व्यक्ति वैसा ही मान लेता, दूसरा जो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है; इनमें से प्रथम व्यक्ति ही सत्य जान पाता है।
२९. आन्तरिक शुद्धता तथा पवित्रता की अपेक्षा बाह्य शुद्धता तथा पवित्रता का अधिक ध्यान रखना, विषयों में आसक्ति, भोग-प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, यह योग में बाधक है।
३०. यदि कोई अपने संस्कारों के कारण अच्छा जानता हुआ भी बुरे कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह दु:खरूप फल से नहीं बच सकता। क्योंकि पाप का फल दु:ख ही होता है। जो विद्या के प्रकाश में अच्छा जानकर नहीं करता, बुरा जानकर नहीं छोड़ता, वह चोर के समान है जैसे चोर चोरी को बुरा जानता हुआ भी नहीं छोड़ता।
२६. गुरुजनों के जो दोष दिखाई देते हैं उसके विषय में या तो उनसे शंका के रूप में पूछो कि मुझे ये दोष लगते हैं? यदि दोष होगा तो हटाया जाएगा अथवा यदि दोष नहीं है तो समझा दिया जाएगा । मन में क्षोभ नहीं रखना चाहिए, इससे राग-द्वेष पैदा होगा। दोष बताने का यह भी अर्थ नहीं है कि थोड़ी सी गलती हुई तुरन्त बता दिया, यह भी अच्छा नहीं है। कुछ सीमा तक सहन भी करना है । परन्तु जहाँ सामाजिक हानि होती हो, वहाँ कोमल भाषा में बताना चाहिए । बोलते समय भाषा मधुर, कोमल शब्द, दूसरे को ऐसा लगे कि ये मेरा हितैषी है, शब्दों में जितना समय लगाना चाहिए, उतना लगाना, धीरे-धीरे स्पष्ट बोलना; यह उत्तम भाषा व्यवहार है, इसी से यमनियमों का पालन होता है।
२७. जैसा बाहर व्यवहार है वैसा ही मन में भी होना चाहिए। जैसे बाहर से सत्य बोल तो रहे हैं परन्तु मन में दोष दिखाने, अपमानित करने, नीचा दिखाने अथवा डॉट लगवाने की भावना हो तो यमनियमों का पालन नहीं होगा।
२८. जो गुरुजी, वेद, ऋषि कहते हैं एक व्यक्ति वैसा हटाया जाएगा अथवा यदि दोष नहीं है तो समझा दिया जाएगा। मन में क्षोभ नहीं रखना चाहिए, इससे राग-द्वेष पैदा होगा। दोष बताने का यह भी अर्थ नहीं है कि थोड़ी सी गलती हुई तुरन्त बता दिया, यह भी अच्छा नहीं है। कुछ सीमा तक सहन भी करना है। परन्तु जहाँ सामाजिक हानि होती हो, वहाँ कोमल भाषा में बताना चाहिए। बोलते समय भाषा मधुर, कोमल शब्द, दूसरे को ऐसा लगे कि ये मेरा हितैषी है, शब्दों में जितना समय लगाना चाहिए, उतना लगाना, धीरे-धीरे स्पष्ट बोलना; यह उत्तम भाषा व्यवहार है, इसी से यमनियमों का पालन होता है।
२७. जैसा बाहर व्यवहार है वैसा ही मन में भी होना चाहिए। जैसे बाहर से सत्य बोल तो रहे हैं परन्तु मन में दोष दिखाने, अपमानित करने, नीचा दिखाने अथवा डॉट लगवाने की भावना हो तो यमनियमों का पालन नहीं होगा।
२८. जो गुरुजी, वेद, ऋषि कहते हैं एक व्यक्ति वैसा ही मान लेता, दूसरा जो केवल अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है; इनमें से प्रथम व्यक्ति ही सत्य जान पाता है।
२९. आन्तरिक शुद्धता तथा पवित्रता की अपेक्षा बाह्य शुद्धता तथा पवित्रता का अधिक ध्यान रखना, विषयों में आसक्ति, भोग-प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, यह योग में बाधक है।
३०. यदि कोई अपने संस्कारों के कारण अच्छा जानता हुआ भी बुरे कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह दु:खरूप फल से नहीं बच सकता। क्योंकि पाप का फल दु:ख ही होता है। जो विद्या के प्रकाश में अच्छा जानकर नहीं करता, बुरा जानकर नहीं छोड़ता, वह चोर के समान है जैसे चोर चोरी को बुरा जानता हुआ भी नहीं छोड़ता।
३१. जैसे गाय अपने नए जन्मे बछड़े को अपनी प्राणों से भी अधिक प्यार करती है, चाहती है; वैसे ही सब प्राणियों से सर्वथा सर्वदा वैर- भाव छोड़कर प्रेम की भावना बनाना, यही योगाभ्यास का आरम्भ है । हमें अपना परीक्षण करना चाहिए कि हम इस कसौटी पर कितना उतरते हैं। बाहर वालों की बात तो दूर रही, अपने साथ रहनेवालों से कैसा व्यवहार करते हैं ?
३२. ईश्वर हमारा माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा है। हम सब उसकी सन्तान, शिष्य, प्रजा हैं तो हम सब का एक ईश्वर ही सब कुछ (माता, पिता आदि ) है पुनः वैरभाव क्यों? न्याय भी यही कहता है कि हम ऐसा वैरभाव रखते हैं तो दण्ड के भागी होंगे, क्योंकि प्रेम की भावना रखना ईश्वर की आज्ञा है ।
३३. सहोदर भाईयों में जैसा मन में परस्पर उन्नति की भावना, प्रेम होता है वैसा व्यवहार योगाभ्यासियों में सब के प्रति होना चाहिए। यह योगाभ्यास में साधक है। मूल में ईश्वर हमारा माता - पिता है , तो " वसुधैव-कुटुम्बकम्" सभी भाई -भाई हुए, अत: वैसा ही व्यवहार होना चाहिए ।
३४. यदि कोई व्यक्ति हमारा किसी भी रूप में हमारा उपकार करता है तो हम भी उसी का, वैसा ही उपकार करें; यह आवश्यक नहीं है, किन्तु अन्यत्र कहीं भी उपकार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति में राग की भी सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त सारे संसार का ऐश्वर्य ईश्वर का है और हम ईश्वर के हैं तो किसी का अपना कुछ नहीं है। परन्तु हमें पुरुषार्थ करना है, अप्राप्त की प्राप्ति , प्राप्त की रक्षा, वृद्धि और धर्मकार्य में लगाना है ।
३५. प्राय: व्यक्ति अपने सम्बद्ध लोगों के द्वारा अपने प्रति अनुकूल व्यवहार न होने पर अथवा दोष कर देने पर क्षुब्ध, दुःखी हो जाता है । वह सोचता है कि बार-बार समझाए जाने पर भी ऐसा क्यों करता है? निकट रहनेवालों के साथ ऐसा अधिक होता है तथा दूरस्थ के साथ ऐसा कम होता है, क्योंकि साथ रहनेवाले से अधिक व्यवहास्-सम्बन्ध होने से अधिक दोष दिखते हैं, दूरस्थ के कम, अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। परन्तु इस प्रकार का व्यवहार योग में बाधक हैं| सामनेवाला स्वतंत्र है, हम उसे अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकते । सामनेवाला अनुकूल भी कर सकता है प्रतिकूल भी। इसलिए अतिसावधानीपूर्वक मानसिक स्तर पर यम-नियमों का पालन करना है।
३६. साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने कार्य को समय पर नहीं करता हो और अधिकारी को सूचना देने पर भी रुष्ट होता हो कि हमने उसका दोष दिखाने की दृष्टि से ऐसा किया है तो प्रथम उसी को सूचना दें। स्वयं उसी से पूछे कि यदि आपके पास समय न हो तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ? स्वयं भी न करने को तैयार हो, न आपको करने को कहे तब अधिकारी से पूछे। परन्तु मन में उसके कल्याण की भावना हो, ऐसा नहीं कि यह कार्य ही नहीं करता है तो मुझे तो करना ही है, ऐसा सोचकर उपेक्षा करे तो योग मे गति नहीं होगी ।
३७. अपने से सम्बद्ध व्यक्ति से पूछना कि मैं आपके साथ किस तरह का व्यवहार करूँ, जो धर्मयुक्त हो जिससे आपको कम से कम कष्ट हो अथवा न हो और सुख अधिक हो। इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। उसके साथ आत्मतुल्य व्यवहार होगा।
३८. मानसिक स्तर पर यह मानना कि मैं सेवा कर रहा हूँ यह मेरा गुण है, मुझे यश मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि यह सब साधन जिन से हम सेवादि कार्य करते हैं वे ईश्वर-प्रदत्त हैं। इसलिय मुख्य सामर्थ्य तो ईश्वर का है हमारा तो नाममात्र है ।
३९. किसी भी नए कार्य को केवल अपनी जिम्मेदारी पर अथवा अपने अधिकार में रखकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कई दोष आ जाएँगे। दूसरे के लिए नया कार्य प्रतिकूल होने पर वह व्यक्ति वाद-विवाद, तू-तू, में-मैं झगड़ा आदि कर सकता है ।
४०. प्रत्येक कार्य को करते समय उसके परिणाम, प्रभाव, फल तक सोचना चाहिए। तभी आर्य समाज का पाँचवाँ नियम पूरा होगा, यह नियम मुक्ति तक के फल को बताता है कि अमुक कार्य मुक्ति प्राप्ति में सहायक है या बाधक ।
३२. ईश्वर हमारा माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा है। हम सब उसकी सन्तान, शिष्य, प्रजा हैं तो हम सब का एक ईश्वर ही सब कुछ (माता, पिता आदि ) है पुनः वैरभाव क्यों? न्याय भी यही कहता है कि हम ऐसा वैरभाव रखते हैं तो दण्ड के भागी होंगे, क्योंकि प्रेम की भावना रखना ईश्वर की आज्ञा है ।
३३. सहोदर भाईयों में जैसा मन में परस्पर उन्नति की भावना, प्रेम होता है वैसा व्यवहार योगाभ्यासियों में सब के प्रति होना चाहिए। यह योगाभ्यास में साधक है। मूल में ईश्वर हमारा माता - पिता है , तो " वसुधैव-कुटुम्बकम्" सभी भाई -भाई हुए, अत: वैसा ही व्यवहार होना चाहिए ।
३४. यदि कोई व्यक्ति हमारा किसी भी रूप में हमारा उपकार करता है तो हम भी उसी का, वैसा ही उपकार करें; यह आवश्यक नहीं है, किन्तु अन्यत्र कहीं भी उपकार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति में राग की भी सम्भावना रहती है । इसके अतिरिक्त सारे संसार का ऐश्वर्य ईश्वर का है और हम ईश्वर के हैं तो किसी का अपना कुछ नहीं है। परन्तु हमें पुरुषार्थ करना है, अप्राप्त की प्राप्ति , प्राप्त की रक्षा, वृद्धि और धर्मकार्य में लगाना है ।
३५. प्राय: व्यक्ति अपने सम्बद्ध लोगों के द्वारा अपने प्रति अनुकूल व्यवहार न होने पर अथवा दोष कर देने पर क्षुब्ध, दुःखी हो जाता है । वह सोचता है कि बार-बार समझाए जाने पर भी ऐसा क्यों करता है? निकट रहनेवालों के साथ ऐसा अधिक होता है तथा दूरस्थ के साथ ऐसा कम होता है, क्योंकि साथ रहनेवाले से अधिक व्यवहास्-सम्बन्ध होने से अधिक दोष दिखते हैं, दूरस्थ के कम, अन्य भी कई कारण हो सकते हैं। परन्तु इस प्रकार का व्यवहार योग में बाधक हैं| सामनेवाला स्वतंत्र है, हम उसे अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकते । सामनेवाला अनुकूल भी कर सकता है प्रतिकूल भी। इसलिए अतिसावधानीपूर्वक मानसिक स्तर पर यम-नियमों का पालन करना है।
३६. साथ में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने कार्य को समय पर नहीं करता हो और अधिकारी को सूचना देने पर भी रुष्ट होता हो कि हमने उसका दोष दिखाने की दृष्टि से ऐसा किया है तो प्रथम उसी को सूचना दें। स्वयं उसी से पूछे कि यदि आपके पास समय न हो तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ? स्वयं भी न करने को तैयार हो, न आपको करने को कहे तब अधिकारी से पूछे। परन्तु मन में उसके कल्याण की भावना हो, ऐसा नहीं कि यह कार्य ही नहीं करता है तो मुझे तो करना ही है, ऐसा सोचकर उपेक्षा करे तो योग मे गति नहीं होगी ।
३७. अपने से सम्बद्ध व्यक्ति से पूछना कि मैं आपके साथ किस तरह का व्यवहार करूँ, जो धर्मयुक्त हो जिससे आपको कम से कम कष्ट हो अथवा न हो और सुख अधिक हो। इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। उसके साथ आत्मतुल्य व्यवहार होगा।
३८. मानसिक स्तर पर यह मानना कि मैं सेवा कर रहा हूँ यह मेरा गुण है, मुझे यश मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि यह सब साधन जिन से हम सेवादि कार्य करते हैं वे ईश्वर-प्रदत्त हैं। इसलिय मुख्य सामर्थ्य तो ईश्वर का है हमारा तो नाममात्र है ।
३९. किसी भी नए कार्य को केवल अपनी जिम्मेदारी पर अथवा अपने अधिकार में रखकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कई दोष आ जाएँगे। दूसरे के लिए नया कार्य प्रतिकूल होने पर वह व्यक्ति वाद-विवाद, तू-तू, में-मैं झगड़ा आदि कर सकता है ।
४०. प्रत्येक कार्य को करते समय उसके परिणाम, प्रभाव, फल तक सोचना चाहिए। तभी आर्य समाज का पाँचवाँ नियम पूरा होगा, यह नियम मुक्ति तक के फल को बताता है कि अमुक कार्य मुक्ति प्राप्ति में सहायक है या बाधक ।
४१. प्रश्न ➧ दूसरे की उन्नति को देखकर कैसे प्रसन्न रहना चाहिए?
उत्तर ➨ सब कुछ ईश्वर का मानना, स्वयं के लिए सुख-सुविधाओं की इच्छा न करना और यह सोचना कि यदि मैं ईश्वर को छोड़कर इनके पीछे भागूँगा तो रागादि क्लेशों से पिस जाऊँगा। इसके अतिरिक्त, विवेक- वैराग्य, ईश्वरोपासना आदि करने से यह स्थिति बनती है। सब कुछ ईश्वर में है, सब में ईश्वर है, ऐसा जानकर वह ईश्वर को नहीं छोड़ता और दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहता है।
४२. प्रत्येक शुभ-कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी चाहिए। इससे एक तो वह कार्य सरलता से हो जाता है, दूसरा मिथ्याभिमान नहीं रहता, तीसरा में और मेरा नष्ट जाता है; यह एक शिष्ट व्यवहार है ।
४३. मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है परन्तु स्वतन्त्र बुद्धि देने से वह नियम में नहीं रहता है। बुद्धि का उचित प्रयोग करे तो वह पशु- पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। अनेक विपदाओं से बच सकता है। ईश्वर ने पशु-पक्षियों को ऐसी बुद्धि दी है कि वे अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध स्वयं कर लेते हैं, परन्तु वे उस सीमित नियम में बँधे रहते हैं ।
४४. विभिन्न योनियों के पशु-पक्षी आदि को देखो कितने अज्ञान अन्धकार में डूबे हैं, कैसे दण्ड भोग रहे हैं ? कोई स्वतन्त्रता नहीं है । उनको देखकर व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मैं कभी ऐसा पाप कर्म न करूँ। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी दण्ड-व्यवस्था निश्चित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार से गम्भीरता से नहीं विचारता वह पाप-कर्म से नहीं बच सकता।
४५. जब किसी से दूर रहने की भावना होती है और उसके पास आने पर क्षोभ होता है तो वह द्वेष है। इससे सम्बन्ध नहीं रखना अथवा कम रखना है, फिर भी उसका हित चाहना, यह उपेक्षा है ।
४६. हजारों चक्रवर्ती सम्राटों का सुख होने पर भी पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि वे भी शरीरधारी होने से रोग-वियोग, मृत्यु आदि से नहीं छूट सकते। अत: लौकिक विषयों के संस्कारों को जानना और उन्हें तत्वज्ञान, विवेक-वैराग्य, प्रतिपक्ष-भावना से निर्बल बनाना और नष्ट करना, योग मार्ग में अति आवश्यक कार्य है ।
४७. अपने शक्ति, सामर्थ्य, वीर्य को व्यर्थ चिन्तन, विचार, भोग विषयों में नहीं लगाना, ईश्वर में लगाना है। इससे भोगों में रुचि कम होगी और ईश्वर में बढ़ेगी ।
४८. प्राय: व्यक्ति आयु अथवा अनुभव में अपने से छोटे व्यक्ति की बात नहीं सुनता । उसमें अभिमान होता है कि मैं अधिक जानता हूँ, परन्तु प्रतिकूल व्यवहार किए जाने पर राग-द्वेष से युक्त होता है। यह सब लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं। यहाँ योगाभ्यासी को सोचना चाहिए कि व्यक्ति गौण होता है, बात प्रधान होती है। व्यक्ति जो बात कह रहा है वह सत्य व ग्राह्य है या नहीं? यदि हमें कार्य स्मरण दिला रहा है तो उस समय उसे अपना हितकारी माने क्योंकि जीवात्मा के अल्पज्ञ होने से भूलने की सम्भावना रहती है। यदि कार्य में सुझाव देता है तो सौहार्द स्वीकार करें कि मेरे कार्य को अच्छा हुआ देखना चाहता है। परन्तु सुझाव मानना या न मानना, यह अलग बात है। इस प्रकार करने से राग-द्वेष नहीं होगा और प्रेम, श्रद्धा, सहयोग की भावना बढ़ेगी।
४९. प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की उपस्थिति के कारण बुरा कार्य नहीं करता तो वह सीख रहा है कि बुरा कार्य ठीक नहीं है।
५०. दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम उससे अपने लिए चाहते हैं तभी आत्मवत् व्यवहार होगा। तभी योग में रुचि और गति होगी। अन्यथा अहिंसादि यम नियमों के उल्लंघन से नहीं बच सकते ।
५१. भले ही दूसरा बास्- बार त्रुटि करे लेकिन उसके प्रति हिंसा, क्रोध, प्रतिकार लेने आदि अन्य बुरी भावना नहीं रखनी। सामनेवाला स्वतन्त्र है, उसकी बुद्धि-चिंतन-योग्यता अलग है तो उस पर अधिकार अनुशासन वाली, व्यंग्यात्मक, नीचा दिखानेवाली भाषा का प्रयोग करके उसकी स्वतन्त्रता नहीं भंग करनी चाहिए। जैसे हम अपनी स्वतन्त्रता भंग नहीं होने देना चाहते । यही योगाभ्यास है । यही योग में गति करने का मार्ग है ।
५२. जब तक व्यक्ति साथ रहता है तब तक उसके दोष दिखाई देते हैं, जब दूर जाता है तब उसके गुण दिखने लगते हैं। क्योंकि साथ रहने में व्यवहार में छोटी-छोटी त्रुटियाँ होते रहने से केवल दोष दिखने प्रधान हो जाते हैं। जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है व्यक्ति उसे नहीं सोचता अथवा गौण मानता है। परन्तु वही व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो उससे सिद्ध होनेवाले प्रयोजन वर्तमान में पूरे नहीं होते तब उसके गुण दिखने लगते हैं। इसलिए साथ रहनेवालों के गुणों को देखकर उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए, इससे प्रेम की भावना आएगी। कई बार व्यक्ति अपनी चतुराई से अपने दोषों को छुपा लेता है परन्तु वही चतुर व्यक्ति जब दूर जाता है तो उसके दोष प्रत्यक्ष-परोक्षरूप में सामने आने लगते हैं ।
५३. सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः अहिंसा ॥ व्यास भाष्य २/३०। जो व्यक्ति इस प्रकार के आदर्शों को सामने लेकर चलता है। वही इस योग मार्ग पर बढ़ सकता है। अन्यथा व्यक्ति अवसरवादी होता है। कभी भी धोखा दे सकता है ।
उत्तर ➨ सब कुछ ईश्वर का मानना, स्वयं के लिए सुख-सुविधाओं की इच्छा न करना और यह सोचना कि यदि मैं ईश्वर को छोड़कर इनके पीछे भागूँगा तो रागादि क्लेशों से पिस जाऊँगा। इसके अतिरिक्त, विवेक- वैराग्य, ईश्वरोपासना आदि करने से यह स्थिति बनती है। सब कुछ ईश्वर में है, सब में ईश्वर है, ऐसा जानकर वह ईश्वर को नहीं छोड़ता और दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न रहता है।
४२. प्रत्येक शुभ-कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी चाहिए। इससे एक तो वह कार्य सरलता से हो जाता है, दूसरा मिथ्याभिमान नहीं रहता, तीसरा में और मेरा नष्ट जाता है; यह एक शिष्ट व्यवहार है ।
४३. मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है परन्तु स्वतन्त्र बुद्धि देने से वह नियम में नहीं रहता है। बुद्धि का उचित प्रयोग करे तो वह पशु- पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। अनेक विपदाओं से बच सकता है। ईश्वर ने पशु-पक्षियों को ऐसी बुद्धि दी है कि वे अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध स्वयं कर लेते हैं, परन्तु वे उस सीमित नियम में बँधे रहते हैं ।
४४. विभिन्न योनियों के पशु-पक्षी आदि को देखो कितने अज्ञान अन्धकार में डूबे हैं, कैसे दण्ड भोग रहे हैं ? कोई स्वतन्त्रता नहीं है । उनको देखकर व्यक्ति के मन में भावना होती है कि मैं कभी ऐसा पाप कर्म न करूँ। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी दण्ड-व्यवस्था निश्चित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस प्रकार से गम्भीरता से नहीं विचारता वह पाप-कर्म से नहीं बच सकता।
४५. जब किसी से दूर रहने की भावना होती है और उसके पास आने पर क्षोभ होता है तो वह द्वेष है। इससे सम्बन्ध नहीं रखना अथवा कम रखना है, फिर भी उसका हित चाहना, यह उपेक्षा है ।
४६. हजारों चक्रवर्ती सम्राटों का सुख होने पर भी पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि वे भी शरीरधारी होने से रोग-वियोग, मृत्यु आदि से नहीं छूट सकते। अत: लौकिक विषयों के संस्कारों को जानना और उन्हें तत्वज्ञान, विवेक-वैराग्य, प्रतिपक्ष-भावना से निर्बल बनाना और नष्ट करना, योग मार्ग में अति आवश्यक कार्य है ।
४७. अपने शक्ति, सामर्थ्य, वीर्य को व्यर्थ चिन्तन, विचार, भोग विषयों में नहीं लगाना, ईश्वर में लगाना है। इससे भोगों में रुचि कम होगी और ईश्वर में बढ़ेगी ।
४८. प्राय: व्यक्ति आयु अथवा अनुभव में अपने से छोटे व्यक्ति की बात नहीं सुनता । उसमें अभिमान होता है कि मैं अधिक जानता हूँ, परन्तु प्रतिकूल व्यवहार किए जाने पर राग-द्वेष से युक्त होता है। यह सब लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं। यहाँ योगाभ्यासी को सोचना चाहिए कि व्यक्ति गौण होता है, बात प्रधान होती है। व्यक्ति जो बात कह रहा है वह सत्य व ग्राह्य है या नहीं? यदि हमें कार्य स्मरण दिला रहा है तो उस समय उसे अपना हितकारी माने क्योंकि जीवात्मा के अल्पज्ञ होने से भूलने की सम्भावना रहती है। यदि कार्य में सुझाव देता है तो सौहार्द स्वीकार करें कि मेरे कार्य को अच्छा हुआ देखना चाहता है। परन्तु सुझाव मानना या न मानना, यह अलग बात है। इस प्रकार करने से राग-द्वेष नहीं होगा और प्रेम, श्रद्धा, सहयोग की भावना बढ़ेगी।
४९. प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी की उपस्थिति के कारण बुरा कार्य नहीं करता तो वह सीख रहा है कि बुरा कार्य ठीक नहीं है।
५०. दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा हम उससे अपने लिए चाहते हैं तभी आत्मवत् व्यवहार होगा। तभी योग में रुचि और गति होगी। अन्यथा अहिंसादि यम नियमों के उल्लंघन से नहीं बच सकते ।
५१. भले ही दूसरा बास्- बार त्रुटि करे लेकिन उसके प्रति हिंसा, क्रोध, प्रतिकार लेने आदि अन्य बुरी भावना नहीं रखनी। सामनेवाला स्वतन्त्र है, उसकी बुद्धि-चिंतन-योग्यता अलग है तो उस पर अधिकार अनुशासन वाली, व्यंग्यात्मक, नीचा दिखानेवाली भाषा का प्रयोग करके उसकी स्वतन्त्रता नहीं भंग करनी चाहिए। जैसे हम अपनी स्वतन्त्रता भंग नहीं होने देना चाहते । यही योगाभ्यास है । यही योग में गति करने का मार्ग है ।
५२. जब तक व्यक्ति साथ रहता है तब तक उसके दोष दिखाई देते हैं, जब दूर जाता है तब उसके गुण दिखने लगते हैं। क्योंकि साथ रहने में व्यवहार में छोटी-छोटी त्रुटियाँ होते रहने से केवल दोष दिखने प्रधान हो जाते हैं। जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है व्यक्ति उसे नहीं सोचता अथवा गौण मानता है। परन्तु वही व्यक्ति जब दूर चला जाता है तो उससे सिद्ध होनेवाले प्रयोजन वर्तमान में पूरे नहीं होते तब उसके गुण दिखने लगते हैं। इसलिए साथ रहनेवालों के गुणों को देखकर उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए, इससे प्रेम की भावना आएगी। कई बार व्यक्ति अपनी चतुराई से अपने दोषों को छुपा लेता है परन्तु वही चतुर व्यक्ति जब दूर जाता है तो उसके दोष प्रत्यक्ष-परोक्षरूप में सामने आने लगते हैं ।
५३. सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः अहिंसा ॥ व्यास भाष्य २/३०। जो व्यक्ति इस प्रकार के आदर्शों को सामने लेकर चलता है। वही इस योग मार्ग पर बढ़ सकता है। अन्यथा व्यक्ति अवसरवादी होता है। कभी भी धोखा दे सकता है ।
५४. जब किसी से वाणी व्यवहार करते हैं तो उस समय यह सोचकर बोले कि सामनेवाले को आनन्द हो जो ऐसा सोचकर नहीं बोलता वह वाणी-व्यवहार तथा उससे मिलनेवाले फलों को नहीं जानता, उसका व्यवहार भी नहीं सुधर सकता।
५५. अनेक कारणों से व्यक्ति पर दुःख, रोग आदि आते हैं। जैसे अवस्था-परिवर्तन से जो कि शरीर का धर्म है - यथा बालक, किशोर, युवा, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु आदि। इसके अतिरिक्त ईश्वर का न्याय है, नियम है, हमारा कर्मफल कुछ इस जन्म के कुछ पूर्व जन्म के। इसके साथ राजा, प्रजा, माता पिता भी कारण हैं । इसलिए इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।
५६. व्यक्ति को गुण-ग्रहण करने और दोष- छोड़ने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति गुणग्रहण नहीं करता, दोषों को नहीं छोड़ता। उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए ।
५७. जो व्यक्ति ईश्वरोपासना करता है, व्यवहार में ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन - अध्यापन- स्वाध्याय करता है, निष्काम-कर्म ही करता है, उसे अन्य कोई लौकिक विषय विचारने, भोगने का समय ही नहीं होता । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता अथवा इनमें से किसी को छोड़ता है, वह बुराई, लौकिक विषयभोगों से बच ही नहीं सकता।
५८. किसी से राग-द्वेष तब तक है, जब तक वह ( सामनेवाला) शरीर से सम्बद्ध है । शरीर नाशवान् है और ईश्वर प्रदत्त साधन के रूप में ईश्वर की सम्पत्ति है । मन बुद्धि, आदि भी इस प्रकार के साधन हैं। सामनेवाला अपने सदृश ही जीव है । सीधा उससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है तो क्यों इतना राग-द्वेष करना ।
५९. जो राग-द्वेष करते हैं वह शरीर के कारण या अन्य वस्तुओं के कारण, जो कि ईश्वर की हैं। दूसरे की वस्तु के कारण झगड़ा करना ठीक नहीं है, दोष है ।
६०. सामनेवाला यदि हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, वह उसका दोष है। वह ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको ईश्वर स्वयं न्यायानुसार फल देंगे। हमें उससे उलझना नहीं है। उलझेंगे तो हमारा योगाभ्यास असफल हो जाएगा, उल्टा हमें दण्ड मिलेगा ।
६१. जब व्यक्ति ईश्वर-प्रणिधान से युक्त रहता है और मन, बुद्धि, आदि ईश्वर का मानकर चलता है तो इन साधनों को, ईश्वर की सम्पत्ति मानकर, ईश्वर की आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करता है। जैसे अपने शरीरादि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही अन्यों के पदार्थों की भी रक्षा करता है क्योंकि सभी पदार्थ ईश्वर की सम्पत्ति है। यदि ईश्वर प्रदत्त इन साधनों का दुरुपयोग करेंगे तो उसका भयानक दण्ड मिलेगा, जब व्यक्ति ऐसा सोचता, विचारता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं तो उसका सारा मिथ्याभिमान टूट जाता है ।
६२. ईश्वर वायु के समान प्राणवत् प्रिय और हृदय की बातें जानने हारे हैं अर्थात् हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ईश्वर सभी को हर क्षण देख, सुन, जान रहे हैं। क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। इसलिए किसी समस्या का समाधान जानना हो तो बड़ी श्रद्धा से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए ।
६३. जो व्यक्ति परिश्रमपूर्वक अन्यों को सुख देना चाहता है दुःख नहीं, वह हमेशा आनन्दित रहता है। इसके साथ जब व्यक्ति व्यवहार करते समय अन्तिम परिणाम देखता है तब उचित व्यवहार कर पाता है। क्योंकि सभी कार्य धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए ।
६४. जब तक व्यक्ति के मन में यह बात है कि मैं बहुत कम जानता हूँ, मेरी जानने की इच्छा, जिज्ञासा, रुचि है, मैं और जानना चाहता हूँ, तब तो कुछ सीख सकता है । उसकी बुद्धि यह काम करती है कि चाहे वह उस कार्य को पूरा जानता है परन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् होने से कभी भी गलती कर सकता है । जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हर समय बनी रहती है वह उन्नति कर सकता है, अन्यथा जो अभिमान में रहता है कि में जानता हूँ वह बहुत सिखाने पर भी नहीं सीखता ।
६५. व्यक्ति प्राय: अपनी बुद्धि, अनुभव, मापदण्ड से दूसरे को मापता है तब गलती करता है। जाने-अनजाने में, अभ्यास होने से अथवा अच्छा मानने के कारण वह व्यक्ति अनुचित निर्णय देता रहता है। वह नहीं जानता कि यम-नियमों का भंग हो रहा है। कितने परीक्षण के पश्चात् व्यक्ति सत्य बोल पाता है, वह उसको नहीं जानता।
६६. योग-मार्ग पर चलने वाले के लिए सूक्ष्म अनुशासन का एक भाग यह है कि एक बार बताए जाने पर उस कार्य को, जो दोषयुक्त है, नहीं करे। स्थूल अनुशासन यथा मन से बिना पाँच परीक्षाएँ किए किसी भी बात को न मानना। वाणी और शरीरादि साधनों का सदुपयोग करना, उपासना में एक भी वृत्ति न उठाना आदि। जो इस प्रकार के स्थूल सूक्ष्म अनुशासन में चलता है वही आगे योग-मार्ग पर चल सकता है। इसलिए उपनिषद् में इस मार्ग पर चलना छुरे की धार पर चलना बताया है ।
५५. अनेक कारणों से व्यक्ति पर दुःख, रोग आदि आते हैं। जैसे अवस्था-परिवर्तन से जो कि शरीर का धर्म है - यथा बालक, किशोर, युवा, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु आदि। इसके अतिरिक्त ईश्वर का न्याय है, नियम है, हमारा कर्मफल कुछ इस जन्म के कुछ पूर्व जन्म के। इसके साथ राजा, प्रजा, माता पिता भी कारण हैं । इसलिए इसमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए ।
५६. व्यक्ति को गुण-ग्रहण करने और दोष- छोड़ने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना चाहिए। जो व्यक्ति गुणग्रहण नहीं करता, दोषों को नहीं छोड़ता। उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए ।
५७. जो व्यक्ति ईश्वरोपासना करता है, व्यवहार में ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहता है, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन - अध्यापन- स्वाध्याय करता है, निष्काम-कर्म ही करता है, उसे अन्य कोई लौकिक विषय विचारने, भोगने का समय ही नहीं होता । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता अथवा इनमें से किसी को छोड़ता है, वह बुराई, लौकिक विषयभोगों से बच ही नहीं सकता।
५८. किसी से राग-द्वेष तब तक है, जब तक वह ( सामनेवाला) शरीर से सम्बद्ध है । शरीर नाशवान् है और ईश्वर प्रदत्त साधन के रूप में ईश्वर की सम्पत्ति है । मन बुद्धि, आदि भी इस प्रकार के साधन हैं। सामनेवाला अपने सदृश ही जीव है । सीधा उससे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है तो क्यों इतना राग-द्वेष करना ।
५९. जो राग-द्वेष करते हैं वह शरीर के कारण या अन्य वस्तुओं के कारण, जो कि ईश्वर की हैं। दूसरे की वस्तु के कारण झगड़ा करना ठीक नहीं है, दोष है ।
६०. सामनेवाला यदि हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, वह उसका दोष है। वह ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको ईश्वर स्वयं न्यायानुसार फल देंगे। हमें उससे उलझना नहीं है। उलझेंगे तो हमारा योगाभ्यास असफल हो जाएगा, उल्टा हमें दण्ड मिलेगा ।
६१. जब व्यक्ति ईश्वर-प्रणिधान से युक्त रहता है और मन, बुद्धि, आदि ईश्वर का मानकर चलता है तो इन साधनों को, ईश्वर की सम्पत्ति मानकर, ईश्वर की आज्ञा अनुसार उनका प्रयोग करता है। जैसे अपने शरीरादि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही अन्यों के पदार्थों की भी रक्षा करता है क्योंकि सभी पदार्थ ईश्वर की सम्पत्ति है। यदि ईश्वर प्रदत्त इन साधनों का दुरुपयोग करेंगे तो उसका भयानक दण्ड मिलेगा, जब व्यक्ति ऐसा सोचता, विचारता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं तो उसका सारा मिथ्याभिमान टूट जाता है ।
६२. ईश्वर वायु के समान प्राणवत् प्रिय और हृदय की बातें जानने हारे हैं अर्थात् हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ईश्वर सभी को हर क्षण देख, सुन, जान रहे हैं। क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। इसलिए किसी समस्या का समाधान जानना हो तो बड़ी श्रद्धा से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए ।
६३. जो व्यक्ति परिश्रमपूर्वक अन्यों को सुख देना चाहता है दुःख नहीं, वह हमेशा आनन्दित रहता है। इसके साथ जब व्यक्ति व्यवहार करते समय अन्तिम परिणाम देखता है तब उचित व्यवहार कर पाता है। क्योंकि सभी कार्य धर्मानुसार सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए ।
६४. जब तक व्यक्ति के मन में यह बात है कि मैं बहुत कम जानता हूँ, मेरी जानने की इच्छा, जिज्ञासा, रुचि है, मैं और जानना चाहता हूँ, तब तो कुछ सीख सकता है । उसकी बुद्धि यह काम करती है कि चाहे वह उस कार्य को पूरा जानता है परन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान् होने से कभी भी गलती कर सकता है । जिसकी इस प्रकार की बुद्धि हर समय बनी रहती है वह उन्नति कर सकता है, अन्यथा जो अभिमान में रहता है कि में जानता हूँ वह बहुत सिखाने पर भी नहीं सीखता ।
६५. व्यक्ति प्राय: अपनी बुद्धि, अनुभव, मापदण्ड से दूसरे को मापता है तब गलती करता है। जाने-अनजाने में, अभ्यास होने से अथवा अच्छा मानने के कारण वह व्यक्ति अनुचित निर्णय देता रहता है। वह नहीं जानता कि यम-नियमों का भंग हो रहा है। कितने परीक्षण के पश्चात् व्यक्ति सत्य बोल पाता है, वह उसको नहीं जानता।
६६. योग-मार्ग पर चलने वाले के लिए सूक्ष्म अनुशासन का एक भाग यह है कि एक बार बताए जाने पर उस कार्य को, जो दोषयुक्त है, नहीं करे। स्थूल अनुशासन यथा मन से बिना पाँच परीक्षाएँ किए किसी भी बात को न मानना। वाणी और शरीरादि साधनों का सदुपयोग करना, उपासना में एक भी वृत्ति न उठाना आदि। जो इस प्रकार के स्थूल सूक्ष्म अनुशासन में चलता है वही आगे योग-मार्ग पर चल सकता है। इसलिए उपनिषद् में इस मार्ग पर चलना छुरे की धार पर चलना बताया है ।
६७. अपने जीवन में ऐसे सिद्धान्त निश्चित कर लेने चाहिए कि मैं इसी पर चलूँगा इससे इधर-उधर नहीं । अपना ही अनुशासन अपने ऊपर रखें, वही योग की उत्तम अवस्था है ।
६८. व्यक्ति ऐसा विचार मन में रखेगा कि मैं जो बात कहूँगा अथवा कहने जा रहा हूँ, वह सामनेवाले के हृदय में उतर जाए, उसे एक ही बार में सारी समझ आ जाए, तब वाणी का सदुपयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा विचार नहीं रखेगा तो वाणी में कई दोष आ जाएँगे, जैसे कठोर बोलेगा, आदेशात्मक, अभिमान आदि से युक्त होकर बोलेगा। उसके चेहरे के हाव-भाव भी बदल जाएँगे। इस प्रकार न जानने से व्यक्ति मन-वचन-शरीर से अनेक प्रकार के शुभाशुभ मिश्रित कर्म करता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता। बुद्धिमान् इतने ही संकेत को समझकर तुरन्त सत्य को ग्रहण करता और असत्य को छोड़ देता है ।
६९. सामनेवाला हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो शरीर, वाणी की बात दूर रही मन में भी उसके प्रति अहित की भावना, प्रतिकार की भावना, चेष्टा मात्र भी न हो, बल्कि आनन्दित होना चाहिए कि वह मेरी सहनशक्ति को बढ़ा रहा है। मन ही मन उसका धन्यवाद करना चाहिए इसलिए तो सार्वभौममहाव्रत कहा है और 'क्षुरस्य धारा' कहा है तभी व्यक्ति इस योग मार्ग पर चल सकता है ।
७०. सामनेवाला यदि ठीक व्यवहार नहीं करता तो वह स्वतन्त्र है, उसका दोष है। हम क्यों उससे उलझकर दोषी बने। इससे राग -द्वेष बढ़ेगा। यदि ब्राह्मण बनना है तो इसी प्रकार तप करना पड़ेगा। अन्यथा इस मार्ग को छोड़कर क्षत्रिय बनकर देश की रक्षा करो अथवा अन्य धनादि की उन्नति करो ।
७१. सबसे ऊँचे स्तर का व्यक्ति प्रेम से मिलकर रहता, झगड़ा-तनाव उत्पन्न नहीं करता है। दूसरे स्तर वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग भी देता है। तीसरे स्तर वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग नहीं देता। निकृष्ट स्तरवाला स्वतन्त्र कार्य करता हुआ दूसरे का विरोध करता है ।
७२. जब तक व्यक्ति ज्ञान-कर्म-उपासना शुद्ध नहीं करता अर्थात् वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं करता तब तक न तो स्वयं सुखी रह सकता और न ही अन्यों को सुख दे सकता है अर्थात् स्वयं दुःखी रहेगा, अन्यों को भी दुःख देगा।
७३. व्यक्ति पूर्णरूपेण ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर का ज्ञान, बल अनन्त है, परन्तु अनेक ऋषियों जितना तो कर ही सकता है। क्योंकि ऋषि मनुष्य होते हैं और एक मनुष्य जितना कर सकता है उतना दूसरा भी कर सकता है ।
७४. मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने में पूर्ण समर्थ है परन्तु इसके लिए अत्यन्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ न कर सकने के कारण व्यक्ति अपने हठ, दुराग्रह अविद्यादि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य को ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति यदि अच्छा बनने के लिए व्रत, संकल्प, पुरुषार्थ करे तो उसे दुनिया की कोई वस्तु अच्छा बनने से रोक नहीं सकती ।
७५. जो कोई भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह ईश्वर प्रदत्त है क्योंकि जीवात्मा में तो अपना ज्ञान करने का भी सामर्थ्य नहीं है। अत: सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी वस्तु से सम्बद्ध पूर्वज्ञान हो अथवा नवीनज्ञान करना हो तो उस वस्तु से सम्बद्ध वास्तविक, निश्चित्, सत्यज्ञान करना चाहिए, वही ईश्वरीय ज्ञान होगा। जो ऐसा प्रयत्न करता है वही व्यक्ति सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो सकता है ।
७६. यदि व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है कि जिससे अन्यों को हँसी आए, रोचक लगे तो वह लौकिक बन जाता है। आध्यात्मिक स्थिति=ईश्वर को छोड़ देता है। यह पतन की स्थिति है ।
७८. यदि व्यक्ति मन-मस्तिष्क में हमेशा यह बात बिठाए रखता है कि ईश्वर मेरे प्रत्येक, मन-वचन-शरीर से किये जानेवाले कर्मों को देख, जान, सुन रहे हैं और न्यायानुसार उन कर्मों का फल भी देंगे तो व्यक्ति पाप करने से बचता है। जब तक यह स्थिति नहीं है तो पाप करने से नहीं डरता,न यम-नियमों का पालन करता,न समाधि को प्राप्त करता, न ईश्वरप्रदत्त साधनों का सदुपयोग करता है ।
७९. बार बार बताने, समझाने पर भी सामनेवाला व्यक्ति यदि अपने दोष, हठता नहीं छोड़ता तो हम क्यों उससे दु:खी होकर अपनी सज्जनता आदि गुणों को छोड़कर दोष करने लगे। ऐसा करने से तो उसमें और हम में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो सिद्ध है कि सामनेवाला दोषों में पक्का है। हम अभी गुणों में पक्के नहीं है ।
६८. व्यक्ति ऐसा विचार मन में रखेगा कि मैं जो बात कहूँगा अथवा कहने जा रहा हूँ, वह सामनेवाले के हृदय में उतर जाए, उसे एक ही बार में सारी समझ आ जाए, तब वाणी का सदुपयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा विचार नहीं रखेगा तो वाणी में कई दोष आ जाएँगे, जैसे कठोर बोलेगा, आदेशात्मक, अभिमान आदि से युक्त होकर बोलेगा। उसके चेहरे के हाव-भाव भी बदल जाएँगे। इस प्रकार न जानने से व्यक्ति मन-वचन-शरीर से अनेक प्रकार के शुभाशुभ मिश्रित कर्म करता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता। बुद्धिमान् इतने ही संकेत को समझकर तुरन्त सत्य को ग्रहण करता और असत्य को छोड़ देता है ।
६९. सामनेवाला हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो शरीर, वाणी की बात दूर रही मन में भी उसके प्रति अहित की भावना, प्रतिकार की भावना, चेष्टा मात्र भी न हो, बल्कि आनन्दित होना चाहिए कि वह मेरी सहनशक्ति को बढ़ा रहा है। मन ही मन उसका धन्यवाद करना चाहिए इसलिए तो सार्वभौममहाव्रत कहा है और 'क्षुरस्य धारा' कहा है तभी व्यक्ति इस योग मार्ग पर चल सकता है ।
७०. सामनेवाला यदि ठीक व्यवहार नहीं करता तो वह स्वतन्त्र है, उसका दोष है। हम क्यों उससे उलझकर दोषी बने। इससे राग -द्वेष बढ़ेगा। यदि ब्राह्मण बनना है तो इसी प्रकार तप करना पड़ेगा। अन्यथा इस मार्ग को छोड़कर क्षत्रिय बनकर देश की रक्षा करो अथवा अन्य धनादि की उन्नति करो ।
७१. सबसे ऊँचे स्तर का व्यक्ति प्रेम से मिलकर रहता, झगड़ा-तनाव उत्पन्न नहीं करता है। दूसरे स्तर वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग भी देता है। तीसरे स्तर वाला स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है और साथ में एक-दूसरे को सहयोग नहीं देता। निकृष्ट स्तरवाला स्वतन्त्र कार्य करता हुआ दूसरे का विरोध करता है ।
७२. जब तक व्यक्ति ज्ञान-कर्म-उपासना शुद्ध नहीं करता अर्थात् वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं करता तब तक न तो स्वयं सुखी रह सकता और न ही अन्यों को सुख दे सकता है अर्थात् स्वयं दुःखी रहेगा, अन्यों को भी दुःख देगा।
७३. व्यक्ति पूर्णरूपेण ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर का ज्ञान, बल अनन्त है, परन्तु अनेक ऋषियों जितना तो कर ही सकता है। क्योंकि ऋषि मनुष्य होते हैं और एक मनुष्य जितना कर सकता है उतना दूसरा भी कर सकता है ।
७४. मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने में पूर्ण समर्थ है परन्तु इसके लिए अत्यन्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ न कर सकने के कारण व्यक्ति अपने हठ, दुराग्रह अविद्यादि दोषों के कारण सत्य को छोड़कर असत्य को ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति यदि अच्छा बनने के लिए व्रत, संकल्प, पुरुषार्थ करे तो उसे दुनिया की कोई वस्तु अच्छा बनने से रोक नहीं सकती ।
७५. जो कोई भी ज्ञान उत्पन्न होता है वह ईश्वर प्रदत्त है क्योंकि जीवात्मा में तो अपना ज्ञान करने का भी सामर्थ्य नहीं है। अत: सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी वस्तु से सम्बद्ध पूर्वज्ञान हो अथवा नवीनज्ञान करना हो तो उस वस्तु से सम्बद्ध वास्तविक, निश्चित्, सत्यज्ञान करना चाहिए, वही ईश्वरीय ज्ञान होगा। जो ऐसा प्रयत्न करता है वही व्यक्ति सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो सकता है ।
७६. यदि व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है कि जिससे अन्यों को हँसी आए, रोचक लगे तो वह लौकिक बन जाता है। आध्यात्मिक स्थिति=ईश्वर को छोड़ देता है। यह पतन की स्थिति है ।
७८. यदि व्यक्ति मन-मस्तिष्क में हमेशा यह बात बिठाए रखता है कि ईश्वर मेरे प्रत्येक, मन-वचन-शरीर से किये जानेवाले कर्मों को देख, जान, सुन रहे हैं और न्यायानुसार उन कर्मों का फल भी देंगे तो व्यक्ति पाप करने से बचता है। जब तक यह स्थिति नहीं है तो पाप करने से नहीं डरता,न यम-नियमों का पालन करता,न समाधि को प्राप्त करता, न ईश्वरप्रदत्त साधनों का सदुपयोग करता है ।
७९. बार बार बताने, समझाने पर भी सामनेवाला व्यक्ति यदि अपने दोष, हठता नहीं छोड़ता तो हम क्यों उससे दु:खी होकर अपनी सज्जनता आदि गुणों को छोड़कर दोष करने लगे। ऐसा करने से तो उसमें और हम में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो सिद्ध है कि सामनेवाला दोषों में पक्का है। हम अभी गुणों में पक्के नहीं है ।
८०. अपने प्रत्येक व्यवहार को, सत्यासत्य को जानने की जो पाँच परीक्षाएँ हैं, उन पर सदा आकलन करते रहना चाहिए। ईश्वर और वेद, का संग और उनके कृत ग्रन्थ, सृष्टिक्रम ये मुख्य हैं, शेष गौण हैं। जब जीवात्मा देखता है कि मेरी मान्यता वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, सत्पुरुषों के आचरण, ग्रन्थों, सिद्धान्तों के विरुद्ध है तो वह अपनी बात को ठुकरा देता है और उनकी बात मान लेता है तब ही सत्य को जान सकता है। परन्तु यह जानना भी आवश्यक है कि वेद, ईश्वर, सृष्टिक्रम, सत्पुरुषों की बात क्यों सत्य मानी जाए ? इसके लिए बास्- बार जीवात्मा को इनकी बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि इनके क्या गुण, कर्म, स्वभाव हैं? क्या वे किसी प्रकार से खण्डित होते हैं? तब उसे पता चलेगा कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इनको खण्डित कर सके। जैसे ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव में सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सृष्टिनिर्माण, पालन प्रलयादि, न्यायकारिता, दयालुता ।
८१. जब तक सम्प्रज्ञातसमाधि प्राप्त नहीं होती तब तक या तो देहधारी गुरु जो ईश्वर साक्षात्कारी हो उसके निर्देश में चलो अथवा देहधारी गुरु जितनी योग्यता हो तो सीधा ईश्वर को गुरु बनाकर चलो। यदि दो में से कोई भी नहीं करेंगे तो ईश्वर साक्षात् नहीं होगा ।
८२. योगाभ्यासी जैसे ही ईश्वर को छोड़ेगा तुरन्त प्रकृति, विकृति, अथवा जीव की उपासना में लग जाएगा और अज्ञानान्धकार-क्लेशयुक्त हो जाएगा ।
८३. प्राप्त, अभ्यस्त वस्तु के लिए विशेष बल नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति तथा उसके साथ अन्य कार्य भी किया जा सकता गाड़ी भी चला रहा है और अन्य कार्य सोचना, विचारना, लेना- देना, दूरभाष आदि भी करता रहता है वैसे ही योगी सभी कार्य करता हुआ अपनी स्थिति बनाए रखता है तथा मन के द्वारा बड़ी सूक्ष्मता से अनेक ज्ञान ग्रहण करता है ।
८४. योगी की समाधि लगी रहती है और अन्य भी विचार करता है, जैसे समाधि में ईश्वर की उपासना वेदमन्त्रों से करता हुआ मन्त्रों के अर्थ, धातु, प्रत्यय आदि भी सिद्ध करता रहेगा। इस प्रकार ईश्वर की उपासना भी चलती रहेगी और यह सभी कार्य करते हुए ईश्वर से उस विषय में ज्ञान भी प्राप्त करेगा ।
८५. पूर्वजीवन में किए दोषों, त्रुटियों को स्मरण करके बार-बार दु:खी, निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे कोई लाभ विशेष नहीं होगा। अन्तिम उपाय यही है कि जब से सत्य का बोध हो गया तभी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ आरम्भ करना चाहिए ।
८६. यदि किसी एक भी व्यक्ति से आपका वैर, ईष्ष्या, द्वेष शेष रहा तो वही योग में पर्याप्त बाधक बन जाएगा। यदि उपेक्षा भी रखनी है तो मन में उसके कल्याण की भावना हो। अच्छा तो यह है कि संसार के सभी व्यक्तियों से प्रेम हो। यम नियमों का सार्वभौममहाव्रत के रूप में पालन करते हुए सभी को मित्र बनाए रखना कठिन है ।
८७. हमारे साथी सहयोगी भले ही दोष अधिक करते हैं पुनरपि उत्तम व्यवहार यही है कि जो सेवा उन्होंने की उसकी प्रशंसा करना और दोषों को न देखना, न बताना; इससे व्यक्ति अपना बना रहता है। अन्यथा तो उसके मन में निराशा की भावना आएगी कि मैंने सेवा भी की उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकला, उसका साहस टूटेगा। मन में क्षमा, सहनशीलता, दया, करुणा की भावना बनाए रखना। इससे ही योग मार्ग पर स्थिर रह सकते हैं। ये आत्मा के नैमित्तिक गुण हैं, निमित्त से ही आते हैं। इसलिए ज्ञानपूर्वक इस प्रकार की भावना बनानी चाहिए और व्यवहार में लाने से अभ्यास हो जाएगा।
(१) व्यक्ति मानता है कि मृत्यु के साथ मेरा भी अभाव हो जाएगा इससे व्यक्ति को भय होता है ।
(२) इस शरीर के छूटने पर किसी भी वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहेगा। जो उसने पुरुषार्थ से सुख और सुख के साधन एकत्रित किए हैं उन साधनों से उसका स्वामित्व और सुखभोग, यह सब छूट जाएगा; इससे डर लगता है ।
(३) व्यक्ति संसार में रहते हुए सारी उम्र दूसरों से सम्बन्ध जोड़ने, सुख-साधन जुटाने और भोगने में बिता देता है, अपने को अकेला नहीं रहने देता। मृत्यु हो जाने पर तो संसार की किसी भी वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहता । जीवात्मा बिल्कुल अकेला रह जाता है। ऐसी विचित्र अवस्था देख-सोचकर उसे डर लगता है ।
(४) व्यक्ति को मृत्यु से इसलिए भी भय लगता है कि उसने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं अगला जन्म अच्छा मिलने की सम्भावना भी नहीं दिखती। बुद्धिमान् सत्याग्राही, धार्मिक व्यक्ति इससे भी प्रेरणा लेकर तुरन्त अच्छे कार्य प्रारम्भ कर देता है और बुरे को छोड़ देता है ।
(५) व्यक्ति की प्राय: इच्छा बनी रहती है कि मैं सदा जीता रहूँ, परन्तु ऐसा असम्भव है। इसलिए जब मृत्यु का विचार करता अथवा देखता है तो उसकी इच्छा का विघात होता है कि में तो झूठी इच्छा कर रहा हूँ तब उसे भयंकर डर लगता है ।
(६) पूर्वजन्म में मृत्यु से होनेवाले दुःख के संस्कारों के कारण से भी मृत्यु से भय होता है। क्योंकि इस जन्म में तो उसने मृत्यु दुःख का अनुभव किया नहीं फिर भी मृत्यु से भय होता है। अर्थात् पूर्वजन्मों में प्रत्यक्ष मृत्यु दुःख का अनुभव किया है । इससे जीव अनादि अनन्त भी सिद्ध होता है। यदि जीव भी मृत्यु के साथ ही मर जाता तो इस जन्म में मृत्यु भय न होता ।
८१. जब तक सम्प्रज्ञातसमाधि प्राप्त नहीं होती तब तक या तो देहधारी गुरु जो ईश्वर साक्षात्कारी हो उसके निर्देश में चलो अथवा देहधारी गुरु जितनी योग्यता हो तो सीधा ईश्वर को गुरु बनाकर चलो। यदि दो में से कोई भी नहीं करेंगे तो ईश्वर साक्षात् नहीं होगा ।
८२. योगाभ्यासी जैसे ही ईश्वर को छोड़ेगा तुरन्त प्रकृति, विकृति, अथवा जीव की उपासना में लग जाएगा और अज्ञानान्धकार-क्लेशयुक्त हो जाएगा ।
८३. प्राप्त, अभ्यस्त वस्तु के लिए विशेष बल नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति तथा उसके साथ अन्य कार्य भी किया जा सकता गाड़ी भी चला रहा है और अन्य कार्य सोचना, विचारना, लेना- देना, दूरभाष आदि भी करता रहता है वैसे ही योगी सभी कार्य करता हुआ अपनी स्थिति बनाए रखता है तथा मन के द्वारा बड़ी सूक्ष्मता से अनेक ज्ञान ग्रहण करता है ।
८४. योगी की समाधि लगी रहती है और अन्य भी विचार करता है, जैसे समाधि में ईश्वर की उपासना वेदमन्त्रों से करता हुआ मन्त्रों के अर्थ, धातु, प्रत्यय आदि भी सिद्ध करता रहेगा। इस प्रकार ईश्वर की उपासना भी चलती रहेगी और यह सभी कार्य करते हुए ईश्वर से उस विषय में ज्ञान भी प्राप्त करेगा ।
८५. पूर्वजीवन में किए दोषों, त्रुटियों को स्मरण करके बार-बार दु:खी, निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे कोई लाभ विशेष नहीं होगा। अन्तिम उपाय यही है कि जब से सत्य का बोध हो गया तभी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ आरम्भ करना चाहिए ।
८६. यदि किसी एक भी व्यक्ति से आपका वैर, ईष्ष्या, द्वेष शेष रहा तो वही योग में पर्याप्त बाधक बन जाएगा। यदि उपेक्षा भी रखनी है तो मन में उसके कल्याण की भावना हो। अच्छा तो यह है कि संसार के सभी व्यक्तियों से प्रेम हो। यम नियमों का सार्वभौममहाव्रत के रूप में पालन करते हुए सभी को मित्र बनाए रखना कठिन है ।
८७. हमारे साथी सहयोगी भले ही दोष अधिक करते हैं पुनरपि उत्तम व्यवहार यही है कि जो सेवा उन्होंने की उसकी प्रशंसा करना और दोषों को न देखना, न बताना; इससे व्यक्ति अपना बना रहता है। अन्यथा तो उसके मन में निराशा की भावना आएगी कि मैंने सेवा भी की उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकला, उसका साहस टूटेगा। मन में क्षमा, सहनशीलता, दया, करुणा की भावना बनाए रखना। इससे ही योग मार्ग पर स्थिर रह सकते हैं। ये आत्मा के नैमित्तिक गुण हैं, निमित्त से ही आते हैं। इसलिए ज्ञानपूर्वक इस प्रकार की भावना बनानी चाहिए और व्यवहार में लाने से अभ्यास हो जाएगा।
दोष-दर्शन
- १. व्यक्ति को प्रायः अन्यों के दोष देखने और उन्हें दूसरों को बताने में सुख मिलता है तथा दोष देखते-देखते व्यक्ति का स्वभाव इतना बिगड़ जाता है कि वह केवल दोष ही देखना प्रारम्भ कर देता है। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है ।
- २. जो वास्तव में योगाभ्यासी है उसे अपने में ही इतने दोष दिखाई देते हैं कि उन दोषों को जानने; उनको दूर करने के लिए जो उपाय, प्रयत्न किए जाते हैं उन उपायों, प्रयत्नों का प्रयोग करते हुए अवकाश ही नहीं मिलता ।
- ३. योगाभ्यासी के मन में केवल यही इच्छा रहती है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति की योग्यता बनानी है। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या द्वेष आदि वितर्कों को उठाने का समय ही नहीं मिलता। क्योंकि उसके पास, अपने दोषों को जानने, उनको दूर करने के लिए उपाय, प्रयत्न करने का इतना कार्य होता है कि मन पर वृत्तिक बनना पड़ता है। यदि वह इस प्रकार के हानिकारक और अनावश्यक पूर्ण रूप से नियन्त्रण, मौन, गम्भीर, अन्तः वृत्तिक बनना पड़ता है। यदि वह इस प्रकार के हानिकारक और अनावश्यक विचारों और वस्तुओं का संग्रह करता रहे तो इन सूक्ष्म विषयों को जान नहीं सकता और इसके संग्रह से स्वयं को क्लेशों से पिसता हुआ भी देखता है। इसलिए कहा जाता है कि योगाभ्यासी को तो किसी से भी कोई शिकायत ही नहीं रहती। वह तो केवल अपनी ही उन्नति व दोषों को दूर करने में लगा रहता है ।
- ४. सामनेवाला यदि दोष करता है तो योगाभ्यासी सोचता है कि यह मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं रहा है। ईश्वर की सृष्टि है। यदि सामने वाला दोष करेगा तो ईश्वर ही न्याय करेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल अपना कार्य ठीक, व्यवस्थित , सत्य और न्याय के अनुकूल करना है ।
- ५. योगाभ्यासी बौद्धिक दृष्टि से स्वयं को, सामनेवाले को मृत्यु के मुँह में देखता है तो उसे राग, द्वेष, ईष्ष्या आदि करने की बात ही नहीं सूुझती। जिसका आध्यात्मिक स्तर इस प्रकार का नहीं है अथवा लौकिक वृत्तियुक्त है, बही इन बातों को सोच सकता है।
- ६. अपने साथ रहनेवाले को इतना निर्भीक बना देना चाहिए कि वह नि:संकोच हमारा दोष बता दे। दोष बताने पर प्रसन्नता से स्वीकार करके हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि दोष बताकर वह हमारा उपकार कर रहा है। यदि दोष ठीक बताया है तो उसे दूर करें। यदि मिथ्या दोष बताया है तब भी उसे प्रसन्नतापूर्वक सुन लें ।
- ७. जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में तत्पर नहीं रहता और अत्यन्त पुरुषार्थ नहीं करता तब तक योग मार्ग पर बढ़ सके और ईश्वर प्राप्ति कर सके, ऐसा असम्भव है ।
- ८. यह नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी बुद्धि शत-प्रतिशत एक जैसी अर्थात् अनुकूल हो इसलिए विरोध होगा ही, तो व्यर्थ है कि हम इसके विपरीत सोचें कि सभी मेरे अनुकूल ही आचरण करें। इसलिए व्यक्ति जो राग, ढ्वेष, ईर्ष्या आदि करता है वह इस नियम को ठीक प्रकार से नहीं जानता अर्थात् वह सभी को अपने अधीन, अनुकूल ही चलाना चाहता है। यह कारण हट जाने पर उपरोक्त दोष भी नहीं आएँगे ।
- ९. यह सारी सृष्टि ईश्वर की है। हमारे पास यह ईश्वर की धरोहर है। हमें अपना कर्तव्य कर्म करते रहना है। उसकी आज्ञा का पालन करना है। दूसरा करे या न करे उसकी ओर ध्यान नहीं देना। हाँ, यदि सामनेवाला जिज्ञासु हो, कुछ सुनना, जानना चाहे तो प्रेमपूर्वक उसे ईश्वर के नियम बता देने चाहिएँ। फिर भी यह इच्छा नहीं रखनी कि सामने वाला इन नियमों का पालन करे; ऐसा करने पर ही व्यक्ति वितर्कों से बच सकता है, निष्कामकर्मी बन सकता है।
- १०. संसार का यह नियम है कि यहाँ अच्छे-बुरे लोग होते ही हैं, इसलिए इस नियम को दृष्टि में रखते हुए, चाहे कोई कितना विरोध करे, दुर्व्यवहार करे परन्तु उसके प्रति ईष्ष्या, द्वेष नहीं करना ।
- ११. सामनेवाले से जितनी सहायता मिल रही है तथा जो उसके गुण हैं उनको ग्रहण करो, उनकी प्रशंसा करो इससे उसका उत्साह बढ़ेगा। जो दोष हैं उनकी उपेक्षा कर दो। यदि सामनेवाला दोष सुननेवाला हो और अपनी स्थिति न बिगड़ती हो तो प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक, दूसरे के सुधार के दृष्टिकोण से दोष बता सकते हैं ।
- १२. जब व्यक्ति समाधि में ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ता है तो अविद्या, अज्ञान, अन्याय, विषय-वासनाओं को हेय, त्याज्य, हानिकारक देखता है। जब वह ईश्वर से सम्बन्ध तोड़ देता है तो इनको प्रिय मानकर ग्रहण करता है। यह मापदण्ड है। इससे अपना-अपना परीक्षण कर लेना चाहिए।
- १३. सभी जीवात्मा मिलकर अपने ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति से सृष्टि में एक तिल का दाना भी न बना सकते, न पालन कर सकते और न ही विनाश कर सकते हैं ।
- १४. जब व्यक्ति ऐसा जान-समझकर व्यवहार में लाता है तो उसका सारा मिथ्या अभिमान नष्ट हो जाता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, गुणवान् हूँ। जिन वस्तुओं से अपना स्वामित्व जोड़ रखा था , वह भी छूट जाता है। वह देखता है कि प्रकृति तो जड़ होने से स्वयं कुछ नहीं कर सकती। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसमें इतना शक्ति सामर्थ्य है।
- १५. ईश्वर ही प्रकृति के परमाणुओं से सृष्टि बनाता, पालन करता और विनाश भी करता है। ईश्वर के दिए सामर्थ्य, ज्ञान, बल, साधनों से हम कुछ निर्माण, पालन, विनाश करने में समर्थ हो पाते हैं। जब व्यक्ति ऐसा जान लेता है तो ईश्वर उसे अत्यन्त प्रिय लगने लगता है। वह सारी सांसारिक वासनाएँ, विषय-सेवन छोड़ देता है। यह श्रवण,मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार से आनेवाली विद्या है।
- १६. यदि व्यक्ति ईश्वर से सम्बद्ध नहीं रहता तो परीक्षण कर सकते हैं कि जैसे ही विरोधी व्यवहार करनेवाली वस्तु सामने आएगी विशेषकर साथ रहने वाला यदि विपरीत व्यवहार करता है तो मन में क्लेश दुःख , क्षोभ बना ही रहता है। इधर ईश्वर किसी से क्षोभ नहीं करता, दु:खी क्लेशित नहीं होता जो ईश्वर से सम्बद्ध रहेगा वह भी क्षोभरहित क्लेशरहित होगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि जो उपाय बताए हैं वे योगमार्ग पर दृढ़ करनेवाले हैं। ऐसा ब्रह्मविज्ञान देनेवाला और सुननेवाला आज दोनों ही नहीं मिलते। शाब्दिक विद्या और उसे जाननेवाले तो बहुत हैं।
- १७. भले ही आज शाब्दिक विद्वान् हैं लेकिन वे यदि हमें ठीक बता रहे हैं तो भी उनका उपदेश ग्रहण करना चाहिए, चाहे उनका आचरण विपरीत हो अथवा आचरण में कमी हो। किन्तु जो केवल उनके गुणों को न देखकर दोषों को देखता है कि वे स्वयं तो आचरण नहीं करते, दूसरों को उपदेशमात्र देते हैं; वह कभी सीख नहीं सकता। वह विपरीत बुद्धिवाला व्यक्ति है।
- १८. जीवात्मा मूर्खतापूर्ण कार्य करता रहता है। वह स्वयं ही वितर्क उठाता है और स्वयं ही उससे संघर्ष करता है। फिर यह कहता है कि मन वितर्क उठाता है; कितना व्यर्थ का पुरुषार्थ है? जैसे कोई स्वयं तो कार को तेज चलाए टक्कर भी मारे और फिर कहे कि मैंने कुछ नहीं किया तो उसे सभी मूर्ख कहेंगे या नहीं?
- १९. जब कोई व्यक्ति विपरीत व्यवहार करता है तो भी मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं करना चाहिए, भले ही न्याय की दृष्टि से सामने वाले ने ठीक नहीं किया हो। क्योंकि ईश्वर कभी क्षोभ नहीं करता इसलिए हमें भी क्षोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर जो करता है वही धर्म है, सत्य है यह प्रमाण की प्रथम कसौटी है।
- २०. ऋषियों ने भी क्षोभ करना निषेध किया है, फिर जीवात्मा की पवित्रता, जिज्ञासा, आत्मवत् व्यवहार की दृष्टि से उचित है कि सामनेवाला स्वतन्त्र है, अत: वह अनुकूल भी कर सकता है प्रतिकूल भी कर सकता है परन्तु हमें क्षोभ नहीं करना चाहिए, साथ में यह भी सोचना चाहिए कि सभी की बुद्धि तो एक जैसी नहीं है तो कोई न कोई तो प्रतिकूल व्यवहार करेगा तब क्या हम ऐसे ही दुःखी, क्लेशित, क्षुब्ध होते रहेंगे । इस प्रकार सोचता विचारता व्यक्ति जब ईश्वर से जुड़़ता है तो ईश्वर के सान्निध्य से उसे ज्ञान, बल, साहस, पराक्रम, सहनशक्ति की प्राप्ति होती है।
मृत्युभय के कारण
(१) व्यक्ति मानता है कि मृत्यु के साथ मेरा भी अभाव हो जाएगा इससे व्यक्ति को भय होता है ।
(२) इस शरीर के छूटने पर किसी भी वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहेगा। जो उसने पुरुषार्थ से सुख और सुख के साधन एकत्रित किए हैं उन साधनों से उसका स्वामित्व और सुखभोग, यह सब छूट जाएगा; इससे डर लगता है ।
(३) व्यक्ति संसार में रहते हुए सारी उम्र दूसरों से सम्बन्ध जोड़ने, सुख-साधन जुटाने और भोगने में बिता देता है, अपने को अकेला नहीं रहने देता। मृत्यु हो जाने पर तो संसार की किसी भी वस्तु से सम्बन्ध नहीं रहता । जीवात्मा बिल्कुल अकेला रह जाता है। ऐसी विचित्र अवस्था देख-सोचकर उसे डर लगता है ।
(४) व्यक्ति को मृत्यु से इसलिए भी भय लगता है कि उसने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं अगला जन्म अच्छा मिलने की सम्भावना भी नहीं दिखती। बुद्धिमान् सत्याग्राही, धार्मिक व्यक्ति इससे भी प्रेरणा लेकर तुरन्त अच्छे कार्य प्रारम्भ कर देता है और बुरे को छोड़ देता है ।
(५) व्यक्ति की प्राय: इच्छा बनी रहती है कि मैं सदा जीता रहूँ, परन्तु ऐसा असम्भव है। इसलिए जब मृत्यु का विचार करता अथवा देखता है तो उसकी इच्छा का विघात होता है कि में तो झूठी इच्छा कर रहा हूँ तब उसे भयंकर डर लगता है ।
(६) पूर्वजन्म में मृत्यु से होनेवाले दुःख के संस्कारों के कारण से भी मृत्यु से भय होता है। क्योंकि इस जन्म में तो उसने मृत्यु दुःख का अनुभव किया नहीं फिर भी मृत्यु से भय होता है। अर्थात् पूर्वजन्मों में प्रत्यक्ष मृत्यु दुःख का अनुभव किया है । इससे जीव अनादि अनन्त भी सिद्ध होता है। यदि जीव भी मृत्यु के साथ ही मर जाता तो इस जन्म में मृत्यु भय न होता ।
मृत्युभय से बचने के उपाय➪
७. व्यक्ति क्यों जीवित रहना चाहता है? इसलिए कि जीवात्मा चेतन है, उसका स्वभाव है कि में सदा होश=चेतन अवस्था में रहूँ, वह भी उच्च-कोटि वाले मनुष्य शरीर में। जब व्यक्ति को यह निश्चित होता है कि मुझे अगला जन्म अच्छा मिलेगा अथवा मुक्ति मिलेगी तो उसका भय छूट जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय हैं ➢(i) ईश्वर, जीव, प्रकृति को अनादि अनन्त मानना ।
(ii) सब कुछ ईश्वर का ही मानना ।
(iii) सांसारिक पदार्थों में इच्छा न रखना, उनको अनित्य, अशुचि, दुःखयुक्त और अनात्मा देखना ।
८. यह एक नियम है कि किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव हो नहीं सकता। जीव तो काल की दृष्टि से अनादि, अनन्त है इसलिए उसके अभाव होने का भी प्रसंग नहीं उठता ।
९. सभी जीवात्माओं की सभी अवस्थाएँ होती हैं। यथा बन्ध, मोक्ष। बन्ध अवस्था में बाल्यावस्था से लेकर किशोर, युवा, प्रौढ, वृद्धावस्था आदि भी आएँगी। प्रवाह से अनादि काल से यह चक्र चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। ईश्वर ने यह उचित व्यवस्था बनाकर रखी है, इसे भी कोई तोड़ नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। ईश्वर ने ये नियम हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं, इनमें कोई दोष नहीं हो सकता, न ही इनसे उत्तम कोई नियम होगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, दु:खी नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए ।
१०. प्रत्येक जीवमात्र मोक्ष जैसी उच्चावस्था से लेकर नीच से नीच योनि में जाता है। यह ईश्वर का बनाया हुआ अटल नियम है, यही सत्य है। इसलिए इसी के अनुकूल ही वर्तना, व्यवहार करना चाहिए। यह पाँच कसौटियों में से एक कसौटी है । इनके अनुकूल जो वर्तता है वह सुखी रहता है अन्यथा दुःख को भोगता है ।
११. ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत ॥ अथर्ववेद ब्रह्मचर्य सूक्त। ब्रह्मचर्य का सेवन कर विद्वान् मृत्यु को जीत लेता है ब्रह्मचर्य कहते हैं - ब्रह्मणि चरितुं व्रतं शीलमस्य स ब्रह्मचारी - जिसका व्यवहार ब्रह्म= १. ईश्वर २. वेद ३. जितेन्द्रियता से सम्बन्धित है वह ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य के तीन स्तम्भ हैं जिनके आधार पर ब्रह्मचारी टिका रहता है। (i) ब्रह्म (ईश्वरोपासना) (ii) वेद (वेद - विद्या) (iii) ब्रह्मचर्य (जितेन्द्रियता) ।
i. ब्रह्मचारी जब विद्या पढ़ता, रोटी खाता, व्यायाम करता, व्यवहार करता है तो एक क्षण भी ईश्वर को नहीं छोड़ता। सदा ईश्वरोपासना में रहता है ।
ii. सदा सत्यविद्या ही ग्रहण करता है ।
iii. वीर्य-रक्षा करता है, इसके साथ मन आदि इन्द्रियों को संयम में रखता है,। किसी भी प्रकार से यमनियमों का भंग नहीं होने देता। उसका सारा जीवन असाधारण होता है। जो ऐसा जीवन जीएगा उसका सारा व्यवहार संसार से अलग ही होगा। वही योग की भूमि को प्राप्त करेगा। इससे अलग होकर इन तीनों में से किसी न किसी का भंग करेगा।
१२. ब्रह्मचारी के ये दोनों यज्ञ प्रतिदिन करने आवश्यक हैं ➢ ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ ।
(i) ब्रह्मयज्ञ - वेदादि शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना, संध्या, योगाभ्यास करना।
(ii) देवयज्ञ - श्राद्ध, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति करना।
१३. श्राद्ध - श्राद्ध नाम सत्य का है। जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए उसे श्रद्धा कहते हैं, जो श्रद्धा से कर्म किया जाए वह श्राद्ध है ।
संन्यास की न्यूनतम योग्यता
- (१) "दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्" के अनुसार वैराग्य की योग्यता लावे ।
- (२) लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा का त्याग करे ।
- (३) स्वाध्यायरूप में महर्षि दयानन्द कृत यजुर्वेदभाष्य का अध्ययन।
- (४) कम से कम ५ दर्शन व दस उपनिषदों का अध्ययन करे ।
- (५) आदर्शरूप में यम-नियमों का पालन करे ।
- (६) कम से कम दो घण्टे देनिक उपासना करे ।
- (७) दिनभर आत्मनिरीक्षण करे व योगदर्शन के २/५ सूत्र के अनुसार विद्या-अविद्या का दिनभर विवेचन करते रहे।
- (८) वैदिक संन्यासी के लक्षणों को जीवन में लाने का पूर्ण प्रयत्न करे ।
- (९) मन-वचन-कर्म से समस्त पदार्थों के साथ स्व-स्वामिसम्बन्ध का परित्याग व ईश्वर का सम्बन्ध स्वीकार करे ।
- (१०) मन-वचन-कर्म से निष्काम ही करना और सकाम कर्म न करना।
- (११) खान - पान पर पूर्णनियन्त्रण रखे, सात्विक भोजन ही करे।
- (१२) पारिवारिक-सम्बन्धों का पूर्णतया परित्याग कर सम्पूर्ण विश्व को एक ही दृष्टि से देखे ।
- (१३) ईश्वर-प्राप्ति ही मनुष्य (निज) जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इस बात को सन्देहरहित बनाना ।
स्वानुभवविशेष
ऐसा योग्य व्यक्ति जिसे ईश्वर संकल्पमात्र से अपना साक्षात् करवाता है, वह व्यक्ति चलते-फिरते, सकल व्यवहार करते अपनी स्थिति बनाए रखता है। उसका मन पूर्ण नियन्त्रण में रहता है। ऐसी स्थिति बनाने हेतु वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है मौन, गम्भीर, आवश्यक ही बोलना, देखना इस प्रकार से स्थिति परिपक्व करनी पड़ती है। किसी विशेष संकट की स्थिति में कुछ कमी आती है परन्तु वह योगी पुरुषार्थ से तुरन्त उसी स्थिति को बना लेता है। जब वह इसी स्थिति को छोड़ लौकिक स्थिति में जाता है तो तुरन्त उसे क्लेश सताने लगते हैं। इसलिए योगी ईश्वरप्रणिधान की स्थिति को नहीं छोड़ना चाहता। मेरी ऐसी स्थिति पहले आँख बन्द करके होती थी। परन्तु आगे मैंने आँख खुली रखकर भी ऐसी स्थिति परिपक्व बनाई। आँख खुली रखते समय सामने विषय का विशेष ज्ञान नहीं होता, अन्दर मन की स्थिति वैसी ही बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति दीवार को देख रहा है और अपनी प्रिय वस्तु को खा रहा है। जब तक वह अपनी प्रिय वस्तु का आनन्द लेता रहेगा तब तक उसे दीवार का विशेष ज्ञान नहीं होगा। जब वह दीवार के बारे में सोचेगा कि इसमें कितनी ईंटें, किस क्रम और व्यवस्था से लगाई है तो उसके आनन्द में कमी आएगी। इसी प्रकार योगी बाह्य विषयों को अपना विषय न बनाता हुआ भी अपनी स्थिति बनाए रखता है ।
🙏🙏🙏 नमस्ते 🙏🙏🙏


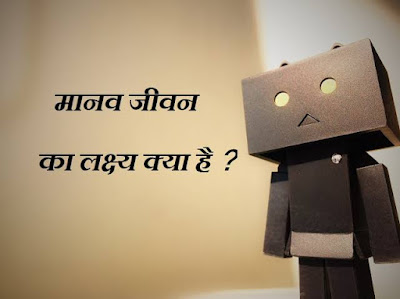







कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें