✍️ रणसिंह आर्य
वैदिक धर्म में जीवात्मा का स्वरूप
वैदिक धर्म में जीवात्मा का स्वरूप
जीवात्मा (स्वयं) के ज्ञान की आवश्यकता :-
जो जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी शक्ति, गुण, स्वरूप को जाने बिना ईश्वर को नहीं जान सकता। जब व्यक्ति शीशे में देखता है तो विचारता है कि मैं पुरुष वा सत्री हूँ। काला, गोरा, नाटा, बालक, वृद्ध हूँ। यह मिथ्या ज्ञान है। परन्तु में स्त्री, पुरुष आदि शरीर वाला हूँ यह विचार करना चाहिये। आज व्यक्ति ने पृथ्वी का चप्पा-चप्पा खोज मारा, चन्द्रमादि ग्रहों तक पहुँच गया है; प्राकृतिक (भौतिक) अनेक पदार्थों को जान लिया है, परन्तु स्वयं के बारे में मानव को बहुत अल्पज्ञान है।
परिभाषाएँ व सिद्धान्त बदल जाने से विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। कुरान-बाईबल में आत्मा के बारे में बहुत कम बातें लिखी हैं। जो लिखी हैं वे भी प्राय: गलत हैं। जैसे मनुष्य को छोड़कर किसी में आत्मा नहीं मानी। स्त्री में पूरी आत्मा मानते ही नहीं। पाकिस्तान में स्त्री को आधी आत्मायुक्त मानने से उसे चुनाव में आधे वोट का अधिकार है ।
अग्नि आदि भौतिक पदार्थों के बारे में हमारा जैसा व्यावहारिक ज्ञान है, वैसा आत्मा के बारे में भी हो । मुझ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती इतना समझ लेने मात्र से कितनी शक्ति व निर्भयता आ जाती है। दयानन्द पर विष प्रयोग हुआ, मतीदास को चीरा गया, वैरागी की खाल नुचवायी गई, गुरु गोविन्दसिंह के बच्चे दीवार में चिनवाये गये, कोई कढ़ाई में तले गये, परन्तु उन्होंने आत्मा का सच्चा नित्य स्वरूप
जानकर कहा कि हमारे आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने अपने अनित्य शरीर को आत्मा नहीं माना। आत्मा को जानकर व्यक्ति महान् सामर्थ्यवान् हो जाता है। यह वास्तविक ज्ञान के कारण है।
जीवात्मा का कोई रंग-रूप नहीं, कोई भार नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुओं में रंग, रूप, स्पर्श, लम्बाई, चौड़ाई आदि गुण पाये जाते हैं वैसे जीवात्मा में नहीं हैं।
एक रोचक बात; एक पुस्तक है "५०१ आश्चर्यजनक तथ्य" उसमें जीवात्मा का भार लिखा है कि जीवात्मा २१ ग्राम का है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। मरते हुए एक व्यक्ति को एक बक्से में बन्द करके तुला में तोला गया। थोड़े काल में वह मर गया अर्थात् आत्मा निकल गई उसे फिर तोला गया तो २१ ग्राम भार कम हुआ। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवात्मा २१ ग्राम का है। अब इस २१ ग्राम में कितनी चींटियाँ समा जायेंगी? हजारों... कितना अज्ञान है आत्मा के विषय में।
जैनी लोग कहते हैं कि आत्मा घटता-बढ़ता है। हाथी में जायेगा तो बढ़ जायेगा, चींटी में जायेगा तो घट जायेगा ।
सत्य वैदिक सिद्धान्त यह है कि जीवात्मा अपरिणामी होने से घटता-बढ़ता नहीं है व अभौतिक वस्तु होने से स्थान नहीं घेरता। एक सुई की नोक में विश्व के सभी जीवात्मा समा सकते हैं ।(२) इन्द्रियान्तरविकारात् । (न्याय द. ३/१/१२) हमने कभी नीबू खाया था, मिष्टान्न खाया था। बहुत स्वादिष्ट था । कालान्तर में वही भोग्य वस्तु (नीबू, मिष्टान्न) दिखाई दी तो मुंह में पानी भर आया। देखा आँखों से, लार आई मुंह में। अत: इन दोनों को जोड़ने वाला हमारे शरीर में है, वह जीवात्मा है।
(३) सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात् । (न्याय द. ३/१/७) हम दोनों आंखें बन्द करते हैं। एक नई वस्तु को बाँयी आँख से देखा, उसी को दाँयी से देखा और ज्ञान बन रहा है कि जिसको बाँयी आँख से देखा था उसी वस्तु को दूसरी दाँयी आँख ने देखा। इस ज्ञान को जोड़ने वाला आत्मा है।
(४) इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगम् ।(न्याय द. १/१/१०) ईच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान जिस वस्तु में हों वहाँ आत्मा की सिद्धि होती है। (५) षष्ठीव्यपदेशादपि । (सांख्य द. ६/३) मेरी आँख, मेरा कान, मेरा नाक, यह स्वामित्त्व भावना वाला आत्मा है।
(६) देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् । (सांख्य द. ६/२) आत्मा के लक्षण शरीर, इन्द्रिय आदि से भिन्न प्रकार के होने से वह इन शरीर, इन्द्रिय आदि से अतिरिक्त ( भिन्न-पृथक्) है।
(७) अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम् । (वैशे.द.३/२/९) "मैं हूँ" यह प्रत्यक्ष अनुभव है सो सिद्ध होता है कि आत्मा है। "मैं हूँ" की अनुभूति यह प्रत्यक्ष ज्ञान है।
(८) अनुमान प्रमाण - इन्द्रियों के विषय बन्द करके फिर स्थिर आसन में शरीर की अनुभूति भी बन्द होने पर जब विचार भी समाप्त हो जायें तो जो शेष रहे वह "मै हूँ" आत्मा है।
see also: वेद सौरभ (भाग २)
जीवात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप
जीवात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप
(१) आत्मा एक सत्तात्मक चीज है, वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है क्योंकि उसमें गुण हैं। जिसमें क्रिया हो, गुण हो अथवा केवल गुण हो; गुणों को धारण करने वाला द्रव्य-पदार्थ-वस्तु कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि जो जगह घेरे और ठोस हो वही द्रव्य हो। अतः प्रकृति के साथ साथ जीव-ईश्वर भी वस्तु हैं।
गुण - आत्मा के नैमित्तिक और स्वाभाविक दोनों गुण है। स्वाभाविक गुण, ज्ञान, प्रयत्न आदि। नैमित्तिक गुण सुख, दु:ख आदि। "मै हूँ" इतना ज्ञान अर्थात् अपने अस्तित्त्व का ज्ञान ही स्वाभाविक है शेष चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह नैमित्तिक है।
कर्म - ईश्वर प्रदत्त उपकरणों के बिना जीव का सामर्थ्य निरुपयोगी है। जीव मोक्ष में बिना प्राकृतिक साधनों के ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष-सुख अनुभव करता है। जब शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति होती है तो पाप कम हो जाते हैं। शक्तियाँ व्यर्थ नहीं जातीं। जीवन बदल जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने विषय होते हुए भी उसका भोग नहीं करता। उसमें सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करता। ज्ञान तो होता है पर सुख की अनुभूति नहीं करता। यह तभी सम्भव है जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानें।
(२) जीवात्मा का स्वरूप :- जीवात्मा नित्य अनादि, काल की दृष्टि से अनन्त, निर्विकार, निराकार, अल्पज्ञ, एकदेशी, अल्पशक्तिमान् है। तात्त्विक दृष्टि से अविकारी है।
मनुष्य की देह जड़ है और आत्मा चेतन है। इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं। कर्त्तृत्व उसकी शक्ति है। अहंज्ञान उसका स्वरूप बोधक है। जीवात्मा भी अनादि है और मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। उसकी शक्ति परिमित है। स्वभाव से अपूर्ण है। वह कर्मानुसार अनेक लोकों में भ्रमण करता है और मुक्त होकर परमात्मा में विश्राम करता है।
(३) शरीर में रहता कहां है ?- जीवात्मा स्थान विशेष हृदय में रहता है। कई मानते हैं मस्तिष्क स्थित हृदय में और कई वक्ष स्थल के मध्य। महर्षि दयानन्द जी ने वक्षस्थलवाला हृदय कहा है। दो स्तनों के बीच, कण्ठ से नीचे नाभि से ऊपर हृदय प्रदेश में। उपनिषद् में ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा का स्थान एक न होकर अनेक हैं। महर्षि दयानन्द ने कहा है जीवात्मा को सुख-दुःख भोगने के लिये कई स्थान ईश्वर ने बनाये हैं। स्थान विशेष में ईश्वर ने बाँधा नहीं, पर जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर के साथ रहता है। इसका संकेत ब्रह्मोपनिषद् के एक प्रकरण में आया है कि जीव के शरीर में तीन स्थान हैं। जागृत अवस्था में आँखों में। हम एक दूसरे को, तथा पशु भी आंखों में देखते हैं। स्वप्न में कण्ठ में और सुषुप्ति काल में हृदय में रहता है। अनेक सम्प्रदाय जैसे ब्रह्माकुमारी मानते हैं कि सब योनियों के अलग अलग प्रकार के जीवात्मा हैं, कुत्ते का आत्मा सदा कुत्ता ही रहेगा (जन्मेगा)। परन्तु यह वेद और ऋषियों से उलटी मान्यता है। सब जीवात्माएँ एक ही प्रकार की हैं। परन्तु कर्मानुसार अलग-अलग योनियों को प्राप्त होती हैं।
प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण पर मतभेद होने पर केवल अनुमान प्रमाण ही वस्तु को शतप्रतिशत सत्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। यदि पूर्णरूप से सिद्ध न करे तो वह अनुमान प्रमाण नहीं, वह सम्भावना कहलायेगा।
(४) नित्यता :- जीव व ईश्वर 'कूटस्थ नित्य' और प्रकृति 'परिणामी नित्य' है।
(५) लिंग : - जीवात्मा में स्त्री, पुरुष वा नपुंसक लिंग भेद नहीं है ।
(६) आकार :- बहुत ही सूक्ष्म अणुरूप है। इतना सूक्ष्म जीव हाथी जैसे बड़े शरीर और अतिसूक्ष्म जीवाणु के शरीर को चला लेता है। आत्मा अभौतिक है वह हजारों स्टील की परतों को भी पार कर सकता है।
(७) क्या जीवात्मा जन्म लेता और मरता है ? जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है वह अजर है, अमर है, नित्य है। अनादि, अनन्त है। जब जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर से होता है तो कहते हैं जन्म; शरीर छोड़ता है तो मृत्यु।
(८) जीवात्माओं की संख्या कितनी हैं ? :- जीवात्माएँ अनन्त हैं। हम जीवात्माओं की संख्या की परिगणना नहीं कर सकते। केवल एक भवन में कितने मच्छर, मकड़ी, चींटी हैं और सब भवनों में कितनी हैं कोई गणना कर सकता है ? कोई नहीं कर सकता। किन्तु ईश्वर जानता है। ईश्वर की गणना में जीवात्मा सीमित हैं। हमारे लिये असीमित हैं ।
(९) जीवात्मा के शरीर कितने हैं ? कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीन हैं। कारण शरीर 'प्रकृति' सब का समान है। सूक्ष्म शरीर १८ त्त्वों का सृष्टि के आदि में मिलता है। जब तक मुक्ति या प्रलय न हो जाये तब तक रहता है। यह १८ तत्त्व प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ तन्मात्रायें, १ मन, १ अहंकार और एक बुद्धि। किन्हीं प्राणियों में भले ही गोलक न हों, पर इन्द्रियाँ रहती हैं। जैसे सांप के पैर भले ही न हों, पर पाद कर्मेन्द्रिय होती है।
(१०) आत्मा की शरीर में कितनी अवस्थाएँ हैं ? - आत्मा की शरीर में चार अवस्थाएँ हैं। एक जाग्रत, दूसरी स्वप्न, तीसरी निद्रा (सुषुप्ति) और चतुर्थ तुरीय जो कि समाधि अवस्था है।
(११) जीवात्मा के शरीर में कोष कितने हैं ? - जीवात्मा के शरीर में पांच कोष हैं। ये पांच अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय हैं ।
(१२) क्या जीवात्माओं में भेद हैं ? - नहीं, सब जीवात्माएँ समान हैं। स्वरूप व स्वभाव से कोई भेद नहीं। भेद का कारण न्यूनाधिक ज्ञान-विज्ञान, संस्कार व कर्म हैं ।
(१३) जीवात्मा में शक्तियाँ कितनी हैं ? - जीवात्मा में २४ प्रकार की शक्ति देखने, सुनने, विचारने, निर्णय लेने आदि की हैं। जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से आनन्द लेता है ।
(१४) जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब तक करता है ? - जीवात्मा नये कर्मों को करने और किये कर्मं का फल पाने के लिये शरीर धारण करता है। कब तक करता है? जब तक अविद्या रहती है। जन्म-मरण का चक्कर अविद्या के कारण है। ईश्वर के सानिध्य से अज्ञान समाप्त हो जाये तो आवागमन का चक्कर भी समाप्त ।
(१५) जीव की मुक्ति और बन्धन क्या है ? दु:खों से छूट जाना मुक्ति है "ज्ञानान्मुक्ति, बन्धो विपर्ययात्" जब जीवात्मा अज्ञानी होता है तो बद्ध हो जाता है और ज्ञानी होने पर मुक्त। जब प्रकृति से छूटता है तो दु:ख उत्पन्न नहीं होता, वह ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जो व्यक्ति अपने अविद्या के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पहुंचा देता है वह मुक्ति में पहुँचता है। बचे हुए शेष कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति के बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है।
(१६) मुक्ति कितने समय तक रहती है ? ३१ नील, १० खरब, ४० अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति के आनन्द को भोगता है ।
(१७) एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने में कितना समय लगता है ? बहुत थोड़ा काल लगता है। उपनिषद् में है कि "जैसे एक कीड़ा अपने एक पांव को उठाकर आने वाले स्थान में रखता है उतना काल लगता है"। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टे, प्रत्येक निमिष काल में ब्रह्माण्ड में प्राणी लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अपवाद भी हैं। कोई महान् जीवात्मा जिसे महान् घर में जन्म लेना है, यदि ऐसा परिवार उस समय नहीं है तो उस जीवात्मा को थोड़े काल के लिये ईश्वर अपनी व्यवस्था में रखेगा। फिर उसे योग्य परिवार मिलने पर जन्म देगा ।
(१८) क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से एक शरीर को छोड़ बाहर जा सकता है ? नहीं। ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा बांध दिया है कि जब तक शरीर नष्ट-भ्रष्ट न हो जाये नहीं निकलेगा ।
(१९) शरीर के अन्दर कत्त्ता कौन और भोक्ता कौन है ? एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है, लोग शरीर को ही कतर्ता मान लेते हैं। पर नहीं, आत्मा कर्त्ता है, भोक्ता भी वही है। मन, शरीर आदि नहीं। फिर भोजन कौन खाता है? न केवल शरीर खाता है न केवल आत्मा खाता है। हम चाहे कितना ही खायें आत्मा तो उतना ही रहता है। और केवल शरीर भी आत्मा के बिना नहीं खा सकता। जिस शरीर में जीवात्मा है वह अपने उस शरीर की रक्षा के लिये
अपने शरीर को खिलाता है। पर सुख-दुःख की अनुभूति जीवात्मा करता है।
(२०) प्रलय में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है ? प्रलय में बद्ध जीवात्मा मूर्च्छित अवस्था (बेहोशी) में रहते हैं और जो मुक्त जीवात्मा हैं। वो आनन्द में रहेंगे।
(२१) मृत्यु समय शरीर कैसे छोड़ता है ? कोई कहते हैं कि मृत्यु होने पर जीवात्मा कान से, आँख से, मुंह आदि से अथवा सिर फोड़ के निकलता है। यह ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, वह कहीं से भी निकल जायेगा। उसके लिये कोई अवरोधक नहीं, कहीं से भी जा सकता है।
(२२) क्या एक जीवात्मा दूसरे के द्वारा किये कर्मों का फल प्राप्त करता है ? नहीं, किंचित् मात्र भी नहीं। दूसरे के किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता, लेकिन दूसरे के किये हुए कर्मों से सुख-दुःख भोगता है।
(२३) क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है ? नहीं। जीवात्मा ईश्वर में रहता है, परन्तु अंश नहीं है। अगर यह ईश्वर का अंश होता तो सदा आनन्दित होता। मूर्ख-अज्ञानी नहीं होता।
(२४) क्या जीव और ईश्वर में समानता है ?
उत्तर - साधर्म्य गुणों से जीव और ईश्वर में समानता है, और वैधम्म्य गुणों से दोनों में भेद भी है।
समानता - दोनों नित्य, निराकार, अपरिणामी और निरवयवी हैं।
see also: वेद सौरभ (भाग १)
मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना न तो स्वयं पूर्णरूपेण सुखी हो सकता है न अन्यों को कर सकता है। आज करोड़ों व्यक्ति पशु-पक्षी की आत्मा को आत्मा ही नहीं समझते। किसी वस्तु से सम्बन्धित परिभाषा बदल जाने से व्यवहार बदल जाते हैं। इस उलटे ज्ञान से आज पशु-पक्षियों के साथ अनर्थ, उनका विनाश हो रहा है। हम भी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, यह हमारा अज्ञान है।
विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं पर आत्मा का विषय नहीं पढ़ाया जाता। जिस अज्ञान के कारण पशु-पक्षी दु:खी रहते हैं उससे स्वयं मानव भी दुःखी व अशान्त है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, चाहे भौतिक उन्नति कितनी ही क्यों न कर ली हो ।
जीवात्माएँ स्वरूप से सब समान हैं, पर कर्मानुसार अलग अलग योनि मिलती है। मस्तिष्क हमारे अंत:करण मन का कार्यालय (गोलक) है । मुमुक्षु व्यक्ति मन को प्रकृति की सड़क से मोड़कर ईश्वर की राह पर मोड़ देता है।
शरीर के विषय में जब तक हमारा ज्ञान व्यावहारिक, क्रियावाला, जीवन में नहीं उतरता तब तक फलदायी नहीं होता जैसे बिजली के तार को छूना = मरना है । जहर लें या सर्प काटे तो मृत्यु का भय होना यह व्यावहारिक ज्ञान होने से व्यक्ति इनसे बचता है। शरीर के विषय में यह अयथार्थ ज्ञान है कि यह शरीर न बूढ़ा होगा न मरेगा ही। यह नित्य, पवित्र, चेतन मात्र सुखदायी है, ऐसा मानकर इससे प्यार-मोह करना अज्ञान (अविद्या) दोष है।
यथार्थ ज्ञान - यह सुन्दर दिखने वाला शरीर गन्दगी का घर है। इसमें से प्रत्येक क्षण पसीना आदि मल निकलते रहते हैं। मुख में हलवा डाल कर कुछ देर रखने के बाद निकालने पर देखने को मन न हो। जहाँ यह उल्टी करे वहाँ कोई बैठे भी नहीं। शुद्ध वायु ली, छोड़ने पर विषैली गन्दी। शरीर की चमड़ी हटाने पर क्या उसे देखने, चूमने को लालायित होगा? क्या सुन्दर बाल खाने में लेंगे? ईश्वर की कृपा है कि अपनी माया से इस शरीर को सुन्दर चमड़ी से ढका हुआ है। इसके अन्दर मांस मज्जा, नसों के जाल, कंकाल व मल भरे हैं। कुष्ठ, चेचक आदि रोग होने पर किसके मन को भायेगा। विवेक होने पर शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जायेगी। कितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, मृत्यु होने पर कोई छूना भी नहीं चाहेगा ।
शरीर से उपयोग लेना है, पर यह भोग्य नहीं है। इससे ईश्वर प्राप्ति करनी है। इसमें आसक्त न होकर त्यागपूर्वक भोग करना है। स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास छोड़ देने से निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक या अभावात्मक में बदल जाता है। अनभ्यास के कारण विवेक दबकर चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि को ठीक मानने लग जाता है। सुन्दर कपड़ों में सुन्दर शरीर पर आसक्त डाक्टर को उसी सुन्दर शरीर का आपरेशन करते समय वासना नहीं उभरती। वहाँ उसका विवेक काम करता है। वस्तु को गहराई से जानकर ज्ञान को दृढ़ बना लें ।
लोक (संसार) में मानव जो कार्य करता है दूसरे से सम्बन्धित होकर करता है। अपने अकेले से कुछ भी कार्य स्वतन्त्र रूपेण नहीं कर सकता। संसार में जो व्यक्ति अपने से सम्बन्धित लोगों को जानकर, उनसे उचित व्यवहार करता है वह सफल होता है। यदि गुरु-शिष्य का उचित सम्बन्ध नहीं है तो विद्या नहीं सीखी जाती है जो स्वयं से भी उचित व्यवहार नहीं करना जानता, वह सफल नहीं हो सकता।
जीवात्मा तथा शरीर सम्बन्धी ज्ञान
जीवात्मा तथा शरीर सम्बन्धी ज्ञान
मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना न तो स्वयं पूर्णरूपेण सुखी हो सकता है न अन्यों को कर सकता है। आज करोड़ों व्यक्ति पशु-पक्षी की आत्मा को आत्मा ही नहीं समझते। किसी वस्तु से सम्बन्धित परिभाषा बदल जाने से व्यवहार बदल जाते हैं। इस उलटे ज्ञान से आज पशु-पक्षियों के साथ अनर्थ, उनका विनाश हो रहा है। हम भी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, यह हमारा अज्ञान है।
विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं पर आत्मा का विषय नहीं पढ़ाया जाता। जिस अज्ञान के कारण पशु-पक्षी दु:खी रहते हैं उससे स्वयं मानव भी दुःखी व अशान्त है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, चाहे भौतिक उन्नति कितनी ही क्यों न कर ली हो ।
जीवात्माएँ स्वरूप से सब समान हैं, पर कर्मानुसार अलग अलग योनि मिलती है। मस्तिष्क हमारे अंत:करण मन का कार्यालय (गोलक) है । मुमुक्षु व्यक्ति मन को प्रकृति की सड़क से मोड़कर ईश्वर की राह पर मोड़ देता है।
शरीर के विषय में जब तक हमारा ज्ञान व्यावहारिक, क्रियावाला, जीवन में नहीं उतरता तब तक फलदायी नहीं होता जैसे बिजली के तार को छूना = मरना है । जहर लें या सर्प काटे तो मृत्यु का भय होना यह व्यावहारिक ज्ञान होने से व्यक्ति इनसे बचता है। शरीर के विषय में यह अयथार्थ ज्ञान है कि यह शरीर न बूढ़ा होगा न मरेगा ही। यह नित्य, पवित्र, चेतन मात्र सुखदायी है, ऐसा मानकर इससे प्यार-मोह करना अज्ञान (अविद्या) दोष है।
यथार्थ ज्ञान - यह सुन्दर दिखने वाला शरीर गन्दगी का घर है। इसमें से प्रत्येक क्षण पसीना आदि मल निकलते रहते हैं। मुख में हलवा डाल कर कुछ देर रखने के बाद निकालने पर देखने को मन न हो। जहाँ यह उल्टी करे वहाँ कोई बैठे भी नहीं। शुद्ध वायु ली, छोड़ने पर विषैली गन्दी। शरीर की चमड़ी हटाने पर क्या उसे देखने, चूमने को लालायित होगा? क्या सुन्दर बाल खाने में लेंगे? ईश्वर की कृपा है कि अपनी माया से इस शरीर को सुन्दर चमड़ी से ढका हुआ है। इसके अन्दर मांस मज्जा, नसों के जाल, कंकाल व मल भरे हैं। कुष्ठ, चेचक आदि रोग होने पर किसके मन को भायेगा। विवेक होने पर शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जायेगी। कितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, मृत्यु होने पर कोई छूना भी नहीं चाहेगा ।
शरीर से उपयोग लेना है, पर यह भोग्य नहीं है। इससे ईश्वर प्राप्ति करनी है। इसमें आसक्त न होकर त्यागपूर्वक भोग करना है। स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास छोड़ देने से निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक या अभावात्मक में बदल जाता है। अनभ्यास के कारण विवेक दबकर चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि को ठीक मानने लग जाता है। सुन्दर कपड़ों में सुन्दर शरीर पर आसक्त डाक्टर को उसी सुन्दर शरीर का आपरेशन करते समय वासना नहीं उभरती। वहाँ उसका विवेक काम करता है। वस्तु को गहराई से जानकर ज्ञान को दृढ़ बना लें ।
आत्मा को आवश्यकता है ईश्वरानन्द की। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है, वही शत्रु भी है। ईश्वर जीव का सम्बन्ध पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। "त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।" (ऋ ८/९८/११) यदि इसको समझते हैं तो योग में सफल होंगे। यदि इसको नहीं जानते या ईश्वर से अयोग्य सम्बन्ध जोड़ते हैं तो विफल होंगे। लोक के माता-पिता से ईश्वर का मातृत्व-पितृत्व अधिक है। लोक में अच्छे धार्मिक पुत्र-पुत्रियां अपने माता-पिता से ठीक/अच्छे सम्बन्ध रखते हैं; परन्तु क्या उनके ईश्वर से भी ऐसे सम्बन्ध हैं ? यदि नहीं तो विफल होंगे। ईश्वर से तो नाम मात्र का सम्बन्ध रखते हैं। ईश्वर की सत्ता ही में संशय या भ्रान्ति होगी तो उसके साथ उचित व्यवहार क्या करेंगे? संशय दूर होने पर ही ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ने की बात होती है। हम सिद्धान्त में ईश्वर का और व्यवहार में टार्च का मूल्य अधिक समझते हैं। जब तक व्यवहार में ईश्वर के मूल्य का पता न लगे, तब तक उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा। साधकों को शब्द व अनुमान प्रमाण से ईश्वर को मान कर, संशय दूर करके फिर अभ्यास से प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव करना चाहिए।
व्यवहार में प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण करते रहना चाहिए। नाम और नामी का पता जिज्ञासु को होना चाहिए। नाम-नामी का अर्थ व फल जानने से विद्या प्राप्त होती है। हमारा पिता सर्वव्यापक ईश्वर 'ओ३म्' नाम वाला सर्वरक्षक है। उसके बिना संसार टिक नहीं सकता। जड़ पदार्थ और प्राणधारी सब उसके सहारे टिके हुए हैं।
(१) माता-पिता, राजा-गुरु:- वेद में ईश्वर को जीव का स्वामी, सहायक, सुहृद्-मित्र, माता-पिता, राजा और गुरु स्वीकार किया है। लोक में यह जीव अपने बच्चों की रक्षा ईश्वर की सहायता से करता है। अत: लौकिक माता-पिता से बड़ा माता-पिता ईश्वर है। लौकिक मां तो मोह-अज्ञानता के कारण, उलटे काम करने वाले अपने बालक को भी सारी सम्पत्ति का मालिक बना देती है; परन्तु ईश्वर ने यह धरती आर्य को दी 'आर्य ईश्वरपुत्रः' (निरुक्त) श्रेष्ठ, आज्ञाकारी, ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को धारण करने वाले उद्यमी को दी; अवज्ञाकारी, अनाड़ी सन्तान को नहीं। पिता की आज्ञानुसार चले सो पुत्र वरना नहीं। क्योंकि ईश्वर हमारा माता-पिता है, अत: यदि हम उस के विचार के साथ चलते हैं तो उसके पुत्र हैं, अन्यथा नहीं। ईश्वर के आदेश मानने पड़ेंगे यदि उसका पुत्र बनना चाहते हैं ।
(२) गुरु- शिष्य व स्वामी-सेवक सम्बन्ध - ईश्वर हमारा गुरु, हम उसके शिष्य हैं, ईश्वर स्वामी हम सेवक हैं तो उसकी आज्ञा, आदेश हमारे लिये क्या हैं? उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है, विरुद्ध चलना अधर्म, अन्याय, अविद्या, अज्ञान है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् आनन्द से परिपूर्ण होने से कभी भूल नहीं करता। ईश्वर परिपूर्ण है, अत: अपनी कमी पूर्ण करने हेतु कोई स्वार्थ का काम नहीं करता, जब कि लौकिक गुरु में ऐसी सम्भावना है। ईश्वर सर्वोपरि है अत: उसका निर्णय अन्तिम होगा। जब कोई कहे ये अच्छा, कोई कहे वह अच्छा, सो क्या अच्छा क्या बुरा यह अन्तिम निर्णय परम गुरु परमेश्वर का ही मान्य होगा।
(३) उपास्य-उपासक सम्बन्ध - ईश्वर भजनीय-उपासना करने योग्य है ऐसा समझकर उपासना करते हैं तो हम उसका लाभ उठा पायेंगे। एक वैज्ञानिक प्रकृति-विकृति की उपासना यह मानकर करता है कि उससे मेरा पूर्ण कल्याण हो जायेगा। उन सांसारिक वस्तुओं को उपास्य मानता है, जिनसे यह कामना कभी पूर्ण नहीं होती । चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक, धनवान्, चक्रवर्ती राजा हो जाये, प्रकृति-विकृति के उपासक कभी पूर्ण सुखी नहीं हुए । किसी के साथ सुख के लिये सम्बन्ध जोड़ना उसकी उपासना है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र, फल भोगने में ईश्वराधीन है, यह जीव-ईश्वर सम्बन्ध है।
संसार की उपासना में चार प्रकार के दु:खों से मिश्रित सुख मिलेगा, परन्तु ईश्वर की उपासना से ईश्वर का विशुद्ध ज्ञान, बल, आनन्द प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिये भी ज्ञान-कर्म-उपासना से रहित नहीं रह सकता। या तो संसार की उपासना या ईश्वर की उपासना बनी रहती है।
(४) व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध - जीव-ईश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध किस रूप में रहता है ? एक लोहे के गोले को तपाने के बाद अग्नि के अन्दर-बाहर गोला 'अग्निवत्' दिखाई देगा। गोला व्याप्य और अग्नि व्यापक है। जो अग्नि अन्दर-बाहर रहती है वह व्यापक और जिसके अन्दर रहे वह गोला व्याप्य। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो साधक ईश्वर को कहाँ ढूँढ़ता है ? लोक में जिस वस्तु को ढूँढ़ते हैं, वह प्राय: दूर होती है। इस तरह जो व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध को नहीं जानता, वह ईश्वर को भी नहीं जानता। उसे वह कहीं दूर ढूँढ़ते हुए प्राप्त करना चाहता है। साधक की पहली भूल-ईश्वर को कहीं दूर ढूँढ़ता है। दूसरा अपने निकट ऊपर-नीचे दायें-बायें तो स्वीकार करता है, पर शरीर में नहीं समझता। तीसरा बाहर मानता हुआ, अपने शरीर में भी खोजना आरम्भ करता है, परन्तु जीव स्वयं जहाँ रहता है वहाँ अपने आप को छोड़कर शेष शरीर में ईश्वर को खोजता है, क्योंकि उसको व्याप्य-व्यापक संबंध का सही ज्ञान नहीं। जब साधक यह जानेगा कि ईश्वर मेरे में भी है तभी तो उसे स्वयं में पा सकेगा। अपने को छोड़कर अन्यत्र ईश्वर को ढूंढ़ेगा तो कदापि नहीं मिलेगा ।
ईश्वर में गोता लगाने की विद्या आनी चाहिए। जैसे समुद्र में गोता लगाता है। अज्ञान, अधर्म जलाने पर लक्कड़रूपी संसार जल जाता है तो ज्ञानाग्नि में ईश्वर दीखने लगता है। शरीर, भोजन, मकान, भाई, पड़ोसी, बाजार आदि में व्यक्ति भूला रहता है। व्याप्य को व्यापक के प्रभाव से दबा देना चाहिए। व्याप्य (लक्कड़) का प्रभाव समाप्त हो तो व्यापक (अग्नि) का प्रभाव दीखेगा।
see also: स्वाध्याय का महत्व
ईश्वर के सम्बन्ध से व्यक्ति का निर्माण
ईश्वर के सम्बन्ध से व्यक्ति का निर्माण
ईश्वर की सहायता के बिना मानव निम्माण नहीं होता। जहाँ पाश्चात्यों का दर्शन समाप्त होता है वहां वैदिक दर्शन शुरू होता है। ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव और वेद का आदेश अन्तिम आदेश है। ईश्वर की आज्ञा मानने वाले को कोई डिगा नहीं सकता, चाहे मृत्यु भी क्यों न आ जाये। सत्य को जानने के लिये पाँच कसौटियाँ हैं (१) जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य। (२) जो-जो सृष्टिक्रम के अनुकूल वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य। जैसे कोई कहे, 'बिना माता-पिता के योग से लड़का हुआ' ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य मानना चाहिए (३) "आप्त" अर्थात् धार्मिक विद्वान् सत्यवादी सत्यमानी निष्कपटियों के उपदेशानुकूल। (४) अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दु:ख अप्रिय है वैसा सर्वत्र समझना। (५) आठों प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव के अनुकूल। अत: जो सत्य है उस पर डट जायें। असत्य को उखाड़कर फेंक दें। सत्य जानना, मानना, करना ही ईश्वर का काम है। हम भी सत्य पर चलेंगे। ईश्वर के निषेध को छोड़ेंगे और आदेश को मानेंगे। अच्छे कार्य से धन कमाएँ। जो अपने झूठ, छल-कपट, कुवासनाओं, अविद्या, चोरी आदि से सन्धि करता है, वह दूसरों की चोरी आदि से भी सन्धि कर लेता है। अपने दोषों को दूर करें तो अन्य के दोष दूर कर सकते हैं। जब हमारा पिता-माता-आचार्य-राजा ईश्वर है तो यह दो मुठ्ठी वाला मानव क्या हानि करेगा? सत्य कार्य को सिद्ध करो या मरो।
see also: ब्रह्म विज्ञान (भाग ३)
वैदिक धर्म में प्रकृति का स्वरूप
वैदिक धर्म में प्रकृति का स्वरूप
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।
(योग दर्शन २/१८)
समस्त मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अतः दृश्य =3 कार्य प्रकृति भी तीन गुणों वाली है, क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। सत्त्वगुण प्रकाशात्मक, रजोगुण क्रियाशील=प्रवृत्ति करने वाला और तमोगुण स्थितिशील = प्रकाश व क्रिया को स्थिर करने वाला होता है। यह दृश्य का स्वभाव बताया। फिर उसका स्वरूप बताया भूतेन्द्रियात्मक होना। 'भूत' शब्द से सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का ग्रहण है। 'इन्द्रिय', शब्द से बाह्य तथा आंतरिक दोनों इन्द्रियों का ग्रहण है। इस प्रकार महतत्त्व, अहंकार, पाँच सूक्ष्म भूत, ग्यारह इन्द्रियाँ और पृथ्वी आदि पांच स्थूल भूत तक सभी प्रकृति-विकृतियों का ग्रहण है। समस्त कार्य रूप यह जगत् 'दृश्य' कहलाता है।दृश्य का प्रयोजन - इस दृश्य जगत् का प्रयोजन पुरुष को भोग तथा अपवर्ग प्राप्त करना है। दोनों को जीवात्मा बुद्धि की सहायता से प्राप्त करता है। अत: यह बुद्धिकृत् कहलाते हैं। परन्तु बुद्धि अचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती। पुरुष की प्रेरणा से ही बुद्धि का समस्त व्यापार होने से बुद्धिकृत् भोग व अपवर्ग, पुरुष ही भोगता है। जैसे राजा के आदेश से योद्धा लड़ते हैं परन्तु इसका परिणाम 'हार जीत ' राजा की ही मानी जाती है, योद्धाओं की नहीं।
जीवात्मा बाह्य विषयों से सम्पर्क करने की इच्छा करता है तो बुद्धि से निश्चय करके मन को प्रेरित करता है और मन बाह्य इन्द्रियों को प्रेरित करता है। इसी प्रकार इन्द्रियों से जो भी ज्ञान होता है वह मन के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि के द्वारा पुरुष को मिलता है। अत: इस पुरुष के अतिशय निकट रहने वाली बुद्धि प्रधान मन्त्री की भाँति होती है। अत: हम भ्रम से बुद्धि को भोक्ता मानने लगते हैं। प्रकृतिजन्य प्रत्येक कार्य-वस्तु में ये त्रिगुण मुख्य- गौण भाव से रहते हैं। एक समय में एक ही गुण प्रधान होने से वह दूसरे गौण भाव प्राप्त दो गुणों पर हावी होकर अपना प्रभाव प्रकट करता है। ये सभी पृथक्-पृथक् अपनी शक्ति बनाये हुए प्रधान गुण के साथ सहकारी भाव से कार्य करते हैं। गौण रूप से रहने वाले गुण भी उचित अवसर तथा उपयुक्त निमित्त को पाकर अपने-अपने कार्यों को प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं अत: शान्त घोर और मूढ़ परिणामों का क्रम न्यूनाधिक रूप में सदा चलता रहता है।
"बुद्धेरेव पुरुषार्थऽपरिसमाप्तिर्बन्धः" (व्यास भाष्य) अर्थात् बुद्धि आदि जो सूक्ष्म शरीर के घटक हैं वे जन्मजन्मान्तर में भी पुरुष के साथ रहते हैं। पुरुष इनकी सहायता से ही सुख-दुःख का भोग करता है। अत: मोक्ष होने तक बुद्धि आदि पुरुष के लिये कार्य करते रहते हैं और इनके कार्य की समाप्ति न होना ही पुरुष का बन्धन है तथा "तदर्थावसानो मोक्षः'' (व्यास भाष्य) अर्थात् उस बुद्धि का कार्य जब विवेकख्याति होने पर समाप्त हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप को समझ लेता है, तो यह प्रकृति के सम्पर्क से पृथक् होना ही पुरुष का "मोक्ष" कहलाता है।
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ (सांख्य द. १/६१)
अर्थात् सत्त्व, रजस्, तमस् इन तीन वस्तुओं (गुणों ) के संघात का नाम प्रकृति है। प्रकृति से महत्त्व = बुद्धि बुद्धि से अहंकार, उससे पांच तन्मात्राएँ (सूक्ष्म भूत) और दस इन्द्रियाँ तथा ग्यारहवाँ मन, पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पांच स्थूलभूत ये चौबीस और पच्चीसवाँ पुरुष (= जीव और ईश्वर ) ये पच्चीस का गण है।
ईश्वर सृष्टिकर्ता, जीव भोक्ता, और प्रकृति भोग्या है। सृष्टि एक महायज्ञ है, इसके रचयिता ओ३म् (= ईश्वर) ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड (अनेक प्रकार के ब्रह्माण्ड) रचाये। इस संपूर्ण सृष्टि का राजा परमेश्वर है, जो कि महान् है। प्रकृति सूक्ष्म और जड़ है, जो कि ईश्वर के आधार पर रहती है। ईश्वर महान् व सूक्ष्मतम है। माता-पिता के वल कर्म करते हैं। रचना ईश्वर करता है। मातायें भोजन को केवल पेट में डालती हैं स्तनस्थ दूध ईश्वर बनाता है।
see also: ब्रह्म विज्ञान (भाग १)
सृष्टि रचना
सृष्टि रचना
लगभग दो अरब वर्ष पहले यह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रादि कुछ नहीं था। बद्ध जीवात्माएँ मूरचछित अवस्था में थीं। जैसे निद्रा में कोई अनुभूति नहीं होती उसी तरह प्रलयकाल में भी नहीं होती है। सत्त्व-रज-तम करणों को इकठ्ठा कर ईश्वर ने अपने ज्ञान-सामर्थ्य से महत्तत्त्व, फिर अहंकार, फिर पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, मन व पांच तन्मात्रायें (सूक्ष्मभूत) कुल अठारह तत्त्व, फिर पांच स्थूलभूत-उनसे सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी आदि यह स्थूल जगत बनाया। वनस्पति, मछलियाँ, कीट, पतंग, पशु आदि के उपरान्त अन्त में मनुष्यों के शरीरों की रचना हुई। मनुष्य सब युवा शरीरवाले उत्पन्न हुए। अमैथुनी सृष्टि बनी।
प्राणी उत्पत्ति चार प्रकार की है -
(१) जरायुज = मनुष्य, पशु आदि ।
(२) अण्डज = पक्षी, कीट आदि ।
(३) उद्भिज = वृक्ष आदि पृथ्वी में से निकलते हैं ।
(४) स्वेदज = पसीने से जुएँ, गेहूं आदि में कीड़े-कीटाणु आदि।
ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों को चार वेदों का ज्ञान दिया। १ अरब ९६ करोड़ ८ लाख ५३ हजार १२० वर्ष बीत गये अमैथुनी सृष्टि को हुए। ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष इस सृष्टि की कुल आयु है। फिर विनाश की प्रक्रिया होती है, जिसे विचार कर वैराग्य की भावना जगा सकते हैं। जीवन और पृथ्वी का आधार 'सूर्य की गर्मी', दो अरब कुछ करोड़ वर्ष उपरान्त कम होती जायेगी, तब इस पर आधारित मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति आदि धीरे-धीरे क्षीण होते-होते नष्ट हो जायेंगे। इस उत्पत्ति-प्रलय की प्रक्रिया से संसार की नश्वरता ज्ञात होती है व प्रलयावस्था के सम्पादन से वृत्ति निरोध होकर जीवात्मा ईश्वर की शरण में समाधि प्राप्त कर लेता है।
संसार सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान
पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। कोई वस्तु आकस्मिक (ओटोमैटिक) है ही नहीं। जो वस्तु संघातरूप (अवयववाली) है, जोड़कर बनी है वह अवश्य कभी बनी है, जैसे कपड़ा, घड़ा संघात से बना हुआ है। बनी हुई वस्तु नष्ट भी हो जायेगी। पृथ्वी संघात से बनी है तो वह जरूर टूटेगी। जिसने बनाई है वह तोड़ेगा। ये सब नाशवान् चीजें हैं।
पदार्थ
भोग
पञ्च क्लेश
(१) अविद्या - विद्या से अन्य अयथार्थ ज्ञान ही अविद्या है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महान् है तो भी इन चार विभागों के अन्तर्गत अविद्या का समावेश हो जाता है। 'अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या'। (यो. द. २/५)
१. अनित्य - अर्थात् कार्य जो शरीरादि स्थूल पदार्थ व लोकलोकान्तर में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य पदार्थ अर्थात् ईश्वर, जीव व जगत का कारण, इनमें अनित्य बुद्धि होना।
२. अशुचि - मलमूत्रादि के समुदाय, दुर्गन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना तथा तालाब, बावड़ी, कुण्ड, कुंआ और नदी में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत पीना, एकादशी
आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दु:खों को सहना। स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्य विद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता,
सर्वोपकार, सब में प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना।
३. दुःख में सुख बुद्धि अर्थात् विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईष्ष्या, द्वेषादि दुःख स्वरूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना; जितेन्द्रियता, निष्कामता, शम, सन्तोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दु:ख बुद्धि करना।
४. अनात्मा में आत्म बुद्धि अर्थात् जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। अविद्या से विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसी बुद्धि रखना 'विद्या' है इससे जीव बन्धन से छूट कर मुक्ति के आनन्द को प्राप्त करता है।
(२) अस्मिता - बुद्धि (मन-चित्त) को आत्मा से भिन्न न समझना ।
(३) राग - सुख में प्रीति यह राग है।
(४) द्वेष - दुःख में अप्रीति द्वेष है ।
(५) अभिनिवेश - सब प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ, मरू नहीं । मृत्यु दु:ख से त्रास अभिनिवेश कहाता है ।
इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के, ब्रह्म को प्राप्त होके, मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये।
क्लेशों की अवस्थायें पांच हैं -
(१) प्रसुप्त - जन्मजन्मान्तर में भोगे हुए भोगों के संस्कार जो सोये पड़े हैं।
(२) तनु - सतत् सत्संग, उपदेश आदि से जो कमजोर बन गये हैं वे
(३) विच्छिन्न - एक संस्कार उभरता, तो उससे विपरीत दबा रहता है। जैसे द्वेष की स्थिति में प्रेम का न उभरना।
(४) उदार - प्रकट या उभार की स्थिति। जैसे जवानी में प्रेम।
(५) दग्धबीजभाव - योग में विशिष्ट सिद्धि होने पर जले हुए दाने के समान।
see also: संकलित पोस्ट (भाग २)
संसार में स्थायी सुख नहीं
संसार में स्थायी सुख नहीं
जब तक संसार में दु:ख की अनुभूति नहीं करोगे, उस से नहीं ऊबोगे तब तक ईश्वर के सुख, ज्ञान, बल, आनन्द के प्रति रुचि नहीं होगी। संसार में सुख तो है पर पूर्ण सुख नहीं है। कोई न कोई दुःख लगा हुआ है। जो थोड़ा सुख है वह भी दु:ख मिश्रित है। अतः बुद्धिमान् ऋषि लोग उसे भी दुःख मानकर छोड़ देते हैं व पूर्ण सुख (=मुक्ति, ब्रह्मानन्द, ईश्वर प्राप्ति) चाहते हैं ।
(१) कुत्रापि कोऽपि सुखी न। (सांख्य ६/७) अर्थात् संसार में कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है ।
(२) विविधबाधनायोगाद् दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः। (न्याय ४/१/५५) अनेक प्रकार के दु:खों के साथ सम्बन्ध होने से शरीर में आना (जन्म लेना) दु:ख ही है।
(३) अथाऽतो ब्रह्म जिज्ञासा। (वेदान्त १/१/१) संसार को भोग कर देख लिया, दु:ख ही दुःख है। अब ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिये।
(४) आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे। (वैशे. द. ५/२/१५) आत्मा जब मन, इन्द्रिय व विषय के साथ सम्बद्ध होता है तब सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है।
(५) परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिन:॥ (यो. २/१५) इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें विवेकी व्यक्ति के लिये चार प्रकार का दुःख मिला हुआ है। यह भावना कि भोगों को भोगने से मैं तृप्त हो जाऊँगा, मिथ्या है। इन्द्रियों का सामर्थ्य शिथिल या समाप्त हो जाने पर भी मन की तो भोगने की इच्छा बनी ही रहती है यह 'परिणाम दु:ख' है। भोगने के लिये तैयार, परन्तु उसमें कोई बाधा आये, कोई बाधक बने तो यह 'ताप दु:ख ' अच्छा पुत्र बिगड़ न जाये, कुकर्मी न हो जाये यह 'ताप दु:ख'। मिलने में बिछुड़ने का यह 'ताप दु:ख' है।
भोगने में हम सुख दुःख की अनुभूति करते हैं, उसकी छाप चित्त पर पड़ती है, तो उन्हें फिर भोगने की इच्छा होती है। वही भोग यदि न मिले अथवा कम, घटिया, महंगा या समय पर न मिले तो दुःख होगा, यह 'संस्कार दु:ख' है। और 'गुणवृत्तिविरोधदुःख' - सत्त्व, रज, तम गुणों का एक दूसरे से परस्पर विरोध होने से कभी कुछ विचार तो कभी कुछ विचार, करूँ कि न करूँ, पाप-पुण्य करने का वृत्तिविरोधरूपी घर्षण-दुःख होना।
(६) न वै सशरीरस्य सतः प्रियाऽप्रियोरपहतिरस्ति। (छां. उप. ८/१२/१) शरीर के रहते सांसारिक सुख-दुःख हुए बिना नहीं रहते। निष्काम भाव से प्रयोग करते यदि सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये दुःख नहीं सतायेंगे, जैसे ऋषि लोगों को। विपरीत दु:ख की अनुभूति योगावस्था में नहीं होगी।
उपसंहार
मैं-मेरा का सम्बन्ध इतना गहरा है कि व्यक्ति एक क्षण भी इस से अलग नहीं हो पाता। यह स्वस्वामी सम्बन्ध छूटने पर ही ईश्वर प्राप्ति की अधिक रुचि होती है। यह शरीर भी अपना नहीं, हम तो केवल इसके प्रयोक्ता हैं स्वामी नहीं हैं। जहाँ ममत्त्व वहाँ अविद्या, और जहाँ अविद्या है वहाँ दु:ख है। इस सम्पूर्ण पिण्ड और ब्रह्माण्ड का बनाने वाला स्वामी तो ईश्वर है। इराक में लाखों मर गये कोई नहीं रोया। पञ्जाब-काश्मीर में रोज मारे जाते हैं कोई नहीं रोता परन्तु घर से तार आ जाये तो क्या हाल होगा? यह स्व-स्वामी सम्बन्ध है।ईश्वर-जीव-प्रकृति का ठीक- ठीक ज्ञान (विवेक) होने पर व व्यावहारिक अनुभूतियाँ होने पर अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। उपनिषद् में आया है 'किसके जान लेने पर अन्य किसी का जानना शेष नहीं रहता ? ब्रह्म पदार्थ के जानने के बाद अन्य के जानने की इच्छा नहीं रहती।' जीव ज्ञान, बल, आनन्द चाहता है। ईश्वर के जानने के पश्चात् उसे सब कुछ मिल जाता है।
प्रकृति को जाना, विकृति को जाना, स्वयं आत्मा को भी जाना परन्तु जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है तो कृतकृत्य हो जाता है उसे पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति के पश्चात् कुछ भी प्रापणीय शेष नहीं रहता।
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।
(मु.उप.२/२/८)
दूर से दूर और समीप से समीप विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर आत्मा की अविद्या नष्ट हो जाती है। सारे संशय नष्ट हो जाते है और सारे कुसंस्कारों का नाश हो जाता है।see also: आर्य संस्कृति का संक्षेप में संपूर्ण वैदिक ज्ञान
कर्म
कर्म
कर्म की परिभाषा व लक्षण : - सुख की प्राप्ति करने और दुःख से छूटने के लिये जीवात्मा मन, इन्द्रिय, शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है : 'कर्म' है
कर्म के भेद - कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। (यो.द.४/७) योगी का अशुक्लाकृष्ण (निष्काम) कर्म होता है। तथा अन्य संसारी मनुष्यों का तीन प्रकार का (१) शुक्ल=सकाम शुभकर्म, (२) कृष्ण अशुभ कर्म (३) शुक्ल कृष्ण=मिश्रित कर्म होता है। कर्म कोई भी निष्फल नहीं जाता। कर्म फल कत्ता ही भोगता है अन्य नहीं। सिद्धान्त की तात्त्विक समझ से पवित्र मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी संसार का उपकार करने में जीवनभर रत रहता है।
योगी राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करता है वह निष्काम। जो भी शुभ कर्म, कर्त्तव्य भावना से, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप और ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर करे वह निष्काम। परोपकार आदि शुभ कर्मों के साथ-साथ ईश्वर उपासना भी आवश्यक है। केवल परोपकार आदि कर्मों से ही मुक्ति नहीं होती पर ये मुक्ति में सहायक जरूर हैं।
फल की दृष्टि से भेद - (१) क्रियमाण - जिन कर्मों को कर रहे हैं। (२) संचित - जिन कम्मों को कर चुके, (३) प्रारब्ध - जिन किये हुए कर्मों का फल मिलने लगे।
साधनों के आधार पर भेद - (१) शारीरिक (२) वाचनिक (३) मानसिक कत्त्ता की परिभाषा - कर्त्तुम्, अकर्त्तुम् अन्यथा कर्त्तुम् यःस्वतंत्रः स कत्त्ता। अर्थात् जो किसी कार्य को करने, न करने या उल्टा करने में स्वतंत्र है, वह कर्त्ता कहलाता है।
see also: संकलित पोस्ट (भाग १)
कर्म का फल, परिणाम व प्रभाव
कर्म का फल, परिणाम व प्रभाव
एक बालक अज्ञानता से ब्लेड से उंगली काट लेता है यह 'परिणाम'। दूसरा बच्चा उसके निकलते खून को देख कर रोता है यह 'प्रभाव'। मां आकर उसे चांटा लगाती है, यह कर्म का 'फल' हुआ।
कर्म का फल है - जाति, आयु और भोग।
जाति = योनि यथा मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की।
आयु = जन्म से मृत्यु तक का समय। जैसे कीट-पतंग की कुछ घण्टे ही, पशु-पक्षी की कुछ वर्ष, मनुष्य की सौ वर्ष। मनुष्य अपनी आयु एक सीमा तक ही बढ़ा सकता है। अमुक दिन इतने बजे मरेगा, इस रूप में आयु निश्चित नहीं होती।
भोग = सुख और दुःख के साधनों का मिलना यह योनि (=शरीर) के अनुसार होता है। मांस खानेवाले शेर आदि, घास खाने वाले गाय-घोड़ा आदि, अन्न-फल-वनस्पति खाने वाले मनुष्य।
मिलकर फल देना - एक साथ एक कर्म का फल सुख व दूसरे कर्म का दु:ख भी मिल रहा है। जैसे घर में फ्रीज, टी. वी. से सुख तो मिल रहा है। पर साथ साथ बीमारी का दु:ख भी भोग रहा है।
कर्म फल का नाश होना - मुक्ति के काल तक भोगने से शेष बचे कर्मों का फल अभी न मिलना, लौट कर आने पर मिलना।
व्यक्ति स्वयं दण्ड ले ले अथवा माता-पिता, गुरु-राजा आदि दण्ड दे दें तो इन कर्मों का फल ईश्वर से नहीं मिलेगा। यदि न्यूनाधिक मात्रा में लिया-दिया होगा तो शेष दण्ड (फल) ईश्वर देगा। कर्मों की वासना (= संस्कार) समाप्त कर दिये तो सकाम कर्म नहीं होंगे। उन निष्काम कर्मों का लौकिक फल नहीं मिलेगा। जीवनमुक्त योगी को पहले के किये कर्म का दण्ड मिलता है तो उसे वह ज्ञान के ऊँचे स्तर के कारण अनुभव नहीं करेगा। काल का प्रभाव कर्मों पर नहीं पड़ता। शुभकर्म करते हुए भी यदि अच्छा फल नहीं मिला तो समझें कि कर्म विधि में भूल हुई या कत्त्ता आलसी है या साधन उपयुक्त नहीं है। मुक्ति के लिये सब कर्म फलों का नाश होना आवश्यक नहीं, पर अविद्या का नाश जरूरी है।
see also: रामायण भ्रांतियां का समाधान
कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिये भी कार्य किये बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपने तीन प्रकार के साधनों मन, वाणी व शरीर से या तो कुछ चाह रहा होता है अथवा छोड़ रहा होता है। जीवात्मा के कर्म प्रवाह से अनादि हैं व वे उसके साथ ही हैं। जो मुक्त जीव सृष्टि में घूम रहे हैं, उनके भी कर्म अवशिष्ट हैं। कर्म अलग हैं, संस्कार अलग। पुरुषार्थ से कर्मों के संस्कार नष्ट हो सकते हैं। आज भी यदि अच्छे बुरे सकाम कर्मों के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पलट दें और निष्काम कर्म करते रहें तो मुक्ति हो जायेगी ।
वेद की आज्ञा है कि व्यक्ति कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। शुभ कर्म करने से एक यह लाभ भी होता है कि व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है। जीवात्मा जब दुरित को छोड देता है तो सदा आनन्द से भरपूर रहता है।
ध्यान देने की बात है कि क्या कभी ईश्वर विश्राम करता है ? व्यक्ति प्राय: काम से बचना चाहता है। वर्तमान में प्रायः ऐसी मानोवृत्ति बन गई है कि :
(१) काम करने को कोई तैयार नहीं, पर फल सभी पाना चाहते हैं ।
(२) आज का व्यक्ति काम गलत करता है, पर फल अच्छा चाहता है।
(३) परिश्रम करता कम (कौड़ी का) फल चाहता अधिक (रुपये का)
विचार धारा बन गई कि जो सतत काम करता है वह दु:खी होता है। किन्तु कर्म करने से दुःख नहीं होता। यदि कर्म करने से दु:ख होता तो ईश्वर को भी दुःख होता। हाँ, ईश्वर को खैंचातानी नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को बल लगता है, कठिनाई महसूस होती है।
ईश्वर को ठीक नहीं जानने से लोग मानने लगे कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान् होने का अर्थ है ईश्वर चाहे जो कर सकता है। ईश्वर चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। बिना उपादान कारण के ईश्वर भी कार्य -सृष्टि नहीं बना सकता। ऐसा कहने का साहस बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। चोरी करने में डरें पर जैसा ईश्वर है उसे वैसा कहने में नहीं डरना चाहिये। ईश्वर में अनन्त सामर्थ्य है, अनन्त बल है, निरन्तर कार्य करता रहता है।
ईश्वर काम से कभी नहीं ऊबता, अत: हमें भी अच्छे कामों से कभी नहीं ऊबना चाहिये। ईश्वर का सदा अनुकरण करें। ईश्वर कर्म करता ही रहता है। जो व्यक्ति धर्म में, अच्छे कामों में दान नहीं देता उसका धन बुरे कामों में नष्ट होता है। अच्छे काम सकाम से लेकर निष्काम की कोटि तक होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य पालन से, पुरुषार्थ से आयु को बढ़ाना सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। जान बूझकर निष्काम कर्म करते रहें तो ही योगी बन सकते हैं।
कर्म करते हुए जीना
कर्म करते हुए जीना
कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिये भी कार्य किये बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपने तीन प्रकार के साधनों मन, वाणी व शरीर से या तो कुछ चाह रहा होता है अथवा छोड़ रहा होता है। जीवात्मा के कर्म प्रवाह से अनादि हैं व वे उसके साथ ही हैं। जो मुक्त जीव सृष्टि में घूम रहे हैं, उनके भी कर्म अवशिष्ट हैं। कर्म अलग हैं, संस्कार अलग। पुरुषार्थ से कर्मों के संस्कार नष्ट हो सकते हैं। आज भी यदि अच्छे बुरे सकाम कर्मों के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पलट दें और निष्काम कर्म करते रहें तो मुक्ति हो जायेगी ।
वेद की आज्ञा है कि व्यक्ति कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। शुभ कर्म करने से एक यह लाभ भी होता है कि व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है। जीवात्मा जब दुरित को छोड देता है तो सदा आनन्द से भरपूर रहता है।
ध्यान देने की बात है कि क्या कभी ईश्वर विश्राम करता है ? व्यक्ति प्राय: काम से बचना चाहता है। वर्तमान में प्रायः ऐसी मानोवृत्ति बन गई है कि :
(१) काम करने को कोई तैयार नहीं, पर फल सभी पाना चाहते हैं ।
(२) आज का व्यक्ति काम गलत करता है, पर फल अच्छा चाहता है।
(३) परिश्रम करता कम (कौड़ी का) फल चाहता अधिक (रुपये का)
विचार धारा बन गई कि जो सतत काम करता है वह दु:खी होता है। किन्तु कर्म करने से दुःख नहीं होता। यदि कर्म करने से दु:ख होता तो ईश्वर को भी दुःख होता। हाँ, ईश्वर को खैंचातानी नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को बल लगता है, कठिनाई महसूस होती है।
ईश्वर को ठीक नहीं जानने से लोग मानने लगे कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान् होने का अर्थ है ईश्वर चाहे जो कर सकता है। ईश्वर चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। बिना उपादान कारण के ईश्वर भी कार्य -सृष्टि नहीं बना सकता। ऐसा कहने का साहस बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। चोरी करने में डरें पर जैसा ईश्वर है उसे वैसा कहने में नहीं डरना चाहिये। ईश्वर में अनन्त सामर्थ्य है, अनन्त बल है, निरन्तर कार्य करता रहता है।
ईश्वर काम से कभी नहीं ऊबता, अत: हमें भी अच्छे कामों से कभी नहीं ऊबना चाहिये। ईश्वर का सदा अनुकरण करें। ईश्वर कर्म करता ही रहता है। जो व्यक्ति धर्म में, अच्छे कामों में दान नहीं देता उसका धन बुरे कामों में नष्ट होता है। अच्छे काम सकाम से लेकर निष्काम की कोटि तक होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य पालन से, पुरुषार्थ से आयु को बढ़ाना सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। जान बूझकर निष्काम कर्म करते रहें तो ही योगी बन सकते हैं।
see also: दुःख का कारण और निवारण
कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्मफल देने का कार्य मुख्यरूप से ईश्वर द्वारा संचालित व नियंत्रित है, वही इसके पूरे विधान को जानता है। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है, उसका सामर्थ्य ही इतनी है। ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में कर्मफल की कुछ मुख्य-मुख्य महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है, उन्हें इस लेख में व सम्बन्धित चित्र (CHART) में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।
कर्मफल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। १. सकाम कर्म २. निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कमों को कहते हैं, जो लौकिक फल (धन, पुत्र, यश आदि) को प्राप्त करने की इच्छा से किये जाते हैं। तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किये जायें बल्कि ईश्वर/मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किये जायें।
सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं - अच्छे, बुरे व मिश्रित। अच्छे कर्म-जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, बुरे कर्म-जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म - जैसे खेती करना आदि इसमें पाप व पुण्य (कुछ अच्छा व कुछ बुरा) दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनन्द की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है।
जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें 'दृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के होते हैं - १ जाति २. आयु ३. भोग। समस्त कर्मों का समावेश इन तीन विभागों में हो जाता है। जाति - अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग , वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियाँ, आयु-अर्थात् जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच का समय, भोग-अर्थात् विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग - इन तीनों से जो 'सुख-दु:ख' की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल तो वही है। किन्तु सुख-दुःख रूपी फल का साधन होने के कारण 'जाति, आयु, भोग' को फल नाम दे दिया गया है।
'दृष्टजन्मवेदनीय' कर्म किसी एक फल व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए
केवल आयु या केवल भोग, अथवा दो फल= आयु व भोग को दे सकते हैं जैसे उचित आहार-विहार, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है तथा बल-वीर्य, पुष्टि, भोग सामर्थ्य व आयु को बढ़ाया जा सकता है। जब कि अनुचित आहार, विहार आदि से बल, आयु आदि घट भी जाते हैं ।
दृष्टजन्मवेदनीय कर्म 'जाति रूप फल' को देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जाति (=योनि) तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता; जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु का शरीर बदल लेना। हाँ मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला कर्म 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहा जायेगा, न कि 'दृष्टजन्मवेदनीय' ।
अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं - १. नियत विपाक २. अनियत विपाक। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो, और जो अगले जन्म में फल देने वाला हो उसे 'नियत विपाक' कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में व कब मिलेगा, यह निश्चित न हुआ हो उसे 'अनियतविपाक' कहते हैं। कर्म समूह को शास्त्र में 'कर्माशय' नाम से कहा गया है। 'नियत विपाक कर्माशय' के सभी कर्म परस्पर मिलकर (संमिश्रित रूप में) अगले जन्म में जाति, आयु, भोग प्रदान करते हैं। इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है।
१. जाति - इस जन्म किये गये कर्मों का सबसे बड़ा वा महत्त्व पूर्ण फल अगले जन्म में जाति-शरीर के रूप में मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर=वृक्ष से शरीरों को जाति के अन्तर्गत ग्रहण किया जाता है। यह जाति भी अच्छे व निम्न स्तर की होती है यथा मनुष्यों में पूर्णाङ्ग-विकलाङ्ग, सुन्दर-कुरूप, बुद्धिमान्-मूर्ख आदि, पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर आदि।
२. आयु - नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु-अर्थात् जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति (=शरीर योनि) होती है, उसी के अनुसार आयु भी होती है। यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया १०० वर्ष, गाय, घोड़ा, आदि पशुओं की २५ वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की २-४ वर्ष, मक्खी, मच्छर, भोंरा, तितली आदि कीट पतंगों की २-४-६ मास की आयु होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ ही दिनों की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से घटा-बढ़ा भी सकता है।
३. भोग - 'नियत विपाक कर्माशय' का तीसरा फल भोग (=सुख-दुःख को प्राप्त कराने वाले साधन) के रूप में मिलता है। जैसी जाति (शरीर-योनि) होती है, उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, हवाई जहाज, मिठाई, पॅखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर, उनके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है। किन्तु गाय-भैंस-घोड़ा-कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार-कोठी नहीं बना सकते। शेर-चीत्ता-भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं वे मिठाई, गाड़ी, मकान वस्त्र आदि की सुविधाएँ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व कहा गया कि 'नियत विपाक कर्माशय' से मिली आयु व भोग पर 'दृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय' का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु व भोग घट-बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक (उस जाति के अनुरूप सीमा में) ही बढ़ सकते हैं।
'अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय' के अन्तर्गत 'अनियत विपाक' कर्मों का फल भी जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है। परन्तु यह फल कब व किस विधि से मिलता है इस के लिए शास्त्र में तीन स्थितियाँ (= गतियाँ) बतायी गयी हैं। १. कर्मों का नष्ट हो जाना २. साथ मिल कर फल देना ३. दबे रहना।
१. प्रथम गति - कर्मों का नष्ट हो जाना-वास्तव में बिना फल को दिये कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लम्बे काल तक लुप्त हो जाना है। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते, जीव के समान वे भी अनादि-अनन्त हैं। कुछ न कुछ मात्रा-संख्या में तो रहते ही हैं, व चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जावे। अविद्या (=राग-द्वेष आदि) के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात् जीव को पुन: मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है।
२. दूसरी गति - साथ मिलकर फल देना - अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ-साथ भी दे देता है। अर्थात् अच्छे व बुरे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किन्तु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल-दु:ख भी भुगा देता है। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किन्तु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला किन्तु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अन्धा, लूला या कोढ़ी बना दिया। दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय-कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला किन्तु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला परिणाम स्वरूप सेवा भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले।
३. तीसरी गति - कर्मों का दबे रहना-मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि-शरीर में मिल जाये, यह संभव नहीं है। अत: जिन कर्मों की प्रधानता होती है, उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है, वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं, और तब तक फल नहीं देते, जब तक उन्हीं के सदृश, किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिये जायें। इस तीसरी स्थिति को 'कर्मों का दबे रहना' नाम से कहा जाता है।
उदाहरण - किसी मनुष्य ने अपने जीवन में 'मनुष्य की जाति आयु-भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ-साथ, कुछ कर्म 'सूअर की जाति आयु-भोग' दिलाने वाले भी कर दिये। प्रधानता-अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दब रहेंगे जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाय ।
उपर्युक्त विवरण का सार यह निकलता कि इस जन्म में दु:खों से बचने तथा सुख को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म करने चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए ।
कर्मफल विवरण
कर्मफल विवरण
कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्मफल देने का कार्य मुख्यरूप से ईश्वर द्वारा संचालित व नियंत्रित है, वही इसके पूरे विधान को जानता है। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है, उसका सामर्थ्य ही इतनी है। ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में कर्मफल की कुछ मुख्य-मुख्य महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है, उन्हें इस लेख में व सम्बन्धित चित्र (CHART) में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।
कर्मफल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। १. सकाम कर्म २. निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कमों को कहते हैं, जो लौकिक फल (धन, पुत्र, यश आदि) को प्राप्त करने की इच्छा से किये जाते हैं। तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किये जायें बल्कि ईश्वर/मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किये जायें।
सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं - अच्छे, बुरे व मिश्रित। अच्छे कर्म-जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, बुरे कर्म-जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म - जैसे खेती करना आदि इसमें पाप व पुण्य (कुछ अच्छा व कुछ बुरा) दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनन्द की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है।
जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें 'दृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के होते हैं - १ जाति २. आयु ३. भोग। समस्त कर्मों का समावेश इन तीन विभागों में हो जाता है। जाति - अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग , वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियाँ, आयु-अर्थात् जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच का समय, भोग-अर्थात् विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग - इन तीनों से जो 'सुख-दु:ख' की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल तो वही है। किन्तु सुख-दुःख रूपी फल का साधन होने के कारण 'जाति, आयु, भोग' को फल नाम दे दिया गया है।
'दृष्टजन्मवेदनीय' कर्म किसी एक फल व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए
केवल आयु या केवल भोग, अथवा दो फल= आयु व भोग को दे सकते हैं जैसे उचित आहार-विहार, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है तथा बल-वीर्य, पुष्टि, भोग सामर्थ्य व आयु को बढ़ाया जा सकता है। जब कि अनुचित आहार, विहार आदि से बल, आयु आदि घट भी जाते हैं ।
दृष्टजन्मवेदनीय कर्म 'जाति रूप फल' को देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जाति (=योनि) तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता; जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु का शरीर बदल लेना। हाँ मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला कर्म 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहा जायेगा, न कि 'दृष्टजन्मवेदनीय' ।
अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं - १. नियत विपाक २. अनियत विपाक। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो, और जो अगले जन्म में फल देने वाला हो उसे 'नियत विपाक' कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में व कब मिलेगा, यह निश्चित न हुआ हो उसे 'अनियतविपाक' कहते हैं। कर्म समूह को शास्त्र में 'कर्माशय' नाम से कहा गया है। 'नियत विपाक कर्माशय' के सभी कर्म परस्पर मिलकर (संमिश्रित रूप में) अगले जन्म में जाति, आयु, भोग प्रदान करते हैं। इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है।
१. जाति - इस जन्म किये गये कर्मों का सबसे बड़ा वा महत्त्व पूर्ण फल अगले जन्म में जाति-शरीर के रूप में मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर=वृक्ष से शरीरों को जाति के अन्तर्गत ग्रहण किया जाता है। यह जाति भी अच्छे व निम्न स्तर की होती है यथा मनुष्यों में पूर्णाङ्ग-विकलाङ्ग, सुन्दर-कुरूप, बुद्धिमान्-मूर्ख आदि, पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर आदि।
२. आयु - नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु-अर्थात् जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति (=शरीर योनि) होती है, उसी के अनुसार आयु भी होती है। यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया १०० वर्ष, गाय, घोड़ा, आदि पशुओं की २५ वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की २-४ वर्ष, मक्खी, मच्छर, भोंरा, तितली आदि कीट पतंगों की २-४-६ मास की आयु होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ ही दिनों की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से घटा-बढ़ा भी सकता है।
३. भोग - 'नियत विपाक कर्माशय' का तीसरा फल भोग (=सुख-दुःख को प्राप्त कराने वाले साधन) के रूप में मिलता है। जैसी जाति (शरीर-योनि) होती है, उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, हवाई जहाज, मिठाई, पॅखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर, उनके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है। किन्तु गाय-भैंस-घोड़ा-कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार-कोठी नहीं बना सकते। शेर-चीत्ता-भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं वे मिठाई, गाड़ी, मकान वस्त्र आदि की सुविधाएँ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व कहा गया कि 'नियत विपाक कर्माशय' से मिली आयु व भोग पर 'दृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय' का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु व भोग घट-बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक (उस जाति के अनुरूप सीमा में) ही बढ़ सकते हैं।
'अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय' के अन्तर्गत 'अनियत विपाक' कर्मों का फल भी जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है। परन्तु यह फल कब व किस विधि से मिलता है इस के लिए शास्त्र में तीन स्थितियाँ (= गतियाँ) बतायी गयी हैं। १. कर्मों का नष्ट हो जाना २. साथ मिल कर फल देना ३. दबे रहना।
१. प्रथम गति - कर्मों का नष्ट हो जाना-वास्तव में बिना फल को दिये कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लम्बे काल तक लुप्त हो जाना है। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते, जीव के समान वे भी अनादि-अनन्त हैं। कुछ न कुछ मात्रा-संख्या में तो रहते ही हैं, व चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जावे। अविद्या (=राग-द्वेष आदि) के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात् जीव को पुन: मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है।
२. दूसरी गति - साथ मिलकर फल देना - अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ-साथ भी दे देता है। अर्थात् अच्छे व बुरे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किन्तु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल-दु:ख भी भुगा देता है। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किन्तु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला किन्तु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अन्धा, लूला या कोढ़ी बना दिया। दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय-कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला किन्तु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला परिणाम स्वरूप सेवा भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले।
३. तीसरी गति - कर्मों का दबे रहना-मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि-शरीर में मिल जाये, यह संभव नहीं है। अत: जिन कर्मों की प्रधानता होती है, उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है, वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं, और तब तक फल नहीं देते, जब तक उन्हीं के सदृश, किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिये जायें। इस तीसरी स्थिति को 'कर्मों का दबे रहना' नाम से कहा जाता है।
उदाहरण - किसी मनुष्य ने अपने जीवन में 'मनुष्य की जाति आयु-भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ-साथ, कुछ कर्म 'सूअर की जाति आयु-भोग' दिलाने वाले भी कर दिये। प्रधानता-अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दब रहेंगे जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाय ।
उपर्युक्त विवरण का सार यह निकलता कि इस जन्म में दु:खों से बचने तथा सुख को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म करने चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए ।
see also: वैदिक विज्ञान
उपासना की परिभाषा - 'जिसे करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं'। यह नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से ईश उपासना करें और आनन्द की प्राप्ति न हो। यदि आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो सूक्ष्मता से परीक्षण करें, कहीं आपके व्यवहार से कोई दु:खी तो नहीं या फिर ईश्वर के साथ किए गये व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं ? क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है, उससे अधिक जीव का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ शुद्ध सुख प्राप्ति के लिये सम्बन्ध जोड़ना-यह उपासना है।
प्रकृति-विकृति से उपयोग तो लेना है परन्तु उसकी उपासना नहीं करनी, उपासना तो ईश्वर की ही करनी है। जो प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं। वे अन्धकार रूप कूप में गिरकर दु:खों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति की प्रशंसा होती है पूजा नहीं। पृथ्वी आदि पांच भूत व उनसे बने पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही कारण-प्रकृति से बनाई हुई कृति है। फिर प्रकृति-पूजा से भी खराब व्यक्ति पूजा है। स्वार्थी तथा अज्ञानी मनुष्यों ने प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यक्तियों की पूजा कराना अपना आजीविका का साधन बनाया है यह उनका बिना ही परिश्रम के लड्ड खाने की एक युक्ति मात्र है।
उपासना
उपासना
उपासना की परिभाषा - 'जिसे करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं'। यह नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से ईश उपासना करें और आनन्द की प्राप्ति न हो। यदि आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो सूक्ष्मता से परीक्षण करें, कहीं आपके व्यवहार से कोई दु:खी तो नहीं या फिर ईश्वर के साथ किए गये व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं ? क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है, उससे अधिक जीव का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ शुद्ध सुख प्राप्ति के लिये सम्बन्ध जोड़ना-यह उपासना है।
प्रकृति-विकृति से उपयोग तो लेना है परन्तु उसकी उपासना नहीं करनी, उपासना तो ईश्वर की ही करनी है। जो प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं। वे अन्धकार रूप कूप में गिरकर दु:खों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति की प्रशंसा होती है पूजा नहीं। पृथ्वी आदि पांच भूत व उनसे बने पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही कारण-प्रकृति से बनाई हुई कृति है। फिर प्रकृति-पूजा से भी खराब व्यक्ति पूजा है। स्वार्थी तथा अज्ञानी मनुष्यों ने प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यक्तियों की पूजा कराना अपना आजीविका का साधन बनाया है यह उनका बिना ही परिश्रम के लड्ड खाने की एक युक्ति मात्र है।
see also: ईश्वर की उपासना
साधक को पक्ष-प्रतिपक्ष व जय-पराजय की शैली में नहीं बोलना चाहिये। प्रारम्भिक जिज्ञासु को प्रमाण तर्कों के बजाय आचरण पर अधिक जोर देना चाहिये। जिज्ञासु को खण्डनात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रमाण-तर्क से सिद्ध होने पर भी यदि आचरण न करें तो कुछ लाभ नहीं। जैसे गुरु विरजानन्द के इशारे (बोल) मात्र से कि पहले पढ़ी अनार्ष विद्या की पोटली जमुना में फेंक आवो तब आर्ष विद्या आयेगी; तो उसका पालन महर्षि ने तत्परता से कर डाला। इसी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष की गठरी फेंकने पर ही योगानन्द की सुगन्ध महकेगी। ईश्वर के बारे में लोग कितने पढ़ते, सुनते, चर्चा करते, गाते, बजाते हुए भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते-समझते; क्योंकि ऋषि परम्परा लुप्त हो गई। ऋषि दयानन्द ने पुन: प्रचलित की, परन्तु उनके पश्चात्- आर्यजगत में योग्य गुरु परीक्षक न मिलने तथा आचरण में न लाने से बहुत प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। ईश्वर तत्त्व को भी जब हम अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता के समान निश्चयात्मक स्वीकार करेंगे तभी उसका साक्षात्कार, दर्शन होगा। जैसे प्रकृति एक चीज है, पदार्थ है, वस्तु है वैसे ही ईश्वर भी एक चीज-पदार्थ-वस्तु है। तभी तो उसका ध्यान-भक्ति हो सकती है। ईश्वर भी एक सत्तात्मक वस्तु है। जिसके दिये हुए उपकरण बुद्धि बिना हम सोच भी नहीं सकते, केवल एक नाड़ी बिगड़ जाये तो एम.ए, पी. एच. डी., मानव नंगा बजार में घूमने लगता है। ईश्वर सब के शरीरों की रचना करता, पालन करता और मन में भय-शंका-लज्जा करके बुरे कामों से रोकता है।
आलस्य प्रमाद को दूर करके जिज्ञासु विद्यार्थी विद्या को पढ़े तो विद्या ग्रहण करने में सफल होता है। अध्ययन काल में मुख्य विषय को छोड़ अन्य विषयों में मन न दौड़ायें। श्रद्धा, रुचि, प्रेम से इसमें मन लगायें। समाज में व्यवहार करते समय योगांगों का प्रयोग कीजिए। बिना व्यवहार में लाये कोई फल नहीं। उपासना में बाहर के सम्बन्धों को विचारना छोड़ देवें। ईश्वर से मिलने का, ईश्वर साक्षात्कार करने का एक उपाय है श्रद्धा के साथ ओ३म् का जप। साधक अर्थ का विचार मन में रखता हुआ ईश्वर समर्पित भाव से (मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ) जप करे भले ही यह सम्बन्ध आगम (शब्द) वा अनुमान प्रमाण के आधार पर हो। इस प्रकार ईश्वर समर्पित होकर देखो फिर ईश्वर अवश्य तुम्हारी समाधि लगा देगा। ध्यान दें कि संगीत के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में ईश्वर से सम्बन्ध और ईश्वर से प्रेम भाव भी बना रहता है या संगीत में मन लग जाता है ? आप नाम बोलते, गाते, वैसा मान-जान नहीं रहे तो समझो अभी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। साधक को ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों के स्वरूप को समझना पड़ता है। यदि ज्ञान ठीक न हो तो सफलता नहीं मिलती। इसी तरह कर्म, उपासना भी यदि ठीक नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती।
उपासक का आचरण
उपासक का आचरण
साधक को पक्ष-प्रतिपक्ष व जय-पराजय की शैली में नहीं बोलना चाहिये। प्रारम्भिक जिज्ञासु को प्रमाण तर्कों के बजाय आचरण पर अधिक जोर देना चाहिये। जिज्ञासु को खण्डनात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रमाण-तर्क से सिद्ध होने पर भी यदि आचरण न करें तो कुछ लाभ नहीं। जैसे गुरु विरजानन्द के इशारे (बोल) मात्र से कि पहले पढ़ी अनार्ष विद्या की पोटली जमुना में फेंक आवो तब आर्ष विद्या आयेगी; तो उसका पालन महर्षि ने तत्परता से कर डाला। इसी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष की गठरी फेंकने पर ही योगानन्द की सुगन्ध महकेगी। ईश्वर के बारे में लोग कितने पढ़ते, सुनते, चर्चा करते, गाते, बजाते हुए भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते-समझते; क्योंकि ऋषि परम्परा लुप्त हो गई। ऋषि दयानन्द ने पुन: प्रचलित की, परन्तु उनके पश्चात्- आर्यजगत में योग्य गुरु परीक्षक न मिलने तथा आचरण में न लाने से बहुत प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। ईश्वर तत्त्व को भी जब हम अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता के समान निश्चयात्मक स्वीकार करेंगे तभी उसका साक्षात्कार, दर्शन होगा। जैसे प्रकृति एक चीज है, पदार्थ है, वस्तु है वैसे ही ईश्वर भी एक चीज-पदार्थ-वस्तु है। तभी तो उसका ध्यान-भक्ति हो सकती है। ईश्वर भी एक सत्तात्मक वस्तु है। जिसके दिये हुए उपकरण बुद्धि बिना हम सोच भी नहीं सकते, केवल एक नाड़ी बिगड़ जाये तो एम.ए, पी. एच. डी., मानव नंगा बजार में घूमने लगता है। ईश्वर सब के शरीरों की रचना करता, पालन करता और मन में भय-शंका-लज्जा करके बुरे कामों से रोकता है।
आलस्य प्रमाद को दूर करके जिज्ञासु विद्यार्थी विद्या को पढ़े तो विद्या ग्रहण करने में सफल होता है। अध्ययन काल में मुख्य विषय को छोड़ अन्य विषयों में मन न दौड़ायें। श्रद्धा, रुचि, प्रेम से इसमें मन लगायें। समाज में व्यवहार करते समय योगांगों का प्रयोग कीजिए। बिना व्यवहार में लाये कोई फल नहीं। उपासना में बाहर के सम्बन्धों को विचारना छोड़ देवें। ईश्वर से मिलने का, ईश्वर साक्षात्कार करने का एक उपाय है श्रद्धा के साथ ओ३म् का जप। साधक अर्थ का विचार मन में रखता हुआ ईश्वर समर्पित भाव से (मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ) जप करे भले ही यह सम्बन्ध आगम (शब्द) वा अनुमान प्रमाण के आधार पर हो। इस प्रकार ईश्वर समर्पित होकर देखो फिर ईश्वर अवश्य तुम्हारी समाधि लगा देगा। ध्यान दें कि संगीत के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में ईश्वर से सम्बन्ध और ईश्वर से प्रेम भाव भी बना रहता है या संगीत में मन लग जाता है ? आप नाम बोलते, गाते, वैसा मान-जान नहीं रहे तो समझो अभी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। साधक को ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों के स्वरूप को समझना पड़ता है। यदि ज्ञान ठीक न हो तो सफलता नहीं मिलती। इसी तरह कर्म, उपासना भी यदि ठीक नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती।
see also: जीवन जीने का उपदेश
किस प्रक्रिया द्वारा साधना-योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय इस 'साधना से मुक्ति' पत्रक में महरषि पतञ्जलि रचित योगदर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
योग दर्शन में बताये गये यम नियम आदि आठ अंगो का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गरन्ध इन पॉच विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम 'साधना' है और मरणादि सब दु:खों से छूटकर ईश्वरीय आनन्द भोगने का नाम मुक्ति है ।
इस चित्र में १० पर्वत बताये गए हैं जो क्रमश: अधिक-अधिक उँचे हैं। इन पर्वतों की ऊँचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों-त्यों उसका स्तर ऊँचा होता जाता है।
१. साधना के प्रारम्भिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए 'प्राणायाम' करता है ।
२. मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बन्द कर देती हैं इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार' है ।
३. इस प्रकार अधिकार में किये मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम 'धारणा' है। धारणा की स्थिति सम्पादित करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म-स्वभाव का निरंतर चिंतन कर पाना 'ध्यान' कहलाता है।
४. ध्यान करने से साधक को संसार के तीन अनादि तत्त्वों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, इस स्थिति को 'विवेकख्याति' कहते हैं।
५. विवेकख्याति की प्राप्ति के पश्चात् योगाभ्यासी व्यक्ति का सांसारिक विषय भोगों के प्रति राग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को 'अपर वैराग्य' नाम से कहा गया है।
६. अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात् साधक को सम्प्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को ही धारण करने वाली) बन जाती है। सम्प्रज्ञात समाधि की चार अवस्थायें होती हैं - वितर्क-विचार-आनन्द व अस्मिता। ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। इनमें साधक को ५ स्थूल भूतों , ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन, १ बुद्धि, १ अहंकार, मूलप्रकृति तथा स्वयं अपना (जीवात्मा का) साक्षात्कार होता है।
७. सम्प्रज्ञात समाधि के बाद साधक को 'पर वैराग्य' की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल, आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात् सत्त्व-रज-तम नामक तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है।
८. पर वैराग्य के पश्चात् साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में 'असंप्रज्ञात-समाधि' नाम से कहा गया है।
९. असंप्रज्ञात-समाधि को लम्बे काल तक (वर्षों तक) लगा लगाकर साधक ईश्वर से विशेष ज्ञान बलादि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे-धीरे अपनी अविद्या के समस्त संस्कारों का नाश (दग्धबीज-भावावस्था में पहुँचाना) कर देता है। यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को 'कुशल' 'चरम देह' 'जीवनमुक्त' नाम से कहा गया है।
१०. जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे नया शरीर नहीं मिलता, वह परम पिता परमात्मा के समीप रहता हुआ ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्ष तक आनंद भोगता है। इसी को नितान्त मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है।
साधना से मुक्ति
साधना से मुक्ति
किस प्रक्रिया द्वारा साधना-योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय इस 'साधना से मुक्ति' पत्रक में महरषि पतञ्जलि रचित योगदर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
योग दर्शन में बताये गये यम नियम आदि आठ अंगो का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गरन्ध इन पॉच विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम 'साधना' है और मरणादि सब दु:खों से छूटकर ईश्वरीय आनन्द भोगने का नाम मुक्ति है ।
इस चित्र में १० पर्वत बताये गए हैं जो क्रमश: अधिक-अधिक उँचे हैं। इन पर्वतों की ऊँचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों-त्यों उसका स्तर ऊँचा होता जाता है।
१. साधना के प्रारम्भिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए 'प्राणायाम' करता है ।
२. मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बन्द कर देती हैं इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार' है ।
३. इस प्रकार अधिकार में किये मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम 'धारणा' है। धारणा की स्थिति सम्पादित करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म-स्वभाव का निरंतर चिंतन कर पाना 'ध्यान' कहलाता है।
४. ध्यान करने से साधक को संसार के तीन अनादि तत्त्वों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, इस स्थिति को 'विवेकख्याति' कहते हैं।
५. विवेकख्याति की प्राप्ति के पश्चात् योगाभ्यासी व्यक्ति का सांसारिक विषय भोगों के प्रति राग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को 'अपर वैराग्य' नाम से कहा गया है।
६. अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात् साधक को सम्प्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को ही धारण करने वाली) बन जाती है। सम्प्रज्ञात समाधि की चार अवस्थायें होती हैं - वितर्क-विचार-आनन्द व अस्मिता। ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। इनमें साधक को ५ स्थूल भूतों , ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन, १ बुद्धि, १ अहंकार, मूलप्रकृति तथा स्वयं अपना (जीवात्मा का) साक्षात्कार होता है।
७. सम्प्रज्ञात समाधि के बाद साधक को 'पर वैराग्य' की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल, आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात् सत्त्व-रज-तम नामक तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है।
८. पर वैराग्य के पश्चात् साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में 'असंप्रज्ञात-समाधि' नाम से कहा गया है।
९. असंप्रज्ञात-समाधि को लम्बे काल तक (वर्षों तक) लगा लगाकर साधक ईश्वर से विशेष ज्ञान बलादि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे-धीरे अपनी अविद्या के समस्त संस्कारों का नाश (दग्धबीज-भावावस्था में पहुँचाना) कर देता है। यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को 'कुशल' 'चरम देह' 'जीवनमुक्त' नाम से कहा गया है।
१०. जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे नया शरीर नहीं मिलता, वह परम पिता परमात्मा के समीप रहता हुआ ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्ष तक आनंद भोगता है। इसी को नितान्त मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है।
see also: वेदों के विषय में भ्रांति निवारण
केवल विद्या (भले ही वेद-उपनिषद्-गीता आदि) पढ़ने जानने से, नारद की तरह मन्त्रविद् होने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिये आत्मविद् होना जरूरी है। विद्या भी चार प्रकार से आती है। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन और व्यवहारकालेन। उपासक चारों को अपनाये ।
ऋषि लोग ब्रह्म को जानने वाले को ही विद्वान् मानते हैं। अर्थापत्ति से कह सकते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति और जीव को भी जान लिया है। लाखों-करोड़ों व्यक्ति इस विद्या में लगे हुए ईश्वर उपासना करते हैं, परन्तु कोई विरला ही ईश्वर-जीव-प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को समझकर ज्ञान-कर्म-उपासना की शुद्ध वैदिक पद्धति अपनाता है। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसकी और इस संसार की रचना एक बड़ा भारी विज्ञान है। जो व्यक्ति वेद और ऋषिकृत ग्रन्थों को छोड़कर चलेगा वह अवश्य भटक जायेगा, इसे नहीं समझ पायेगा।
उपासक यदि गवेषणा करके देखे तो ज्ञात होगा कि लौकिक चीजों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव अत्यन्त न्यून ही रहता है। जिन जिन कारणों से ईश्वर का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता उन उन कारणों को ढूंढें और दूर करें। यह विचारना चाहिए कि जब माता, पिता, गुरु, राजा से बात करते हैं तो हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या उपासना काल में भी इतना ही प्रभाव ईश्वर की हाजरी का पड़ता है? ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? जब तक ईश्वर का प्रभाव अधिक और लौकिक चीजों का प्रभाव कम नहीं होता तब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। व्यक्ति जिसको अधिक लाभप्रद समझता है उसकी तरफ दौड़ लगाता है। जिसको लाभप्रद नहीं जानता उसकी उपेक्षा कर छोड़ देता है। एक खिलाड़ी प्रथम आने के लिये उसके लाभ यश-मान धन आदि को देख स्पर्धा से पूर्व कितनी अधिक तैयारी करता है? तब ही उसके प्रथम आने की संभावना बनती है। ओ३म् का जप, ज्ञान-प्राप्ति, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। सो साधक को पूर्व तैयारी करनी चाहिये। उपासक मान की अपेक्षा अपमान को अमृत तुल्य समझे ।
ब्रह्मविद्या की श्रेष्ठता
ब्रह्मविद्या की श्रेष्ठता
केवल विद्या (भले ही वेद-उपनिषद्-गीता आदि) पढ़ने जानने से, नारद की तरह मन्त्रविद् होने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिये आत्मविद् होना जरूरी है। विद्या भी चार प्रकार से आती है। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन और व्यवहारकालेन। उपासक चारों को अपनाये ।
ऋषि लोग ब्रह्म को जानने वाले को ही विद्वान् मानते हैं। अर्थापत्ति से कह सकते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति और जीव को भी जान लिया है। लाखों-करोड़ों व्यक्ति इस विद्या में लगे हुए ईश्वर उपासना करते हैं, परन्तु कोई विरला ही ईश्वर-जीव-प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को समझकर ज्ञान-कर्म-उपासना की शुद्ध वैदिक पद्धति अपनाता है। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसकी और इस संसार की रचना एक बड़ा भारी विज्ञान है। जो व्यक्ति वेद और ऋषिकृत ग्रन्थों को छोड़कर चलेगा वह अवश्य भटक जायेगा, इसे नहीं समझ पायेगा।
उपासना का प्रभाव
उपासना का प्रभाव
उपासक यदि गवेषणा करके देखे तो ज्ञात होगा कि लौकिक चीजों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव अत्यन्त न्यून ही रहता है। जिन जिन कारणों से ईश्वर का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता उन उन कारणों को ढूंढें और दूर करें। यह विचारना चाहिए कि जब माता, पिता, गुरु, राजा से बात करते हैं तो हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या उपासना काल में भी इतना ही प्रभाव ईश्वर की हाजरी का पड़ता है? ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? जब तक ईश्वर का प्रभाव अधिक और लौकिक चीजों का प्रभाव कम नहीं होता तब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। व्यक्ति जिसको अधिक लाभप्रद समझता है उसकी तरफ दौड़ लगाता है। जिसको लाभप्रद नहीं जानता उसकी उपेक्षा कर छोड़ देता है। एक खिलाड़ी प्रथम आने के लिये उसके लाभ यश-मान धन आदि को देख स्पर्धा से पूर्व कितनी अधिक तैयारी करता है? तब ही उसके प्रथम आने की संभावना बनती है। ओ३म् का जप, ज्ञान-प्राप्ति, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। सो साधक को पूर्व तैयारी करनी चाहिये। उपासक मान की अपेक्षा अपमान को अमृत तुल्य समझे ।
२. वह संसार का निर्माता है।
३. वह वेद ज्ञान का दाता है।
४. वह सर्वरक्षक और परम हितैषी है ।
५. उपासना से मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण होता है ।
६. इससे सहन शक्ति बढ़ती है ।
७. इससे कर्म निष्काम बनते हैं।
८. बुरे संस्कार नष्ट होकर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं ।
९. विशुद्ध सुख की प्राप्ति होती है।
१०. ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है ।
११. आत्म-साक्षात्कार होता है।
१२. ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है ।
ओ३म् प्रणव से स्तुति = प्र उपसर्ग पूर्वक णु स्तुतौ धातु से अप् प्रत्यय करने से प्रणव शब्द बनता है। जिसके द्वारा उत्कृष्टता से ईश्वर की स्तुति की जाये वह प्रणव है, ओ३म् है।
स्तुति - ईश्वर सच्चिदानन्द, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम्, दयालु, सर्व जगत् पिता, माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव, आनन्ददायक, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष प्रदाता है। इन विशेषणों से परमात्मा की ही स्तुति (=गुण कीर्तन) करनी चाहिये ।
प्रार्थना - ईश्वर से स्वप्रयत्नोपरान्त सब श्रेष्ठ कार्यों में सहाय चाहना।
उपासना - प्रभु के आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना, सो पूर्वोक्त ने पर निराकार आदि लक्षण वाले की ही भक्ति करना, उससे अतिरिक्त किसी और की कभी न करना। जैसे सुख-दुःख का ध्यान मन में होता है वैसे ईश्वर का ध्यान मन में होना चाहिये। मूर्ति की कुछ आवश्यकता नहीं। ईश्वर को सुख-दुःख की भाँति पहचाना या अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की सत्ता सभी प्राणियों में सर्वत्र एक समान है, परन्तु जिसकी आत्मा में उस चेतन ईश्वर के जितने ज्ञान का अनुभव स्व स्व सामर्थ्यानुसार होगा उसकी आत्मा उतने ही सुख को प्राप्त होगी। जो ईश्वर द्युलोक, पृथ्वी लोक, आन्तरिक मन-इन्द्रियों आदि सारे पदार्थों में ओत-प्रोत है उसी ईश्वर को जानो। वही मुक्ति का अमृत सेतु है। अन्य बातों का परित्याग करो।
see also: श्रीमद्भागवत पुराण समीक्षा
ईश्वर आनन्द से परिपूर्ण है। जैसे भूखे व्यक्ति को अत्यन्त स्वादिष्ट उचित भोजन मिलने पर लौकिक सुख मिलता है (परन्तु यह हीन उपमा है)। ऐसे ही दुःख की निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा ईश्वर-प्राप्ति में होगी।
सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख मिश्रित है, मिश्री-हलवे की मिठास अन्तत: कम होते होते गारा मिट्टी के समान नीरस लगने लगेगी। परन्तु ईश्वर उपासना से आनन्द बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख से रोगी, ईश्वरीय सुख सेवन से निरोगी होता है। ईश्वर का आनन्द नित्य और विशुद्ध है।
जब तक व्यक्ति सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख नहीं अनुभव करता, तब तक ईश्वर के आनन्द में प्रवृत्त नहीं होता। जीवन काल में ही दुःखों से मुक्ति मिलने पर मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिलती है। केवल मरने से ही मुक्ति नहीं मिलती। जीवित रहते-रहते जिसने ब्रह्म को जान लिया सो वह कृतकृत्य हो गया। ईश्वर अनुपम होने से उसके लिये उपमा नहीं दी जा सकती परन्तु समझने की दृष्टि से हीन उपमा दी गई है। जो सर्वशक्तिमान् को सच्चा जानता-मानता है, उसके उचित न्याय पर भरोसा करता है वह कभी दु:खी नहीं होता। राजा तो अल्पज्ञता से उचित-अनुचित निर्णय भी देता है पर ईश्वर सदा उचित करेगा और वह भी सुधारने के हेतु दया ही करता है। धन सम्पत्ति की तुलना में योग विद्या की प्राप्ति में सहस्र गुणा सुख (आनन्द) अधिक है। में प्रभु को जानूँ, प्राप्त करूँ, साक्षात्कार करूँ यह भावना तीव्र रूप में बनाये रखें। केवल नाम स्मरण करते जाना परन्तु तदनुसार अपना चरित्र न सुधारना ईश्वर को प्राप्त करने का निष्फल प्रयास है ।
जो काम जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से करना चाहिये, तभी सफलता मिलती है। आसन पर बैठते ही सब विचार छोड़ देना। ऐसा न हो कि छेड़ना था ईश्वर का चिन्तन-मनन और छेड़ दिया व्यापार, धन्धा, पढ़ना आदि अन्य विषय। दिया समय ईश्वर को मिलने का और मुख फेर कर बातें-विचार करने लग गये संसार की संसार के साथ तो यह बुलाये हुए अतिथि के समान ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया, सो कैसे उसे प्राप्त कर सकेंगे?
इन्द्रिय दोष से और संस्कार दोष से अविद्या पैदा होती है। अज्ञान उद्वेग को पैदा करता है। सन्ध्या में बैठते ही निश्चय करो कि विषयों में मन को नहीं चलाऊँगा। जप अर्थ सहित, अपने को ईश्वर अर्पण करते हुए, प्रभु प्रेम में विह्वल हो, प्रभु से बातें करते हुए होना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से संध्या उपासना में मन लगने लगता है। कहा भी है-
व्यवहार काल में चोरी, जारी, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की प्रवृत्तियों को रोककर, स्वार्थ की जगह परोपकार, असत्य छोड़कर सत्य प्रवृत्तियों को जगायें। परन्तु उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों-विचारों को भी रोकना पड़ता है। जैसे वेद का पढ़ना-पढ़ाना, धर्म है। यज्ञ करना, दान, पठन-पाठन का विचार आदि को यदि उपासना काल में करेंगे तो ईश्वर से सम्बन्ध नहीं जुड़ पायेगा। व्यवहार काल में भी मन-इन्द्रियों को खुला नहीं छोड़ना, इन्हें यम-नियम से आबद्ध रखें।
उपासना काल - बालक का व्यवहार जैसे अपने माता-पिता-गुरु के साथ होता है वैसा ही व्यवहार जीवात्मा को परमात्मा के साथ करना चाहिए। प्रातः काल उपासना में बैठने की तैयारी जगते ही करनी पड़ती है। इस काल में कोई भी सांसारिक बातचीत, चर्चा- विचारणा न करके मौन धारण करना। दोनों काल की उपासना से पूर्व छोड़ने योग्य कार्य व विचारों को छोड़ना और करने योग्य कार्य व विचारों को ही करना। पहले जप, फिर अर्थ विचार, फिर समर्पण। जप में अज्ञान वश भूल से जो विचार उठें उसे पकड़ना और हटा देना। उलटे संस्कारों के कारण यदि कोई विचार असावधानी से उठा लें तो उसी समय सावधानी पूर्वक उसे हटा दिया जाये। पश्चात् भगवान की तरफ सहयोग के लिये दौड़ेंगे तब निश्चय ही हमें ईश्वर सहाय देगें।
योगविद्या का ज्ञान-विज्ञान जानने के लिये पहले चित्त की अवस्थायें जाननी पड़ेगी। पठित विद्वान् होने पर भी व्यक्त अनुभव करता है कि चित्त बलात् विषयों की ओर जा रहा है। गया कब? किसने भेजा ? यह वह भूल जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मन-इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बुद्धिपूर्वक की गई कुछ क्रियायें भी स्वभावतः होती लगती हैं। ईश्वर बुद्धिपूर्वक सृष्टि की रचना, पालन, व प्रलय करता है। इसी प्रकार जीव इन्द्रियों का चलाना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, चित्त का रोकना आदि क्रियाएँ करता है। वस्तुत: आपने स्वयं मन को चलाया, पर भूल यह हुई कि उसे पकड़ (जान) न सके कब चलाया ? ध्यान देंगे तो पता चल जायेगा कि मैं ही इसे विषयान्तर में ले गया था।
मन में तरंगें विचार उत्पन्न होते रहते हैं पर पता नहीं लगता। परन्तु सावधानी पूर्वक ध्यान देने से पता लगेगा कि मेंने एक मास पहले एक व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा था, महीनों-वर्षों बाद विशेष ध्यान देने पर पूर्व सोचा हुआ विचार याद आ जाता है। उपासक इसके कारण उपासना में चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता। लगा था संध्या करने सोचने लग गया अन्य विचार फिर १५ मिनट बाद पता लगा में कहीं चला गया मन को निरुद्ध करने का अभ्यास करते-करते उपासक को फिर ५ मिनट, एक मिनट, कुछ सेकण्ड बाद ही पता लग जाता है, कि मन को अन्य विषयों में लगा दिया, पर कब लगाया यह पता नहीं लगता। लगने के बाद पता चलता है कि मन विषयान्तर हो गया। अनेक बार पकड़ में आने पर भी, पता लगने पर भी व्यक्ति उन सांसारिक विचारों को चाहता है। तब उसे लगता है कि में खींचता हूँ ईश्वर की ओर पर मन खींचता है विषय चिन्तन की ओर। वास्तव में एक ही चेतनात्मा है जो मन को चलाता है। जीवात्मा अपनी सूक्ष्म इच्छा से ही मन को इतनी तीव्रता से चलाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि मन को चलाने वाला में हूँ वा यह स्वयं चल रहा है। ये सब बेकार का चिंतन असावधानी के कारण होता है। चेतना पूर्वक (तीव्र ज्ञान इच्छा पूर्वक) प्रयास करने से वृत्तियों का पता लग जाता है। जो क्रियायें सूक्ष्म इच्छाओं से होती हैं उनका पता साधक को नहीं चल पाता। इसे वैज्ञानिक अचेतन मन कहते हैं। वास्तव में सावधान-असावधान तो जीवात्मा ही होता है ।
अनुभव से संस्कार बनता है। संस्कार से स्मृति, और स्मृति से मानव चरित्र बनता है। अच्छे बुरे विचारों की टक्कर होती रहती है तब संघर्ष करने से विजय होगी। उस समय मन को चलाना छोड़ दो, शान्त हो जायेगा। जीतने पर गद्गद् हो जाता है, तब जो आनन्द आता है वह वर्णनातीत है। मन को जड़ मानकर साधक बार-बार यह वाक्य दोहराये "मेरी इच्छा के बिना यह जड़ मन इन्द्रियाँ चलेंगे ही नहीं। मैं जहाँ चलाऊँगा, विचारूँगा वहीं मेरे पीछे जायेंगे।"
अभ्यास - श्रद्धापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक व तपपूर्वक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान में निरन्तर लगे रहना अभ्यास कहलाता है। साधक अपने आचरण-व्यवहार को दीर्घ काल तक अर्थात् जब तक बुरे संस्कार दग्धबीज भाव को प्राप्त न हो जायें विधि पूर्वक निरन्तर अभ्यास करते हुए स्वच्छ व परिपक्व बनाये। यदि योगाभ्यास बीच में छोड़ दिया तो स्थिति वही की वही हो जायेगी। संस्कार तेजी से बिजली की तरह एक दूसरे को दबाते हैं। बुद्धिमान् अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करता है, बुरों को दबा देता है। परन्तु मूर्ख अच्छों को दबा देता है, बुरों को उभार कर विचारने लगता है। बड़ी तीव्रता से विचार चलते हैं। व्यवहार काल में ईश्वर को समक्ष नहीं रखा तो उपासना काल में प्राप्त करना कठिन होगा ।
संघर्ष - स्वस्थ (= योगस्थ) अवस्था में जीव के अधीन विचार तरंगें रहती हैं। निरोध के संस्कारों को जगाता है तो ईश्वर में आनन्द आने लगता है; और जब संसारी तरंगें जगाने लगता है तो दु:ख सागर में डूबता जाता है। मन को खुला छोड़ देने पर अन्यथा विचारेगा अन्यथा विचारने से बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। महान् बनने के लिये कुछ आदर्श हैं, नियम हैं, व्रत हैं, संकल्प हैं, उन्हें लेकर चलना पड़ता है, नहीं लेने से नीचे गिरता चला जायेगा। ईश्वर भी अपने अटल नियम पर चलता रहता है। साधक कभी निराश न हो। प्रयत्न करने पर भी मन डिग जाये तो प्रायश्चित्त करके पुन: सन्मार्ग पर चलना शुरू कर दे। गिरने पर पुनः चलने की प्रक्रिया से उन्नति होगी, न कि बिलकुल ही न चलने से। मन-वचन-कर्म से अपने वा अन्य के दोषों से सन्धि न करें। बुराईयों के साथ बड़ा भारी अथक संघर्ष/युद्ध करना पड़ता है।
मन की विचार तरंगें (वृत्तियां) स्वयं उठती हैं या मैं उठाता हूँ? मन-इन्द्रियाँ अथवा ईश्वर उठाता है ? सूक्ष्मता से विचारने पर ज्ञात होगा कि निश्चय ही केवल में स्वयं ही उठाता हूँ। इस प्रकार विचार करने से साधक को ऐसा प्रतीत होगा कि मुझ में साहस, श्रद्धा, शक्ति आ गई कि यह मेरे हाथ में है कि कब किस विचार को में उठाता हूँ। परन्तु यह सब ईश्वर प्रदत्त मानें। यदि 'अहम्' मैं करने वाला विचार लायेगा तो मिथ्या अभिमान होगा। लोकैषणा व स्वामित्त्व से अभिमान होता है जो साधक को पथ भ्रष्ट कर देता है।
सोते समय प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण करें। इन्द्रिय निग्रह अर्थात् उन्हें सदा अपने अधिकार में रखें ताकि बुराई में न फँसें रात्रि में सोने से पूर्व सोचें आज क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, फिर अन्तिम क्षण में ईश्वर चिन्तन के सिवाय अन्य कुछ न विचारें।
प्रात: उठते समय 'ओ३म्' सच्चिदानन्द स्वरूप आदि का ध्यान करते हुए फिर मुंह हाथ धोकर ईश्वर को याद रखते हुए अन्य कार्य करें। ईश स्मरण में (१) कोई अन्य वृत्ति न उठायें। (२) केवल ईश्वर में ध्यान लगाकर उसके गुणों का अर्थ सहित चिन्तन करें। (३) मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखें। एक ही स्थान पर नित्य प्रति बैठें ताकि उसी जगह बैठने पर वही ईश्वर मिलन के विचार आयेंगे। बैठने का समय भी निश्चित हो।
आसन पर बैठने का लक्ष्य दोहराएँ कि मैं प्रभु से मिलने बैठा हूँ, अन्य विचार नहीं करूँगा। मन जड़ है इसे मैं चलाऊँगा। जड़-चेतन का विवेक रखना। ईश्वर-प्रणिधान, प्रलयावस्था का सम्पादन करने से ईश्वर समर्पित होकर मन वश में हो जायेगा। सुन्दर दिखने वाले शरीर में मांस, हड्डी, मलमूत्र भरा है इस विचार से आकर्षण समाप्त हो जायेगा। परन्तु इसका उपयोग धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की उपलब्धि के लिये करना है
सर्वरक्षक-सर्वदाता ईश्वर - सृष्टि में सब पदार्थों को बना (रचना) कर सब प्राणियों को जीवन दे रहा है। ईश्वर रोटी, कपड़ा, मकान बनाकर नहीं देता परन्तु इनके लिये गेहूँ, कपास, लोहा, मिट्टी, पानी आदि देता है। आगे का काम जीव का है। ईश्वर की सहायता के बिना कोई भी जड़-चेतन वस्तु व्यक्ति का कुछ भी भला नहीं कर सकती। जो कुछ भला करते हैं वह ईश्वर प्रदत्त पदार्थों से ही सहायता प्राप्त करते हैं। ईश्वर नित्य कल्याण करता है, कभी प्रतिशोध नहीं करता। उपासक ईश्वर से उचित व्यवहार, उसे पाने की तीव्र इच्छा (जिज्ञासा), पुरुषार्थ, तप आदि करता है तो अपनी सत्य कामना पूर्ण करता है।
ईश खोज के लिये ध्यान - उपासक ऋषियों, गुरुओं से सुनकर उसको खोजता है। एक उच्च तत्त्व की खोज करता है। लौकिक चीजों से ध्यान हटाकर निष्क्रिय होकर बैठना, कुछ भी नहीं सोचना यह ध्यान नहीं। ''तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्" = जहाँ धारणा की है वहाँ एक ज्ञान का बना रहना ध्यान है। निर्विषय = सांसारिक विषय वस्तुओं से मन को हटाकर ईश्वर को जपता हुआ खोजता है - यह ध्यान है।
ईश्वर से बातें - हे प्रभु ! मैं आपका दर्शन साक्षात्कार करने बैठता हूँ। आपका स्वरूप वेदों के अनुसार और आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार है उसको मैं देखना चाहता हूँ। आप सच्चिदानन्द स्वरूप कष्ट-क्लेश रहित, शुभ अशुभ कर्म से रहित, भोग-वासनाओं से रहित पुरुष विशेष हैं। आप अनन्त ज्ञान के भण्डार हैं। आप मेरे पिता के भी पिता, गुरु के भी गुरु हैं। आप मुझे विद्या भी देते हैं। आपका नाम 'ओ३म्' है। आप के नाम जप विचार के फल से सब विघ्नों का नाश हो जाता है। हे प्रभु ! वेद आपको"सपर्यगात्, अकायम्" कहा है...।
जैसे एक अच्छे भूखे बालक को मां गोद में उठा दूध पिलाकर तृप्त कर देती है। इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीव को ईश्वर अपने ज्ञानानन्द से भरपूर करके समाधि लगा देता है ।
गुण-गुणी एक - गुण और गुणी की अलग-अलग व्याख्या की जाती है। किन्तु गुण और गुणी एक हैं, स्वतन्त्र वस्तु नहीं । ईश्वर साक्षात्कार में ईश्वर के गुणों द्वारा ही उसका प्रत्यक्ष-अनुभव-दर्शन होता है। जैसे अग्नि का गुण दाह प्रकाश है, इससे भिन्न अग्नि कुछ भी नहीं ।
ईश्वर का आनन्द कैसा ?
ईश्वर का आनन्द कैसा ?
ईश्वर आनन्द से परिपूर्ण है। जैसे भूखे व्यक्ति को अत्यन्त स्वादिष्ट उचित भोजन मिलने पर लौकिक सुख मिलता है (परन्तु यह हीन उपमा है)। ऐसे ही दुःख की निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा ईश्वर-प्राप्ति में होगी।
सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख मिश्रित है, मिश्री-हलवे की मिठास अन्तत: कम होते होते गारा मिट्टी के समान नीरस लगने लगेगी। परन्तु ईश्वर उपासना से आनन्द बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख से रोगी, ईश्वरीय सुख सेवन से निरोगी होता है। ईश्वर का आनन्द नित्य और विशुद्ध है।
जब तक व्यक्ति सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख नहीं अनुभव करता, तब तक ईश्वर के आनन्द में प्रवृत्त नहीं होता। जीवन काल में ही दुःखों से मुक्ति मिलने पर मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिलती है। केवल मरने से ही मुक्ति नहीं मिलती। जीवित रहते-रहते जिसने ब्रह्म को जान लिया सो वह कृतकृत्य हो गया। ईश्वर अनुपम होने से उसके लिये उपमा नहीं दी जा सकती परन्तु समझने की दृष्टि से हीन उपमा दी गई है। जो सर्वशक्तिमान् को सच्चा जानता-मानता है, उसके उचित न्याय पर भरोसा करता है वह कभी दु:खी नहीं होता। राजा तो अल्पज्ञता से उचित-अनुचित निर्णय भी देता है पर ईश्वर सदा उचित करेगा और वह भी सुधारने के हेतु दया ही करता है। धन सम्पत्ति की तुलना में योग विद्या की प्राप्ति में सहस्र गुणा सुख (आनन्द) अधिक है। में प्रभु को जानूँ, प्राप्त करूँ, साक्षात्कार करूँ यह भावना तीव्र रूप में बनाये रखें। केवल नाम स्मरण करते जाना परन्तु तदनुसार अपना चरित्र न सुधारना ईश्वर को प्राप्त करने का निष्फल प्रयास है ।
ईश्वर से उचित व्यवहार
ईश्वर से उचित व्यवहार
जो काम जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से करना चाहिये, तभी सफलता मिलती है। आसन पर बैठते ही सब विचार छोड़ देना। ऐसा न हो कि छेड़ना था ईश्वर का चिन्तन-मनन और छेड़ दिया व्यापार, धन्धा, पढ़ना आदि अन्य विषय। दिया समय ईश्वर को मिलने का और मुख फेर कर बातें-विचार करने लग गये संसार की संसार के साथ तो यह बुलाये हुए अतिथि के समान ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया, सो कैसे उसे प्राप्त कर सकेंगे?
इन्द्रिय दोष से और संस्कार दोष से अविद्या पैदा होती है। अज्ञान उद्वेग को पैदा करता है। सन्ध्या में बैठते ही निश्चय करो कि विषयों में मन को नहीं चलाऊँगा। जप अर्थ सहित, अपने को ईश्वर अर्पण करते हुए, प्रभु प्रेम में विह्वल हो, प्रभु से बातें करते हुए होना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से संध्या उपासना में मन लगने लगता है। कहा भी है-
पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे
तू नहीं जान पाये तो मैं क्या करू? (कवि प्रकाश)
व्यवहार काल - व्यवहार काल में यम-नियम का पालन करते हुए बुरी वृत्तियों को रोकना पड़ता है और अच्छी वृत्तियों को जगाना पड़ता है। व्यवहार काल में मन को देव मार्ग पर चलाये। जैसा कि वेद में कहा है-
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव ।
पुनर्ददताघ्नता जानता संगमेमहि । (ऋग्वेद)
ददता- अर्थात् दानी पुरुषों के साथ चलें। अष्नता- अहिंसक (द्वेष भावना रहित) पुरुषों के साथ चलें। जानता- ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का अनुकरण करें। सूर्य समान- बिना विश्राम लिए योग (= कल्याण) मार्ग पर लगातार चलें। कष्ट आने पर सस्मित रहें।व्यवहार काल में चोरी, जारी, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की प्रवृत्तियों को रोककर, स्वार्थ की जगह परोपकार, असत्य छोड़कर सत्य प्रवृत्तियों को जगायें। परन्तु उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों-विचारों को भी रोकना पड़ता है। जैसे वेद का पढ़ना-पढ़ाना, धर्म है। यज्ञ करना, दान, पठन-पाठन का विचार आदि को यदि उपासना काल में करेंगे तो ईश्वर से सम्बन्ध नहीं जुड़ पायेगा। व्यवहार काल में भी मन-इन्द्रियों को खुला नहीं छोड़ना, इन्हें यम-नियम से आबद्ध रखें।
उपासना काल - बालक का व्यवहार जैसे अपने माता-पिता-गुरु के साथ होता है वैसा ही व्यवहार जीवात्मा को परमात्मा के साथ करना चाहिए। प्रातः काल उपासना में बैठने की तैयारी जगते ही करनी पड़ती है। इस काल में कोई भी सांसारिक बातचीत, चर्चा- विचारणा न करके मौन धारण करना। दोनों काल की उपासना से पूर्व छोड़ने योग्य कार्य व विचारों को छोड़ना और करने योग्य कार्य व विचारों को ही करना। पहले जप, फिर अर्थ विचार, फिर समर्पण। जप में अज्ञान वश भूल से जो विचार उठें उसे पकड़ना और हटा देना। उलटे संस्कारों के कारण यदि कोई विचार असावधानी से उठा लें तो उसी समय सावधानी पूर्वक उसे हटा दिया जाये। पश्चात् भगवान की तरफ सहयोग के लिये दौड़ेंगे तब निश्चय ही हमें ईश्वर सहाय देगें।
योगविद्या का ज्ञान-विज्ञान जानने के लिये पहले चित्त की अवस्थायें जाननी पड़ेगी। पठित विद्वान् होने पर भी व्यक्त अनुभव करता है कि चित्त बलात् विषयों की ओर जा रहा है। गया कब? किसने भेजा ? यह वह भूल जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मन-इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बुद्धिपूर्वक की गई कुछ क्रियायें भी स्वभावतः होती लगती हैं। ईश्वर बुद्धिपूर्वक सृष्टि की रचना, पालन, व प्रलय करता है। इसी प्रकार जीव इन्द्रियों का चलाना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, चित्त का रोकना आदि क्रियाएँ करता है। वस्तुत: आपने स्वयं मन को चलाया, पर भूल यह हुई कि उसे पकड़ (जान) न सके कब चलाया ? ध्यान देंगे तो पता चल जायेगा कि मैं ही इसे विषयान्तर में ले गया था।
मन में तरंगें विचार उत्पन्न होते रहते हैं पर पता नहीं लगता। परन्तु सावधानी पूर्वक ध्यान देने से पता लगेगा कि मेंने एक मास पहले एक व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा था, महीनों-वर्षों बाद विशेष ध्यान देने पर पूर्व सोचा हुआ विचार याद आ जाता है। उपासक इसके कारण उपासना में चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता। लगा था संध्या करने सोचने लग गया अन्य विचार फिर १५ मिनट बाद पता लगा में कहीं चला गया मन को निरुद्ध करने का अभ्यास करते-करते उपासक को फिर ५ मिनट, एक मिनट, कुछ सेकण्ड बाद ही पता लग जाता है, कि मन को अन्य विषयों में लगा दिया, पर कब लगाया यह पता नहीं लगता। लगने के बाद पता चलता है कि मन विषयान्तर हो गया। अनेक बार पकड़ में आने पर भी, पता लगने पर भी व्यक्ति उन सांसारिक विचारों को चाहता है। तब उसे लगता है कि में खींचता हूँ ईश्वर की ओर पर मन खींचता है विषय चिन्तन की ओर। वास्तव में एक ही चेतनात्मा है जो मन को चलाता है। जीवात्मा अपनी सूक्ष्म इच्छा से ही मन को इतनी तीव्रता से चलाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि मन को चलाने वाला में हूँ वा यह स्वयं चल रहा है। ये सब बेकार का चिंतन असावधानी के कारण होता है। चेतना पूर्वक (तीव्र ज्ञान इच्छा पूर्वक) प्रयास करने से वृत्तियों का पता लग जाता है। जो क्रियायें सूक्ष्म इच्छाओं से होती हैं उनका पता साधक को नहीं चल पाता। इसे वैज्ञानिक अचेतन मन कहते हैं। वास्तव में सावधान-असावधान तो जीवात्मा ही होता है ।
अनुभव से संस्कार बनता है। संस्कार से स्मृति, और स्मृति से मानव चरित्र बनता है। अच्छे बुरे विचारों की टक्कर होती रहती है तब संघर्ष करने से विजय होगी। उस समय मन को चलाना छोड़ दो, शान्त हो जायेगा। जीतने पर गद्गद् हो जाता है, तब जो आनन्द आता है वह वर्णनातीत है। मन को जड़ मानकर साधक बार-बार यह वाक्य दोहराये "मेरी इच्छा के बिना यह जड़ मन इन्द्रियाँ चलेंगे ही नहीं। मैं जहाँ चलाऊँगा, विचारूँगा वहीं मेरे पीछे जायेंगे।"
अभ्यास - श्रद्धापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक व तपपूर्वक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान में निरन्तर लगे रहना अभ्यास कहलाता है। साधक अपने आचरण-व्यवहार को दीर्घ काल तक अर्थात् जब तक बुरे संस्कार दग्धबीज भाव को प्राप्त न हो जायें विधि पूर्वक निरन्तर अभ्यास करते हुए स्वच्छ व परिपक्व बनाये। यदि योगाभ्यास बीच में छोड़ दिया तो स्थिति वही की वही हो जायेगी। संस्कार तेजी से बिजली की तरह एक दूसरे को दबाते हैं। बुद्धिमान् अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करता है, बुरों को दबा देता है। परन्तु मूर्ख अच्छों को दबा देता है, बुरों को उभार कर विचारने लगता है। बड़ी तीव्रता से विचार चलते हैं। व्यवहार काल में ईश्वर को समक्ष नहीं रखा तो उपासना काल में प्राप्त करना कठिन होगा ।
संघर्ष - स्वस्थ (= योगस्थ) अवस्था में जीव के अधीन विचार तरंगें रहती हैं। निरोध के संस्कारों को जगाता है तो ईश्वर में आनन्द आने लगता है; और जब संसारी तरंगें जगाने लगता है तो दु:ख सागर में डूबता जाता है। मन को खुला छोड़ देने पर अन्यथा विचारेगा अन्यथा विचारने से बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। महान् बनने के लिये कुछ आदर्श हैं, नियम हैं, व्रत हैं, संकल्प हैं, उन्हें लेकर चलना पड़ता है, नहीं लेने से नीचे गिरता चला जायेगा। ईश्वर भी अपने अटल नियम पर चलता रहता है। साधक कभी निराश न हो। प्रयत्न करने पर भी मन डिग जाये तो प्रायश्चित्त करके पुन: सन्मार्ग पर चलना शुरू कर दे। गिरने पर पुनः चलने की प्रक्रिया से उन्नति होगी, न कि बिलकुल ही न चलने से। मन-वचन-कर्म से अपने वा अन्य के दोषों से सन्धि न करें। बुराईयों के साथ बड़ा भारी अथक संघर्ष/युद्ध करना पड़ता है।
मन की विचार तरंगें (वृत्तियां) स्वयं उठती हैं या मैं उठाता हूँ? मन-इन्द्रियाँ अथवा ईश्वर उठाता है ? सूक्ष्मता से विचारने पर ज्ञात होगा कि निश्चय ही केवल में स्वयं ही उठाता हूँ। इस प्रकार विचार करने से साधक को ऐसा प्रतीत होगा कि मुझ में साहस, श्रद्धा, शक्ति आ गई कि यह मेरे हाथ में है कि कब किस विचार को में उठाता हूँ। परन्तु यह सब ईश्वर प्रदत्त मानें। यदि 'अहम्' मैं करने वाला विचार लायेगा तो मिथ्या अभिमान होगा। लोकैषणा व स्वामित्त्व से अभिमान होता है जो साधक को पथ भ्रष्ट कर देता है।
सोते समय प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण करें। इन्द्रिय निग्रह अर्थात् उन्हें सदा अपने अधिकार में रखें ताकि बुराई में न फँसें रात्रि में सोने से पूर्व सोचें आज क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, फिर अन्तिम क्षण में ईश्वर चिन्तन के सिवाय अन्य कुछ न विचारें।
प्रात: उठते समय 'ओ३म्' सच्चिदानन्द स्वरूप आदि का ध्यान करते हुए फिर मुंह हाथ धोकर ईश्वर को याद रखते हुए अन्य कार्य करें। ईश स्मरण में (१) कोई अन्य वृत्ति न उठायें। (२) केवल ईश्वर में ध्यान लगाकर उसके गुणों का अर्थ सहित चिन्तन करें। (३) मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखें। एक ही स्थान पर नित्य प्रति बैठें ताकि उसी जगह बैठने पर वही ईश्वर मिलन के विचार आयेंगे। बैठने का समय भी निश्चित हो।
आसन पर बैठने का लक्ष्य दोहराएँ कि मैं प्रभु से मिलने बैठा हूँ, अन्य विचार नहीं करूँगा। मन जड़ है इसे मैं चलाऊँगा। जड़-चेतन का विवेक रखना। ईश्वर-प्रणिधान, प्रलयावस्था का सम्पादन करने से ईश्वर समर्पित होकर मन वश में हो जायेगा। सुन्दर दिखने वाले शरीर में मांस, हड्डी, मलमूत्र भरा है इस विचार से आकर्षण समाप्त हो जायेगा। परन्तु इसका उपयोग धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की उपलब्धि के लिये करना है
सर्वरक्षक-सर्वदाता ईश्वर - सृष्टि में सब पदार्थों को बना (रचना) कर सब प्राणियों को जीवन दे रहा है। ईश्वर रोटी, कपड़ा, मकान बनाकर नहीं देता परन्तु इनके लिये गेहूँ, कपास, लोहा, मिट्टी, पानी आदि देता है। आगे का काम जीव का है। ईश्वर की सहायता के बिना कोई भी जड़-चेतन वस्तु व्यक्ति का कुछ भी भला नहीं कर सकती। जो कुछ भला करते हैं वह ईश्वर प्रदत्त पदार्थों से ही सहायता प्राप्त करते हैं। ईश्वर नित्य कल्याण करता है, कभी प्रतिशोध नहीं करता। उपासक ईश्वर से उचित व्यवहार, उसे पाने की तीव्र इच्छा (जिज्ञासा), पुरुषार्थ, तप आदि करता है तो अपनी सत्य कामना पूर्ण करता है।
ईश खोज के लिये ध्यान - उपासक ऋषियों, गुरुओं से सुनकर उसको खोजता है। एक उच्च तत्त्व की खोज करता है। लौकिक चीजों से ध्यान हटाकर निष्क्रिय होकर बैठना, कुछ भी नहीं सोचना यह ध्यान नहीं। ''तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्" = जहाँ धारणा की है वहाँ एक ज्ञान का बना रहना ध्यान है। निर्विषय = सांसारिक विषय वस्तुओं से मन को हटाकर ईश्वर को जपता हुआ खोजता है - यह ध्यान है।
ईश्वर से बातें - हे प्रभु ! मैं आपका दर्शन साक्षात्कार करने बैठता हूँ। आपका स्वरूप वेदों के अनुसार और आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार है उसको मैं देखना चाहता हूँ। आप सच्चिदानन्द स्वरूप कष्ट-क्लेश रहित, शुभ अशुभ कर्म से रहित, भोग-वासनाओं से रहित पुरुष विशेष हैं। आप अनन्त ज्ञान के भण्डार हैं। आप मेरे पिता के भी पिता, गुरु के भी गुरु हैं। आप मुझे विद्या भी देते हैं। आपका नाम 'ओ३म्' है। आप के नाम जप विचार के फल से सब विघ्नों का नाश हो जाता है। हे प्रभु ! वेद आपको"सपर्यगात्, अकायम्" कहा है...।
जैसे एक अच्छे भूखे बालक को मां गोद में उठा दूध पिलाकर तृप्त कर देती है। इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीव को ईश्वर अपने ज्ञानानन्द से भरपूर करके समाधि लगा देता है ।
गुण-गुणी एक - गुण और गुणी की अलग-अलग व्याख्या की जाती है। किन्तु गुण और गुणी एक हैं, स्वतन्त्र वस्तु नहीं । ईश्वर साक्षात्कार में ईश्वर के गुणों द्वारा ही उसका प्रत्यक्ष-अनुभव-दर्शन होता है। जैसे अग्नि का गुण दाह प्रकाश है, इससे भिन्न अग्नि कुछ भी नहीं ।
see also: वैदिक धर्म प्रश्नोत्तरी
योग के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल न हुआ, न हो रहा है और न होगा। जीवन व्यवहार में शुभ कर्मों का करना अशुभ को छोड़ना। शुभ कर्मों को भी इतना उच्च बनाना कि केवल निष्काम कर्म रह जायें। कोई बात केवल कहने मात्र से सिद्ध नहीं होती, प्रमाणों से जो सिद्ध हो उसे सत्य जानें। योग चित्त की एक विशिष्ट अवस्था है। यह मन (चित्त) जड़ वस्तु है, फिर भी दो मिनट वश में नहीं रह सकता, भले ही वर्षों से जानता, मानता, करता रहा हो। जड़-चेतन की अलग-अलग विशेषतायें हैं; परन्तु बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी चेतन को जड़ का मिश्रण ही मान रहे हैं ।
दर्शन और विज्ञान दोनों स्वीकार करते हैं कि कारण के गुण कार्य में आते हैं। जैसे पीले रंग के धागे से पीला वस्त्र बनेगा सत्त्व-रज-तम रूप प्रकृति से बना मन भी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु की तरह जड़ है। परन्तु चेतना (= आत्मा) का संयोग होने से मन चेतन जैसा दीखता है, अनुभव होता है। जैसे हमारा शरीर जड़ होते हुए भी आत्म संयोग से चेतन दीखता है। जो ज्ञानादि संवेदनशीलता का अनुभव नहीं करता वह जड़ है। चेतन तत्व 'आत्मा' शरीर रूपी साधन से सम्बद्ध होने पर अपनी क्रियायें करने लगता है, इसलिये जिनके मत में पांच भूतों के संघात मात्र से ही शरीर चेतन होकर क्रियाएँ करने लगता है उनका मत ठीक नहीं। उनका मत मानने पर तो मृत्यु का हीअभाव हो जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है।
जड़ तत्त्व में क्रिया उत्पन्न करने के लिये चेतन की जरूरत पड़ती है। व्यवहार, विज्ञान, दर्शन से यह सिद्ध है। स्थिर वस्तु बिना बाह्य शक्ति के स्थिर ही रहेगी और चलायमान वस्तु चलती ही रहेगी जब तक कोई बाह्य शक्ति (=चेतन त्त्व) गति या स्थिर न करे। एक चलने वाला दूसरा चलाने वाला। एक रुकने वाला दूसरा रोकने वाला। एक जड़ दूसरा चेतन दो तत्त्व (= पदार्थ ) हुए ।
मन जड़ है - चित्त (मन) जड़ है, पर यह जीवात्मा के बाह्य विषयों का ज्ञान कराने का साधन है। जैसे टेलीफोन (साधन) को नहीं पता होता कि उस पर क्या बात हो रही है।
मन रोका जा सकता है। जैसे विद्यार्थी जड़ मन को परीक्षा देते समय तीन घण्टे रोक लेता है उस समय उसे खाने-पीने देखने व सैर करने आदि की बात कुछ नहीं सुहाती, कोई विचार नहीं आता क्योंकि वह परीक्षा के महत्त्व को जानता है। इसी प्रकार विषय (ईश्वर) का महत्त्व समझने पर योगाभ्यासी का मन रुक जाता है।
सामान्य इच्छायें नियम बनाने संकल्प करने से व तीव्र इच्छायें अभ्यास करने से रुकती हैं। सदा स्मरण रखें कि ईश्वर के बनाये हुए इस मन को मैं (ईश्वर की दी हुई शक्ति से) चलाता हूँ, न कि यह जड़ मन स्वयं चला (भाग) जाता है ।
रोकने में कठिनाई - नियम (संकल्प) के बिना मन को स्वतन्त्रता से विचारने दिया जाता है। दूसरे मन को चेतन मान रखा है कि वह जैसे स्वयं चला जाता है परन्तु जो ज्ञान से युक्त है वह चेतन है, जो इससे उलटा हो वह जड़। जैसे आँख के लिये कहें कि यह देखती है मानती नहीं। यह बात युक्ति संगत नहीं क्योंकि चक्षु को हम अपनी इच्छा अनुसार खोल या बन्द कर सकते हैं। इसी प्रकार मन को भी अपनी इच्छा शक्ति से विषयों से खींच सकते हैं, हटा सकते हैं। विचार स्वयं कदापि नहीं आते बल्कि हम विचारते हैं। विपरीत ज्ञान से, संस्कार दोष से ये विचार उभरते हैं अर्थात् हम उभारते हैं ।
मन की पांच अवस्थायें - (१) क्षिप्त=चञ्चल (२) मूढ=मूरच्छित, ज्ञान-विज्ञान से शून्य। (३) विक्षिप्त=इसमें चित्त की एकाग्रता आरम्भ होती है तो किसी बाधा से भंग हो जाती है। यथा बाहर की आवाज आदि से और आन्तरिक वृत्तियों से। (४) एकाग्र=इसमें चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। (५) निरुद्ध=ऊँचे ज्ञान-विज्ञान-विवेक के बाद
अनन्त ईश्वर में वृत्ति निरोध होने पर यह अवस्था आती है। उस काल में सर्दी-गर्मी एक सीमा तक नहीं सतायेगी। काम, क्रोध, लोभादि मर नहीं जाते, रुक जाते हैं। असावधानी से यदि क्लेश आये तो विवेक अभ्यास से तुरंत रोक सकता है। इस अवस्था में योगी देखता है कि भोगी- संसार क्लेश में पिस रहा है। पर में इनसे ऊपर आनन्द के पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ।
योगाभ्यासी मन को रोकने में समर्थ हो सकता है
यदि वह...
(१) मन को जड़ समझ ले ।
(२) स्वयं को मन का चलाने वाला जान ले।
(३) संसार के विषयों में दु:ख अनुभव करे।
(४) स्व-स्वामी सम्बन्ध का नाश कर दे ।
(५) व्याप्य-व्यापक का ज्ञान कर ले।
(६) भोक्ता-भोग्यपन को नष्ट कर दे ।
(७) ईश्वर प्रणिधान बना ले।
(८) शरीर व संसार को अनित्य समझ ले ।
(९) ऋषियों के निर्णयों पर विश्वास करे।
(१०) व्यवहार काल में भी मन को नियत्रित रखने का अभ्यास करे ।
(११) प्रलय अवस्था का सम्पादन कर ले।
योग में बाधक अविरति - अविरति=विरति (वैराग्य) का न होना अर्थात् संसार की वस्तुओं से वैराग्य भाव न होना, हर समय मन में कोई न कोई सांसारिक सुख का विचार बना रहता है। सुख के बाद राग भी होता है, वस्तु के सेवन के पश्चात् पुनः सेवन की इच्छा बनी रहती है। वैराग्य का अभाव एक रोग है। यह उपासना में बड़ा बाधक है। विवेक वैराग्य के अभाव में हम उपासना में मन नहीं लगा सकते। सांसारिक सुख की इच्छायें
उत्पन्न करते ही रहते हैं। इसे दूर करें।
योग विद्या व विज्ञान
योग विद्या व विज्ञान
योग के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल न हुआ, न हो रहा है और न होगा। जीवन व्यवहार में शुभ कर्मों का करना अशुभ को छोड़ना। शुभ कर्मों को भी इतना उच्च बनाना कि केवल निष्काम कर्म रह जायें। कोई बात केवल कहने मात्र से सिद्ध नहीं होती, प्रमाणों से जो सिद्ध हो उसे सत्य जानें। योग चित्त की एक विशिष्ट अवस्था है। यह मन (चित्त) जड़ वस्तु है, फिर भी दो मिनट वश में नहीं रह सकता, भले ही वर्षों से जानता, मानता, करता रहा हो। जड़-चेतन की अलग-अलग विशेषतायें हैं; परन्तु बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी चेतन को जड़ का मिश्रण ही मान रहे हैं ।
दर्शन और विज्ञान दोनों स्वीकार करते हैं कि कारण के गुण कार्य में आते हैं। जैसे पीले रंग के धागे से पीला वस्त्र बनेगा सत्त्व-रज-तम रूप प्रकृति से बना मन भी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु की तरह जड़ है। परन्तु चेतना (= आत्मा) का संयोग होने से मन चेतन जैसा दीखता है, अनुभव होता है। जैसे हमारा शरीर जड़ होते हुए भी आत्म संयोग से चेतन दीखता है। जो ज्ञानादि संवेदनशीलता का अनुभव नहीं करता वह जड़ है। चेतन तत्व 'आत्मा' शरीर रूपी साधन से सम्बद्ध होने पर अपनी क्रियायें करने लगता है, इसलिये जिनके मत में पांच भूतों के संघात मात्र से ही शरीर चेतन होकर क्रियाएँ करने लगता है उनका मत ठीक नहीं। उनका मत मानने पर तो मृत्यु का हीअभाव हो जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध है।
जड़ तत्त्व में क्रिया उत्पन्न करने के लिये चेतन की जरूरत पड़ती है। व्यवहार, विज्ञान, दर्शन से यह सिद्ध है। स्थिर वस्तु बिना बाह्य शक्ति के स्थिर ही रहेगी और चलायमान वस्तु चलती ही रहेगी जब तक कोई बाह्य शक्ति (=चेतन त्त्व) गति या स्थिर न करे। एक चलने वाला दूसरा चलाने वाला। एक रुकने वाला दूसरा रोकने वाला। एक जड़ दूसरा चेतन दो तत्त्व (= पदार्थ ) हुए ।
मन जड़ है - चित्त (मन) जड़ है, पर यह जीवात्मा के बाह्य विषयों का ज्ञान कराने का साधन है। जैसे टेलीफोन (साधन) को नहीं पता होता कि उस पर क्या बात हो रही है।
मन रोका जा सकता है। जैसे विद्यार्थी जड़ मन को परीक्षा देते समय तीन घण्टे रोक लेता है उस समय उसे खाने-पीने देखने व सैर करने आदि की बात कुछ नहीं सुहाती, कोई विचार नहीं आता क्योंकि वह परीक्षा के महत्त्व को जानता है। इसी प्रकार विषय (ईश्वर) का महत्त्व समझने पर योगाभ्यासी का मन रुक जाता है।
सामान्य इच्छायें नियम बनाने संकल्प करने से व तीव्र इच्छायें अभ्यास करने से रुकती हैं। सदा स्मरण रखें कि ईश्वर के बनाये हुए इस मन को मैं (ईश्वर की दी हुई शक्ति से) चलाता हूँ, न कि यह जड़ मन स्वयं चला (भाग) जाता है ।
रोकने में कठिनाई - नियम (संकल्प) के बिना मन को स्वतन्त्रता से विचारने दिया जाता है। दूसरे मन को चेतन मान रखा है कि वह जैसे स्वयं चला जाता है परन्तु जो ज्ञान से युक्त है वह चेतन है, जो इससे उलटा हो वह जड़। जैसे आँख के लिये कहें कि यह देखती है मानती नहीं। यह बात युक्ति संगत नहीं क्योंकि चक्षु को हम अपनी इच्छा अनुसार खोल या बन्द कर सकते हैं। इसी प्रकार मन को भी अपनी इच्छा शक्ति से विषयों से खींच सकते हैं, हटा सकते हैं। विचार स्वयं कदापि नहीं आते बल्कि हम विचारते हैं। विपरीत ज्ञान से, संस्कार दोष से ये विचार उभरते हैं अर्थात् हम उभारते हैं ।
मन की पांच अवस्थायें - (१) क्षिप्त=चञ्चल (२) मूढ=मूरच्छित, ज्ञान-विज्ञान से शून्य। (३) विक्षिप्त=इसमें चित्त की एकाग्रता आरम्भ होती है तो किसी बाधा से भंग हो जाती है। यथा बाहर की आवाज आदि से और आन्तरिक वृत्तियों से। (४) एकाग्र=इसमें चित्त की एकाग्रता बनी रहती है। (५) निरुद्ध=ऊँचे ज्ञान-विज्ञान-विवेक के बाद
अनन्त ईश्वर में वृत्ति निरोध होने पर यह अवस्था आती है। उस काल में सर्दी-गर्मी एक सीमा तक नहीं सतायेगी। काम, क्रोध, लोभादि मर नहीं जाते, रुक जाते हैं। असावधानी से यदि क्लेश आये तो विवेक अभ्यास से तुरंत रोक सकता है। इस अवस्था में योगी देखता है कि भोगी- संसार क्लेश में पिस रहा है। पर में इनसे ऊपर आनन्द के पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ।
योगाभ्यासी मन को रोकने में समर्थ हो सकता है
यदि वह...
(१) मन को जड़ समझ ले ।
(२) स्वयं को मन का चलाने वाला जान ले।
(३) संसार के विषयों में दु:ख अनुभव करे।
(४) स्व-स्वामी सम्बन्ध का नाश कर दे ।
(५) व्याप्य-व्यापक का ज्ञान कर ले।
(६) भोक्ता-भोग्यपन को नष्ट कर दे ।
(७) ईश्वर प्रणिधान बना ले।
(८) शरीर व संसार को अनित्य समझ ले ।
(९) ऋषियों के निर्णयों पर विश्वास करे।
(१०) व्यवहार काल में भी मन को नियत्रित रखने का अभ्यास करे ।
(११) प्रलय अवस्था का सम्पादन कर ले।
योग में बाधक अविरति - अविरति=विरति (वैराग्य) का न होना अर्थात् संसार की वस्तुओं से वैराग्य भाव न होना, हर समय मन में कोई न कोई सांसारिक सुख का विचार बना रहता है। सुख के बाद राग भी होता है, वस्तु के सेवन के पश्चात् पुनः सेवन की इच्छा बनी रहती है। वैराग्य का अभाव एक रोग है। यह उपासना में बड़ा बाधक है। विवेक वैराग्य के अभाव में हम उपासना में मन नहीं लगा सकते। सांसारिक सुख की इच्छायें
उत्पन्न करते ही रहते हैं। इसे दूर करें।
see also: सनातन धर्म के ग्रंथों के तथ्य
आपने उत्तम-उत्तम पदार्थों का निर्माण किया। उत्तम भोजन बनाय। स्वयं भी खाया तथा अन्यों को भी खिलाया। भावना यह बनी कि ये मेरे पदार्थ थे, मैंने भोजन का प्रबन्ध किया। यह मेरा, मैंने किया आदि विचार अज्ञान के कारण अच्छे लगते हैं, परन्तु जिन पदार्थों से प्रबन्ध किया वे सब ईश्वर के हैं। जिस शरीर से किया यह भी ईश्वर का दिया हुआ है। मेरी विद्या, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरा चातुर्य यह सब अपना मानने लगता है। अत: छोड़ते समय कष्ट होता है, परन्तु सच्चा योगी सब ईश्वर का मानता है। वह अपने सम्मान से विष तुल्य डरता है व अपमान को अमृत तुल्य मानता है। मेरा-मेरी की समझ, मेरा सम्मान हो आदि यह उलटी स्थिति क्यों बनी ? इसका कारण बाल्यावस्था से ही उलटी शिक्षा मिलते रहना है। बाल्यावस्था से लौकिक रस लेना सिखाया पर ईश्वर का रस लेना नहीं सिखाया।
भोग्य पदार्थ ईश्वर के मानकर सेवन करें, अपना न मानकर ईश्वर के समर्पण करें। ईश्वर के मानकर उनका रक्षण करते हुए प्रयोग करें। वास्तव में न्याय की बात यह है कि यह सब ईश्वर के बनाये हुए पदार्थ उसी के हैं। बिना शरीर के संसार भर के संपूर्ण जीव कुछ भी नहीं बना सकते।
स्व-स्वामी सम्बन्ध ही उपासना में बड़ा बाधक है, निष्काम कर्म में विघ्न है। लौकिक व्यक्ति अधिक से अधिक लौकिक वस्तुओं का संग्रह करके अपने आप को निर्भय, सुखी, बलवान् समझता है यह सब जीवन यापन के लिये साधन रूप में कुछ अंश में ठीक है परन्तु इसे साध्य समझना भूल है।
योगी तो स्व-स्वामी सम्बन्ध तोड़कर जितना भौतिक वस्तुओं का त्याग करेगा उतना ही अपने को निर्भय पायेगा तथा आनन्दित रहेगा। स्व-स्वामी सम्बन्ध में राग का कारण अविद्या है। जहाँ अधर्म होगा वहाँ दुःख होगा। जो भी धन, बल, रूप मिला है वह परमात्मा का मानकर चलेगा तो सुखी होगा।
व्यक्ति जितना अधिक संग्रह करेगा उतना ही अधिक पांच प्रकार का दोष उपस्थित होगा।
(१) अर्जन दोष, (२) रक्षण दोष, (३) क्षय दोष, (४) संग दोष , (५) हिंसा दोष। बिना प्राणियों को कष्ट दिये कोई भोग नहीं भोगा जा सकता।
आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा जहाँ अपने स्थायी निवास के आश्रम बनाये हुए हैं, उन स्व-स्वामी (=संग) दोष आता है। उसके द्वारा किये गये धर्म प्रचार, लेखन कार्य आदि सभी का उद्देश्य अपने आश्रम को भव्य बनाना होता है। उसकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है। इस बारे में एक देश विदेश में प्रतिष्ठित योगाचार्य का एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है। जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने अभिमान में आकर ऋषिकेश में लाखों रूपये संग्रह करके बड़े परिश्रम से, लगभग बीस वर्षों का समय लगाकर एक भव्य आश्रम बनाया। अन्त में उनके मुख से दुःखी मन से यह सुनने को मिला कि इस आश्रम की कुटियायें मुझे कूट रही हैं। उनको स्व-स्वामी सम्बन्ध सता रहा था। उन्हें सौपने के लिये योग्य पात्र अधिकारी नहीं मिले। संन्यासियों द्वारा अपने मठ-आश्रम बनाने में कुछ दोष समाज का भी है। समाज की कुव्यवस्था के कारण शरीर रक्षण के लिये संन्यासी उपदेशक को आश्रम बनाने पड़ते हैं।
उपासना काल में उपासक को नाम-रूप को तोड़ना पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं। जो चीज हम लेकर नहीं आये वह साथ भी नहीं जायेगी। अविद्या के कारण शरीर, धन, पुत्र, पत्नी को हम अपने आत्मा का अंग मान कर चलते हैं। व्यक्तम् = सगे सम्बन्धी आदि और अव्यक्तम् द्रव्य-धन-मकान-फैक्ट्री जब बढ़ते हैं तो में बढ़ रहा हूँ ऐसा मानता है। जब नष्ट होता है तो मेरा टुकड़ा टूट गया, में कमजोर हो गया, मर गया ऐसा समझ दु:खी होता है। यहाँ तक कि संन्यासी, आचार्य भी शिष्य, विद्यार्थी के आश्रम-गुरुकुल से चले जाने पर स्व-स्वामी सम्बन्ध के कारण रोने लगते हैं।
उपासना का अंग जप - ईश्वर की उपासना से उपासक में ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं। बार बार मंत्र का उच्चारण जप कहलाता है। वह मंत्र-श्लोक ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को जताने वाला हो।
जप तीन प्रकार से किया जाता है - (१) मानसिक विचार द्वारा। (२) अत्यल्प ध्वनि जिसमें केवल होठ हिलते हों। (३) वाचिक उच्च स्वर सें। इसलिये नहीं कि ईश्वर कहीं दूर है उसे पुकारें, परन्तु नवीन अभ्यासी के लिये बाह्य दूसरी ध्वनि बाधा न डाल सके और वह अपने ही स्वर को सुनकर अर्थ का विचार करके ईश्वर समर्पित हो सके।
साधक जब ज्ञान पूर्वक परिश्रम करता है तो उसे सफलता मिलती है। साधक को सदा बोध हो कि जिस-जिस काम के लिये मैं इच्छा व प्रयत्न करूँगा वही कार्य होगा। ऐसा न समझे कि मन में जैसे विचार आयेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। यह न समझे कि मेरी इच्छा के बिना मन-इन्द्रियाँ स्वत: कार्य में लग जाते हैं। शब्द को बोलते ही अर्थ बोध होना चाहिये। उस काल निरीक्षण करें कि क्या जप में गायत्री के पदों का अर्थ उच्चारण काल में रहता है या नहीं। धुन में, उच्चारण में भूल हो सकती है यह गौण है, मुख्य तो अर्थ में भूल न होना है। हमें ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ना है। उसका ज्ञान, बल, आनन्द लेना है। ऐसा समझ कर योगाभ्यास करना चाहिए। लम्बे स्वर से पदोच्चारण करते, शब्दार्थ करते हुए अन्य विचार आयें तो दूर कर फिर अर्थ पर ध्यान रखते हुए ईश्वर समर्पण (ईश्वर सम्बन्ध) भी बनाये रखें।
योग में बाधक स्व-स्वामी सम्बन्ध
योग में बाधक स्व-स्वामी सम्बन्ध
आपने उत्तम-उत्तम पदार्थों का निर्माण किया। उत्तम भोजन बनाय। स्वयं भी खाया तथा अन्यों को भी खिलाया। भावना यह बनी कि ये मेरे पदार्थ थे, मैंने भोजन का प्रबन्ध किया। यह मेरा, मैंने किया आदि विचार अज्ञान के कारण अच्छे लगते हैं, परन्तु जिन पदार्थों से प्रबन्ध किया वे सब ईश्वर के हैं। जिस शरीर से किया यह भी ईश्वर का दिया हुआ है। मेरी विद्या, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरा चातुर्य यह सब अपना मानने लगता है। अत: छोड़ते समय कष्ट होता है, परन्तु सच्चा योगी सब ईश्वर का मानता है। वह अपने सम्मान से विष तुल्य डरता है व अपमान को अमृत तुल्य मानता है। मेरा-मेरी की समझ, मेरा सम्मान हो आदि यह उलटी स्थिति क्यों बनी ? इसका कारण बाल्यावस्था से ही उलटी शिक्षा मिलते रहना है। बाल्यावस्था से लौकिक रस लेना सिखाया पर ईश्वर का रस लेना नहीं सिखाया।
भोग्य पदार्थ ईश्वर के मानकर सेवन करें, अपना न मानकर ईश्वर के समर्पण करें। ईश्वर के मानकर उनका रक्षण करते हुए प्रयोग करें। वास्तव में न्याय की बात यह है कि यह सब ईश्वर के बनाये हुए पदार्थ उसी के हैं। बिना शरीर के संसार भर के संपूर्ण जीव कुछ भी नहीं बना सकते।
स्व-स्वामी सम्बन्ध ही उपासना में बड़ा बाधक है, निष्काम कर्म में विघ्न है। लौकिक व्यक्ति अधिक से अधिक लौकिक वस्तुओं का संग्रह करके अपने आप को निर्भय, सुखी, बलवान् समझता है यह सब जीवन यापन के लिये साधन रूप में कुछ अंश में ठीक है परन्तु इसे साध्य समझना भूल है।
योगी तो स्व-स्वामी सम्बन्ध तोड़कर जितना भौतिक वस्तुओं का त्याग करेगा उतना ही अपने को निर्भय पायेगा तथा आनन्दित रहेगा। स्व-स्वामी सम्बन्ध में राग का कारण अविद्या है। जहाँ अधर्म होगा वहाँ दुःख होगा। जो भी धन, बल, रूप मिला है वह परमात्मा का मानकर चलेगा तो सुखी होगा।
व्यक्ति जितना अधिक संग्रह करेगा उतना ही अधिक पांच प्रकार का दोष उपस्थित होगा।
(१) अर्जन दोष, (२) रक्षण दोष, (३) क्षय दोष, (४) संग दोष , (५) हिंसा दोष। बिना प्राणियों को कष्ट दिये कोई भोग नहीं भोगा जा सकता।
आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा जहाँ अपने स्थायी निवास के आश्रम बनाये हुए हैं, उन स्व-स्वामी (=संग) दोष आता है। उसके द्वारा किये गये धर्म प्रचार, लेखन कार्य आदि सभी का उद्देश्य अपने आश्रम को भव्य बनाना होता है। उसकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है। इस बारे में एक देश विदेश में प्रतिष्ठित योगाचार्य का एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है। जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने अभिमान में आकर ऋषिकेश में लाखों रूपये संग्रह करके बड़े परिश्रम से, लगभग बीस वर्षों का समय लगाकर एक भव्य आश्रम बनाया। अन्त में उनके मुख से दुःखी मन से यह सुनने को मिला कि इस आश्रम की कुटियायें मुझे कूट रही हैं। उनको स्व-स्वामी सम्बन्ध सता रहा था। उन्हें सौपने के लिये योग्य पात्र अधिकारी नहीं मिले। संन्यासियों द्वारा अपने मठ-आश्रम बनाने में कुछ दोष समाज का भी है। समाज की कुव्यवस्था के कारण शरीर रक्षण के लिये संन्यासी उपदेशक को आश्रम बनाने पड़ते हैं।
उपासना काल में उपासक को नाम-रूप को तोड़ना पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं। जो चीज हम लेकर नहीं आये वह साथ भी नहीं जायेगी। अविद्या के कारण शरीर, धन, पुत्र, पत्नी को हम अपने आत्मा का अंग मान कर चलते हैं। व्यक्तम् = सगे सम्बन्धी आदि और अव्यक्तम् द्रव्य-धन-मकान-फैक्ट्री जब बढ़ते हैं तो में बढ़ रहा हूँ ऐसा मानता है। जब नष्ट होता है तो मेरा टुकड़ा टूट गया, में कमजोर हो गया, मर गया ऐसा समझ दु:खी होता है। यहाँ तक कि संन्यासी, आचार्य भी शिष्य, विद्यार्थी के आश्रम-गुरुकुल से चले जाने पर स्व-स्वामी सम्बन्ध के कारण रोने लगते हैं।
उपासना का अंग जप - ईश्वर की उपासना से उपासक में ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं। बार बार मंत्र का उच्चारण जप कहलाता है। वह मंत्र-श्लोक ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को जताने वाला हो।
जप तीन प्रकार से किया जाता है - (१) मानसिक विचार द्वारा। (२) अत्यल्प ध्वनि जिसमें केवल होठ हिलते हों। (३) वाचिक उच्च स्वर सें। इसलिये नहीं कि ईश्वर कहीं दूर है उसे पुकारें, परन्तु नवीन अभ्यासी के लिये बाह्य दूसरी ध्वनि बाधा न डाल सके और वह अपने ही स्वर को सुनकर अर्थ का विचार करके ईश्वर समर्पित हो सके।
साधक जब ज्ञान पूर्वक परिश्रम करता है तो उसे सफलता मिलती है। साधक को सदा बोध हो कि जिस-जिस काम के लिये मैं इच्छा व प्रयत्न करूँगा वही कार्य होगा। ऐसा न समझे कि मन में जैसे विचार आयेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। यह न समझे कि मेरी इच्छा के बिना मन-इन्द्रियाँ स्वत: कार्य में लग जाते हैं। शब्द को बोलते ही अर्थ बोध होना चाहिये। उस काल निरीक्षण करें कि क्या जप में गायत्री के पदों का अर्थ उच्चारण काल में रहता है या नहीं। धुन में, उच्चारण में भूल हो सकती है यह गौण है, मुख्य तो अर्थ में भूल न होना है। हमें ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ना है। उसका ज्ञान, बल, आनन्द लेना है। ऐसा समझ कर योगाभ्यास करना चाहिए। लम्बे स्वर से पदोच्चारण करते, शब्दार्थ करते हुए अन्य विचार आयें तो दूर कर फिर अर्थ पर ध्यान रखते हुए ईश्वर समर्पण (ईश्वर सम्बन्ध) भी बनाये रखें।
see also: मूर्ति पूजा- समीक्षा | विश्लेषण
(१) मंत्र का उच्चारण। (२) मन्त्र का अर्थ | (३) ईश्वर समर्पण। मैं ईश्वर के सामने उपस्थित होकर यह उच्चारण व अर्थ भावना कर रहा हूँ ऐसी भावना मन में बनाए रखें। यह ध्यान की रीति है। 'धीमहि' का अर्थ है हम आपके ज्ञान, बल, आनन्द, तेज को धारण कर रहे हैं। धारण करने का प्रयास कर रहे हैं।
कोई नई चीज सीखने में कठिनाई तो होगी। वर्षों के अभ्यास से विधि आयेगी। फिर क्रियारूप में करता है तब सफलता मिलती है। आठ अङ्गों का आचरण करने पर अशुद्धि का नाश होने पर आत्मा-परमात्मा का ज्ञान होने तक निरंतर ज्ञान में वृद्धि होती है। साधक के अविद्या- अधर्म का नाश होने पर समाधि प्राप्त होती है। यदि नहीं हो रही तो समझना चाहिए कुछ कमी-दोष है। मन-वाणी- शरीर से योगाङ्गों का ठीक आचरण नहीं कर रहे है ।
जिससे विचार, मनन, संकल्प, विकल्प करते हैं वह मन है, मन से विविध प्रकार की तरंगें उठती हैं उनको रोकना योग है। कई बार विपरीत समाचार सुन कर मन की तरंगों पर नियन्त्रण न कर पाने से हृदय गति रुकने से कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। उसी मन को समझ पूर्वक रोकने पर योगी बन जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर उपासना से जो ज्ञान-विज्ञान मिलता है वह जीवन निर्माण में अद्भुत होता है। जो ऋषि दयानन्द में ईश्वर की उपासना न होती तो सारे संसार का विरोध कैसे सहते? एक ओर काशी के सैकड़ों विद्वान् पण्डित और काशी नरेश अपने हजारों अनुयायी लोगों सहित शास्त्रार्थ समर में ऋषि को पराजित करने पर उतारु, तो दूसरी और निर्द्न्द्ध दयानन्द अकेले। उनकी भाषा ऐसी कि जैसे परमात्मा के सामने खड़े होकर बात कर रहे हों ।
ईश्वर उपासना की औपचारिकता निभाने के लिये प्रातः सायं केवल पन्द्रह मिनट मंत्र बोल लिये, इस प्रकार से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर ईश्वर की उपासना करता है, उससे सम्बन्ध जोड़े रखता है उसका सारा जीवन कार्य करते हुए ईश्वर के आनन्द, ज्ञान, बल से परिपूर्ण रहता है।
ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा मन में इतनी अधिक होवे कि ईश्वर को छोड़कर अन्य कुछ भी न भावे (=अच्छा लगे)। यदि ईश्वर प्राप्ति के संस्कार नहीं हैं तो बनाये जा सकते हैं। ईश्वर के तुल्य या ईश्वर से अधिक किसी पदार्थ को न मानें। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए साधक को ईश्वर शीघ्र अपना कर अपना स्वरूप दिखा देता है।
गायत्री मन्त्र या अन्य किसी मंत्र को लेकर केवल हजार-लाख बार पाठ करने से नहीं परन्तु धीमी गति से अर्थ और भक्ति भाव सहित जप से आनन्द आता है। धीमी गति में सावधानी से अर्थ सहित जप करते हुए यदि साधक मन को विषयान्तर करता है तो पकड़ में आ जाता धीमी लम्बी गति से शब्द का अर्थ करने से और स्वर मधुर होने से ऋषिकृत अर्थ पर प्रेम भाव होता है। इसके साथ अन्य विषय में मन को नहीं लगाना| याद रहे हमारी आत्मा के प्रयत्न बिना मन अपने आप कहीं नहीं जायेगा। क्रिया करने वाले पदार्थ केवल दो ही हैं। हम और ईश्वर| यही दो
ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाले हैं, अन्य प्राण, इन्द्रियाँ, मन, वायु, जल, आकाश आदि नहीं।
हमारे मन में आत्मा के प्रयत्न बिना कभी भी विचार नहीं आता। वस्तुत: यह विचार कौन उठाता है? हताशा, निराशा, कौन ले आता है? अपने मन को शरीर के किसी एक भाग पर स्थित करते हुए एक केन्द्र पर विचारो कि "यह विचार कहाँ से आते हैं ?" देखें, निरीक्षण करें कहीं से नहीं आते। इससे सरल जप करते जाओ अर्थ करते जाओ। यदि असावधानी से मन गया, (नहीं-नहीं भेज दिया) फिर वृत्ति रोकते जाओ चलते जाओ। जैसे मोटर ड्राईवर सामने आजू-बाजू भी देखता है, ब्रेक भी लगाता है, स्टीयरिंग भी काबू में रखता है। ध्यान ईश्वर में लगाने से विषयान्तर में नहीं जायेगा। कठिनाई तब उत्पन्न होती है, जब मन में ईश्वर के प्रति शंका उत्पन्न होती है, कि 'जिसका में ध्यान कर रहा हूँ वह ईश्वर है या नहीं? यह विचारों की टक्कर चलेगी । जैसे कार चालक चौराहे पर सोचेगा कौन सा मार्ग मेरे गंतव्य की ओर आता है? वह रुकेगा, पर जब पता चलेगा कि यह रास्ता मेरे लिये है तो बिना हिचके चला जायेगा। अत: शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण पर विश्वास रख कर यह 'ऋषियों के प्रयोग' स्वयं करके देखें।
परिभाषा : 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'। (यो. द. ३/२) अर्थात् धारणा करने वाले स्थान पर मन को स्थिर करके, ईश्वर की खोज सम्बन्धी ज्ञान का लगातार बने रहना ध्यान है।
मुण्डक उपनिषद् में ध्यान की विधि -
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥
अर्थ - प्रणव : (ब्रह्मवाचक) ओम् (पद) ही धनुष है, और आत्मा बाण है तथा ब्रह्म (परमात्मा) ही उस जीवात्मा का लक्ष्य कहा जाता है। उस लक्ष्यरूपी ब्रह्म को प्रमाद रहित सावधान होकर बींधना चाहिये। बाण की तरह उस लक्ष्य में घुस जाये (लीन होवें)।
प्रश्न - क्या निराकार का भी ध्यान हो सकता है ?
उत्तर - हाँ। निराकार का भी ध्यान होता है। यदि निराकार वस्तु को आकार=रंग, रूप, सीमा वाली मानकर ध्यान करेंगे तो उस वस्तु का ध्यान नहीं होगा, बल्कि अध्यान होगा। पदार्थ का जो गुण है उसे लेकर ही ध्यान हो सकता है। जैसा ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव नहीं है वैसा ध्यान करने से कभी भी उसका ध्यान नहीं हो सकता है। गलत रूप में वस्तु का ध्यान करने से ही आज दु:ख की वृद्धि हो रही है, परम सुख अप्राप्य है। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति का (पर्स) बटुआ जिसका रंग नीला, ६ x ४, इंच लम्बा चौड़ा दस हजार रुपये से भरा हुआ अंधेरी गली में खो गया। अब उस बटुए को हम अन्धेरी गली में खोजते हैं, वह जब तक नहीं मिलता तब तक खोज चलती ही रहती है यही ध्यान कहलाता है। मिलने पर ध्यान समाप्त।
'ध्यानं निर्विषयं मनः' इस सूत्र की व्याख्या 'जिसमें कुछ भी पता न लगें इस प्रकार के कुछ विद्वानों ने योग के क्षेत्र में यह महा भ्रम फैलाया हुआ है। कुछ भी पता न लगे का यथार्थ अर्थ है बाहर के वातावरण से हट जाना। जो दु:ख का कारण है वह हट जाये। परन्तु शान्त होते हुए भी बुद्धिपूर्वक ईश्वर तत्त्व से संबन्ध जुड़े बिना विशेष सफलता नहीं मिलती। कई कहते हैं। अपने शरीर में दुःख ढूंढ़ने लगो। उससे बाहर से कुछ राहत तो होगी, परन्तु यह अशुद्ध है। कई श्वास पर ध्यान रखने को कहते हैं, यह भी अपूर्ण है।
जैसे अनजाना विदेशी लाल किले को देखने आता है जैसा वर्णन उसने सुना वैसा ही मन में रखते हुए लाल किले की खोज करेगा। यदि जामा-मस्जिद को ध्यान में रख रहा है और ढूंढ़ता है लाल किले को तो वह कभी भी लाल किले के दर्शन नहीं कर सकेगा। एक वस्तु को इस जन्म में देखा नहीं परन्तु शब्द प्रमाण से या अनुमान से गुण, कर्म, स्वभाव दिमाग में रखकर ढूँढ़ता है तो मिलती है। उस वस्तु को जिसे वह ढूँढ़ता है उसका शाब्दिक ज्ञान या आनुमानिक ज्ञान होना चाहिए। ध्यान करते हुए ईश्वर नामक वस्तु को ढूँढ़ते हुए साधक ऐसा लालायित रहे विह्वल हो जाये जैसे छोटा बालक माँ के लिये रहता है।
ध्यान में अन्य सब कार्य विचार रोक देना, केवल ईश्वर तत्त्व का ही विचार करना। अच्छे-बुरे सभी विचार त्याग देना। विचार प्रारम्भ से ही न उठाए जायें। व्यवहार काल में जिससे अनबन या मन मुटाव खींचातानी हुई उसको सजा देने का ख्याल उपासना में बैठते ही यदि नहीं दबाया तो उपासना कर ही नहीं पायेगा। उसे तुरन्त रोकना वरना बाद में काफी देर तक यह विचार ही पीछा नहीं छोड़ेगा।
प्रलयवत् संसार - बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत् देखने, अनुभव करने से समाधि प्राप्त होती है। शरीर उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उत्पन्न होने के बाद कालान्तर में नहीं रहेगा। दूसरे शरीर आयेंगे, वे भी जायेंगे। एक दिन ऐसा आयेगा कि कोई भी नहीं रहेगा इसी प्रकार ये सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी भी नहीं रहेंगे। इस अवस्था में केवल ईश्वर शेष रहने पर जीवात्मा उस अनन्त में चक्कर काटने पर ईश्वर में स्थिर (समाधि प्राप्त) हो जायेगा। इसी तरह मृत्यु में (जो अवश्यम्भावी है) अपने शरीर को पहुँचा दें। मृत्यु भय से भागें तो जायें कहाँ? इस प्रकार वृत्तियों की सब दौड़-धूप समाप्त हो जायेगी। साधक ज्ञान के स्तर पर सब से नाता तोड़ता, छोड़ता जाता है और समाधि को प्राप्त होता है।
ईश्वर का प्रत्यक्ष - जैसे अग्नि का अपने गुण गर्मी, प्रकाश, दाहक शक्ति से प्रत्यक्ष होता है। मिश्री का अपने रूप व मिठास से प्रत्यक्ष होता है। वैसे ही ईश्वर अपने गुण आनन्द-बल-ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष अवस्था में साधक, सारे संसार को ईश्वर में डूबा हुआ जानता
व्याप्य - व्यापक का विज्ञान जाने बिना सफलता नहीं मिलती। हम व लोक लोकान्तर व्याप्य और ईश्वर व्यापक है। जब अन्य वस्तु में मन लगायें तो वहाँ भी ईश्वर को व्यापक देखें। फिर दूसरी तीसरी वस्तु में जहाँ भी साधक देखेगा। वहाँ ईश्वर दिखाई देगा। सूर्य व्याप्य में ईश्वर व्यापक देखें। सम्बोधित करें हे ओ३म् ! आदित्य आपके बाण हैं हमारी रक्षा के लिये। व्यापक के प्रभाव से व्याप्य का प्रभाव समाप्त हो जायेगा जैसे व्याप्य लोहे का गोला व्यापक अग्नि के प्रभाव से अग्निवत् लाल हो जाता है।
जैसे ही साधक बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत् बना देता है उस अवस्था में वृत्ति निरोध होकर समाधि आरम्भ हो जायेगी। यह प्रारम्भिक अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि है। इस में ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे बंकर में बैठा व्यक्ति बमों की मार से सुरक्षित होता है, इसी प्रकार प्रलयवत् अवस्था में बाहर के काम, क्रोध, मोह आदि बमों की मार से योग साधक सुरक्षित रहता है।
ईश्वर - नियामक तत्त्व - आज का वैज्ञानिक भी सृष्टि में हर जगह नियम देखता है। बिना नियामक के नियम नहीं होता। अचानक दुर्घटना में चोट आदि का कम-अधिक लगना, मरना या बचना सो कार्य ईश्वर का नहीं। यह तो 'क्रियाभेदात् परिणामभेदः ' ही है जिसका परिणाम अनिश्चित है। परन्तु जहाँ क्रिया बार-बार एक ही प्रकार हो वहाँ यह ज्ञान होता है कि इन क्रियाओं का नियामक कोई शक्तिमान् त्त्व अवश्य है। जो इस सृष्टि को चलाता है। एक ऐसा जड़ तत्त्व जो चलाए बिना चले नहीं, गतिशील पत्थर स्वयं विचार कर रुके नहीं। परन्तु चेतन जीव स्वयं विचार कर सकता है। इन गतिमान् सूर्य, पृथ्वी, तारों आदि को चलाने वाला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् तत्त्व ईश्वर है। क्योंकि अप्राप्य देश में कत्ता के बिना क्रिया नहीं होती।
जप में तीन काम
जप में तीन काम
(१) मंत्र का उच्चारण। (२) मन्त्र का अर्थ | (३) ईश्वर समर्पण। मैं ईश्वर के सामने उपस्थित होकर यह उच्चारण व अर्थ भावना कर रहा हूँ ऐसी भावना मन में बनाए रखें। यह ध्यान की रीति है। 'धीमहि' का अर्थ है हम आपके ज्ञान, बल, आनन्द, तेज को धारण कर रहे हैं। धारण करने का प्रयास कर रहे हैं।
कोई नई चीज सीखने में कठिनाई तो होगी। वर्षों के अभ्यास से विधि आयेगी। फिर क्रियारूप में करता है तब सफलता मिलती है। आठ अङ्गों का आचरण करने पर अशुद्धि का नाश होने पर आत्मा-परमात्मा का ज्ञान होने तक निरंतर ज्ञान में वृद्धि होती है। साधक के अविद्या- अधर्म का नाश होने पर समाधि प्राप्त होती है। यदि नहीं हो रही तो समझना चाहिए कुछ कमी-दोष है। मन-वाणी- शरीर से योगाङ्गों का ठीक आचरण नहीं कर रहे है ।
जिससे विचार, मनन, संकल्प, विकल्प करते हैं वह मन है, मन से विविध प्रकार की तरंगें उठती हैं उनको रोकना योग है। कई बार विपरीत समाचार सुन कर मन की तरंगों पर नियन्त्रण न कर पाने से हृदय गति रुकने से कईयों की मृत्यु भी हो जाती है। उसी मन को समझ पूर्वक रोकने पर योगी बन जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर उपासना से जो ज्ञान-विज्ञान मिलता है वह जीवन निर्माण में अद्भुत होता है। जो ऋषि दयानन्द में ईश्वर की उपासना न होती तो सारे संसार का विरोध कैसे सहते? एक ओर काशी के सैकड़ों विद्वान् पण्डित और काशी नरेश अपने हजारों अनुयायी लोगों सहित शास्त्रार्थ समर में ऋषि को पराजित करने पर उतारु, तो दूसरी और निर्द्न्द्ध दयानन्द अकेले। उनकी भाषा ऐसी कि जैसे परमात्मा के सामने खड़े होकर बात कर रहे हों ।
ईश्वर उपासना की औपचारिकता निभाने के लिये प्रातः सायं केवल पन्द्रह मिनट मंत्र बोल लिये, इस प्रकार से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति दिन भर ईश्वर की उपासना करता है, उससे सम्बन्ध जोड़े रखता है उसका सारा जीवन कार्य करते हुए ईश्वर के आनन्द, ज्ञान, बल से परिपूर्ण रहता है।
ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा मन में इतनी अधिक होवे कि ईश्वर को छोड़कर अन्य कुछ भी न भावे (=अच्छा लगे)। यदि ईश्वर प्राप्ति के संस्कार नहीं हैं तो बनाये जा सकते हैं। ईश्वर के तुल्य या ईश्वर से अधिक किसी पदार्थ को न मानें। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते हुए साधक को ईश्वर शीघ्र अपना कर अपना स्वरूप दिखा देता है।
जप की विधि
जप की विधि
गायत्री मन्त्र या अन्य किसी मंत्र को लेकर केवल हजार-लाख बार पाठ करने से नहीं परन्तु धीमी गति से अर्थ और भक्ति भाव सहित जप से आनन्द आता है। धीमी गति में सावधानी से अर्थ सहित जप करते हुए यदि साधक मन को विषयान्तर करता है तो पकड़ में आ जाता धीमी लम्बी गति से शब्द का अर्थ करने से और स्वर मधुर होने से ऋषिकृत अर्थ पर प्रेम भाव होता है। इसके साथ अन्य विषय में मन को नहीं लगाना| याद रहे हमारी आत्मा के प्रयत्न बिना मन अपने आप कहीं नहीं जायेगा। क्रिया करने वाले पदार्थ केवल दो ही हैं। हम और ईश्वर| यही दो
ज्ञान पूर्वक क्रिया करने वाले हैं, अन्य प्राण, इन्द्रियाँ, मन, वायु, जल, आकाश आदि नहीं।
हमारे मन में आत्मा के प्रयत्न बिना कभी भी विचार नहीं आता। वस्तुत: यह विचार कौन उठाता है? हताशा, निराशा, कौन ले आता है? अपने मन को शरीर के किसी एक भाग पर स्थित करते हुए एक केन्द्र पर विचारो कि "यह विचार कहाँ से आते हैं ?" देखें, निरीक्षण करें कहीं से नहीं आते। इससे सरल जप करते जाओ अर्थ करते जाओ। यदि असावधानी से मन गया, (नहीं-नहीं भेज दिया) फिर वृत्ति रोकते जाओ चलते जाओ। जैसे मोटर ड्राईवर सामने आजू-बाजू भी देखता है, ब्रेक भी लगाता है, स्टीयरिंग भी काबू में रखता है। ध्यान ईश्वर में लगाने से विषयान्तर में नहीं जायेगा। कठिनाई तब उत्पन्न होती है, जब मन में ईश्वर के प्रति शंका उत्पन्न होती है, कि 'जिसका में ध्यान कर रहा हूँ वह ईश्वर है या नहीं? यह विचारों की टक्कर चलेगी । जैसे कार चालक चौराहे पर सोचेगा कौन सा मार्ग मेरे गंतव्य की ओर आता है? वह रुकेगा, पर जब पता चलेगा कि यह रास्ता मेरे लिये है तो बिना हिचके चला जायेगा। अत: शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण पर विश्वास रख कर यह 'ऋषियों के प्रयोग' स्वयं करके देखें।
जप के विशेष वाक्यः
ओ३म् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।
ओ३म् असतो मा सद्गमय ।
ओ३म् तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
ओ३म् मृत्योर्माऽमृतं गमय ।
उपासना का अंग ध्यान
उपासना का अंग ध्यान
परिभाषा : 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'। (यो. द. ३/२) अर्थात् धारणा करने वाले स्थान पर मन को स्थिर करके, ईश्वर की खोज सम्बन्धी ज्ञान का लगातार बने रहना ध्यान है।
मुण्डक उपनिषद् में ध्यान की विधि -
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत् तन्मयो भवेत् ॥
अर्थ - प्रणव : (ब्रह्मवाचक) ओम् (पद) ही धनुष है, और आत्मा बाण है तथा ब्रह्म (परमात्मा) ही उस जीवात्मा का लक्ष्य कहा जाता है। उस लक्ष्यरूपी ब्रह्म को प्रमाद रहित सावधान होकर बींधना चाहिये। बाण की तरह उस लक्ष्य में घुस जाये (लीन होवें)।
प्रश्न - क्या निराकार का भी ध्यान हो सकता है ?
उत्तर - हाँ। निराकार का भी ध्यान होता है। यदि निराकार वस्तु को आकार=रंग, रूप, सीमा वाली मानकर ध्यान करेंगे तो उस वस्तु का ध्यान नहीं होगा, बल्कि अध्यान होगा। पदार्थ का जो गुण है उसे लेकर ही ध्यान हो सकता है। जैसा ईश्वर का गुण-कर्म-स्वभाव नहीं है वैसा ध्यान करने से कभी भी उसका ध्यान नहीं हो सकता है। गलत रूप में वस्तु का ध्यान करने से ही आज दु:ख की वृद्धि हो रही है, परम सुख अप्राप्य है। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति का (पर्स) बटुआ जिसका रंग नीला, ६ x ४, इंच लम्बा चौड़ा दस हजार रुपये से भरा हुआ अंधेरी गली में खो गया। अब उस बटुए को हम अन्धेरी गली में खोजते हैं, वह जब तक नहीं मिलता तब तक खोज चलती ही रहती है यही ध्यान कहलाता है। मिलने पर ध्यान समाप्त।
'ध्यानं निर्विषयं मनः' इस सूत्र की व्याख्या 'जिसमें कुछ भी पता न लगें इस प्रकार के कुछ विद्वानों ने योग के क्षेत्र में यह महा भ्रम फैलाया हुआ है। कुछ भी पता न लगे का यथार्थ अर्थ है बाहर के वातावरण से हट जाना। जो दु:ख का कारण है वह हट जाये। परन्तु शान्त होते हुए भी बुद्धिपूर्वक ईश्वर तत्त्व से संबन्ध जुड़े बिना विशेष सफलता नहीं मिलती। कई कहते हैं। अपने शरीर में दुःख ढूंढ़ने लगो। उससे बाहर से कुछ राहत तो होगी, परन्तु यह अशुद्ध है। कई श्वास पर ध्यान रखने को कहते हैं, यह भी अपूर्ण है।
जैसे अनजाना विदेशी लाल किले को देखने आता है जैसा वर्णन उसने सुना वैसा ही मन में रखते हुए लाल किले की खोज करेगा। यदि जामा-मस्जिद को ध्यान में रख रहा है और ढूंढ़ता है लाल किले को तो वह कभी भी लाल किले के दर्शन नहीं कर सकेगा। एक वस्तु को इस जन्म में देखा नहीं परन्तु शब्द प्रमाण से या अनुमान से गुण, कर्म, स्वभाव दिमाग में रखकर ढूँढ़ता है तो मिलती है। उस वस्तु को जिसे वह ढूँढ़ता है उसका शाब्दिक ज्ञान या आनुमानिक ज्ञान होना चाहिए। ध्यान करते हुए ईश्वर नामक वस्तु को ढूँढ़ते हुए साधक ऐसा लालायित रहे विह्वल हो जाये जैसे छोटा बालक माँ के लिये रहता है।
ध्यान में अन्य सब कार्य विचार रोक देना, केवल ईश्वर तत्त्व का ही विचार करना। अच्छे-बुरे सभी विचार त्याग देना। विचार प्रारम्भ से ही न उठाए जायें। व्यवहार काल में जिससे अनबन या मन मुटाव खींचातानी हुई उसको सजा देने का ख्याल उपासना में बैठते ही यदि नहीं दबाया तो उपासना कर ही नहीं पायेगा। उसे तुरन्त रोकना वरना बाद में काफी देर तक यह विचार ही पीछा नहीं छोड़ेगा।
प्रलयवत् संसार - बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत् देखने, अनुभव करने से समाधि प्राप्त होती है। शरीर उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उत्पन्न होने के बाद कालान्तर में नहीं रहेगा। दूसरे शरीर आयेंगे, वे भी जायेंगे। एक दिन ऐसा आयेगा कि कोई भी नहीं रहेगा इसी प्रकार ये सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी भी नहीं रहेंगे। इस अवस्था में केवल ईश्वर शेष रहने पर जीवात्मा उस अनन्त में चक्कर काटने पर ईश्वर में स्थिर (समाधि प्राप्त) हो जायेगा। इसी तरह मृत्यु में (जो अवश्यम्भावी है) अपने शरीर को पहुँचा दें। मृत्यु भय से भागें तो जायें कहाँ? इस प्रकार वृत्तियों की सब दौड़-धूप समाप्त हो जायेगी। साधक ज्ञान के स्तर पर सब से नाता तोड़ता, छोड़ता जाता है और समाधि को प्राप्त होता है।
ईश्वर का प्रत्यक्ष - जैसे अग्नि का अपने गुण गर्मी, प्रकाश, दाहक शक्ति से प्रत्यक्ष होता है। मिश्री का अपने रूप व मिठास से प्रत्यक्ष होता है। वैसे ही ईश्वर अपने गुण आनन्द-बल-ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष अवस्था में साधक, सारे संसार को ईश्वर में डूबा हुआ जानता
व्याप्य - व्यापक का विज्ञान जाने बिना सफलता नहीं मिलती। हम व लोक लोकान्तर व्याप्य और ईश्वर व्यापक है। जब अन्य वस्तु में मन लगायें तो वहाँ भी ईश्वर को व्यापक देखें। फिर दूसरी तीसरी वस्तु में जहाँ भी साधक देखेगा। वहाँ ईश्वर दिखाई देगा। सूर्य व्याप्य में ईश्वर व्यापक देखें। सम्बोधित करें हे ओ३म् ! आदित्य आपके बाण हैं हमारी रक्षा के लिये। व्यापक के प्रभाव से व्याप्य का प्रभाव समाप्त हो जायेगा जैसे व्याप्य लोहे का गोला व्यापक अग्नि के प्रभाव से अग्निवत् लाल हो जाता है।
जैसे ही साधक बौद्धिक स्तर पर संसार को प्रलयवत् बना देता है उस अवस्था में वृत्ति निरोध होकर समाधि आरम्भ हो जायेगी। यह प्रारम्भिक अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि है। इस में ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे बंकर में बैठा व्यक्ति बमों की मार से सुरक्षित होता है, इसी प्रकार प्रलयवत् अवस्था में बाहर के काम, क्रोध, मोह आदि बमों की मार से योग साधक सुरक्षित रहता है।
ईश्वर - नियामक तत्त्व - आज का वैज्ञानिक भी सृष्टि में हर जगह नियम देखता है। बिना नियामक के नियम नहीं होता। अचानक दुर्घटना में चोट आदि का कम-अधिक लगना, मरना या बचना सो कार्य ईश्वर का नहीं। यह तो 'क्रियाभेदात् परिणामभेदः ' ही है जिसका परिणाम अनिश्चित है। परन्तु जहाँ क्रिया बार-बार एक ही प्रकार हो वहाँ यह ज्ञान होता है कि इन क्रियाओं का नियामक कोई शक्तिमान् त्त्व अवश्य है। जो इस सृष्टि को चलाता है। एक ऐसा जड़ तत्त्व जो चलाए बिना चले नहीं, गतिशील पत्थर स्वयं विचार कर रुके नहीं। परन्तु चेतन जीव स्वयं विचार कर सकता है। इन गतिमान् सूर्य, पृथ्वी, तारों आदि को चलाने वाला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान् तत्त्व ईश्वर है। क्योंकि अप्राप्य देश में कत्ता के बिना क्रिया नहीं होती।
see also: ईश्वरीय ज्ञान – वेद
ध्यान के समय में नींद को या आलस्य को रोकना आवश्यक होता है। अनेक साधकों को तो यह पता भी नहीं चलता कि वे ध्यान करते हुए सो जाते हैं। अनेकों को पता तो चल जाता है, किन्तु उपासना काल में नींद या आलस्य क्यों आता है, वे कारणों को ठीक-ठीक जान नहीं पाते हैं। नींद तथा आलस्य आने के कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है -
साधक लोगों को देखना चाहिए कि उपर्युक्त कारणों में से कौन सा कारण मुझ पर लागू होता है। उसे जानकर दूर करना चाहिए, जिससे योगाभ्यास में सफलता मिले ।
मनुष्य यदि अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ, आदर्श, महान् बनाना चाहता है तो नित्य सोने से पूर्व आत्मनिरीक्षण करे, अपने अन्तःकरण में झांके कि दिन भर मैंने क्या-क्या त्रुटियाँ-दोष-भूलें की हैं। विचारें 'क्या किया जो नहीं करना चाहिये था और क्या नहीं किया जो करना चाहिये था'। त्रुटियों को पकड़ें, प्रायश्चित्त करें, स्वयं दण्ड लें और भविष्य में न करने का प्रयत्न करें। कोई व्यक्ति बाहरी तौर से कितना ही धन से, बल से, कपड़ों से साफ-सुथरा सभ्य और सबल हो, परन्तु अन्त:करण से मलिन, कमजोर, खिन्न व दु:खी होगा तो वह गिर जायेगा।
बाह्य दु:ख के बजाय मानसिक शोक-दुःख-पीड़ा-काम, क्रोध, लोभ, मोह से व्यक्ति अधिक दु:खी रहता है। आज चिन्तन की शैली उलटी है। व्यक्ति अन्य के दोष तो देखता है परन्तु स्वयं के नहीं। चाहे कोई कितना ही पढ़ लिख जाये, परन्तु जब तक कथनी-करनी एक न होगी तब तक ऋषियों का जमाना धरती पर नहीं उतारा जा सकता।
अपने आप को व्यक्ति बढ़ा-चढ़ा कर दूसरे के सामने पेश करने का प्रयत्न करता है कि उसे यश-बड़ाई-मान मिले, परन्तु आगे चल कर यह उसके हास्यास्पद पतन का कारण होता है। ईश्वर विश्वासी को भौतिक साधनों द्वारा अपने को बड़ा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।
आज माता-पिता, शिक्षक-गुरु, समाज व राज दण्ड का भय समाप्त हो गया है अत: अपराध बहुत बढ़ गये हैं एक व्यक्ति अपनी क्रिया से सैकडों हजारों को दुःखी करता है; परन्तु आत्मनिरीक्षण करने वाला स्वयं अपनी त्रुटियों को, उलटी आदतों को पकड़ता, सुधारता, दूर करता जाता है।
महत्त्व - एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिये वेद, उपनिषद् आदि शास्त्रों को पढ़ने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण अपने मन को पढ़ना है। प्रशंसा का मोह, यश की कामना, आहंकारिक प्रतिक्रिया आदि वस्तुओं को छोड़ना साधक के लिये अनिवार्य है।
यदि अन्त:करण ठीक होगा तो सब कार्य सफल होंगे। अगले जन्मों में साथ चलने वाली वस्तु अन्तःकरण है। सांसारिक उपकरण यहीं रह जायेंगे। वेद में कहा है 'कृतं स्मर'=अपने किये कर्मों को देख। आन्तरिक शल्य चिकित्सा तो स्वयं करनी पड़ती है। अपने अन्तःकरण को स्वयं देखें। आन्तरिक शुद्धि हमें ही करनी पड़ेगी। नित्य देखें की काम की वासना, क्रोधाग्नि, द्वेषादि पहले थे वैसे ही हैं या कुछ कम हुए?
कर्मों का लेखा-जोखा देखने के साथ इन दोषों का निरीक्षण-परीक्षण भी करते जायें। अपने जीवन की ऋषियों आप्त पुरुषों के जीवन से तुलना करें, उन्हों ने क्या किया क्या नहीं किया व हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमारा जीवन सत्पुरुषों जैसा है या पशु समान। आन्तरिक निर्माण के बिना सुख-चैन-शान्ति नहीं। अगले जन्मों में शुभाशुभ कर्मों के संस्कार ही, सम्पत्ति के रूप में साथ जायेंगे, अन्य कुछ नहीं। बाहर से तो चमक- दमक पर अन्दर निपट अन्धेरा। व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता है। पर ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। ईश्वर सब कुछ देख-सुन-जान रहा है।
एक दोष आ जाये तो उसके साथ-साथ अनेक दोष प्रवेश कर जायेंगे, एक सद्गुण जायेगा तो साथ में अनेक सद्गुण चले जायेंगे। एक दोष बीड़ी-सिगरेट का आने से फिर शराब, क्लब, जुआ, देर में सोना-उठना, प्रमाद-आलस्य, झूठ-कपट-क्लेश, टन्टा-फिसाद एक के पीछे एक ऐसे अनेक दोष व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। एक गुण-नियम 'यज्ञ करना' अपनाने से प्रात: उठना, स्नान, व्यायाम, सत्संग, वेदपाठ, सन्ध्या, फिर समय पर सांसारिक कार्यों में जुटना आदि अनेक गुण प्रवेश कर जाते हैं। शुद्ध ज्ञान वाला दोषों से बच सकता है वरना गिरता-गिरता व्यक्ति कहाँ का कहाँ गिर जाता है। कामी में अन्य दस दोष अपने आप आ जाते हैं। क्रोधी को आठ दोष स्वयं आ जाते हैं।
जो खराब जानकर भी छोड़ते नहीं और अच्छा जानकर भी अपनाते नहीं वे असफल हैं। जो छूटने वाली हैं उन चीजों को एकत्र कर रहे हैं, जो साथ जायेगा उसका धर्म का बैंक बैलेन्स शून्य
आत्मा की वास्तविक इच्छा - स्वतन्त्रता, आनन्द, ईश्वर-प्राप्ति है। दोषों से युक्त रहे या मुक्त रहे यह स्वयं के हाथ में है। जो लोग अपने अधिकारियों के समक्ष अपने दोष बतला देते हैं वे पवित्र हो जाते हैं।
ईश्वरोपासना में मन क्यों नहीं लगता ?
ईश्वरोपासना में मन क्यों नहीं लगता ?
- १. हमारा मन-इन्द्रियों के विषय में ज्ञान कम है।
- २. हमारा अपने विषय (आत्मा) में ज्ञान कम है।
- ३. हमारा संसार के विषय में ज्ञान कम है।
- ४. हम विषय भोगों से प्राप्त होने वाले दुःखों की अनुभूति नहीं करते। विषय भोगों के सुख को दु:ख मिश्रित अनुभव नहीं करते।
- ५. ईश्वर की उपासना से होने वाले लाभों को नहीं जानते।
- ६. संसार की वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को नहीं जानते।
- ७. उपासना से पहले मानसिक सज्जा (तैयारी) नहीं करते।
- ८. ईश्वर को व्यापक और संसार को व्याप्य नहीं स्वीकार करते।
- ९. उपासन काल में संघर्ष नहीं करते।
- १०. व्यवहार काल में यम-नियम का पालन व मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण नहीं रखते।
- ११. उपासना काल में आसन ठीक नहीं लगाते। प्राणायाम और जप विधिवत् नहीं करते।
- १२. सन्ध्या के मंत्रो के शब्दार्थ ठीक प्रकार से स्मरण नहीं करते ।
- १३. शब्द प्रमाण में हमारी श्रद्धा और विश्वास अल्प है।
उपासना काल में नींद का कारण और निवारण
उपासना काल में नींद का कारण और निवारण
ध्यान के समय में नींद को या आलस्य को रोकना आवश्यक होता है। अनेक साधकों को तो यह पता भी नहीं चलता कि वे ध्यान करते हुए सो जाते हैं। अनेकों को पता तो चल जाता है, किन्तु उपासना काल में नींद या आलस्य क्यों आता है, वे कारणों को ठीक-ठीक जान नहीं पाते हैं। नींद तथा आलस्य आने के कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है -
- (१) रात्री में नींद पूरी नहीं होना या अच्छी न होना।
- (२) पेट की शुद्धि न होना - (शौच खुलकर न आना)।
- (३) शारीरिक परिश्रम या व्यायाम अधिक मात्रा करना।
- (४) भोजन प्रतिकूल, गरिष्ठ (= भारी), अधिक मात्रा में करना।
- (५) तामसिक या नशीली वस्तु (= तम्बाकू भांग आदि) का प्रयोग करना।
- (६) शरीर में ज्वरादि रोग का होना।
- (७) शरीर मे निर्बलता का होना।
- (८) आसन ठीक प्रकार से नहीं लगाना (=कमर सीधी करके न बैठना)।
- (९) उपासना से पूर्व स्नान न करना।
- (१०) उचित मात्रा में व्यायाम, भ्रमण, आसन आदि न करना।
- (११) ठण्ड के दिनों में रजाई आदि गर्मी देने वाले वस्त्रों को अधिक मात्रा में धारण करना (ओढ़कर बैठना)
- (१२) मानसिक परिश्रम अध्ययन-चिन्तन आदि अधिक करना।
- (१३) आलसी व्यक्तियों के साथ बैठना ।
- (१४) सन्ध्या के मन्त्रों का शब्दार्थ न जानना ।
- (१५) उचित मात्रा में प्राणायाम न करना।
- (१६) ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, रुचि का न होना ।
- (१७) योगाभ्यास के महत्त्व या लाभों को न समझना।
साधक लोगों को देखना चाहिए कि उपर्युक्त कारणों में से कौन सा कारण मुझ पर लागू होता है। उसे जानकर दूर करना चाहिए, जिससे योगाभ्यास में सफलता मिले ।
योगी बनने का उपाय - आत्मनिरीक्षण
योगी बनने का उपाय - आत्मनिरीक्षण
मनुष्य यदि अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ, आदर्श, महान् बनाना चाहता है तो नित्य सोने से पूर्व आत्मनिरीक्षण करे, अपने अन्तःकरण में झांके कि दिन भर मैंने क्या-क्या त्रुटियाँ-दोष-भूलें की हैं। विचारें 'क्या किया जो नहीं करना चाहिये था और क्या नहीं किया जो करना चाहिये था'। त्रुटियों को पकड़ें, प्रायश्चित्त करें, स्वयं दण्ड लें और भविष्य में न करने का प्रयत्न करें। कोई व्यक्ति बाहरी तौर से कितना ही धन से, बल से, कपड़ों से साफ-सुथरा सभ्य और सबल हो, परन्तु अन्त:करण से मलिन, कमजोर, खिन्न व दु:खी होगा तो वह गिर जायेगा।
बाह्य दु:ख के बजाय मानसिक शोक-दुःख-पीड़ा-काम, क्रोध, लोभ, मोह से व्यक्ति अधिक दु:खी रहता है। आज चिन्तन की शैली उलटी है। व्यक्ति अन्य के दोष तो देखता है परन्तु स्वयं के नहीं। चाहे कोई कितना ही पढ़ लिख जाये, परन्तु जब तक कथनी-करनी एक न होगी तब तक ऋषियों का जमाना धरती पर नहीं उतारा जा सकता।
अपने आप को व्यक्ति बढ़ा-चढ़ा कर दूसरे के सामने पेश करने का प्रयत्न करता है कि उसे यश-बड़ाई-मान मिले, परन्तु आगे चल कर यह उसके हास्यास्पद पतन का कारण होता है। ईश्वर विश्वासी को भौतिक साधनों द्वारा अपने को बड़ा दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।
आज माता-पिता, शिक्षक-गुरु, समाज व राज दण्ड का भय समाप्त हो गया है अत: अपराध बहुत बढ़ गये हैं एक व्यक्ति अपनी क्रिया से सैकडों हजारों को दुःखी करता है; परन्तु आत्मनिरीक्षण करने वाला स्वयं अपनी त्रुटियों को, उलटी आदतों को पकड़ता, सुधारता, दूर करता जाता है।
महत्त्व - एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिये वेद, उपनिषद् आदि शास्त्रों को पढ़ने से भी अधिक महत्त्वपूर्ण अपने मन को पढ़ना है। प्रशंसा का मोह, यश की कामना, आहंकारिक प्रतिक्रिया आदि वस्तुओं को छोड़ना साधक के लिये अनिवार्य है।
यदि अन्त:करण ठीक होगा तो सब कार्य सफल होंगे। अगले जन्मों में साथ चलने वाली वस्तु अन्तःकरण है। सांसारिक उपकरण यहीं रह जायेंगे। वेद में कहा है 'कृतं स्मर'=अपने किये कर्मों को देख। आन्तरिक शल्य चिकित्सा तो स्वयं करनी पड़ती है। अपने अन्तःकरण को स्वयं देखें। आन्तरिक शुद्धि हमें ही करनी पड़ेगी। नित्य देखें की काम की वासना, क्रोधाग्नि, द्वेषादि पहले थे वैसे ही हैं या कुछ कम हुए?
कर्मों का लेखा-जोखा देखने के साथ इन दोषों का निरीक्षण-परीक्षण भी करते जायें। अपने जीवन की ऋषियों आप्त पुरुषों के जीवन से तुलना करें, उन्हों ने क्या किया क्या नहीं किया व हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमारा जीवन सत्पुरुषों जैसा है या पशु समान। आन्तरिक निर्माण के बिना सुख-चैन-शान्ति नहीं। अगले जन्मों में शुभाशुभ कर्मों के संस्कार ही, सम्पत्ति के रूप में साथ जायेंगे, अन्य कुछ नहीं। बाहर से तो चमक- दमक पर अन्दर निपट अन्धेरा। व्यक्ति अपने दोषों को छिपाता है। पर ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। ईश्वर सब कुछ देख-सुन-जान रहा है।
एक दोष आ जाये तो उसके साथ-साथ अनेक दोष प्रवेश कर जायेंगे, एक सद्गुण जायेगा तो साथ में अनेक सद्गुण चले जायेंगे। एक दोष बीड़ी-सिगरेट का आने से फिर शराब, क्लब, जुआ, देर में सोना-उठना, प्रमाद-आलस्य, झूठ-कपट-क्लेश, टन्टा-फिसाद एक के पीछे एक ऐसे अनेक दोष व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। एक गुण-नियम 'यज्ञ करना' अपनाने से प्रात: उठना, स्नान, व्यायाम, सत्संग, वेदपाठ, सन्ध्या, फिर समय पर सांसारिक कार्यों में जुटना आदि अनेक गुण प्रवेश कर जाते हैं। शुद्ध ज्ञान वाला दोषों से बच सकता है वरना गिरता-गिरता व्यक्ति कहाँ का कहाँ गिर जाता है। कामी में अन्य दस दोष अपने आप आ जाते हैं। क्रोधी को आठ दोष स्वयं आ जाते हैं।
जो खराब जानकर भी छोड़ते नहीं और अच्छा जानकर भी अपनाते नहीं वे असफल हैं। जो छूटने वाली हैं उन चीजों को एकत्र कर रहे हैं, जो साथ जायेगा उसका धर्म का बैंक बैलेन्स शून्य
आत्मा की वास्तविक इच्छा - स्वतन्त्रता, आनन्द, ईश्वर-प्राप्ति है। दोषों से युक्त रहे या मुक्त रहे यह स्वयं के हाथ में है। जो लोग अपने अधिकारियों के समक्ष अपने दोष बतला देते हैं वे पवित्र हो जाते हैं।
see also: वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वत:प्रमाण हैं?
(१) जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है वह स्वयं भूल और दोष करता है।
(२) माता-पिता, गुरु-आचार्य मित्रों आदि के द्वारा भी व्यक्ति में दोष आते हैं। माता-पिता स्वयं बच्चों को मांसाहारी बनाते हैं। उपरोक्त मातापिता आदि ठीक हों तो सुधरने में सहायक सिद्ध होते हैं।
(३) समाज की परम्परायें, शैली, ढांचे के कारण भी दोष आ जाते हैं। आज लोग खुल्लम-खुल्ला शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बीभत्स बोलते हैं। तुझे क्या और मुझे क्या यह परम्परा चली हुई है। कोई रोक-टोक नहीं।
(४) राज्य-शासन गलत होने से भी जीवन पद्धति में बड़ा परिवर्तन होता है ।
यदि हम पुरुषार्थ करें तो अन्यों से प्राप्त दोषों को हटा सकते हैं। गलत विचार उठने पर 'प्रतिपक्षभावना' उठायें तो दोष दब जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अंत में दग्धबीज हो जाते हैं। अपने दोषों को जड़ मानकर उनको हटाने का प्रयत्न करें। ज्यों ही दोष उत्पन्न हों तुरन्त एक तरफ धकेल दें। उससे विरुद्ध विचारना आरम्भ कर दें।
मन-वाणी-कर्म से एक होने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर चलता है वही दोष रहित होता है। दोष आने के समय सतर्क हो जायें। पुरुषार्थ से, मन को विचलित करने वाली तरंगों को रोक दें। साधक दोष को चाहते नहीं फिर भी हो जाते हैं। इसका एक कारण है। कि साधक उन्हें रोकने के उपाय नहीं जानता। अभद्र करने के बाद हताश निराश होकर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में दोष आने पर प्रतिपक्ष भावना उठाएँ। आपत्तिकाल में ईश्वर सब से बड़ा सहयोगी होता है। उससे शान्तचित्त होकर सहायता मांगो, धैर्य-ज्ञान-बल मांगो। उलटे काम करने की अभद्र भावना हो तब अवश्य उसे पुकारें। यह दोष दूर करने की विधि है, एक विज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ आदि आ सकते हैं, पर मैं इन्हें हावी नहीं होने दूँगा, इन पर हावी हो जाऊँगा। एक विषय पर अच्छे- बुरे दो तरह के संस्कार काम करते हैं। करूँ या न करूँ। किसी की वस्तु ले लँ, कौन देखता है, फिर सोचता है नहीं लँगा। पुन: सोचता है आज अवसर है, इस बार ले लँ, फिर नहीं लूँगा, इत्यादि विचारते-विचारते ले ही लेता है। परन्तु जो ईश्वर को सामने रखता है वह बच जाता है।
दोषी होने के चार कारण
दोषी होने के चार कारण
(१) जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है वह स्वयं भूल और दोष करता है।
(२) माता-पिता, गुरु-आचार्य मित्रों आदि के द्वारा भी व्यक्ति में दोष आते हैं। माता-पिता स्वयं बच्चों को मांसाहारी बनाते हैं। उपरोक्त मातापिता आदि ठीक हों तो सुधरने में सहायक सिद्ध होते हैं।
(३) समाज की परम्परायें, शैली, ढांचे के कारण भी दोष आ जाते हैं। आज लोग खुल्लम-खुल्ला शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बीभत्स बोलते हैं। तुझे क्या और मुझे क्या यह परम्परा चली हुई है। कोई रोक-टोक नहीं।
(४) राज्य-शासन गलत होने से भी जीवन पद्धति में बड़ा परिवर्तन होता है ।
यदि हम पुरुषार्थ करें तो अन्यों से प्राप्त दोषों को हटा सकते हैं। गलत विचार उठने पर 'प्रतिपक्षभावना' उठायें तो दोष दब जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अंत में दग्धबीज हो जाते हैं। अपने दोषों को जड़ मानकर उनको हटाने का प्रयत्न करें। ज्यों ही दोष उत्पन्न हों तुरन्त एक तरफ धकेल दें। उससे विरुद्ध विचारना आरम्भ कर दें।
दोषों के विषय में मनुष्यों की स्थिति
दोषों के विषय में मनुष्यों की स्थिति
- १. कुछ लोग दोषों को जानते ही नहीं।
- २. कुछ लोग जानते हैं पर दूसरे व्यक्ति से दोष सुनना नहीं चाहते।
- ३. कुछ लोग सुन लेते हैं पर स्वीकार नहीं करते।
- ४. कुछ लोग वाणी से तो स्वीकार कर लेते हैं पर मन से नहीं।
- ५. कुछ लोग मन से स्वीकार करके भूल जाते हैं।
- ६. कुछ लोग दोष हटाने के लिये पुरुषार्थ नहीं करते।
- ७. कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं पर उचित उपायों को नहीं जानते।
- ८. कुछ लोग असफल होने पर निराश हो जाते हैं।
- ९. कुछ लोग ईश्वरादि से सहयोग नहीं लेते हैं।
- १०. कुछ लोग दोषों को दबाये रखते हैं। तनु करते हैं=कमजोर करते हैं।
- ११. कुछ दग्धबीज भाव बना लेते हैं, जिससे आगे कभी दोष नहीं होते।
मन-वाणी-कर्म से एक होने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर चलता है वही दोष रहित होता है। दोष आने के समय सतर्क हो जायें। पुरुषार्थ से, मन को विचलित करने वाली तरंगों को रोक दें। साधक दोष को चाहते नहीं फिर भी हो जाते हैं। इसका एक कारण है। कि साधक उन्हें रोकने के उपाय नहीं जानता। अभद्र करने के बाद हताश निराश होकर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में दोष आने पर प्रतिपक्ष भावना उठाएँ। आपत्तिकाल में ईश्वर सब से बड़ा सहयोगी होता है। उससे शान्तचित्त होकर सहायता मांगो, धैर्य-ज्ञान-बल मांगो। उलटे काम करने की अभद्र भावना हो तब अवश्य उसे पुकारें। यह दोष दूर करने की विधि है, एक विज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ आदि आ सकते हैं, पर मैं इन्हें हावी नहीं होने दूँगा, इन पर हावी हो जाऊँगा। एक विषय पर अच्छे- बुरे दो तरह के संस्कार काम करते हैं। करूँ या न करूँ। किसी की वस्तु ले लँ, कौन देखता है, फिर सोचता है नहीं लँगा। पुन: सोचता है आज अवसर है, इस बार ले लँ, फिर नहीं लूँगा, इत्यादि विचारते-विचारते ले ही लेता है। परन्तु जो ईश्वर को सामने रखता है वह बच जाता है।
see also: सनातन धर्म के शास्त्रों में वेदों का महत्व
सुख शान्ति केवल बाह्य, सुन्दर निर्माण पर नहीं परन्तु आन्तरिक निर्माण पर निर्भर है। इन-इन दोषों के जानने वालों से सहाय लेकर इनको दूर करने का उपाय करें।
अपनी तुलना ऋषियों से करने पर दोषों का पता लगाकर पुरुषार्थ करके सुधार सकते हैं। यदि दोष नहीं जानते-पकड़ते और जीवन जैसा चल रहा है उसी में सन्तुष्ट हो गये तो प्रगति रुक जायेगी। जैसे संविधान न जाना हुआ, न पढ़ा हुआ भी यदि गुनाह करता है तो उसे भी दण्ड अवश्य मिलता है। इसी प्रकार वेद व ऋषिकृत ग्रन्थ नहीं पढ़ा हुआ भी यदि उनके प्रतिकूल चलता है तो दोषी है। यदि गृहस्थी पञ्चमहायज्ञ नहीं करता तो वह ईश्वर विधान के अनुसार दोषी है व दण्डित होगा जो व्यक्ति एकान्त में बैठ अपने
जीवन में झाँक कर अन्त:करण को चमकाते नहीं उन्हें शान्ति और आनन्द कहाँ?
ईश्वर के पा लेने पर सारे प्राणी आत्मवत् दीखने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति जिस जीव से कुछ लाभ प्राप्त करता है उससे तो प्रेम, राग व आसक्ति रखता है और अन्यों में वैसा प्रेम, हित की भावना नहीं रखता है यह व्यक्ति में दोष रहता है। प्राय: देखने में आया है कि व्यक्ति जितना अपना हित चाहता है उतना अन्य का नहीं चाहता। परन्तु ईश्वर प्राप्त योगी इतना ही नहीं आत्मवत् से भी आगे बढ़कर स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख देता है। स्वयं दोष करके व्यक्ति अपने आत्मा को कोमल (नरम) निगाह से देखता है। परन्तु वही दोष अन्य करे तो कठोरता से देखता है। अपना बच्चा मारे तो कोई बात नहीं बालक है, दूसरे का मारे तो कुहराम मचा देते हैं ।
योगाभ्यासी व्यक्ति पहले अपना दोष देखते हैं। साधकों में अन्य के प्रति आत्मवत् भावना उभरती है। जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता। शोक, मोह, अविद्या समाप्त हो जाती है। अविद्या ही सारे अनिष्टों का कारण है। अज्ञान न रहने से परिणाम में आनन्द की उपलब्धि होती है। अज्ञान दोष की निवृत्ति से काम, क्रोध, अधर्माचरण, अन्याय, असत्याचरण आदि स्वयं हट जाते हैं।
दोषों के जाननेवालों से सहायता
दोषों के जाननेवालों से सहायता
सुख शान्ति केवल बाह्य, सुन्दर निर्माण पर नहीं परन्तु आन्तरिक निर्माण पर निर्भर है। इन-इन दोषों के जानने वालों से सहाय लेकर इनको दूर करने का उपाय करें।
- १. कुछ दोष केवल हम जानते हैं। जैसे मानसिक काम, क्रोध, लोभ, हिंसा की भावना आदि।
- २. अपने कुछ दोष हम नहीं जानते दूसरे जानते हैं।
- ३. कुछ को अन्य और हम-दोनों जानते हैं।
- ४. कुछ दोष विद्वान् जानते हैं।
- ५. कुछ दोष योगी-ज्ञानी ही जानते हैं।
- ६. सब दोष तो केवल ईश्वर ही जानता है।
अपनी तुलना ऋषियों से करने पर दोषों का पता लगाकर पुरुषार्थ करके सुधार सकते हैं। यदि दोष नहीं जानते-पकड़ते और जीवन जैसा चल रहा है उसी में सन्तुष्ट हो गये तो प्रगति रुक जायेगी। जैसे संविधान न जाना हुआ, न पढ़ा हुआ भी यदि गुनाह करता है तो उसे भी दण्ड अवश्य मिलता है। इसी प्रकार वेद व ऋषिकृत ग्रन्थ नहीं पढ़ा हुआ भी यदि उनके प्रतिकूल चलता है तो दोषी है। यदि गृहस्थी पञ्चमहायज्ञ नहीं करता तो वह ईश्वर विधान के अनुसार दोषी है व दण्डित होगा जो व्यक्ति एकान्त में बैठ अपने
जीवन में झाँक कर अन्त:करण को चमकाते नहीं उन्हें शान्ति और आनन्द कहाँ?
ईश्वर के पा लेने पर सारे प्राणी आत्मवत् दीखने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति जिस जीव से कुछ लाभ प्राप्त करता है उससे तो प्रेम, राग व आसक्ति रखता है और अन्यों में वैसा प्रेम, हित की भावना नहीं रखता है यह व्यक्ति में दोष रहता है। प्राय: देखने में आया है कि व्यक्ति जितना अपना हित चाहता है उतना अन्य का नहीं चाहता। परन्तु ईश्वर प्राप्त योगी इतना ही नहीं आत्मवत् से भी आगे बढ़कर स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे को सुख देता है। स्वयं दोष करके व्यक्ति अपने आत्मा को कोमल (नरम) निगाह से देखता है। परन्तु वही दोष अन्य करे तो कठोरता से देखता है। अपना बच्चा मारे तो कोई बात नहीं बालक है, दूसरे का मारे तो कुहराम मचा देते हैं ।
योगाभ्यासी व्यक्ति पहले अपना दोष देखते हैं। साधकों में अन्य के प्रति आत्मवत् भावना उभरती है। जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वहाँ अज्ञान नहीं रहता। शोक, मोह, अविद्या समाप्त हो जाती है। अविद्या ही सारे अनिष्टों का कारण है। अज्ञान न रहने से परिणाम में आनन्द की उपलब्धि होती है। अज्ञान दोष की निवृत्ति से काम, क्रोध, अधर्माचरण, अन्याय, असत्याचरण आदि स्वयं हट जाते हैं।
व्यक्ति अपने दोषों से समझौता कैसे करता है ?
- (१) आज तो सारी दुनियाँ ही झूठ, छल- कपट आदि का व्यवहार करती है। मैं अकेला इनसे कैसे बच सकता हूँ। मुझे भी तो इस दुनियाँ में जीना है।
- (२) मैं कोई योगी, ऋषि, महात्मा नहीं हूँ कि मुझसे कोई दोष या भूल न होवे।
- (३) आटे में नमक के बराबर झूठ आदि तो चलते हैं यह कोई बड़ा दोष नहीं है, ऐसा विचारना।
- (४) अधिक दोषी को देखकर यह विचारना कि मैं तो उससे बहुत कम दोष करता हूँ।
- (५) जिन दोषों को हम छोड़ना (सुधारना) नहीं चाहते उन्हें उत्तम स्वरूप दे देना है।
- (६) अपनी छोटी त्रुटियों को एक दम स्वीकार करना, यह दिखाने के लिये मेरे में कोई बड़ा दोष नहीं है।
दोषों से मुक्ति कैसे हो ?
मनोनियन्त्रण द्वारा दोष निवृत्ति
(२) ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ, न है और न होगा जिस पर आरोप या आक्षेप न लगा हो। ईश्वर भी इससे अछूता नहीं।
(३) झूठे आरोप, अन्याय आदि रुकेंगे नहीं, परन्तु अपने संस्कारों को ऐसा बांध करके रखें कि वे भड़कें नहीं।
(४) हम दुसरों की वाणी से दुःखी होते हैं तो उसके कारण हम ही हैं। बिना विचलित हुए सहन करना सीखें।
(५) अपने मन में आग लगाने वाले हम ही हैं । दृढ़ संकल्प करें कि दुनियाँ का कोई भी व्यक्ति, अपने कटु विचार या वाणी से मुझे विचलित नहीं कर सकेगा।
(६) अष्टांग योग से मन का नियंत्रण होगा। यह ईश्वर की उपासना से होगा। 'हे ईश्वर ! मुझे शक्ति दो इन आरोपों से मैं न तो विचलित होऊँ और न ही उससे दुर्भावना रखूँ ।'
(७) सुखी लोगों की विनम्रता उनके मन की शान्ति पर आधारित मैत्री है। और मन की शान्ति धर्मानुष्ठान से प्राप्त प्रसन्नचित्ता से उत्पन्न होती है ।
(३) झूठे आरोप, अन्याय आदि रुकेंगे नहीं, परन्तु अपने संस्कारों को ऐसा बांध करके रखें कि वे भड़कें नहीं।
(४) हम दुसरों की वाणी से दुःखी होते हैं तो उसके कारण हम ही हैं। बिना विचलित हुए सहन करना सीखें।
(५) अपने मन में आग लगाने वाले हम ही हैं । दृढ़ संकल्प करें कि दुनियाँ का कोई भी व्यक्ति, अपने कटु विचार या वाणी से मुझे विचलित नहीं कर सकेगा।
(६) अष्टांग योग से मन का नियंत्रण होगा। यह ईश्वर की उपासना से होगा। 'हे ईश्वर ! मुझे शक्ति दो इन आरोपों से मैं न तो विचलित होऊँ और न ही उससे दुर्भावना रखूँ ।'
(७) सुखी लोगों की विनम्रता उनके मन की शान्ति पर आधारित मैत्री है। और मन की शान्ति धर्मानुष्ठान से प्राप्त प्रसन्नचित्ता से उत्पन्न होती है ।
शयन पूर्व आत्मावलोकन
(१) कहीं मेरा व्यवहार समाज के व्यापक हितों का विरोधी तो नहीं है?
(२) मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये किसी को पीड़ित या वंचित तो नहीं किया?
(३) अच्छे और बुरे का, उचित और अनुचित का विवेक करने में कहीं भूल तो नहीं हुई ?
(४) मैंने कितना निर्माण किया और कितना विध्वंस?
(५) अपेक्षित व्यक्तियों और कार्यों के साथ क्या सहयोग किया ?
(६) अवांछनीय तत्त्वों व घटनाओं का विरोध कर सका या नहीं ?
(७) सामाजिक अन्याय और शोषण में मैं भागीदार बना, उसका शिकार हुआ या सक्षम प्रतिकार किया ?
(८) भविष्य में परिस्थिति विशेष में मेरा व्यवहार और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिये?
(९) ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह आदि से तो युक्त नहीं हुआ ?
(१०) मेरे कारण किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं हुई ?
(११) देश धर्म व मानव समाज के रक्षार्थ कोई परोपकार का कार्य किया ?
(१२) मेरे स्वभाव-वाणी- वर्ताव से कोई दु:खी तो नहीं हुआ ? कोई पीड़ित, खिन्न, भयभीत वा त्रस्त तो नहीं हुआ ?
हमारे जीवन में दु:ख का कारण क्या है, उसे पकड़ने के लिये आत्म-निरीक्षण करें। हम क्रियाव्यवहार, वाणी आदि में दोष करते हैं, उसके पीछे हमारा अज्ञान है, कुवासनाएँ हैं। कूड़ा-कचरा देखेंगे ही नहीं तो साफ क्या करेंगे? अत: पहले सूक्ष्मता से दोषों को पकड़ें फिर दूर करें।
मानव का एक भयंकर दोष - सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में उद्यत नहीं होता।
(२) मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये किसी को पीड़ित या वंचित तो नहीं किया?
(३) अच्छे और बुरे का, उचित और अनुचित का विवेक करने में कहीं भूल तो नहीं हुई ?
(४) मैंने कितना निर्माण किया और कितना विध्वंस?
(५) अपेक्षित व्यक्तियों और कार्यों के साथ क्या सहयोग किया ?
(६) अवांछनीय तत्त्वों व घटनाओं का विरोध कर सका या नहीं ?
(७) सामाजिक अन्याय और शोषण में मैं भागीदार बना, उसका शिकार हुआ या सक्षम प्रतिकार किया ?
(८) भविष्य में परिस्थिति विशेष में मेरा व्यवहार और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिये?
(९) ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह आदि से तो युक्त नहीं हुआ ?
(१०) मेरे कारण किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं हुई ?
(११) देश धर्म व मानव समाज के रक्षार्थ कोई परोपकार का कार्य किया ?
(१२) मेरे स्वभाव-वाणी- वर्ताव से कोई दु:खी तो नहीं हुआ ? कोई पीड़ित, खिन्न, भयभीत वा त्रस्त तो नहीं हुआ ?
हमारे जीवन में दु:ख का कारण क्या है, उसे पकड़ने के लिये आत्म-निरीक्षण करें। हम क्रियाव्यवहार, वाणी आदि में दोष करते हैं, उसके पीछे हमारा अज्ञान है, कुवासनाएँ हैं। कूड़ा-कचरा देखेंगे ही नहीं तो साफ क्या करेंगे? अत: पहले सूक्ष्मता से दोषों को पकड़ें फिर दूर करें।
मानव का एक भयंकर दोष - सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में उद्यत नहीं होता।
(१) प्रणिधानात् भक्तिविशेषात्। (यो. द. १/२३ व्यास भाष्य) ईश्वर की विशेष भक्ति करना अर्थात् ईश्वर में सर्वाधिक प्रेम का होना।
(२) ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा। (यो.द. २/१ व्यास भाष्य) आत्मा, मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली सब क्रियाओं को ईश्वर समर्पित कर देना और लौकिक फल न चाहना।
(३) ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम् । (यो.द. २/३२ व्यास भाष्य)। उस परम गुरु परमात्मा के प्रति सब कर्मों को अर्पित कर देना अर्थात् ईश्वराज्ञानुसार सब क्रियायें करना ।
साधक जप में कभी-कभी पाठ करता है पर अर्थ का विचार नहीं कर पाता। कभी पाठ और अर्थ का विचार दोनों भी कर लेता है पर ईश्वर समर्पित नहीं हो पाता। कई बार समर्पित होता है तो पाठ नहीं कर पाता। जब ये तीनों कार्य होते हैं तो ध्यान की सफलता मानी जाती है।
ईश्वर समर्पण होने में तीन साधनों से काम ले सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण व अनुमान प्रमाण से। जब ईश्वर प्रत्यक्ष है नहीं तो समर्पण कैसे हो ? प्रत्यक्ष तो समाधि अवस्था में होता है। अतः सामान्य साधकों का अनुमान व शब्द प्रमाण से समर्पण हो सकता है।
शब्द प्रमाण से जाना कि ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर है। अनुमान इस संसार को देखने से लगता है कि इसको चलाने वाला कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ही हो सकता है।
ईश्वर की अनन्य भक्ति, उसमें तल्लीन होने की स्थिति में अपने आप को समर्पित करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ऐसा ईश्वर प्रणिधान समाधि का एक विशेष साधन है। यदि यह वैदिक रीति से साधक को करना आ जाये तो शीघ्र समाधि लग जायेगी।
ईश्वर साक्षात्कार करने पर योगी प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य साधक अनुमान और शब्द प्रमाण से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य सब कुछ छोड़कर ईश्वर ही प्रापणीय है। सुनी, सीखी हुई बात को क्रिया रूप में कैसे लायें? इसे प्रातः सायं व्यक्तिगत उपासना में क्रियारूप में लाया जाता है। ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयोग करें। प्रणिधान करते समय ईश्वर से माता-पिता, स्वामी, राजा, व्याप्य-व्यापक आदि सम्बन्ध रहने चाहिए ।
(१) सब कुछ परम गुरु परमेश्वर के अर्पण कर देना। जैसे इस सत्संग भवन में रहन-सहन, योगाभ्यास आदि करते हैं फिर भी इसे अपना नहीं समझते हैं। इसी प्रकार इस संसार व इसके पदार्थों को ईश्वर का मानकर उपयोग तो करें, परन्तु अपना स्वामित्त्व मान कर न चलें ।
(२) यह शरीर हमें ईश्वर से मिला है। हम तो इसमें किराये पर हैं। इसके प्रयोक्ता हैं, मालिक नहीं। जिस बुद्धि पर अभिमान है वह भी ईश्वरप्रदत्त है। यदि ईश्वर अपनी दी हुई सब वस्तुएँ ले-ले तो अकेला जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर की दी हुई वस्तु अपनी मानने लग जाते हैं तो यह चोरी है। कर्मों का फल मिलेगा फल की इच्छा छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान है।
(३) सब मनुष्यों व प्राणियों को प्रभु के परिवार के सदस्य समझना। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का व्यवहार ईश्वर प्रणिधान है।
(२) ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसंन्यासो वा। (यो.द. २/१ व्यास भाष्य) आत्मा, मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली सब क्रियाओं को ईश्वर समर्पित कर देना और लौकिक फल न चाहना।
(३) ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन् परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम् । (यो.द. २/३२ व्यास भाष्य)। उस परम गुरु परमात्मा के प्रति सब कर्मों को अर्पित कर देना अर्थात् ईश्वराज्ञानुसार सब क्रियायें करना ।
साधक जप में कभी-कभी पाठ करता है पर अर्थ का विचार नहीं कर पाता। कभी पाठ और अर्थ का विचार दोनों भी कर लेता है पर ईश्वर समर्पित नहीं हो पाता। कई बार समर्पित होता है तो पाठ नहीं कर पाता। जब ये तीनों कार्य होते हैं तो ध्यान की सफलता मानी जाती है।
ईश्वर समर्पण होने में तीन साधनों से काम ले सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण व अनुमान प्रमाण से। जब ईश्वर प्रत्यक्ष है नहीं तो समर्पण कैसे हो ? प्रत्यक्ष तो समाधि अवस्था में होता है। अतः सामान्य साधकों का अनुमान व शब्द प्रमाण से समर्पण हो सकता है।
शब्द प्रमाण से जाना कि ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर है। अनुमान इस संसार को देखने से लगता है कि इसको चलाने वाला कोई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ही हो सकता है।
ईश्वर की अनन्य भक्ति, उसमें तल्लीन होने की स्थिति में अपने आप को समर्पित करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ऐसा ईश्वर प्रणिधान समाधि का एक विशेष साधन है। यदि यह वैदिक रीति से साधक को करना आ जाये तो शीघ्र समाधि लग जायेगी।
ईश्वर साक्षात्कार करने पर योगी प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य साधक अनुमान और शब्द प्रमाण से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। अन्य सब कुछ छोड़कर ईश्वर ही प्रापणीय है। सुनी, सीखी हुई बात को क्रिया रूप में कैसे लायें? इसे प्रातः सायं व्यक्तिगत उपासना में क्रियारूप में लाया जाता है। ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयोग करें। प्रणिधान करते समय ईश्वर से माता-पिता, स्वामी, राजा, व्याप्य-व्यापक आदि सम्बन्ध रहने चाहिए ।
(१) सब कुछ परम गुरु परमेश्वर के अर्पण कर देना। जैसे इस सत्संग भवन में रहन-सहन, योगाभ्यास आदि करते हैं फिर भी इसे अपना नहीं समझते हैं। इसी प्रकार इस संसार व इसके पदार्थों को ईश्वर का मानकर उपयोग तो करें, परन्तु अपना स्वामित्त्व मान कर न चलें ।
(२) यह शरीर हमें ईश्वर से मिला है। हम तो इसमें किराये पर हैं। इसके प्रयोक्ता हैं, मालिक नहीं। जिस बुद्धि पर अभिमान है वह भी ईश्वरप्रदत्त है। यदि ईश्वर अपनी दी हुई सब वस्तुएँ ले-ले तो अकेला जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ईश्वर की दी हुई वस्तु अपनी मानने लग जाते हैं तो यह चोरी है। कर्मों का फल मिलेगा फल की इच्छा छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान है।
(३) सब मनुष्यों व प्राणियों को प्रभु के परिवार के सदस्य समझना। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का व्यवहार ईश्वर प्रणिधान है।
ईश्वर प्रणिधान की विधि
(२) सब पदार्थों का आदि मूल ईश्वर को समझना।
(३) सब साधनों का प्रयोग ईश्वर की आज्ञानुसार करना।
(४) लौकिक फलों की कामना न करना।
(५) ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है ऐसा विचार बनाये रखना। स्वयं को ईश्वर में डूबा हुआ जानना।
(६) ईश्वर के कारण मैं कार्य करने में समर्थ हुआ हूँ, ऐसा ज्ञान बनाये रखना।
(७) प्रथम स्थूल कार्यों फिर सूक्ष्म कार्यों को करते हुए ईश्वर समर्पित रहना।
(८) कार्यारम्भ से पहले ईश्वर की आज्ञा लेना, अन्त में धन्यवाद देना।
(९) ईश्वर के लिये 'यह-वह' शब्द के प्रयोग की जगह 'आप' का प्रयोग करना।
(१०) प्रत्येक कार्य की सफलता हेतु उसकी सहायता चाहना।
जब यह मित्रवत् एकात्मता की स्थिति ईश्वर- प्रणिधान से उत्पन्न होती है तो ईश्वर जीव को शीघ्र अपना कर उसे अपने ज्ञान-बल-आनन्द से कृतकृत्य कर देता है। यह ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर में अनन्य प्रेम, अट्ूट भक्ति, श्रद्धा, विश्वास) योग की विशेष वस्तु है। इससे साधक को शीघ्र सफलता मिलती है।
योगी व्यक्तियों का दिनभर ईश्वर समर्पण बना रहता है। प्रत्येक कार्य करते हुए
प्रत्येक क्षण ईश्वर को समक्ष रखकर अन्तर्मन से समर्पित रहते हैं।
परिणाम स्वरूप इससे -
(१) व्यक्ति के सब उचित कार्य सिद्ध होते हैं। वह विद्या सहित होकर राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईष्ष्या, अहंकार आदि से मुक्त रहता है।
(२) व्यक्ति कभी हताश-निराश नहीं होता।
(३) शीघ्र ही समाधि को प्राप्त होता है।
(४) सब कार्य ईश्वर की आज्ञा जानकर निष्काम भाव से करता है। सकाम-कर्त्ता प्रणिधान की स्थिति नहीं बना पाता।
पूर्वोक्त सफलता के लिए अनुमान और शब्द प्रमाण से यह भावना बनानी पड़ेगी कि ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है और यह बात मन में बैठानी पड़ेगी कि मेरा और ईश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होने से में ईश्वर में ही हूँ और ईश्वर मेरे बाहर भीतर सर्वत्र है। हम ईश्वर में ही जन्म लेते, पलते और शरीर छोड़ते हैं। ईश्वर यदि हम जीवात्माओं को शरीर नहीं देता तो हम अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते। प्रलय में पत्थर के समान मूर्छित से पड़े रहते हैं। शरीर, बुद्धि मन आदि साधन बिना ईश्वर की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते । 'यह सब स्वयं हो रहा है' यह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। यह सब किसी न किसी तत्त्व (ईश्वर) द्वारा बनाया हुआ है। क्योंकि बिना बनाये कोई भी जड़ पदार्थ कार्यरूप नहीं बन सकता।
प्रारम्भिक काल में आँख बन्द करके अन्तर्वृत्ति बनायें। बाह्य विषयों का विचार बन्द होने पर ही ईश्वर की अखण्डित उपासना कर पायेंगे। ईश्वर से सन्निकटता स्थापित करने के लिये 'आप' शब्द का प्रयोग करें। "आप हमारे पिता हैं" यह सम्बोधन करें।
सफलता के लिये ईश्वर सहाय सदा मौजूद जानें। शब्द व अनुमान प्रमाण से जैसे टी. वी. उद्घोषक जानता-मानता है कि लाखों करोड़ों मुझे देख व सुन रहे हैं तो वह गलत हलन-चलन किये बिना स्वस्थ सावधान होकर ठीक बोलता है। इसी प्रकार उपासक भी जाने कि ईश्वर मेरी प्रत्येक क्रिया-हरकत, यहाँ तक कि मनोभाव भी देख, सुन, जान रहा है।
साधकों का ईश्वर पर शाब्दिक विश्वास तो है पर ताक्त्विक विश्वास नहीं, वरना व्यक्ति कोई उलय कार्य करे ही नहीं। ईश्वर का महत्त्व ( मूल्य) समझने जानने से ईश्वर-प्रणिधान होता है। ईश्वर से प्राप्त सुख का ज्ञान होने पर ईश्वर में रुचि होगी। इन्द्रियों से जो सुख भोग रहे हैं वह दु:ख मिश्रित व क्षणिक होता है और उसको भोगने का सामर्थ्य भी कम होता जाता है। इन्द्रियों के विषय अनित्य हैं अत: उनसे प्राप्त सुख भी अनित्य होते हैं। दूसरे पक्ष में भोगने वाला आत्मा भी नित्य और ईश्वरानन्द रूप भोग्य भी नित्य है। कोई भी भौतिक सुख अन्य प्राणियों को दु:ख दिये बिना नहीं भोगा जा सकता। परन्तु ईश्वरीय आनन्द तो अन्य प्राणियों को पीड़ा दिये बिना ही मिल जाता है।
(३) सब साधनों का प्रयोग ईश्वर की आज्ञानुसार करना।
(४) लौकिक फलों की कामना न करना।
(५) ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है ऐसा विचार बनाये रखना। स्वयं को ईश्वर में डूबा हुआ जानना।
(६) ईश्वर के कारण मैं कार्य करने में समर्थ हुआ हूँ, ऐसा ज्ञान बनाये रखना।
(७) प्रथम स्थूल कार्यों फिर सूक्ष्म कार्यों को करते हुए ईश्वर समर्पित रहना।
(८) कार्यारम्भ से पहले ईश्वर की आज्ञा लेना, अन्त में धन्यवाद देना।
(९) ईश्वर के लिये 'यह-वह' शब्द के प्रयोग की जगह 'आप' का प्रयोग करना।
(१०) प्रत्येक कार्य की सफलता हेतु उसकी सहायता चाहना।
ईश्वर प्रणिधान में जीव की स्थिति
यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम् ।
स्युष्टे सत्या इहाशिषः ।
(ऋग्. ८/४४/२३)
अर्थ - (अग्ने) हे प्रकाश स्वरूप (यद् अहम् त्वं स्याम्) जब में तू हो जाऊँ (वा घा) या (त्वं अहं स्याः) तू में हो जाये, तो (ते इह आशिषः) तेरे इस संसार के वे सब आशीर्वाद (सत्या: स्युः) सत्य /सफल हो जायें।जब यह मित्रवत् एकात्मता की स्थिति ईश्वर- प्रणिधान से उत्पन्न होती है तो ईश्वर जीव को शीघ्र अपना कर उसे अपने ज्ञान-बल-आनन्द से कृतकृत्य कर देता है। यह ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर में अनन्य प्रेम, अट्ूट भक्ति, श्रद्धा, विश्वास) योग की विशेष वस्तु है। इससे साधक को शीघ्र सफलता मिलती है।
योगी व्यक्तियों का दिनभर ईश्वर समर्पण बना रहता है। प्रत्येक कार्य करते हुए
प्रत्येक क्षण ईश्वर को समक्ष रखकर अन्तर्मन से समर्पित रहते हैं।
परिणाम स्वरूप इससे -
(१) व्यक्ति के सब उचित कार्य सिद्ध होते हैं। वह विद्या सहित होकर राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईष्ष्या, अहंकार आदि से मुक्त रहता है।
(२) व्यक्ति कभी हताश-निराश नहीं होता।
(३) शीघ्र ही समाधि को प्राप्त होता है।
(४) सब कार्य ईश्वर की आज्ञा जानकर निष्काम भाव से करता है। सकाम-कर्त्ता प्रणिधान की स्थिति नहीं बना पाता।
पूर्वोक्त सफलता के लिए अनुमान और शब्द प्रमाण से यह भावना बनानी पड़ेगी कि ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है और यह बात मन में बैठानी पड़ेगी कि मेरा और ईश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होने से में ईश्वर में ही हूँ और ईश्वर मेरे बाहर भीतर सर्वत्र है। हम ईश्वर में ही जन्म लेते, पलते और शरीर छोड़ते हैं। ईश्वर यदि हम जीवात्माओं को शरीर नहीं देता तो हम अपनी अनुभूति भी नहीं कर सकते। प्रलय में पत्थर के समान मूर्छित से पड़े रहते हैं। शरीर, बुद्धि मन आदि साधन बिना ईश्वर की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकते । 'यह सब स्वयं हो रहा है' यह मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। यह सब किसी न किसी तत्त्व (ईश्वर) द्वारा बनाया हुआ है। क्योंकि बिना बनाये कोई भी जड़ पदार्थ कार्यरूप नहीं बन सकता।
प्रारम्भिक काल में आँख बन्द करके अन्तर्वृत्ति बनायें। बाह्य विषयों का विचार बन्द होने पर ही ईश्वर की अखण्डित उपासना कर पायेंगे। ईश्वर से सन्निकटता स्थापित करने के लिये 'आप' शब्द का प्रयोग करें। "आप हमारे पिता हैं" यह सम्बोधन करें।
सफलता के लिये ईश्वर सहाय सदा मौजूद जानें। शब्द व अनुमान प्रमाण से जैसे टी. वी. उद्घोषक जानता-मानता है कि लाखों करोड़ों मुझे देख व सुन रहे हैं तो वह गलत हलन-चलन किये बिना स्वस्थ सावधान होकर ठीक बोलता है। इसी प्रकार उपासक भी जाने कि ईश्वर मेरी प्रत्येक क्रिया-हरकत, यहाँ तक कि मनोभाव भी देख, सुन, जान रहा है।
साधकों का ईश्वर पर शाब्दिक विश्वास तो है पर ताक्त्विक विश्वास नहीं, वरना व्यक्ति कोई उलय कार्य करे ही नहीं। ईश्वर का महत्त्व ( मूल्य) समझने जानने से ईश्वर-प्रणिधान होता है। ईश्वर से प्राप्त सुख का ज्ञान होने पर ईश्वर में रुचि होगी। इन्द्रियों से जो सुख भोग रहे हैं वह दु:ख मिश्रित व क्षणिक होता है और उसको भोगने का सामर्थ्य भी कम होता जाता है। इन्द्रियों के विषय अनित्य हैं अत: उनसे प्राप्त सुख भी अनित्य होते हैं। दूसरे पक्ष में भोगने वाला आत्मा भी नित्य और ईश्वरानन्द रूप भोग्य भी नित्य है। कोई भी भौतिक सुख अन्य प्राणियों को दु:ख दिये बिना नहीं भोगा जा सकता। परन्तु ईश्वरीय आनन्द तो अन्य प्राणियों को पीड़ा दिये बिना ही मिल जाता है।
ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि
व्यक्ति जीवन में सतत मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियायें करता रहता है। इन सब क्रियाओं को ईश्वरा्पण करना और कुछ भी फल नहीं चाहना। देखो जैसे एक बालक अपने गुरु जी के पास बैठा हुआ पढ़ता है। इसी तरह हम जीवात्माओं को मानसिक, वाचिक व शारीरिक रूप से ईश्वर के सम्मुख होकर ही सब करना है। यह कठिन इसलिये लगता है कि इसे न माता-पिता ने, न गुरु ने किसी ने भी नहीं सिखाया। और जो बात या विद्या व्यवहार में नहीं लाई जाती वह भी कठिन लगती है और पूरी तरह समझ में भी नहीं आती।
हम जो सोचते-विचारते हैं क्या उसको ईश्वर नहीं देखता-जानता? एक तो श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देना, दूसरा बलात् करना। अच्छे बालक स्वयं चाव-चाव में किये गये पाठ (कार्य) को दिखाते हैं। पर चालाक बालक दोष को लुक-छिप कर इधर-उधर करते हैं। श्रद्धा पूर्वक स्वयं समर्पित कर दो कि हे ईश्वर ! यह हाथ, पॉव, नाक, मुंह, शरीर, मन, बुद्धि सब आपके बनाये हुए हैं और यह जल थल, फल, फूल सब आपने बनाये हैं सो आपसे ओट कभी न हुई न होगी। हमारा क्या लगता है इन ईश्वर की चीजों को उसकी मानने से ? बल्कि इसका लाभ है ईश्वर हमारा सहायक हो, हमारी समाधि लगा, अपने ज्ञान-बल-आनन्द दे देगा। ऋषि कहते हैं- ईश्वर से अत्यन्त प्रेम करना, अपने प्राणों से भी अधिक, इसे भक्ति कहते हैं। उसकी आज्ञा का पालन करना, सब क्रियाओं व चीजों को ईश्वर की मानकर प्रयोग करना, यह बातें दिमाग में रखें। प्रथम सन्ध्या में, फिर व्यवहार में दिन भर के जीवन में ईश्वर के अर्पण रहने का अभ्यास करें। फिर सतत् सब कार्य करते हुए भी समाधि रहती है। यह ऐश्वर्य प्राप्त करना हमारे हाथ में है फिर भी नहीं प्राप्त करते। कहा भी है-
समर्पण भाव में ईश्वर की खोज - जब ध्यान में बैठते हैं तब आत्म-निरीक्षण करें कि क्या ईश्वरापित हूँ? साधक भूल करता है कि ईश्वर को कहीं दूर देश में मानकर उसका ध्यान करता है। जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि वह ईश्वर हमारा राजा, गुरु, पिता है, वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी है। 'वह' शब्द का प्रयोग करते समय ईश्वर को कहीं दूर देश में मान रहा होता है। 'वह' से आगे दिमाग दौड़ाओ। फिर साधक ईश्वर को सब जगह शरीर के बाहर-भीतर, दायें-बायें, ऊपर-नीचे स्वीकार करता है। शरीर में भी है। उसे मस्तक, हृदय, नाभि में भी मानता है परन्तु स्वयं आत्मा को छोड़ देता है, तो इस भूल से भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ दोनों बैठे हैं वहाँ दर्शन होगा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखने से वह दिखाई देगी। जब जीव में भी ईश्वर है तो वही दिखाई देगा। जब देखना चाहेगा तब ईश्वर का दर्शन होगा, सर्वव्यापक का दर्शन वही आत्मा में होगा। ब्रह्मवित् ब्रह्मवत् बन जाता है' इस भावनात्मक कथन को अन्यों ने सिद्धान्त रूप में मान लिया और भूल कर बैठे।
रसो वै स:। ईश्वर आनन्द स्वरूप है, उसके सेवन से जीवात्मा आनन्दी तो बन जाता है पर आनन्द-स्वरूप नहीं बनता। आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हम अपने अन्दर बाहर ईश्वर को विद्यमान मानकर समर्पित हो रहे हैं ? इस ध्यान में पिता-पुत्र, उपास्य-उपासक आदि का सम्बन्ध रहता है या नहीं ? शीघ्रता से कोल्हू के बैल की तरह बार- बार जप करने से कोई लाभ नहीं। माला करने वाले लाख-लाख जप करते हैं ईश्वर-समर्पण के बिना सब निरर्थक रहता है।
हम जो सोचते-विचारते हैं क्या उसको ईश्वर नहीं देखता-जानता? एक तो श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर देना, दूसरा बलात् करना। अच्छे बालक स्वयं चाव-चाव में किये गये पाठ (कार्य) को दिखाते हैं। पर चालाक बालक दोष को लुक-छिप कर इधर-उधर करते हैं। श्रद्धा पूर्वक स्वयं समर्पित कर दो कि हे ईश्वर ! यह हाथ, पॉव, नाक, मुंह, शरीर, मन, बुद्धि सब आपके बनाये हुए हैं और यह जल थल, फल, फूल सब आपने बनाये हैं सो आपसे ओट कभी न हुई न होगी। हमारा क्या लगता है इन ईश्वर की चीजों को उसकी मानने से ? बल्कि इसका लाभ है ईश्वर हमारा सहायक हो, हमारी समाधि लगा, अपने ज्ञान-बल-आनन्द दे देगा। ऋषि कहते हैं- ईश्वर से अत्यन्त प्रेम करना, अपने प्राणों से भी अधिक, इसे भक्ति कहते हैं। उसकी आज्ञा का पालन करना, सब क्रियाओं व चीजों को ईश्वर की मानकर प्रयोग करना, यह बातें दिमाग में रखें। प्रथम सन्ध्या में, फिर व्यवहार में दिन भर के जीवन में ईश्वर के अर्पण रहने का अभ्यास करें। फिर सतत् सब कार्य करते हुए भी समाधि रहती है। यह ऐश्वर्य प्राप्त करना हमारे हाथ में है फिर भी नहीं प्राप्त करते। कहा भी है-
आनन्द स्रोत बह रहा, फिर भी उदास है ।
अचरज है जल में रहके भी मछली को प्यास है ॥
हमारा व ईश्वर का सम्बन्ध - ईश्वर हमारा माता-पिता, गुरु, शासक, नियन्ता, पालक है। फिर भी जीव उसको भूलकर संसार में टक्कर मारता फिरता है। संसार को अपना समझकर दु:खी होता है। प्रथम सन्ध्या-उपासना में ईश्वर सम्बन्ध को कायम रखें कि जो कुछ हम करते हैं वह सब ईश्वर देखता है, तो धीरे-धीरे ईश्वर से हमेशा के लिये सम्बन्ध जुड़ जाता है।समर्पण भाव में ईश्वर की खोज - जब ध्यान में बैठते हैं तब आत्म-निरीक्षण करें कि क्या ईश्वरापित हूँ? साधक भूल करता है कि ईश्वर को कहीं दूर देश में मानकर उसका ध्यान करता है। जैसे हमारे दिमाग में रहता है कि वह ईश्वर हमारा राजा, गुरु, पिता है, वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी है। 'वह' शब्द का प्रयोग करते समय ईश्वर को कहीं दूर देश में मान रहा होता है। 'वह' से आगे दिमाग दौड़ाओ। फिर साधक ईश्वर को सब जगह शरीर के बाहर-भीतर, दायें-बायें, ऊपर-नीचे स्वीकार करता है। शरीर में भी है। उसे मस्तक, हृदय, नाभि में भी मानता है परन्तु स्वयं आत्मा को छोड़ देता है, तो इस भूल से भी ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ दोनों बैठे हैं वहाँ दर्शन होगा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखने से वह दिखाई देगी। जब जीव में भी ईश्वर है तो वही दिखाई देगा। जब देखना चाहेगा तब ईश्वर का दर्शन होगा, सर्वव्यापक का दर्शन वही आत्मा में होगा। ब्रह्मवित् ब्रह्मवत् बन जाता है' इस भावनात्मक कथन को अन्यों ने सिद्धान्त रूप में मान लिया और भूल कर बैठे।
रसो वै स:। ईश्वर आनन्द स्वरूप है, उसके सेवन से जीवात्मा आनन्दी तो बन जाता है पर आनन्द-स्वरूप नहीं बनता। आत्मनिरीक्षण करें कि क्या हम अपने अन्दर बाहर ईश्वर को विद्यमान मानकर समर्पित हो रहे हैं ? इस ध्यान में पिता-पुत्र, उपास्य-उपासक आदि का सम्बन्ध रहता है या नहीं ? शीघ्रता से कोल्हू के बैल की तरह बार- बार जप करने से कोई लाभ नहीं। माला करने वाले लाख-लाख जप करते हैं ईश्वर-समर्पण के बिना सब निरर्थक रहता है।
ईश्वर प्रणिधान से लाभ
- (१) राग, द्वेष आदि दु:ख नहीं देते।
- (२) शरीर, मन व इन्द्रियों पर नियन्त्रण रहता है।
- (३) ईश्वर से ज्ञान, बल, आनन्द, निर्भयता की प्राप्ति होती है।
- (४) स्वार्थ की भावना दबकर परोपकार की भावना उभरती है।
- (५) अभिमान व निराशा का नाश होता है।
- (६) व्यक्ति के कर्म निष्काम होते हैं।
- (७) विषय भोगों की तृष्णा (रुचि) समाप्त हो जाती है।
- (८) आलस्य-प्रमाद दूर होता है।
- (९) आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है।
- (१०) शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है।
ईश्वर प्रणिधान का फल
एक लक्ष्य होने से योग के सभी अङ्गों का एक साथ ही अभ्यास क्रियान्वयन जरूरी है, फिर भी ईश्वर प्रणिधान होने से योगी को समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। इसके बिना योग के दूसरे अंग अपूर्ण हैं।
ईश विश्वास - ईश कृपा
ईश्वर को न मानने वाले ही नास्तिक नहीं हैं। गलत रूप में मानने वाले तथा शाब्दिक रूप में सही मानने वाले आचारहीन भी नास्तिक ही हैं।
मोक्ष प्राप्ति में सब से बड़ी बाधा ईश्वर में विश्वास नहीं होना है। इसका कारण है कि हमें जिस वस्तु में रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द दीख पड़ते हैं उसी का विश्वास करने की आदत पड़ी हुई है।
ईश्वर को मानने का अर्थ है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना व उसकी उपासना करना। जो ईश्वर निर्दिष्ट शुभ कर्मों को करता है वह सुख लाभ पाता है। उसकी आज्ञा का पालन न करके उसे केवल शाब्दिक रूप में मानने से कुछ नहीं बनता। जो नास्तिक ईश्वराज्ञा का पालन करता हुआ भी ईश्वर को नहीं मानता, उसे ईश्वर अपने नियमानुसार कर्म फल तो देता है। परन्तु जो ईश्वर को मानने का समाधि व मोक्ष में आनन्दरूप फल है, वह उसे नहीं मिलता।
वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय व आप्त पुरुषों के सत्संग से ईश्वर ज्ञान तो सम्भव है परन्तु ईश्वरकृपा बिना ईश्वर का आनन्द सम्भव नहीं।
ईश कृपा - जो-जो जितना-जितना संसार का उपकार करता है उतनी-उतनी ईश्वर उस पर कृमा करता है, न कि स्वेच्छा से अनायास ही जिस किसी पर व चाहे जितनी मात्रा में। ईश्वर दया सब पर करता है (समानरूप से) और न्याय भी सब का करता है (अपने-अपने कर्मानुसार)
किसी के मानने न मानने से सत्य (तत्त्व) ईश्वर का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जो मानेगा वह लाभाविन्त होगा जो न मानेगा वह हानि उठायेगा।
इसके लिए निम्नलिखित बातों को जाने, विचारें व समझें कि -
झूठ बोलने की अपेक्षा न बोलना ठीक। बोला तो जाये पर सत्य बोला जाये। सत्य को भी प्रिय करके बोला जाये। सत्य और प्रिय वचन धर्मानुसार हो।
सत्य का फल : सत्याचरण करने वाले का विश्वास उसके शत्रु भी करते हैं। झूठे का विश्वास उसकी पत्नी भी नहीं करती। प्रारम्भ में जब आर्यसमाजी सत्य का पालन किया करते थे तब कोर्ट का न्यायाधीश, जो कुछ आर्य कहता उसे सत्य (प्रमाण) मानकर न्याय (निर्णय) कर देता था। बालक हमेशा आचरण का अनुकरण करता है, उपदेश का नहीं। बच्चा अपने माता-पिता का दर्पण होता है। उसका प्रभाव जाति, राष्ट्र और संसार पर पड़ता है। दोषयुक्त के लिए सत्य प्रथम कड़वा परन्तु परिणाम में अमृत होता है।
योगाभ्यास हो चाहे सांसारिक कार्य, संशय सबसे बड़ा शत्रु (विघ्न) है। इससे व्यक्ति कार्य करने में शिथिल पड़ जाता है। इससे रुचि, उत्साह मंद पड़ जाते हैं। किसी वस्तुतत्त्व को यथार्थ में परीक्षा पूर्वक जानना हो तो संशय सहायक है, परन्तु जानकर भी यह सन्देह बना रहे तो उस वस्तु को न तो प्राप्त करने की और न ही छोड़ने की स्थिति बनती है। 'संशयात्मा विनष्यति'। (गीता)
(१) समान धर्मोत्पत्ति - जब दो वस्तुओं के समान धर्मों की उपलब्धि तो हो रही हो परन्तु विशेष धर्मों की जानकारी न हो, जैसे चाँदनी रात में ढूँठ व मनुष्य की लम्बाई- चौड़ाई तो दीख रहे हैं, परन्तु विशेष धर्म हाथ-पग चलते दीखें नहीं, डाली-शाखा हिलती दिखाई न दे तो वहाँ व्यक्ति सन्देह में पड़ जाता है कि यह वृक्ष है या मनुष्य।
(२) अनेक धर्मोत्पत्ति - द्रव्यों में कई गुण होते हैं। कुछ गुण अन्य द्रव्यों के समान भी होते हैं, परन्तु अपने- अपने विशेष गुणों के कारण वे द्रव्य अन्य द्रव्यों से पृथक् जाने जाते हैं। इन सब की अपनी-अपनी विशेषतायें होती हैं। 'गंध' पृथिवी महाभूत का गुण है। यह 'गंध गुण' पृथिवी महाभूत के सजातीय जल-अग्नि- वायु महाभूत में नहीं पाया जाता है तथा पृथिवी महाभूत के विजातीय गुण व कर्म में भी नहीं पाया जाता। तो संशय होता है कि 'गंध गुण' द्रव्य का है या गुण का या कर्म का।
(३) विपरीत धर्मोत्पत्ति - किसी एक विषय में विपरीत बात सुनना जैसे एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है नहीं है।
(४) उपलब्धि की अव्यवस्था - जैसे दोपहर कड़ी धूप में कहीं रेगिस्तान में चलते हुए दूर जल तरंगें दीख रही हैं तो संशय होता है कि वास्तव में आगे तालाब में जल है या मृग मरीचिका । नेत्रों द्वारा वस्तु की उपलब्धि होते हुए भी अव्यवस्था के कारण संशय बना रहता है।
(५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था - वस्तु होते हुए नहीं मिल रही या है ही नहीं इसलिये नहीं मिल रही। जैसे सुने हुए किसी पुराने खजाने में गड़ा हुआ धन का घड़ा सही ठिकाना न पाने के कारण नहीं मिल रहा या वहाँ घड़ा न होने के कारण नहीं मिल रहा।
मोक्ष प्राप्ति में सब से बड़ी बाधा ईश्वर में विश्वास नहीं होना है। इसका कारण है कि हमें जिस वस्तु में रूप, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्द दीख पड़ते हैं उसी का विश्वास करने की आदत पड़ी हुई है।
ईश्वर को मानने का अर्थ है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना व उसकी उपासना करना। जो ईश्वर निर्दिष्ट शुभ कर्मों को करता है वह सुख लाभ पाता है। उसकी आज्ञा का पालन न करके उसे केवल शाब्दिक रूप में मानने से कुछ नहीं बनता। जो नास्तिक ईश्वराज्ञा का पालन करता हुआ भी ईश्वर को नहीं मानता, उसे ईश्वर अपने नियमानुसार कर्म फल तो देता है। परन्तु जो ईश्वर को मानने का समाधि व मोक्ष में आनन्दरूप फल है, वह उसे नहीं मिलता।
वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय व आप्त पुरुषों के सत्संग से ईश्वर ज्ञान तो सम्भव है परन्तु ईश्वरकृपा बिना ईश्वर का आनन्द सम्भव नहीं।
ईश कृपा - जो-जो जितना-जितना संसार का उपकार करता है उतनी-उतनी ईश्वर उस पर कृमा करता है, न कि स्वेच्छा से अनायास ही जिस किसी पर व चाहे जितनी मात्रा में। ईश्वर दया सब पर करता है (समानरूप से) और न्याय भी सब का करता है (अपने-अपने कर्मानुसार)
किसी के मानने न मानने से सत्य (तत्त्व) ईश्वर का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। जो मानेगा वह लाभाविन्त होगा जो न मानेगा वह हानि उठायेगा।
ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसे हो ?
ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसे हो ?
इसके लिए निम्नलिखित बातों को जाने, विचारें व समझें कि -
- १. ईश्वर हमारे जीवन और संसार का आधार है।
- २. वेदज्ञान का दाता और अन्त:करण में प्रेरणा करता है।
- ३. हमें सुख देने वाले जड़-चेतन सभी पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है।
- ४. ईश्वर हमारे कर्मों का फल दाता है।
- ५. ईश्वर हमारा सर्वाधिक हितैषी है।
- ६. पूर्ण स्थायी सुख ईश्वर से ही मिलता है।
- ७. ईश्वर सर्वगुण सम्पन्न है जबकि जीव और प्रकृति में अनेक दोष हैं।
- ८. ईश्वर हमें इतना अधिक सुख देता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता ।
- ९. ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता।
- १०.ईश्वर की उपासना से व्यक्ति पाप कर्म और दुःखों से बचता है।
ईश्वरीय सुख की विशेषतायें
ईश्वरीय सुख की विशेषतायें
- १. इसकी प्राप्ति में बाह्य साधनों की अपेक्षा कम रहती है ।
- २. यह सर्वत्र प्राप्य है।
- ३. यह नित्य है।
- ४. यह विशुद्ध है, चार प्रकार के दु:खों से रहित है।
- ५. इसे चुराया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता।
- ६. इसकी प्राप्ति के लिये पाप नहीं करना पड़ता।
- ७. इससे व्यक्ति मन-इन्द्रियों का स्वामी बनता है।
- ८. इससे स्वयं सुखी होकर दूसरों को भी आनन्दित करता है।
- ९. यह कुसंस्कारों का नाशक होता है ।
- १०. इससे व्यक्ति स्वस्थ, शान्त, प्रसन्न और संतुष्ट रहता है।
- ११. इससे व्यक्ति निष्काम कर्त्ता बनता है
- १२. ईश्वरीय सुख से व्यक्ति ऊबता नहीं है ।
- १३. इसको भोगने वाला कालान्तर में मुक्ति को प्राप्त करता है।
सत्य की परिभाषा और फल
सत्य की परिभाषा और फल
- (१) जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना, मानना सत्य कहाता है।
- (२) वह सत्य नहीं (होता) कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य का प्रकाश किया जाये।
- (३) जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिये वह सत्यमत को प्राप्त नहीं हो सकता।
- (४) मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है।
- (५) जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो वह सत्य है। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं।
- (६) सदा सत्य की विजय और असत्य की पराजय होती है।
सत्य किस प्रकार बोलें
सत्य किस प्रकार बोलें
- (१) परीक्षा करके, सब के उपकार के लिये बोलें।
- (२) सर्वहितकारी और प्रिय वाणी बोलें।
- (३) आवश्यकता से कम या अधिक न बोलें।
- (४) व्याकरण के अनुसार शुद्ध बोलें।
- (५) अपात्र या अयोग्य स्थान पर न बोलें।
झूठ बोलने की अपेक्षा न बोलना ठीक। बोला तो जाये पर सत्य बोला जाये। सत्य को भी प्रिय करके बोला जाये। सत्य और प्रिय वचन धर्मानुसार हो।
सत्य का फल : सत्याचरण करने वाले का विश्वास उसके शत्रु भी करते हैं। झूठे का विश्वास उसकी पत्नी भी नहीं करती। प्रारम्भ में जब आर्यसमाजी सत्य का पालन किया करते थे तब कोर्ट का न्यायाधीश, जो कुछ आर्य कहता उसे सत्य (प्रमाण) मानकर न्याय (निर्णय) कर देता था। बालक हमेशा आचरण का अनुकरण करता है, उपदेश का नहीं। बच्चा अपने माता-पिता का दर्पण होता है। उसका प्रभाव जाति, राष्ट्र और संसार पर पड़ता है। दोषयुक्त के लिए सत्य प्रथम कड़वा परन्तु परिणाम में अमृत होता है।
संशय महाशत्रु
संशय महाशत्रु
योगाभ्यास हो चाहे सांसारिक कार्य, संशय सबसे बड़ा शत्रु (विघ्न) है। इससे व्यक्ति कार्य करने में शिथिल पड़ जाता है। इससे रुचि, उत्साह मंद पड़ जाते हैं। किसी वस्तुतत्त्व को यथार्थ में परीक्षा पूर्वक जानना हो तो संशय सहायक है, परन्तु जानकर भी यह सन्देह बना रहे तो उस वस्तु को न तो प्राप्त करने की और न ही छोड़ने की स्थिति बनती है। 'संशयात्मा विनष्यति'। (गीता)
संशय उत्पत्ति के कारण
संशय उत्पत्ति के कारण
(१) समान धर्मोत्पत्ति - जब दो वस्तुओं के समान धर्मों की उपलब्धि तो हो रही हो परन्तु विशेष धर्मों की जानकारी न हो, जैसे चाँदनी रात में ढूँठ व मनुष्य की लम्बाई- चौड़ाई तो दीख रहे हैं, परन्तु विशेष धर्म हाथ-पग चलते दीखें नहीं, डाली-शाखा हिलती दिखाई न दे तो वहाँ व्यक्ति सन्देह में पड़ जाता है कि यह वृक्ष है या मनुष्य।
(२) अनेक धर्मोत्पत्ति - द्रव्यों में कई गुण होते हैं। कुछ गुण अन्य द्रव्यों के समान भी होते हैं, परन्तु अपने- अपने विशेष गुणों के कारण वे द्रव्य अन्य द्रव्यों से पृथक् जाने जाते हैं। इन सब की अपनी-अपनी विशेषतायें होती हैं। 'गंध' पृथिवी महाभूत का गुण है। यह 'गंध गुण' पृथिवी महाभूत के सजातीय जल-अग्नि- वायु महाभूत में नहीं पाया जाता है तथा पृथिवी महाभूत के विजातीय गुण व कर्म में भी नहीं पाया जाता। तो संशय होता है कि 'गंध गुण' द्रव्य का है या गुण का या कर्म का।
(३) विपरीत धर्मोत्पत्ति - किसी एक विषय में विपरीत बात सुनना जैसे एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है नहीं है।
(४) उपलब्धि की अव्यवस्था - जैसे दोपहर कड़ी धूप में कहीं रेगिस्तान में चलते हुए दूर जल तरंगें दीख रही हैं तो संशय होता है कि वास्तव में आगे तालाब में जल है या मृग मरीचिका । नेत्रों द्वारा वस्तु की उपलब्धि होते हुए भी अव्यवस्था के कारण संशय बना रहता है।
(५) अनुपलब्धि की अव्यवस्था - वस्तु होते हुए नहीं मिल रही या है ही नहीं इसलिये नहीं मिल रही। जैसे सुने हुए किसी पुराने खजाने में गड़ा हुआ धन का घड़ा सही ठिकाना न पाने के कारण नहीं मिल रहा या वहाँ घड़ा न होने के कारण नहीं मिल रहा।
🕉️🚩🙏 नमस्ते 🕉️🚩🙏



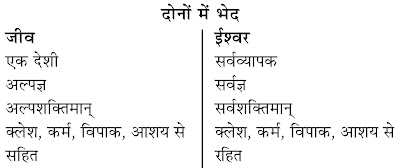










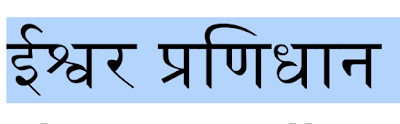
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें